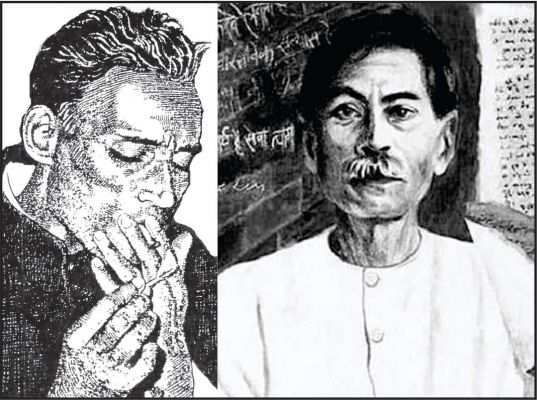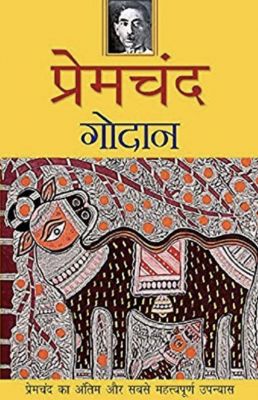विचार/लेख
-गजानन माधव मुक्तिबोध
एक छाया-चित्र है। प्रेमचन्द और प्रसाद दोनों खड़े हैं। प्रसाद गम्भीर सस्मित। प्रेमचन्द के होंठों पर अस्फुट हास्य। विभिन्न विचित्र प्रकृति के दो धुरन्धर हिन्दी कलाकारों के उस चित्र पर नजर ठहरने का एक और कारण भी है। प्रेमचन्द का जूता कैनवैस का है, और वह अँगुलियों की ओर से फटा हुआ है। जूते की कैद से बाहर निकलकर अँगुलियाँ बड़े मजे से मैदान की हवा खा रही हैं। फोटो खिंचवाते वक्त प्रेमचन्द अपने विन्यास से बेखबर हैं। उन्हें तो इस बात की खुशी है कि वे प्रसाद के साथ खड़े हैं, और फोटो निकलवा रहे हैं।
इस फोटो का मेरे जीवन में काफी महत्व रहा है। मैने उसे अपनी माँ को दिखाया था। प्रेमचन्द की सूरत देख मेरी माँ बहुत प्रसन्न मालूम हुई। वह प्रेमचन्द को एक कहानीकार के रूप में बहुत-बहुत चाहती थी। उसकी दृष्टि से, यानी उसके जीवन में महत्व रखने वाले, सिर्फ दो ही कादम्बरीकार (उपन्यास लेखक) हुए हैं - एक हरिनारायण आप्टे, दूसरे प्रेमचन्द। आप्टे की सर्वोच्च मराठी कृति, उनके लेखे, 'पण लक्षात कोण घेतो' है, जिसमें भारतीय परिवार में स्त्री के उत्पीड़न की करुण कथा कही गयी है। वह क्रान्तिकारी करुणा है। उस करुणा ने महाराष्ट्रीय परिवारों को समाज-सुधार की ओर अग्रसर कर दिया। मेरी माँ जब प्रेमचन्द की कृति पढ़ती, तो उसकी आँखों में बार-बार आँसू छलछलाते से मालूम होते। और तब—उन दिनों मैं साहित्य का एक जड़मति विद्यार्थी मात्र, मैट्रिक का एक छोकरा था—प्रेमचन्द की कहानियों का दर्द भरा मर्म माँ मुझे बताने बैठती। प्रेमचन्द के पात्रों को देख, तदनुसारी-तदनरूप चरित्र माँ हमारे पहचानवालों में से खोज-खोजकर निकालती। इतना मुझे मालूम है कि माँ ने प्रेमचन्द का "नमक का दारोगा" आलमारी में से खोजकर निकाला था। प्रेमचन्द पढ़ते वक्त माँ को खूब हँसी भी आती, और तब वह मेरे मूड की परवाह किये बगैर मुझे प्रेमचन्द कथा प्रसूत उसके हास्य का मर्म बताने की सफल-असफल चेष्टा करती।
प्रेमचन्द के प्रति मेरी श्रद्धा व ममता को अमर करने का श्रेय मेरी माँ को ही है। मैं अपनी भावना में प्रेमचन्द को माँ से अलग नहीं कर सकता। मेरी माँ सामाजिक उत्पीड़नों के विरूद्ध क्षोभ और विद्रोह से भरी हुई थी। यद्यपि वह आचरण में परम्परावादी थी, किन्तु धन और वैभवजन्य संस्कृति के आधार पर ऊँच-नीच के भेद का तिरस्कार करती थी। वह स्वयं उत्पीड़ित थी। और भावना द्वारा, स्वयं की जीवन-अनुभूति के द्वारा, माँ स्वयं प्रेमचन्द के पात्रों में अपनी गणना कर लिया करती थी। मेरी ताई (माँ) अब बूढ़ी हो गयी है। उसने वस्तुत: भावना और सम्भावना के आधार पर मुझे प्रेमचन्द पढ़ाया। इस बात को वह नहीं जानती है कि प्रेमचन्द के पात्रों के मर्म का वर्णन-विवेचन करके वह अपने पुत्र के ह्रदय में किस बात का बीज बो रही है। पिताजी देवता हैं, माँ मेरी गुरू है। सामाजिक दम्भ, स्वाँग, ऊँच-नीच की भावना, अन्याय और उत्पीड़नों से कभी भी समझौता न करते हुए घृणा करना उसी ने मुझे सिखाया।
लेकिन मेरी प्यारी श्रद्धास्पदा माँ यह कभी न जान सकी कि वह किशोर-हृदय में किस भीषण क्रान्ति का बीज बो रही है, कि वह भावात्मक क्रान्ति अपने पुत्र को किस उचित-अनुचित मार्ग पर ले जायेगी, कि वह किस प्रकार अवसरवादी दुनिया के गणित से पुत्र को वंचित रखकर, उसके परिस्थिति-सामंजस्य को असम्भव बना देगी।
आज जब मैं इन बातों पर सोचता हूँ तो लगता है कि यदि मैं, माँ और प्रेमचन्द की केवल वेदना ही ग्रहण न कर, उनके चारित्रिक गुण भी सीखता, उनकी दृढ़ता, आत्म-संयम और अटलता को प्राप्त करता, आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति नष्ट कर देता, और उन्हीं के मनोजगत की विशेषताओं को आत्मसात करता, तो शायद, शायद मैं अधिक योग्य पात्र होता। माँ मेरी गुरू थी अवश्य, किन्तु, मैं उनका शायद योग्य शिष्य ना था। अगर होता तो कदाचित् अधिक श्रेष्ठ साहित्यिक होता, केवल प्रयोगवादी कवि बनकर न रह जाता।
मतलब यह कि जब कभी भी प्रेमचन्द के बारे में सोचता हूँ, मुझे अपने जीवन का ख्याल आ जाता है। मुझे महान चरित्रों से साक्षात्कार होता है, और मैं आत्म-विश्लेषण में डूब जाता हूँ। आत्म-विश्लेषण की मन:स्थिति बहुत बुरी चीज है।
जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा तो मेरे कुछ लेखक-मित्रों के पास प्रेमचन्दजी के पत्र आये। मैं उन मित्रों के प्रति ईर्ष्यालु हो उठा। उन दिनों मैं उन लोगों को जीनियस समझता था, और प्रेमचन्द को देवर्षि। अब सोचता हूँ कि दोनों बातें गलत है। मेरे लेखक-मित्र जीनियस थे ही नहीं, बहुत प्रसिद्ध अवश्य थे और अभी भी है। किन्तु वे प्रेमचन्द के लायक न तब थे, न अब हैं। और यहाँ हम हिन्दी साहित्य के इतिहास के एक मनोरंजक और महत्वपूर्ण मोड़ तक पहुँच जाते है। प्रेमचन्द जी भारतीय सामाजिक क्रान्ति के एक पक्ष का चित्रण करते थे। वे उस क्रान्ति के एक अंग थे। किन्तु अन्य साहित्यिक उस क्रान्ति का एक अंग होते हुए भी उसके सामाजिक पक्ष की संवेदना के प्रति उन्मुख नहीं थे। वह क्रान्ति हिन्दी साहित्य में छायावादी व्यक्तिवाद के रूप में विकसित हो चुकी थी। जिस फोटो का मैंने शुरू में जिक्र किया, उसमें के प्रसादजी इस व्यक्तिवादी भाव-धारा के प्रमुख प्रवर्तक थे।
यह व्यक्तिवाद एक वेदना के रूप में सामाजिक गर्भितार्थों को लिये हुए भी, प्रत्यक्षत: किसी प्रत्यक्ष सामाजिक लक्ष्य से प्रेरित नहीं था। जैनेन्द्र में तो फिर भी मुक्तिकामी सामाजिक ध्वन्यर्थ थे, किन्तु आगे चलकर अज्ञेय में वे भी लुप्त हो गये। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचन्द उत्थानशील भारतीय सामाजिक क्रान्ति के प्रथम और अन्तिम महान कलाकार थे। प्रेमचन्द की भाव-धारा वस्तुत: अग्रसर होती रही, किन्तु उसके शक्तिशाली आविर्भाव के रूप में कोई लेखक सामने नहीं आया। यह सम्भव भी नहीं था, क्योंकि इस क्रान्ति का नेतृत्व पढ़े-लिखे मध्यम-वर्ग के हाथ में था, और वह शहरों में रहता था। बाद में वह वर्ग अधिक आत्म-केन्द्रित और अधिक बुद्धि-छन्दी हो गया तथा उसने काव्य में प्रयोगवाद को जन्म दिया।
किन्तु, क्या यह वर्ग कम उत्पीड़ित है? आज तो सामाजिक विषमताएँ और भी बढ़ गयी हैं। प्रेमचन्द का महत्व पहले से भी अधिक बढ़ गया है। उनकी लोकप्रियता अब हिन्दी तक ही सीमित नहीं रह गयी है। अन्य भाषाओं में उनके अनुवादकर्ताओं के बीच होड़ लगी रहती है। प्रेमचन्द द्वारा सूचित सामाजिक सन्देश अभी भी अपूर्ण है। किन्तु हम जो हिन्दी के साहित्यिक है, उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दे पाते। एक तरह से यह यथार्थ से भागना हुआ। उदाहरणत: आज का कथा-साहित्य पढ़कर पात्रों की प्रतिच्छाया देखने के लिए हमारी आँखे आस-पास के लोगों की तरफ नहीं खिंचतीं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है, जैसे पात्रों की छाया ही नहीं गिरती, कि वे लगभग देहहीन है। लगता है कि हमारे यहाँ प्रेमचन्द के बाद एक भी ऐसे चरित्र का चित्रण नहीं हुआ, जिसे हम भारतीय विवेक-चेतना का प्रतीक कह सकें। शायद, अज्ञान के कारण मेरी ऐसी धारणा होगी। कोई मुझे प्रकाश-दान दें।
किन्तु, कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचन्द की जरूरत आज पहले से भी ज्यादा बढ़ी हुई है। प्रेमचन्द के पात्र आज भी हमारे समाज में जीवित हैं। किन्तु वे अब भिन्न स्थिति में रह रहे हैं। किसी के चरित्र का कदाचित् अध:पतन हो गया है। किसी का शायद पुनर्जन्म हो गया है। बहुतेरे पात्र अपने सृजनकर्त्ता लेखक की खोज में भटक रहे है। उन्हें अवश्य ऐसा कोई-न-कोई लेखक शीघ्र ही प्राप्त होगा।
प्रेमचन्द की विशाल छाया में बैठकर आत्म-विश्लेषण की मन:स्थिति मुझे अजीब ख्यालों में डुबो देती है। माना कि आज व्यक्ति पहले जैसा ही जीवन-संघर्ष में तत्पर है, किन्तु अब वह अधिक आत्म-केन्द्रित और आत्म-ग्रस्त हो गया है, माना कि इन दिनों वह समाज-परिवर्तन की, समाजवाद की, वैज्ञानिक विकास की, योजनाबद्ध कार्य की, अधिक बात करता है। किन्तु एक चरित्र के रूप में, एक पात्र के रूप में, वह सघन और निबिड़ आत्म-केन्द्रित होता जा रहा है। माना कि आज वह अधिक सुशिक्षित-प्रशिक्षित है, और अनेक पुराणपंथी विचारों को त्याग चुका है, तथा जीवन जगत से अधिक सचेत और सचेष्ट है किन्तु मानो ये सब बातें, ये सारी योग्यताएँ, ये सारी स्पृहणीय विशेषताएँ, उसे अधिकाधिक स्वयं-ग्रस्त बनाती गयी हैं। कदाचित् मेरा यह मन्तव्य अतिशयोक्तिपूर्ण है, किन्तु यह भी सही है कि वह एक तथ्य की ही अतिशयोक्ति है।
आश्चर्य मुझे इस बात का होता है कि आखिर आदमी को हो क्या गया है। उसकी अन्तरात्मा, एक जमाने में समाजोन्मुख सेवाभावी थी, आज आदर्शवाद की बात करते हुए भी इतनी अजीब क्यों हो गयी ? एक बार बातचीत के सिलसिले में, एक सम्मानीय पुरुष ने मुझे कहा कि व्यक्ति जितना सुशिक्षित-प्रशिक्षित होता जायेगा, उतना ही बौद्धिक होता जायेगा, और उसी अनुपात में उसकी आत्म-केन्द्रिता बढ़ती जायेगी, उतने ही उसके मानवोचित गुण कम होते जायेंगे, जैसे करुणा, क्षमा, दया, शील, उदारता आदि। मेरे ख्याल से उसने जो कहा है, गलत है। किन्तु यह मैं निश्चय नहीं कर पाता कि उसका मन्तव्य निराधार है। शायद, मैं ग़लती कर रहा हूँगा। जीवन के सिर्फ एक पक्ष को (अधूरे ढंग से और अपर्याप्त निरीक्षण द्वारा) आकलित कर मैं इस निराशात्मक मन्तव्य की ओर आकर्षित हूँ।
किन्तु, कभी-कभी निराशा भी आवश्यक होती है। विशेषकर प्रेमचन्द की छाया में बैठे, आज के अपने आस-पास के जीवन के दृश्य देख, वह कुछ तो स्वाभाविक ही है। सारांश यह, कि प्रेमचन्दजी का कथा-साहित्य पढ़कर आज हम एक उदार और उदात्त नैतिकता की तलाश करने लगते है, चाहने लगते हैं कि प्रेमचन्दजी के पात्रों के मानवीय गुण हममें समा जायें, हम उतने ही मानवीय हो जायें जितना कि प्रेमचन्द चाहते हैं। प्रेमचन्दजी का कथा-साहित्य हम पर एक बहुत बड़ा नैतिक प्रभाव डालता है। उनका कथा-साहित्य पढ़ते हुए उनके विशिष्ट ऊँचे पात्रों द्वारा हमारे अन्त:करण में विकसित की गयी भावधाराएँ हमें न केवल समाजोन्मुख करती हैं, वरन् वे आत्मोन्मुख भी कर देती हैं। और जब प्रेमचन्द हमें आत्मोन्मुख कर देते हैं, तब वे हमारी आत्म-केन्द्रिता के दुर्ग को तोड़कर हमें एक अच्छा मानव बनाने में लग जाते हैं। प्रेमचन्द समाज के चित्रणकर्त्ता ही नहीं, वरन् वे हमारी आत्मा के शिल्पी भी हैं।
माना कि हमारे साहित्य का टेकनीक बढ़ता चला जायेगा, माना कि हम अधिकाधिक सचेत और अधिकाधिक सूक्ष्म-बुद्धि होते जायेंगे, माना कि हमारा बुद्धिगत ज्ञान संवेदनाओं और भावनाओं को न केवल एक विशेष दिशा में मोड़ देगा, वरन् उनका अनुशासन-प्रशासन भी करेगा। किन्तु क्या यह सच नहीं है कि मानवीय सत्यों और तथ्यों को देखने की सहज भोली और निर्मल दृष्टि, हृदय का सहज सुकुमार आदर्शवाद, दिल को भीतर से हिला देने वाली कर्त्तव्योन्मुख प्रेरणा भी हमारे लिए उतनी ही कठिन और दुष्प्राप्त होती जायेगी ?
ओह! काश, हम भी भोली कली से खिल सकते! पराये दु:ख में रोकर उसे दूर करने की भोली सक्रियता पा सकते! शायद मैं विशेष मन:स्थिति में ही यह सब कह रहा हूँ। फिर भी मेरी यह कहने की इच्छा होती है कि समाज का विकास अनिवार्यत: मानवोचित नैतिक-हार्दिक विकास के साथ चलता जाए, यह आवश्यक नहीं है। सभ्यता का विकास नैतिक विकास भी करता है, यह ज़रूरी नहीं है।
यह समस्या प्रस्तुत लेख के विषय से सम्बन्धित होते हुए भी उसके बाहर है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रेमचन्द का कथा-साहित्य पढ़कर हमारे मन पर जो प्रभाव होते हैं, वे धीरे-धीरे हमारी चिन्तना को इस सभ्यता-समस्या तक ले आते हैं। क्या यह हमें प्रेमचन्द की ही देन नहीं है ?
राष्ट्रभारती (1953-57 के बीच) में प्रकाशित
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के एक बयान को लेकर महाराष्ट्र के नेता लोग कैसा धमाल मचा रहे हैं ? कोश्यारी ने मारवाडिय़ों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि मारवाड़ी और गुजराती व्यापारियों को हटा दिया जाए तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी। कोश्यारी के इस बयान में गलत क्या है? उन्होंने जो सर्वमान्य तथ्य है, उसे बस कहा भर है। उन्होंने महाराष्ट्र के मराठों और दक्षिण भारतीयों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही, जो अपमानजनक या आपत्तिजनक है।
उन्होंने मुंबई के मारवाड़ी और गुजराती सेठों की पीठ ठोककर महाराष्ट्र का भला ही किया है। सेठों को यह नहीं लगेगा कि वे महाराष्ट्र पर कोई बोझा हैं। कोश्यारी के बयान से वे थोड़े और उत्साहित हो जाएंगे। जहां तक मराठीभाषी लोगों का सवाल है, उन्होंने ऐसा एक शब्द भी नहीं बोला, जिससे उनका अपमान हो या अवमूल्यन हो। जब पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने उनके बयान की आलोचना की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके अभिप्राय को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। वे मराठी लोगों के योगदान के प्रशंसक हैं लेकिन जरा हम देखें कि महाराष्ट्र के सभी नेता कैसी भेड़चाल चल रहे हैं। भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस आदि सभी दलों के नेताओं ने राज्यपाल के बयान को या तो गलत बताया है या उसकी कड़ी भर्त्तसना की है। हर नेता मराठीभाषी मतदाताओं को खुश करने के लालच में फिसलता गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपना मौन तोड़ दिया। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि अधमरी शिवसेना के पति उद्धव ठाकरे को कोई मुंहतोड़ जवाब देता। ठाकरे ने शिष्टता की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि राज्यपाल को इस वक्त ‘कोल्हापुरी चप्पल’ दिखाने का वक्त है। इतना फूहड़ बयान तो किसी नेता का आज तक हमने कभी सुना नहीं। जो व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका हो, वह एक बुजुर्ग राज्यपाल के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी पर ‘नमकहरामी’ होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल से कोश्यारी महाराष्ट्रियनों का नमक खा रहे हैं और फिर भी उनकी निंदा कर रहे हैं। वे मराठी और गैर-मराठी लोगों में दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। उन्हें बर्खास्त किया जाए या जेल भेजा जाए। ये सारे विषाक्त वाक्य क्या बता रहे हैं? यही कि उद्धव ठाकरे की हताशा चरम सीमा पर है। वे अपने खाली झुनझुने को पूरी ताकत से हिला रहे हैं। उनका बयान सुनकर मराठी-मानुस उन पर हंसने के अलावा क्या कर सकते हैं? वे अब चाहें तो मारवाडिय़ों और गुजरातियों को महाराष्ट्र से भगाने का अभियान भी चला सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार कांग्रेस की गोद में बैठकर सत्ता-सुख भोगनेवाले ठाकरे परिवार की बौखलाहट पर अब मराठी लोग कान क्यों देंगे? महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि ठाकरे परिवार ऐसा अभियान चला देगा तो महाराष्ट्र के कई शहरों में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
(नया इंडिया की अनुमति से)
-दिनेश श्रीनेत
भारत में सिनेमा एक ऐसी कला है जिसके बारे में हर कोई साधिकार बोल सकता है। बोलना भी चाहिए। लोकप्रिय सिनेमा का निर्माण एक बड़े समूह को ध्यान में रखकर होता है। लेकिन जब हम उसे आलोचना के दायरे में लाते हैं तो उसकी अपनी एक सैद्धांतिकी और दायरा होता है। इसके माध्यम से हमारी सोसाइटी बहुत कुछ फिल्टर करती है और विमर्श की एक दिशा तय होती है। दुर्भाग्य से सिनेमा के मामले में ऐसा नहीं हुआ।
हिंदी में आरंभ से ही सिनेमा पर गिने-चुने लिखने वाले रहे हैं। एक रूढ़ि बनी रही कि सिनेमा दोयम दर्जे की कला है। मुख्यधारा के अखबारों, पत्रिकाओं और ऑनलाइन मीडिया का हाल तो और भी बुरा रहा है। बीते करीब एक दशक से हिंदी मुख्यधारा का सिनेमा पीआर के चंगुल में था। जैसा ब्रीफ किया जाता था, जैसा वे चाहते थे, वैसा ही लिखा जाता था।
हर फिल्म को पांच में तीन से चार स्टार मिलते थे, हर फिल्म की टुकड़ों में समीक्षा की जाती थी, जैसे कहानी कमजोर-पटकथा अच्छी, लोकेशन भव्य-फोटोग्रॉफी साधारण, संगीत सामान्य-गीत अच्छे। फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू तक पीआर ही मैनेज करते थे। एक ही बात सभी जगह छपती थी। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी शायद इसी शर्त पर मिलते थे कि कोई निगेटिव बात न तो पूछी जाए और न लिखी जाए।
हिंदी के अखबारों में इतनी खराब समीक्षाएं छपती थीं कि फिल्म सचमुच कैसी है इसे जानने का दो ही तरीका था, या तो सोशल मीडिया पर फिल्म प्रेमी मित्रों से मशवरा किया जाए या आईएमडीबी के रिव्यू पढ़े जाएं। मुझे निर्विवाद रूप से आईएमडीबी में लिखे जाने वाले रिव्यू सबसे ईमानदार लगते हैं। कुछ ऑफबीट फिल्में बनाने वाले चालाक निर्माताओं ने अपनी मार्केटिंग के लिए आईएमडीबी पर भी पेड रिव्यू लिखवाने शुरू कर दिए। मगर दो हफ्ते-महीने में कोई न कोई पोल खोलने वाला आ ही जाता था।
इतनी सब कहानी सुनाने के पीछे वजह ये थी कि अब मामला बिल्कुल उलट है। इन दिनों हर फिल्म की जमकर आलोचना हो रही है। जाने-माने समीक्षकों से लेकर यूट्यूबर तक बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। कुल मिलाकर फिल्म पर, उसके कलात्मक पक्ष पर, उसके कंटेंट पर, उसके सामाजिक सरोकारों पर अब भी बात नहीं हो रही है।
अब मुद्दा है नेपोटिज़्म और हिंदूवाद। मुद्दा है दक्षिण का सिनेमा बनाम उत्तर भारत का सिनेमा। बॉलीवुड बनाम साउथ। किसी फिल्म की आलोचना इस आधार पर कैसे हो सकती है कि उसमें किस फिल्म स्टार के बेटे या बेटी ने काम किया है।
सभी जानते हैं कि धर्म के बाद जनमानस के दिल-दिमाग को प्रभावित करने का सबसे सशक्त माध्यम है सिनेमा। एक खास किस्म का लोकहितवाद हमारे लोकप्रिय सिनेमा की पहचान और ताकत रही है। संदेश की दृष्टि से वी शांताराम की 'पड़ोसी', मनमोहन देसाई की 'अमर अकबर एंथोनी' और गोविंद निहलानी की 'तमस' एक जैसे हैं।
असल मकसद है इसमें फांक पैदा करना।
यह सीधे-सीधे तो किया नहीं जा सकता लिहाजा जिम्मा सौंपा गया कुछ औसत प्रतिभा वाले कलाकारों और फिल्मकारों को। समाचार माध्यमों के जरिए एक बहस चली बॉलीवु़ड में नेपोटिज्म की, दूसरा प्रॉपेगैंडा सोशल मीडिया के जरिए चलाया गया और बॉलीवुड बनाम हिंदुत्व का फंडा फैलाया गया। तीसरी तरफ दक्षिण की कुछ गुणवत्ता में औसत दर्जे की मगर सफल फिल्मों के जरिए यह बहस छेड़ी गई कि दक्षिण का सिनेमा बेहतर है।
कुल मकसद यह है कि सिनेमा जैसी सशक्त विधा को एक पॉलिटिकल प्रॉपेगैंडा का हथियार बनाया जाए। मनोरंजन की ताकत का इस्तेमाल परोक्ष रूप से खास राजनीतिक विचारधारा के प्रसार में किया जाए। देखा-देखी कई समझदार लोग भी इसी बहस में शामिल हो गए। कुछ ठीक-ठाक लिखने वाले समीक्षकों को भी नेपोटिज्म में टीआरपी दिख रही है।
दिलीप मंडल ने यही फॉर्मूला अपनाते हुए तय किया कि वे सिनेमा के जातिवादी एंगल की पड़ताल करेंगे। यानी सिनेमा को अब उसकी कला के जरिए नहीं बल्कि इस आधार पर परखा जाएगा कि उसे किसने बनाया है? उसमें जो विषय उठाए गए हैं उनके संवेदनशील निर्वहन पर बात नहीं होगी बल्कि जो लोग उसके रचयिता हैं वो किस जाति-धर्म से आते हैं इस आधार पर मूल्यांकन होगा।
यानी सिनेमा पर अब तक जो अधकचरा लिखा-पढ़ा जा रहा था, आने वाले समय में उसमें और गिरावट ही देखने को मिलेगी। सिनेमा की घरानेदारी की बहस बहुत बेबुनियाद है और गहराई में जाकर चीजों को नहीं देखा जा रहा है। लोकप्रिय सिनेमा एक बिजनेस है और कारोबार पर हमेशा घरानों का ही वर्चस्व रहा है। यकीन न हो तो देश के सबसे बड़े कारोबारियों के परिवार का इतिहास उठाकर देख लें। अमेरिका या हॉलीवुड का सिनेमा भी इसी तरह से विकसित हुआ है। डेविड सोल्जेनिक और वार्नर ब्रदर्स जैसे कई परिवारों का लंबे समय तक इंडस्ट्री पर वर्चस्व रहा है।
भारत में सिनेमा की शुरुआत स्टूडियो सिस्टम से हुई। निर्देशक, लेखक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार तक बाकायदा वेतन पर नौकरी करते थे। एक फिल्म खत्म होती तो उसी टीम के साथ अगली फिल्म शुरू की जाती थी। बांबे टॉकीज और प्रभात कंपनी ने इसी पैटर्न पर यादगार फिल्में दी हैं। लेकिन जैसे-जैसे अभिनेताओं, गीतकारों और संगीतकारों को लोकप्रियता मिलती गई वे इस सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए कसमसाने लगे। इसके बाद शुरू हुआ इंडिपेंडेंट निर्माता-निर्देशकों का दौर।
जहां तक मेरी जानकारी है प्रीतिश नंदी ने फिल्म इंडस्ट्री को कॉरपोरेट का जामा पहनाने में पहल की थी और उसी दौरान प्रीतीश नंदी कम्यूनिकेशंस और एबीसीएल सामने आए। समय से पहले के प्रयास थे सो सफल नहीं हुए। लेकिन घरानों से हटकर ये कलाकार ही थे जिन्होंने सिनेमा को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया। सरोकार वाले निर्माता-निर्देशकों को भूल जाएं, सीधे-सीधे बिजनेस की बात करें।
राज कपूर ने "आवारा हूँ" गीत को तत्कालीन सोवियत रूस के लोगों को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्मों ने एक समय में एनआरआई के बीच भारतीय सिनेमा की पैठ बनाई। केतन मेहता की प्रोडक्शन कंपनी ने तकनीकी पर फोकस बढ़ाया। विधु विनोद चोपड़ा ने बतौर निर्माता कारोबार को जबरदस्त ऊंचाइयां दीं। जिन आमिर खान को लोग कोस रहे हैं उन्होंने 'थ्री ईडियट्स' और 'दंगल' जैसी फिल्में दी हैं जिन्होंने पश्चिम और ईस्ट एशिया में एक साथ कारोबार की संभावनाओं को विस्तार दिया।
अब, जबकि सही समय आ रहा था और भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री को हॉलीवुड, कोरिया और हांगकांग के सिनेमा की तरह अंतरराष्ट्रीय फ़लक पर उड़ान भरनी थी, हम उत्तर और दक्षिण के विवाद में उलझते जा रहे हैं। (फ़ेसबुक से)
-श्रवण गर्ग
मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर कवि-पत्रकार मित्र ध्रुव शुक्ल ने कथा सम्राट के विशाल रचना संसार से ढूँढकर कुछ सवाल ‘अपने आप से पूछने के लिए’ सार्वजनिक किए हैं।पूछे गए सवालों में एक यह भी है कि ‘गोदान के होरी का क्या हुआ ?’ उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि हम प्रेमचंद को क्या जवाब देंगे ?
पिछले साल आज के ही दिन लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार विजय बहादुर सिंह के आमंत्रण पर विदिशा में पंडित ‘गंगाप्रसाद पाठक ललित कला न्यास’ द्वारा प्रेमचंद जयंती पर आयोजित एक संगोष्ठी में ‘पत्रकारिता और लोक समाज’ विषय पर बोलने का अवसर मिला था।अपनी बात प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास ‘गोदान’ से प्रारम्भ की थी।प्रेमचंद ने यह अद्भुत उपन्यास अपने निधन से दो वर्ष पूर्व 1936 में लिखा था।उन्हें तब तक शायद आभास हो गया था कि आने आने वाले भारत में उनके होरी का क्या हश्र होने वाला है ! विदिशा संगोष्ठी में जो कहा था उसे संक्षिप्त रूप में पहली बार बाँट रहा हूँ :
हम चाहें तो शर्म महसूस कर सकते हैं कि साल 1936 से 2021 के बीच गुजरे 85 सालों के बीच मुंशी प्रेमचंद द्वारा ‘गोदान’ में उकेरे गए पात्रों और उनके ज़रिए उठाए गए सवालों में कुछ नहीं बदला है। सिर्फ़ पात्रों के नाम ,उनके चेहरे और स्थान बदल गए हैं। शेष वैसा ही है। देश के जीवन में ग्रामीण भारत या तो ‘गोदान’ के समय जैसा ही है या और ख़राब हो गया है।पत्रकारिता और साहित्य के केंद्र में ग्रामीण के बजाय शहरी भारत हो गया है।
‘गोदान’ उपन्यास में प्रेमचंद का मुख्य पात्र होरी बीमार होकर मरता है, आज का होरी आत्महत्या कर रहा है। उसे सिंघु बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन करना पड़ रहा है। वह पुलिस-प्रशासन की लाठियाँ और गोलियाँ झेल रहा है। क़र्ज़ में डूबकर जान देने वाले हज़ारों किसानों के चेहरों में होरी की शक्ल तलाश की जा सकती है। ‘गोदान’ में वर्णित ज़मींदार की भूमिका सरकारों ने ले ली है और तहसीलदार-पटवारी उसके वसूली एजेंट हो गए हैं।
अखबारी दुनिया में भी कुछ नहीं बदला है। ’गोदान’ में उल्लेखित ‘बिजली’ पत्र के राय साहब जैसे मालिक-सम्पादक व्यवस्था में आज भी न सिर्फ़ उसी तरह उपस्थित हैं बल्कि ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। वे अब होरी की ही तक़दीर नहीं सरकारें बनाने-गिराने की हैसियत में पहुँच गए हैं। ‘गोदान’ की ही तरह सौ या हज़ार ग्राहकों का चंदा भरकर या विज्ञापनों के दम पर आज भी खबरें ‘गोदान’ की तरह रुकवाई-छपवाई जा सकतीं हैं। धर्म और सत्ता की राजनीति के बीच हुई साँठगाँठ ने पत्रकारिता को विज्ञापन और चंदा वसूल करने की मशीन में तब्दील कर दिया है। होरी की मौत मीडिया की नज़रों से ग़ायब है। किसानों को बाँटे जाने वाले नक़ली बीजों और उर्वरकों की तरह ही नक़ली खबरें भी राजनीति के ज़मींदारों के द्वारा राय साहबों के अख़बारों की मदद से जनता को बेची जा रहीं हैं।
मुंशी प्रेमचंद के ‘गोदान’ में जिस गाय की अतृप्त आस में होरी को अंतिम साँस लेना पड़ती है वह गाय इस समय सत्ता की साँस बन गई है। चिंता होरी के मरने की नहीं है, गाय अगर छूट गई तो सत्ता की साँस उखड़ जाएगी। समूची राजनीति को होरी के जन-जल-जंगल-ज़मीन-जानवर से विमुख कर गाय-गोबर-गोमूत्र के चमत्कार में केंद्रित कर दिया गया है।
मुंशी प्रेमचंद को हम कुछ भी जवाब देने की स्थिति में नहीं बचे हैं।
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
भारत के गृहमंत्री अमित शाह जिस मर्दानगी से शिक्षा में भारतीय भाषाओं के माध्यम का समर्थन कर रहे हैं, आज तक वैसी मर्दानगी मैंने भारत के किसी प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री में भी नहीं देखी। यह ठीक है कि मैकाले की गुलामी से भारतीय शिक्षा को मुक्त करवाने का प्रयत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, त्रिगुण सेन, डा. जोशी, भागवत झा आजाद और प्रो. शेरसिंह—जैसे शिक्षा मंत्रियों ने जरुर किया है लेकिन अमित शाह ने अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है।
वे अंग्रेजी की अनिवार्यता के खिलाफ महर्षि दयानंद, गांधी, लोहिया या मेरी तरह नहीं बोल रहे हैं लेकिन वे जो कुछ बोल रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि देश की शिक्षा पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। इसका पहला कदम यह है कि देश में डाक्टरी, वकीली, इंजीनियरी, विज्ञान, गणित आदि की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषाएं या भारतीय भाषाएं ही होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए? क्योंकि अमित शाह कहते हैं कि देश के 95 प्रतिशत बच्चे अपनी प्रारंभिक पढ़ाई स्वभाषा के माध्यम से करते हैं। सिर्फ पांच प्रतिशत बच्चे, निजी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं? ये किनके बच्चे होते हैं? मालदार लोगों, नेताओं, बड़े अफसरों और ऊँची जातिवालों के बच्चे ही मोटी-मोटी फीस भरकर इन स्कूलों में जा पाते हैं। अमित शाह की चिंता उन 95 प्रतिशत बच्चों के लिए हैं, जो गरीब हैं, ग्रामीण हैं, पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक हैं।
ये बच्चे आगे जाकर सबसे ज्यादा फेल होते हैं। ये ही पढ़ाई अधबीच में छोडक़र भाग खड़े होते हैं। बेरोजगारी के शिकार भी ये ही सबसे ज्यादा होते हैं। यदि केंद्र की भाजपा सरकार राज्यों को प्रेरित कर सके तो वे अपनी शिक्षा उनकी अपनी भाषाओं में शुरु कर सकती हैं। 10 राज्यों ने केंद्र से सहमति व्यक्त की है। अब ‘जी’ और ‘नीट’ की परीक्षाएं भी 12 भाषाओं में होंगी। केंद्र अपनी भाषा-नीति राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं कर सकता है लेकिन भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं?
वे अपने राज्यों की सभी पार्टियों के नेताओं से शिक्षा में क्रांति लाने का आग्रह क्यों नहीं करते? गैर-भाजपाई राज्यों से अमित शाह बात कर रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं और शिक्षा मंत्री भी उनसे बात करें तो यह क्रांतिकारी कदम शीघ्र ही अमल में लाया जा सकता है। मध्यप्रदेश की सरकार तो सितंबर से डाक्टरी की पढ़ाई हिंदी में शुरु कर ही रही है।
सिर्फ नई शिक्षा नीति की घोषणा कर देना काफी नहीं है। पिछले 8 साल में बातें बहुत हुई हैं, शिक्षा और चिकित्सा में सुधार की लेकिन अभी तक ठोस उपलब्धि निर्गुण और निराकार ही है। यदि देश की शिक्षा और चिकित्सा को मोदी सरकार औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त कर सकी तो उसे दशकों तक याद किया जाएगा। भारत को महासंपन्न और महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। (नया इंडिया की अनुमति से)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
प. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार भयंकर दुर्गति को प्राप्त हो गई है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ममता बेनर्जी की सरकार इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर सकती है। ममता के राज में मैं जब-जब कोलकाता गया हूँ, वहां के कई पुराने उद्योगपतियों और व्यापारियों से बात करते हुए मुझे लगता था कि ममता के डर के मारे अब वे कोई गलत-सलत काम नहीं कर पा रहे होंगे लेकिन उनके उद्योग और व्यापार मंत्री पार्थ चटर्जी को पहले तो जांच निदेशालय ने गिरफ्तार किया और फिर उनके निजी सहायकों, मित्रों और रिश्तेदारों के घरों से जो नकद करोड़ों रु. की राशियां पकड़ी गई हैं, उन्हें टीवी चैनलों पर देखकर दंग रह जाना पड़ता है।
अभी तो उनके कई फ्लेटों पर छापे पडऩा बाकी है। पिछले एक सप्ताह में जो भी नकदी, सोना, गहने आदि छापे में मिले हैं, उनकी कीमत 100 करोड़ रु. से भी ज्यादा का ही अनुमान है। यदि जांच निदेशालय के चंगुल में उनके कुछ अन्य मंत्री भी फंस गए तो यह राशि कई अरब तक भी पहुंच सकती है। बंगाल के मारवाड़ी व्यवसायियों का खून चूसने में ममता सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्थ चटर्जी सिर्फ तीन विभागों के मंत्री ही नहीं है। उन्हें ममता बेनर्जी का उप-मुख्यमंत्री माना जाता है।
इस हैसियत में ममता का सारा लेन-देन वही करते रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। वे पार्टी के महामंत्री और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें बंगाल के लोग पार्टी की नाक मानते रहे हैं। इसीलिए उनकी गिरफ्तारी के छह दिन बाद तक उनके खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटता रहा। तृणमूल के नेता भाजपा सरकार पर प्रतिशोध का आरोप लगाते रहे।
अब जबकि सारे देश में ममता सरकार की बदनामी होने लगी तो कुछ होश आया और पार्थ चटर्जी को मंत्रिपद तथा पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त किया गया है। यह बर्खास्तगी नहीं, सिर्फ मुअत्तिली है, क्योंकि पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जांच में वे खरे उतरेंगे, तब उनको उनके सारे पदों से पुन: विभूषित कर दिया जाएगा। यह मामला सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार का ही नहीं है। देश की कोई भी पार्टी और कोई भी नेता यह दावा नहीं कर सकता कि वे भ्रष्टाचार-मुक्त हैं।
भ्रष्टाचार के बिना याने नैतिकता और कानून का उल्लंघन किए बिना कोई भी व्यक्ति वोटों की राजनीति कर ही नहीं सकता। रूपयों का पहाड़ लगाए बिना आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? अपने निर्वाचन-क्षेत्र के पांच लाख से 20 लाख तक के मतदाताओं को हर उम्मीदवार कैसे पटाएगा? नोट से वोट और वोट से नोट कमाना ही अपनी राजनीति का मूल मंत्र है। इसीलिए हमारे कई मुख्यमंत्री तक जेल की हवा खा चुके हैं।
नोट और वोट की राजनीति विचारधारा और चरित्र की राजनीति पर हावी हो गई है। यदि हम भारतीय लोकतंत्र को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो राजनीति में या तो आचार्य चाणक्य या प्लेटो के ‘दार्शनिक नेता’ जैसे लोगों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। वरना आप जिस नेता पर भी छापा डालेंगे, वह आपको कीचड़ में सना हुआ मिलेगा। (नया इंडिया की अनुमति से)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति की जगह ‘राष्ट्रपत्नी’ शब्द बोलकर तूफान-सा खड़ा कर लिया है। यह शब्द उन्होंने कल संसद के बाहर कहीं बोल दिया था। भाजपा के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता देश में जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान है। इसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद की कार्रवाई भी इस मुद्दे को लेकर ठप्प हो गई है।
भाजपा के मंत्री और सांसद आग्रह कर रहे हैं कि अधीर रंजन संसद में माफी मांगे। अधीर रंजन का कहना है कि वे भाजपाइयों से माफी क्यों मांगें? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले ही राष्ट्रपति से माफी मांग ली है। उनकी जुबान फिसल जाने का उन्हें दुख है। वे बंगाली है। उन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती। यह तर्क तो कमजोर है। क्या कोई बंगाली कह सकता है कि वह पति और पत्नी शब्दों में अंतर करना नहीं जानता? वैसे अधीर रंजन इस तरह की गल्तियां करने के लिए पहले से जाने जाते हैं।
उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक बार ‘गंदी नाली’ की उपमा दे दी थी। उन्होंने कश्मीर को भारत का सिर्फ भौगोलिक हिस्सा बता दिया था। उन्होंने पं. बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ‘पागल’ तक कह दिया था। उम्मीद है कि भाजपाइयों का यह क्रोध-प्रदर्शन उन्हें अब अधीर रंजन से सुधीर रंजन बना देगा। लेकिन इस विवाद ने मेरी एक पुरानी दुखती रग पर उंगली रख दी है।
पचासों वर्षों पहले मैं सोचता रहता था कि यदि कोई महिला हमारे देश के इस सर्वोच्च पद पर पहुंचेगी तो क्या उसे भी हम ‘राष्ट्रपति’ ही कहेंगे? तब मुझे लगता था कि इस शब्द का कोई विकल्प ढूंढना चाहिए वरना बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी। तब मेरे दिमाग में जो वैकल्पिक शब्द आया, वह था- राष्ट्राध्यक्ष! यदि कोई महिला इस पद पर चुनी गई तो उसे हम ‘राष्ट्राध्यक्षा’ आसानी से कह सकते हैं।
लेकिन अपना देश तो अंग्रेजी का गुलाम है। उसमें ‘प्रेजिडेंट’ शब्द का प्रयोग किसी भी महिला या पुरुष या दोनों के लिए हो सकता है तो अंग्रेजी के ‘प्रेजिडेंट’ का हिंदी अनुवाद ‘राष्ट्रपति’ भी दोनों पर थोपा जा सकता है। मेरी राय में यह गलत है। ‘राष्ट्रपत्नी’ शब्द को आपत्तिजनक बताकर हम क्या भारत के महिला समाज का अपमान नहीं कर रहे हैं?
लेकिन इस प्रश्न का उचित समाधान यही है कि हम पति और पत्नी के दलदल में न फंसें और राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी के बजाय राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्षा शब्दों का प्रयोग करें। यही प्रयोग लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों और अध्यक्षाओं के लिए भी हो सकता है, हालांकि पति शब्द ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग सिर्फ पत्नी के विलोम के रूप में ही इस्तेमाल किया जाए। (नया इंडिया की अनुमति से)
-प्रियंका झा
अपने पहनावों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अब बिना कपड़ों की तस्वीरें खिंचवाने और शेयर करने की वजह से चर्चा में है. दूसरी ओर, इन तस्वीरों की वजह से रणवीर सिंह पर अश्लीलता फैलाने का मामला दर्ज किया गया है.
दरअसल, एक से बढ़कर एक हिट फ़िल्मों में काम कर चुके रणवीर सिंह ने हाल में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ न्यूड तस्वीरें शेयर कीं, जो अमेरिकी मैगज़ीन 'पेपर' के लिए खींची गई थी. रणवीर सिंह की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
वहीं, इन तस्वीरों को आपत्तिजनक मानते हुए दो लोगों ने रणवीर सिंह के ख़िलाफ़ मुंबई के चेंबुर में शिकायत दर्ज कराई है. इनमें से एक महिला हैं और दूसरे शख्स एनजीओ से जुड़े हैं.
शिकायतकर्ताओं के वकील अखिलेश चौबे के अनुसार रणवीर सिंह की न्यूड तस्वीरों को ज़ूम करने पर उनके 'प्राइवेट पार्ट दिख रहे थे'. इससे 'महिलाओं की भावनाएं' आहत हुई और उनकी गरिमा को ठेस पहुँची है.
बॉलीवुड सितारों पर इस तरह के मामले कोई नई बात नहीं है. मॉडलिंग की दुनिया से आए मिलिंद सोमन और पूनम पांडे जैसे कलाकार भी इस तरह के मुकदमे झेल चुके हैं.
न्यूड फ़ोटोग्राफ़ी कुछ लोगों के लिए कला को रचनात्मक ढंग से परोसने का तरीका है तो दूसरा धड़ा इसे अश्लीलता मानता है. इसलिए समय-समय पर ये विषय बहस का मुद्दा बनता रहा है.
मगर कोई काम या सामग्री अश्लीलता के दायरे में कब आ जाती है? और भारत में इसको लेकर कानून क्या कहता है?
क्या है पूरा मामला
रणवीर सिंह ने अमेरिकी पत्रिका 'पेपर' के कवर के लिए कराए न्यूड फ़ोटोशूट की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की. इंस्टाग्राम पर उनके चार करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं.
रणवीर सिंह की पोस्ट को करीब साढ़े 22 लाख लोगों ने इंस्टाग्राम पर पसंद किया है लेकिन इसने कुछ लोगों को असहज भी कर दिया. शिकायत के बाद मुंबई में रणवीर के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 292, 293 और 509 के साथ आईटी एक्ट की धारा 67 (ए) के तहत केस दर्ज किया गया है.
प्राथमिकी में कहा गया है, भारत की एक 'अच्छी संस्कृति' है और ऐसी तस्वीरों की वजह से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं.
बीबीसी हिंदी से बात करते हुए शिकायकर्ता के वकील ने दलील दी कि संभव है कि रणवीर की तस्वीरें 40 से 45 साल के लोगों को अश्लील न लगे लेकिन ये 20 साल के युवक-युवतियों के लिए अश्लील है.
आईपीसी में क्या है प्रावधान?
भारत में क़ानूनी नज़रिये से अश्लीलता एक अपराध है और इसके लिए सज़ा का प्रावधान है.
आईपीसी की धारा 292, 293 और 294 अश्लीलता से जुड़े मामलों के लिए है, लेकिन इनमें ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि अश्लीलता आखिर है क्या.
सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राहुल शर्मा के अनुसार धारा 292 ये बताती है कि किसी रचना या सामग्री को कब अश्लील कहा जा सकता है.
इसके अनुसार अगर कोई शख्स ऐसी अभद्र सामग्री, किताब या अन्य आपत्तिजनक सामान बेचे अथवा उसे सर्कुलेट करे जो दूसरों को नैतिक रूप से परेशानी या तकलीफ़ देती हो तो दोषी पाए जाने पर उसे दो साल की सज़ा और दो हज़ार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर कोई शख्स दूसरी बार ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो सज़ा बढ़कर 5 साल तक हो सकती है.
रणवीर सिंह के ऊपर आईपीसी की जो धारा 293 लगाई गई है उसके तहत अश्लील सामग्री 20 साल से कम के युवक-युवतियों को बेचने या सर्कुलेट करने पर 3 साल से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है.
आईपीसी की धारा 294 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील कृत्य करने वालों के लिए सज़ा का प्रावधान है. हालाँकि, रणवीर सिंह पर दर्ज एफ़आईआर में इस धारा का ज़िक्र नहीं है.
रणवीर पर दर्ज दो अन्य धाराओं में से एक धारा 509 के तहत महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने के मकसद से किया गया कोई काम, कहे गए शब्द या फिर हावभाव आते हैं. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.
वहीं, अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक तरीके यानी सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित करने पर आईटी एक्ट की धारा 67 ए के तहत अधिकतम 5 साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. दोबारा या कई बार ऐसे अपराध करने पर 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. यहाँ जानना ज़रूरी है कि ये गैर-ज़मानती धारा है.
तो गैर-ज़मानती धारा के बावजूद रणवीर सिंह की गिरफ़्तारी क्यों नहीं हुई?
इस सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय के वकील और सायबर कानून के जानकार विराग गुप्ता कहते हैं, "अगर किसी एफ़आईआर में गैर-ज़मानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है तो भी अभियुक्त की गिरफ़्तारी ज़रूरी नहीं है. कानून और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार यदि अभियुक्त जाँच में सहयोग नहीं कर रहा हो, सबूतों के साथ खिलवाड़ होने की आशंका हो या फिर हिरासत में पूछताछ ज़रूरी हो, तभी पुलिस को गिरफ़्तारी करनी चाहिए."
यहाँ सवाल उठता है कि आईपीसी में अश्लीलता की परिभाषा नहीं है तो फिर ये कैसे तय होता है कि कौन सी सामग्री अश्लील है और कौन नहीं?
दिलचस्प है कि इसके लिए भारतीय अदालतें अब तक अंग्रेज़ी कानून का सहारा लेती आई हैं.
अदालतों में कैसे हुए फैसले?
जानकारों के मुताबिक, साल 2014 तक अदालतों में जजों ने 'हिक्लिन टेस्ट' के ज़रिए ये तय किया कि कोई सामग्री अश्लील है या नहीं. इस टेस्ट नाम इंग्लैंड में 1868 में आए एक मामले के आधार पर पड़ा था.
अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिक्लिन टेस्ट को दरकिनार करते हुए इसे अमेरिका में प्रचलित रौथ टेस्ट की कसौटी पर परखा. इसके तहत माना जाता है कि नग्नता को संवेदनशील लोगों के किसी समूह की बजाय तात्कालिक सामाजिक मानकों को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य व्यक्ति के नज़रिए से मापा जाना चाहिए.
वकील राहुल शर्मा कहते हैं, ""हिक्लिन टेस्ट के अंतर्गत देखा जाता है कि क्या कोई अश्लील सामग्री किसी व्यक्ति को अनैतिक रूप से प्रभावित कर रही है. इस परीक्षण की एक बड़ी कमी ये थी कि ये उस सामग्री को भी अश्लील मानता था, जिसने भले ही किसी कमज़ोर मानसिकता वाले को ही प्रभावित क्यों न किया हो."
"चूंकि, नैतिकता समय और समाज के साथ बदलती रहने वाली अवधारणा है, इसलिए सामाजिक मानक परीक्षण अभियव्यक्ति की आज़ादी और मर्यादा तथा नैतिकता के अंकुश के बीच एक संतुलन बैठाता है."
ये मामला टेनिस के महान खिलाड़ी रहे बोरिस बेकर की उनकी मंगेतर के साथ न्यूड तस्वीर से जुड़ा था. तस्वीर मूल रूप से एक जर्मन पत्रिका में छपी थी लेकिन इसे भारत में स्पोर्ट्सवर्ल्ड मैगज़ीन और आनंद बाज़ार पत्रिका अख़बार ने भी छापा था.
आनंद बाज़ार पत्रिका समूह से जुड़े इस मामले की सुनवाई करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि तस्वीर त्वचा से गोरे पुरुष और काली महिला के बीच प्यार को दिखा रही है. तस्वीर का संदेश है कि त्वचा का रंग नहीं बल्कि प्यार मायने रखता है.
रणवीर सिंह को इस मामले में सज़ा हो सकती है या नहीं इस सवाल पर वकील विराग गुप्ता का मानना है, "ऐसे मामले लग्ज़री लिटिगेशन की कैटेगरी में आते हैं. हेडलाइन बनने से शिकायतकर्ता और सेलेब्रिटी सभी को पब्लिसिटी मिल जाती है. शुरुआती दौर में अदालत से राहत मिलने के बाद मुकदमे का आखिरी फैसला आने में अच्छा-खासा वक्त बीत जाता है. इस प्रक्रिया को ही दण्ड माना जाता है. सामान्यतः ऐसे मामलों में लोगों को सज़ा नहीं होती." (bbc.com/hindi)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
उर्दू में एक कहावत है कि माले-मुफ्त और दिले-बेरहम! इसे हमारे सभी राजनीतिक दल चरितार्थ कर रहे हैं याने चुनाव जीतने और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वे वोटरों को मुफ्त की चूसनियाँ पकड़ाते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रेवड़ी संस्कृति कहा है, जो कि बहुत सही शब्द है। असली कहावत तो यह है कि ‘अंधा बांटे रेवड़ी, अपने-अपने को देय’ लेकिन हमारे नेता लोग अंधे नहीं हैं।
उनकी तीन आंखें होती हैं। वे अपनी तीसरी आंख से सिर्फ अपने फायदे टटोलते हैं। इसलिए सरकारी रेवडिय़ां बांटते वक्त अपने-पराए का भेद नहीं करते। उनकी जेब से कुछ जाना नहीं है। वोटरों को मुफ्त माल बांटकर वे अपने लिए थोक वोट पटाना चाहते हैं। वे क्या-क्या बांट रहे हैं, उसकी सूची बनाने लगें तो यह पूरा पन्ना ही भर जाएगा।
शराब की बोतलों और नोटों की गड्डियों की बात को छोड़ भी दें तो वे खुले-आम जो चीजें मुफ्त में बांटते हैं, उनका खर्च सरकारी खजाना उठाता है। इन चीजों में औरतों को एक हजार रु. महिना, सभी स्कूली छात्रों को मुफ्त वेश-भूषा और भोजन, कई श्रेणियों को मुफ्त रेल-यात्रा, कुछ वर्ग के लोगों को मुफ्त इलाज और कुछ को मुफ्त अनाज भी बांटा जाता है। इसका नतीजा यह है कि देश के लगभग सभी राज्य घाटे में उतर गए हैं। कई राज्य तो इतने बड़े कर्जे में दबे हुए हैं कि यदि रिजर्व बैंक उनकी मदद न करे तो उन्हें अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा।
इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस सहित लगभग सभी दलों के राज्य हैं। तमिलनाडु और उप्र पर लगभग साढ़े छह लाख करोड़, महाराष्ट्र, पं. बंगाल, राजस्थान, गुजरात और आंध्रप्रदेश पर 4 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ रु. तक का कर्ज चढ़ा हुआ है। इन राज्यों की हालत श्रीलंका-जैसी है। उसका कारण उनकी रेवड़ी-संस्कृति ही है। इसे लेकर जनहित याचिकाएं लगानेवाले प्रसिद्ध वकील अश्विनी उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटा दिए। अदालत के जजों ने चुनाव आयोग और सरकारी वकील की काफी खिंचाई कर दी।
वित्त आयोग इस मामले में हस्तक्षेप करे, यह अश्विनी उपाध्याय ने कहा। चुनाव आयोग ने अपने हाथ-पांव पटक दिए। उसने अपनी असमर्थता जता दी। उसने कहा कि मुफ्त की इन रेवडिय़ों का फैसला जनता ही कर सकती है। उससे पूछे कि जो जनता रेवडिय़ों का मजा लेगी, वह फैसला क्या करेगी?
मेरी राय में इस मामले में संसद को शीघ्र ही विस्तृत बहस करके इस मामले में कुछ पक्के मानदंड कायम कर देने चाहिए, जिनका पालन केंद्र और राज्यों की सरकारों को करना ही होगा। कुछ संकटकालीन स्थितियां जरुर अपवाद-स्वरूप रहेंगी। जैसे कोरोना-काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा गया। वैसे ये रेवडिय़ां जनता को दी जानेवाली शुद्ध रिश्वत के अलावा कुछ नहीं हैं। (नया इंडिया की अनुमति से)
-अपूर्व गर्ग
दोनों हिन्दुस्तानी कहानीकार ..एक बाद में विवश होकर पाकिस्तान गए .
दोनों सबसे बड़े गालीबाज .
दोनों सबसे विद्रोही और सताए कहानीकार .
एक उर्दू का महान अफ़साना निगार तो दूसरा हिंदी का .
दोनों की ज़िंदगी में शराब में डूबी रही .
सआदत हसन मंटो गले तक डूबे रहे
तो पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र ' उदर तक !
दोनों को सबसे अश्लील कहानीकार माना गया .
दोनों बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में रहे ..
मंटो लम्बा रहे और बड़ी हस्तियों के साथ रहे जबकि उग्र जी 124 A के तहत अंग्रेज़ों के खिलाफ राजद्रोह के आरोपी थे , फरारी काटने के दौरान फिल्मों से जुड़े पर जल्दी पकडे गए .
दोनों ने जिस्म मंडियों को जिस तरह देखा, भोगा उसी तरह लिखा ...
जो देखा वो लिखा ,इसलिए सबसे फसादी लेखक रहे और बहिष्कृत, तिरस्कृत होकर दुर्दिन देखे, भयानक गरीबी देखी .
एक को बार -बार पागलखाने में शरण लेनी पड़ी तो दूसरे ज़िंदगी भर गुस्सैल ओर उग्र रहे ...ये हाल बनाया इस समाज ने दो सबसे महान कहानीकारों का .
टॉलस्टॉय ,गोर्की ,शेक्सपियर ,मिल्टन जैसे लेखकों के नाम उनके देशों ने सब कुछ समर्पित कर दिया ..मूर्तियाँ छोड़िये उनके नाम के नगर भी छोड़िये उनके लेखन और व्यक्तित्व को जितने सम्मान से रखा गया उतना ही अपमान इस देश में हिंदी -उर्दू साहित्यकारों के साथ हुआ .
मणिकर्णिका घाट की ओर 20-25 लोग प्रेमचंद की अर्थी लेकर चलते हैं और पूछने पर बताते हैं कोई मास्टर था !
मंटो एक बैरिस्टर के बेटे ज़रूर रहे पर बहुत जल्दी घर छोड़ा और पूरा जीवन जूझते रहे .
पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' के पैदा होने से पहले उनके एक दर्ज़न से ज़्यादा भाई बहन दम तोड़ चुके थे .
उनके पैदा होने के बाद उनकी माँ जयकली ने महज़ एक टके में बेच दिया और ये हमेशा 'बेचन ' कहलाये .
मंटो की ठंडा गोश्त, काली सलवार, हतक, बू जैसी कहानियों को अश्लील घोषित कर मंटो को हर तरह से पीड़ा दी गई तो पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र ' की 'चॉकलेट' के खिलाफ अश्लीलता फैलाने का प्रचार कर उनके साहित्य को 'घासलेटी साहित्य' घोषित कर मुहिम चलाई गयी .
बनारसीदास चतुर्वेदी ने इस मुहिम की अगुवाई ही नहीं की, गांधीजी से हस्तक्षेप की मांग की .
गांधीजी ने बाक़ायदा पढ़कर चतुर्वेदी जी की मुहिम की हवा निकाल दी और उन्हें पत्र भी लिखा था जो कभी सामने नहीं लाया गया .
मंटो अमृतसर में फैज़ के शिष्य थे, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े .
दिल्ली के रेडियो स्टेशन में मंटो नौकरी पर थे. मंटो के नाटक नियमित प्रसारित होते .
मंटो अपनी दुनिया में रहते, अकेला महसूस करते पर उनका एक साहित्यिक सर्किल था जिसमें
दुश्मनों के साथ कृष्ण चन्दर, बेदी, शाहिद लतीफ़, इस्मत चुगताई जैसे कई थे
बम्बई में मंटो टॉप के फिल्म अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, निर्माताओं की संगत में थे.
निर्माता एस. मुखर्जी, अशोक कुमार, श्याम, देविका रानी, हिमांशु रॉय, नरगिस, नूरजहां ..
मंटो के साथ उनकी हमसफ़र सफ़िया थीं उनके बच्चे भी थे ...
पर एक टके में बिकने के बाद ठोकरें खाते बेचन ...उग्र के सिर्फ एक बड़े भाई थे जो उन पर जम कर ज़ुल्म करते और ऐसी ठोकरें खाकर पांडेय बेचन शर्मा काफी 'उग्र ' बने.
बाद में बेऔलाद चाचा ने बेचन को गोद ज़रूर लिया पर बाद में अपनी औलाद होते ही बेचन को बाहर कर दिया .
'अपनी ख़बर ' लेते हुए उग्र जी ने लिखा भी है 'सच तो ये है शिक्षा शब्द मेरे निकट आते-आते भिक्षा बन जाया करता था .
इसी कड़वाहट के साथ लड़ते भिड़ते पढ़ते रहे. बाद में कभी दैनिक आज में तो कभी कलकत्ता के मतवाले में रहे फ़िल्मी लेखन किया तो चॉकलेट ,,चंद हसीनों के खतूत, फागुन के दिन चार दिल्ली का दरबार, शराबी पीली इमारत, ग़ालिब और उग्र जैसी ढेरों पुस्तकें लिखीं .
हरिशंकर परसाई ने उग्रजी के लिए लिखा है -'बेचन शर्मा उग्र फक्कड़, लीजेंड थे. अक्खड़, फक्कड़ और बदज़बान. जीवन के अँधेरे से अँधेरे कोने में वे घुसे थे और वहां से अनुभव लाये थे .''
परसाई जी बताते हैं एक प्रकाशक ने कहानी संग्रह तैयार करने को कहा. संग्रह में उनकी एक कहानी 'उसकी माँ ' लेना तय हुआ .उग्रजी को लिखा गया प्रकाशक सौ रुपये भेजेगा. प्रकाशक ने संग्रह छापने का विचार छोड़ दिया. 5 महीने बाद उग्रजी का पत्र मिला कि पुस्तक छापकर कोर्स में लग गयी होगी ...प्रकाशक और तुम खूब पैसे कमा रहे होंगे पर मुझे सौ रुपये नहीं भेजे .
मैं तुम जैसे हरामज़ादे, कमीने, बेईमान, लुच्चे लेखकों को जानता हूँ ...परसाई जी ने जवाब दिया -' प्रकाशक ने वह पुस्तक नहीं छापी ...इसलिए आपको पैसे नहीं भेजे गए, जहाँ तक मुझे दी गयी आपकी गालियों का सवाल है, मैंने काफी गालियां आपसे ही सीखी हैं.......''
इसके बाद उग्र जी का पोस्ट कार्ड आया -" वाह पट्ठे ''
अश्कजी ने मंटो को 'मंटो मेरा दुश्मन' में याद कर लिखा है कैसे 'आठ दिन ' की शूटिंग के दौरान मंटो उन्हें गालियां देते हैं और थोड़ी देर बाद हाथ दबाकर माफ़ी भी मांग लेते हैं .
कृष्ण चन्दर ने लिखा है --''मंटो एक बहुत बड़ी गाली था। उसका कोई दोस्त ऐसा नहीं था, जिसे उसने गाली न दी हो । कोई प्रकाशक ऐसा न था, जिससे उसने लड़ाई मोल न ली हो, कोई मालिक ऐसा न था, जिसकी उसने बेइज्ज़ती न की हो। प्रकट रूप से वह प्रगतिशीलों से खुश नहीं था, न अप्रगतिशीलों से, न पाकिस्तान से, न हिन्दुस्तान से, न चचा सैम से, न रूस से। जाने उसकी बेचैन और बेक़रार आत्मा क्या चाहती थी। उसकी ज़बान बेहद तल्ख थी।''
पाकिस्तान जाने के बाद मंटो रेडियो पर प्रतिबंधित थे पर उनकी मौत के बाद रेडियो पाकिस्तान ने आधे घंटे का कार्यक्रम रखा .
उग्रजी पर हरिवंश राय बच्चन ने सबसे सुंदर संस्मरण लिखा है :
बच्चनजी ने उग्र के व्यक्तित्व पर लिखा है '' उग्र महात्मा थे -महान. उनके सम्बन्धियों जाति भाइयों, उनके मित्रों ने भी उन्हें गलत समझा था, उनके साथ बहुत अन्याय किया था. वे अपने को अकेले पाते पर अकेलेपन की हीनता से पीड़ित मैंने उन्हें कभी नहीं देखा ........
एक बार उनके बीमारी की ख़बर पढ़कर मैंने उन्हें कुछ भेजने की आज्ञा चाही थी .उन्होंने मेरे पत्र का उत्तर ही नहीं दिया. मिलने पर उन्होंने कहा था तुमसे पैसे लेकर तुम्हारे सामने कभी आने पर मुझे अहसानमंद होना पड़ता, वह मैं किसी के सामने नहीं हुआ हूँ ........अहसानमंद तो मैं अपनी लाश उठाने वाले का भी न होना चाहूंगा ..... जब मैं मरुँ और तुमको ख़बर मिले तो मेरी लाश हरिजनों से उठवाकर बस्ती से दूर किसी नदी में फिकवा देना .''
बच्चन जी ने आगे लिखा है '' उनके मरने की ख़बर मुझे मिली थी ...मृत्यु के पश्चात मैंने बहुत से चेहरे देखे ,लेकिन जितनी शान्ति उग्र के चेहरे पर थी ,उतनी मैंने किसी मृतक के चेहरे पर न देखी थी. मृत्यु में सच कहूं तो उनका चेहरा सुंदर हो गया था ...''
उग्र निराला से कैसे भिड़ते कैसे पेश आते इसका ज़्यादा ज़िक्र है, पर यही उग्र निराला से दुर्व्यहार करने वाले प्रकाशक महादेव प्रसाद सेठ को विवश करते हैं वो निरालाजी से माफ़ी मांगे . इसके बाद निराला 'मतवाले ' के दरवाज़े पर आकर उग्र से कहते हैं ' तुम मर्द हो ' किसे याद है.
मंटो और उग्र की ज़बान जितनी खराब और ऊपर जितने सख़्त दीखते, अंदर से उतने ही कोमल थे.
मंटो और उग्र की कहानी कुछ बदलाव के साथ एक जैसी रही. मुझे मंटो उर्दू कहानियों के उग्र तो
उग्र हिंदी कहानी के मंटो भी नज़र आते हैं.
-अशोक पांडेय
1921 से आज तक हुई सैकड़ों बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट्स निकाली गयी होंगी और जाहिर है इन सूचियों में जगह पाने वालों की संख्या हजारों में रही होगी। आप हाल के अखबार उठा कर देख लीजिये। सभी टॉपर्स अपने-अपने भविष्य की बड़ी-बड़ी योजनाओं की बाबत आपको सूचित करता नजर आते हैं। इन योजनाओं में देश-संसार को पूरी तरह बदल देने के सपने शामिल होते हैं और उन सपनों को असलियत में बदलने की वैसी ही कार्यनीतियों की डीटेल्स भी होती हैं। कोई आईएएस-आईएफएस बनना चाहता है, कोई गरीबों को पढ़ाना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है तो कोई देश से कूड़ा खत्म करना चाहता है।
इतने हजार टॉपर्स की मेहनत के बाद हमें जैसे मोहल्ले-नगर-राज्य-देश और दुनिया नजर आते हैं उनकी तरफ एक निगाह भर डालने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि सच्चाई कितनी नंगी है।
मैं टॉपर्स के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उनके सपनों के खिलाफ भी नहीं हूँ। मेरी दिलचस्पी फकत इतना जानने में है कि ये टॉपर्स समाज के कितने काम आते हैं। और यह भी कि क्या हमारी शिक्षा पद्धति ने उन्हें इस लायक छोड़ा भी है कि वे समाज में बदलाव ला सकने वाले किसी बड़े काम में हिस्सेदारी कर सकें।
हमारे यहाँ कोई ऐसी रिसर्च हुई या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन बोस्टन अमेरिका की कैरेन आर्नोल्ड ने टॉपर्स को लेकर एक ऐसा शोध किया है और बाकायदा साबित किया है कि 90 प्रतिशत टॉपर्स अपने व्यक्तिगत जीवन में खासे सफल रहे हैं लेकिन उनमें से किसी एक ने भी संसार को नहीं बदला है। वे सब एक बने-बनाए और घिसे-पिटे रास्ते पर चल कर बड़े अफसर और कंपनियों के सीईओ वगैरह तो बने लेकिन दुर्गम जंगल को काटकर नया रास्ता बनाने का काम किसी ने नहीं किया।
पिछले सौ वर्ष की महानतम मानवीय उपलब्धियों पर निगाह डालें तो पता लगता है कि ये सभी बड़े कारनामे करने वाले स्कूली परीक्षाओं में फिसड्डी रहा करते थे अलबत्ता समाज को लेकर उनका ज्ञान और नजरिया विषद था। तो हो सकता है कि आपके नगर का टॉपर डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे मुश्किल सवाल चुटकियों में हल कर देता हो लेकिन उसे यह मालूम न हो कि पॉपकॉर्न भुट्टे से बनता है और बेसन चने की दाल से। और हो यह भी सकता है कि पड़ोस में रहने वाला, बार-बार गणित में कमजोर बताया जाने वाला, भोंदू के नाम से विख्यात कोई लडक़ा आपके उड़े हुए फ्यूज को मिनट से पहले जोड़ देता हो।
मैं ऐसे टॉपर को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिसने सरकारी नौकरी नहीं की और डाक्टरी की बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद उड़ीसा के आदिवासियों के बीच रह कर अपनी जि़ंदगी गुजारी। उसके चाचा अक्सर कहते पाए जाते हैं कि उसने समाजसेवा के चक्कर में अपनी जिन्दगी बर्बाद कर ली है। एक ऐसे दूसरे टॉपर से भी मेरा परिचय है जिसने बड़ा सरकारी अफसर बन कर बीस सालों में इतनी रकम खड़ी कर ली है कि वह अपनी रोलेक्स घडिय़ों की संख्या तक भूल जाता है। वह बताता है कि उसके संग्रह में दुनिया की सबसे महंगी शराबों का जखीरा भरा पड़ा है। उसके बारे में राजधानी के सर्कल्स में चल चुका है कि एक पेटी एक्सक्लूसिव सिंगल माल्ट शराब देकर उससे किसी भी फाइल पर दस्तखत करवाए जा सकते हैं।
हमारे देश के टॉपर्स के बाद के जीवन और उसके योगदान पर जब कोई रिसर्च होगी तब होगी। फिलहाल इस संसार को टॉपर्स से ज्यादा उन जिम्मेदार और समझदार छात्र-नागरिकों की आवश्यकता है जो भीषण संकट से जूझ रही हमारी महान मानव जाति के लिए नई कल्याणकारी इबारतें लिख सकें। फिलहाल टॉपर्स के बहाने अखबारों को अपने लिए सुर्खियाँ बना लेने का लुत्फ उठा लेने दीजिये।
जिनके बच्चों ने टॉप किया उन्हें मुबारकबाद।
और जिनके बच्चों ने टॉप नहीं किया उन्हें डबल मुबारकबाद!
-प्रकाश दुबे
वन में निवास करने वाली महिला को दुनिया का सबसे विशाल राष्ट्राध्यक्ष महल सौंपना प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक प्रयोग है। इससे भी बड़ा प्रयोग इस बीच अनदेखा रह गया। संविधान और राजनीति के ज्ञानी- विश्लेषक तक अनजान हैं। दूसरे दल से अपने दल में शामिल करने की व्यवस्था करने के लिए पहली बार बाकायदा समिति का गठन किया गया। समिति शब्द अटपटा लगे तो वार्ताकार मंडल कह कर तसल्ली कर लें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने एटला राजिन्दर को भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। कुपित राजिन्दर भाजपा में शामिल होकर उपचुनाव जीत कर फिर विधायक बने। वार्ताकार मंडल के अध्यक्ष की हैसियत से गुणीजनों से संपर्क कर राजिन्द्र दल बदल कराने की गति तेज करेंगे। इसे संविधान-सम्मत विशेष अवसर कहकर चतुर सुजान उत्साहित हो सकते हैं। हैदराबाद में भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के दौरान हुए निर्णय का ऐलान न प्रधानमंत्री ने किया और न अनुशासित अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तेलंगाना राष्ट्र समिति निशाने पर है। हालां कि सेंध लगाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है।
व्यक्ति की गरिमा
लाट साहब यानी वाइसराय महल के आसपास बाबुओं के दफ्तर लगाकर भाई सराय बना दिया जाए। यह तो निर्माता लुटियंस नहीं चाहते थे। इसके बावजूद नार्थ ब्लाक और साउथ ब्लाक बने। राष्ट्रपति भवन के पास पेड़ पौधों की समाधि पर सेंट्रल विस्ता में नया संसद भवन बन रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की मौजूदगी में गुर्राते शेर के साथ प्रधानमंत्री मुस्कराए। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू गैरहाजिर थे। शेर के अगवाड़े और घोड़े के पिछवाड़े में बदलाव से दुखी खुराफाती देवदास बने जा रहे हैं। गीता, कुरान, बाइबल की तरह संविधान में दूसरे महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति पद पर नायडू समारोह में नजर नहीं आए। चेहरा चमकाऊ पोथी (फेसबुक) वाले चहकने लगे कि कुछ दिन के मेहमान उपराष्ट्रपति को जानबूझकर न्यौता नहीं भेजा। सेंट्रल विस्ता के प्रभारी शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जानें न जानें, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पक्का पता था कि राष्ट्रपति पद का चुनाव चल रहा था। संवैधानिक क्रम में दूसरे स्थान पर शेर के साथ वैंकैया जी को खड़ा करना पड़ता। प्रधानमंत्री की कल्पनाशीलता की उपेक्षा होती। एक जंगल में दो शेर सिर्फ फिल्मी तरानों में हो सकते हैं। यह जानकारी उन लोगों के लिए, जिन्हें शिकायत है कि संविधान की अनदेखी हो रही है।
पंथनिरपेक्ष
प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को किसान पुत्र और संविधान के अति उत्कृष्ट विशेषज्ञ कहा। विरोधी उनकी जात उछाल रहे हैं। अनेक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति होंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता सरकार में धनखड़ राज्यमंत्री रहे। कुछ महीनों की सरकार में चंद्रशेखर ने उन्हें शामिल नहीं किया। धनखड़ का विरोध करने से पहले विपक्ष सोचे। अयोध्या में ढांचा गिराए जाने के बाद कल्याण सिंह, सुंदर लाल पटवा और भैरोंसिंह शेखावत बर्खास्त हुई। ढांचा ढहाने को अनैतिकता बताने वाले अलवर के कांग्रेस विधायक जगदीप का कांग्रेस ने फिर भी टिकट काट दिया। भारतीय जनता पार्टी में बरसों तपस्या के बाद राज्यपाल बने। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जनता का राज्यपाल कहकर धनखड़ की उम्मीदवारी घोषित की। मुख्यमंत्री से पहले जनता के बीच पहुंचने में उनकी बराबरी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तक नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरे सिंहासन तक पहुंचते पहुंचते रह गए। नड्डा ने एक और बात कही- वे जनता के उम्मीदवार हैं। जनता से पहले भारतीय तो हैं ही। हिरण शिकारी सलमान के वकील की राज्यसभा में नए तेवर वाली भूमिका देखने लायक होगी।
विचार, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता
दर्जन भर विधायकों को गुड़ की डली दिख जाए तो खजुराहो, बंगलूरु, कामरूप सब जगह की सूरत दिख जाती है। झूमते नाचते थरकने लगते हैं। मगर राष्ट्रपति का चुनाव था। हजार दो हजार वोट यहां से वहां हो जाने पर किसी की सरकार नहीं गिरनी थी। कांग्रेस वाले जाने क्यों तमाशा करते फिरे। मतदान से पहले गोवा के अपने 11 विधायकों को पार्टी वाले चेन्नई उड़ा ले गए। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष दोनों को पता नहीं था कि उनको क्यों छोड़ गए। कांग्रेस वाले शायद 13 का अंक अशुभ मानते होंगे। चुनाव में बहुमत न मिलने से दिगम्बर कामत मुख्यमंत्री नहीं बन सके। कांग्रेस में अपने इस तरह नाम के मुताबिक हालत होने का दिगम्बर को अंदाज नहीं था। भाजपा से कांग्रेस में आकर कामत मुख्यमंत्री बने थे। छुटकू से गोवा में दल बदल कर मंत्री, उपमुख्यमंत्री बनने का अवसर हाथ नहीं आया। गोवा राज्य के कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कामत की भरपूर बदनामी कर डाली है।
(सभी शीर्षक संविधान की प्रस्तावना के अंश हैं।)
(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)
-प्रेमसिंह सियाग
सबीर हका ईरान के करमानशाह में सन 1986 में पैदा हुए। अब तेहरान शहर में किराये के कमरे में रहते है। इमारतों के निर्माण कार्य मे मजदूर है और ईरान के युवा कवि भी है।
अपनी हालत को देखते हुए ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए लिखा है....
मैं ईश्वर का दोस्त नहीं हूँ
इसका सिर्फ एक ही कारण है
जिसकी जड़ें बहुत पुराने अतीत में हैं
जब छह लोगों का हमारा परिवार
एक तंग कमरे में रहता था
तब ईश्वर के पास बहुत बड़ा मकान था
जिसमें वह अकेले ही रहता था
सबीर हका ने दुनियाँ भर की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा करते हुए लिखा..
मैं पूरी दुनिया को अपना कह सकता हूँ
दुनिया के हर देश को अपना कह सकता हूँ
मैं आसमान को भी अपना कह सकता हूँ
इस ब्रह्मांड की हरेक चीज को भी
लेकिन तेहरान के इस बिना खिडक़ी वाले
किराए के कमरे को अपना नहीं कह सकता,
मैं इसे अपना घर नहीं कह सकता
जब श्रमिक स्पर्धा में कविता का प्रथम पुरस्कार मिला तो इंटरव्यू देते समय पत्रकार ने पूछा कि आप थके हुए लग रहे हो तो जवाब में कहा- ‘मैं थका हुआ हूँ, बेहद थका हुआ, मैं पैदा होने से पहले से ही थका हुआ हूँ। मेरी माँ मुझे अपने गर्भ में पालते हुए मजदूरी करती थी, मैं तब से ही एक मजदूर हूँ। मैं अपनी माँ की थकान महसूस कर सकता हूँ। उसकी थकान अब भी मेरे जिस्म में है।’
सबीर हका ने आगे कहा कि कविताओं से पेट नहीं भरता।पेट भरने के लिए हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपने कमरे के कोने में यह पुरस्कार रख दूंगा और ईंट-रोड़ा उठाने निकल जाऊंगा। पड़ौसी मजदूरों के बच्चे टूटी खिडक़ी से इस पुरस्कार को देखेंगे।
एक गरीब के लिए,एक मजदूर के लिए साहित्य लेखन बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में ही जीवन संघर्ष चलता रहता है। अगर इसके बीच भी लिखना/बोलना शुरू कर दे तो तमाम राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक ताकतें दायरा दिखाने लगती है कि तुझ गरीब की इतनी हिम्मत!
सबीर हका ने मजदूरों की मौत को सबसे सस्ती बताते हुए लिखा है.....
क्या आपने कभी शहतूत देखा है!
जहां गिरता है, उतनी जमीन पर
उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है.
गिरने से ज़्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं
मैंने कितने मजदूरों को देखा है
इमारतों से गिरते हुए,
गिरकर शहतूत बन जाते हुए!
सबीर हका लिखते है कि पूरी जिंदगी मैंने महसूस किया है कि मौत भी जिंदगी का हिस्सा है फिर भी मरने से डर लगता है कि कहीं दूसरी दुनियाँ में भी मजदूर न बन जाऊं! गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना अपने आपमें जीवन की मुक्ति है अन्यथा हका जैसा युवा जो ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर देता है वो भी सदा मजदूर बने रहने से खौफजदा रहता है।
एक गरीब का, एक मजदूर का दर्द खुद मजदूरी करने वाले सबीर हका जैसे लोग ही व्यक्त कर सकते है। हका लिखते है कि मैं चाहकर भी अपने कैरियर का चुनाव नहीं कर सकता। मैं बैंककर्मी नहीं बन सकता, मैं इन्स्पेक्टर नहीं बन सकता। मेरा पिता मजदूर थे। मेरी माँ मजदूर थी। किराये का मकान था। पिता के गुजरने के बाद मजदूर बनकर घर संभालना मजदूर बनने का जरूरी आधार बन गया।
हर इंसान के अपने सपने होते है व सपनों को पूरा करने की चाहतें दिलों में समेटे रोज जिंदगी के संघर्ष में गतिमान रहता है। सबीर ने लिखा कि जब मर जाऊंगा तो सारी किताबें कफन में बांधकर कब्र में ले जाऊंगा। सिगरेट जलाऊंगा और कस खींचते हुए रोऊंगा उन सपनों के लिए जो जिंदगी में प्राप्त न हो सके। एक डर फिर भी रहेगा कि किसी सुबह कोई कंधा झंझोडक़र न कह दें ‘अबे सबीर उठ! काम पर चलते हंै!’
-डॉ. राजू पाण्डेय
सेंट्रल विस्टा की ऊपरी मंजिल पर स्थापित अशोक स्तंभ की प्रतिकृति के अनावरण के बाद से प्रारंभ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के अनेक जाने माने इतिहासकार अशोक स्तम्भ के मूल स्वरूप के साथ हुई छेड़छाड़ से आहत हैं। हरबंस मुखिया, राजमोहन गांधी, कुणाल चक्रवर्ती तथा नयनजोत लाहिड़ी आदि अनेक इतिहासकारों के मतानुसार अशोक स्तम्भ की वर्तमान प्रतिकृति में शेरों का स्वरूप मूल अशोक स्तंभ से अलग है और ये मूल अशोक स्तंभ के शेरों की भांति शांति और स्थिरता नहीं दर्शाते।
इन सभी इतिहासकारों का मानना है कि यद्यपि शेरों की प्रकृति आक्रामक होती है किंतु अशोक स्तम्भ के शेरों की मुख मुद्रा ऐसी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये हमें संरक्षण दे रहे हैं। इनमें गरिमा, आंतरिक शक्ति एवं आत्मविश्वास परिलक्षित होते हैं। अशोक स्तम्भ के शेर शांति प्रिय, शान्तिकामी और शांति के रक्षक हैं। इनके चेहरे पर दयालुता का भाव है। जबकि नए संसद भवन की छत पर स्थापित प्रतिकृति में शेरों की भाव भंगिमा में गुस्सा है, अशांति है, आक्रामकता है।
प्रतिकृति में दिखने वाले शेरों के दांत अधिक तीखे, बड़े और स्पष्ट हैं। यह हिंसा और आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशोक स्तंभ इस मायने में अनूठा है कि इसमें शेरों की भावभंगिमा को संयमित और शांत दिखाया गया है जबकि सामान्यतया कलाकारों द्वारा शेरों की पाशविक प्रवृत्ति को आधार बनाकर उन्हें हिंसक, आक्रामक और भयोत्पादक रूप में चित्रित किया जाता है। नए संसद भवन पर स्थापित प्रतिकृति अशोक स्तंभ की इस विलक्षण विशेषता को ही विनष्ट कर देती है। जानेमाने मूर्तिकार अनिल सूतार के अनुसार यह रेप्लिका मूल अशोक स्तंभ से एकदम अलग है।
सेंट्रल विस्टा पर स्थापित प्रतिकृति के शेरों के पिचके हुए टेढ़े जबड़े, अधिक खुले हुए मुख, निकले हुए दांत, भयानक नेत्र, हिंसक चेहरा एवं पैरों और नाखूनों की बदली हुई बनावट तथा शेरों के शरीर एवं अयाल में केशों का विन्यास इन्हें एक रौद्र रूप प्रदान करते हैं। अशोक स्तंभ के शेरों की उपस्थिति आश्वासनदायी है जबकि सेंट्रल विस्टा के शेर भयोत्पादक हैं।
अनेक इतिहासकार सेंट्रल विस्टा की ऊपरी मंजिल पर स्थापित प्रतिकृति के तीखे और हिंसक तथा डरावने लगने वाले दांतों को उग्र राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रहे हैं। इनका प्रश्न यह है कि क्या अब भारत एक शांतिप्रिय देश से एक आक्रामक और युद्धप्रिय राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है? इन इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अशोक स्तम्भ के शेरों की प्रकृति में लाए गए इस परिवर्तन को कलाकार की स्वतंत्रता कहकर महत्वहीन बनाने की कोशिश गलत है क्योंकि यहां तो कलाकार ने शांति का संदेश देने वाले अशोक स्तंभ को हिंसा की हिमायत करने वाले स्मारक में बदल दिया है।
किंतु कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि मूल अशोक स्तंभ और सेंट्रल विस्टा पर स्थापित प्रतिकृति के निर्माण काल में 2500 वर्ष का अंतर है, तबसे लेकर अब तक शिल्प कला के स्वरूप एवं कलाकारों की सोच में बहुत बदलाव आ गया है इसलिए मूल एवं प्रतिकृति का एक समान होना न तो संभव है न ही अपेक्षित है। सेंट्रल विस्टा पर स्थापित प्रतिकृति के शेर वास्तविक शेरों के अधिक निकट और जीवंत हैं।
सरकार की ओर से इस मामले पर सफाई केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट संदेशों के रूप में सामने आई है। श्री पुरी के अनुसार नई संसद हेतु निर्मित अशोक स्तंभ सारनाथ के स्तंभ की हूबहू प्रतिकृति है। दोनों की डिजाइन एवं बनावट समान है। केवल लोगों के देखने के नजरिए में अंतर है। नए संसद भवन पर स्थापित प्रतिकृति(6.5 मीटर) सारनाथ के संग्रहालय में स्थित अशोक स्तम्भ(1.6 मीटर) से काफी बड़ी है। यदि मूल अशोक स्तंभ के आकार वाली प्रतिकृति सेंट्रल विस्टा की छत पर रखी जाती तो यह दिखाई ही नहीं पड़ती। विशेषज्ञ यह क्यों भूल रहे हैं कि सारनाथ का मूल अशोक स्तंभ जमीन के स्तर पर है और नया प्रतीक जमीन से 33 मीटर की ऊंचाई पर है। जब हम मूल और प्रतिकृति की तुलना करते हैं तो कोण,लंबाई और स्केल का ध्यान क्यों नहीं रखते? यदि सेंट्रल विस्टा पर रखे रेप्लिका को छोटा कर दिया जाए तो यह हूबहू मूल अशोक स्तंभ की भांति दिखाई देगा। यदि हम मूल अशोक स्तंभ को नीचे से देखें तो इसके शेर रेप्लिका की भांति ही क्रोधित या शांत लगेंगे।
लगभग यही तर्क इस रेप्लिका के निर्माता द्वय लक्ष्मण व्यास और सुनील देवड़े ने दिए हैं और हरदीप पुरी की ही भांति उन्होंने अंग्रेजी की उस उक्ति का आश्रय लिया है जिसके अनुसार सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में होता है।
सरकार और प्रतिकृति के निर्माताओं के तर्क तब अर्थहीन लगने लगते हैं जब हम बनारस के उन कलाकारों की राय से अवगत होते हैं जो वर्षों से काष्ठ, पत्थर और कागज-कैनवास पर अशोक स्तंभ की प्रतिकृतियां बनाकर पर्यटकों को बेचते रहे हैं। न ये इतिहास विशेषज्ञ हैं न ही इन्होंने मूर्तिकला की विधिवत शिक्षा पाई है किंतु अशोक स्तंभ इनके जीवन का अविभाज्य हिस्सा है क्योंकि इसकी सैकड़ों प्रतिकृतियां गढ़ते गढ़ते इन कलाकारों ने अशोक स्तंभ को आत्मसात कर लिया है। यह कलाकार भी प्रथम दृष्टया ही सेंट्रल विस्टा के अशोक स्तम्भ को मूल से भिन्न बताते हैं। इन कलाकारों के संस्कार सैकड़ों बार अशोक स्तम्भ की प्रतिकृतियां गढ़ते समय एक बार भी इन्हें इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ का दुस्साहस नहीं करने देते।
इतिहासकारों एवं बौद्ध धर्म के जानकारों के अनुसार बुद्ध के अनेक नामों में शाक्य सिंह एवं नरसिंह जैसे नाम भी हैं। सारनाथ भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। इसी स्थान से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रारम्भ किया था और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार इस विश्व को दिया था। तदुपरांत शांति, सद्भाव और बंधुत्व के संदेश के वैश्विक प्रसार हेतु उन्होंने अपने शिष्यों को चतुर्दिक भ्रमण हेतु प्रेरित किया था। बुद्ध द्वारा परम सत्य का उद्घोष किसी सिंह नाद से कम नहीं। अशोक स्तंभ के चारों सिंह सम्राट अशोक की धम्म विजय की घोषणा का नाद करते प्रतीत होते हैं। अशोक स्तम्भ की यह धार्मिक-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अशोक स्तंभ के शेरों की सौम्य और शांत मुखमुद्रा का कारण समझने के लिए पर्याप्त है।
इस प्रकार यदि मूल अशोक स्तम्भ के संदेश को सेंट्रल विस्टा पर लगाई गई इसकी प्रतिकृति के माध्यम से उलट देने के आरोप सही हैं तो यह राष्ट्रीय प्रतीक के स्वरूप में परिवर्तन का विषय ही नहीं है अपितु यह बौद्ध धर्म के मर्म और सम्राट अशोक की छवि दोनों को एक भिन्न और संभवतः गलत परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की चेष्टा भी है।
बुद्ध धर्म और सम्राट अशोक के प्रति हिंदुत्व की विचारधारा के प्रतिपादकों और उनके अनुयायियों की नापसंदगी जगजाहिर है। श्री गोलवलकर का कथन है, "बुद्ध के पश्चात यहां उनके अनुयायी पतित हो गए। उन्होंने इस देश की युगों पुरानी प्राचीन परंपराओं का उन्मूलन प्रारंभ कर दिया। हमारे समाज में पोषित महान सांस्कृतिक सद्गुणों का विनाश किया जाने लगा। अतीत के साथ के संबंध-सूत्रों को भंग कर दिया गया। धर्म की दुर्गति हो गई। संपूर्ण समाज-व्यवस्था छिन्न-विच्छिन्न की जाने लगी। राष्ट्र एवं उसके दाय के प्रति श्रद्धा इतने निम्न तल तक पहुंच गई कि धर्मांध बौद्धों ने बुद्ध धर्म का चेहरा लगाए हुए विदेशी आक्रांताओं को आमंत्रित किया तथा उनकी सहायता की। बौद्ध पंथ अपने मातृ समाज तथा मातृ धर्म के प्रति द्रोही बन गया।" यहां श्री गोलवलकर अप्रत्यक्ष रूप से सम्राट अशोक की ओर ही संकेत करते लगते हैं।
श्री गोलवलकर के अभिमत पर आधारित एक लेख लगभग 6 वर्ष पहले राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद (जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आनुषांगिक संगठन है) द्वारा प्रकाशित 'बप्पा रावल' के मई 2016 के अंक में 'भारत : कल, आज और कल' लेखमाला के अंतर्गत छपा।
इसमें 'बप्पा रावल' की संपादिका डॉ. राधिका लढ़ा ने लिखा
- "मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के कारण ही भारतीय राष्ट्र पर बड़े संकटों के पहाड़ टूटे और यूनानी हमलावर भारत को पदाक्रांत करने आ धमके। …..यह भारत का दुर्भाग्य रहा कि जो अशोक भारतीय राष्ट्र की अवनति का कारण बना, उसकी ही हमने 'अशोक महान' कह कर पूजा की। अच्छा होता कि राजा अशोक भी भगवान बुद्ध की तरह साम्राज्य त्यागकर, भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म के प्रचार में लग जाते।……इसके विपरीत उन्होंने सारे साम्राज्य को ही बौद्ध धर्म प्रचारक विशाल मठ के रूप में बदल दिया। इन वजहों से ही यूरोप से फिर एक बार ग्रीक हमलावर भारत को कुचलने आ धमके।"
डॉ. राधिका लढ़ा के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, फिर इसे ही राज धर्म बना दिया। विदेशों से जो भी आता, यदि वह बौद्ध होता तो अशोक तुरंत ही उसे अपना मान लेते थे, जो गलत था। …..उन्होंने (अशोक ने) इतनी शांति फैलाई कि सीमा पर लगे सैनिक ही हटा दिए। इससे हमले बढ़े और राष्ट्र की उसी वक्त अवनति शुरू हो गई।"
संघ के वरिष्ठ सदस्य एवं 'पाथेय कण' पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल चतुर्वेदी ने अधिक संयत ढंग से इसी तर्क को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा-"सम्राट अशोक में अच्छाई थी तो दोष भी थे। उनके आने से भारत में शक्ति पूजा समाप्त हो गई। इससे राष्ट्र कमजोर बनता गया और विदेशियों के आक्रमण बढ़ते गए। अकबर और अशोक को महान बताने वाले जो भी इतिहासकार हैं, वे सभी विदेशी हैं, जो भारत को जानते ही नहीं।"
जब डॉ. राधिका लढ़ा के लेख पर विवाद बढ़ा तो संघ ने इसे लेखिका की निजी राय बताकर खुद को इससे अलग कर लिया।
सम्राट अशोक की छवि धूमिल करने का नवीनतम प्रयास भाजपा के सांस्कृतिक मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक एवं आरएसएस की संस्कार भारती से संबद्ध श्री दया प्रकाश सिन्हा द्वारा किया गया। श्री सिन्हा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स के उपाध्यक्ष भी हैं। श्री सिन्हा 2 अप्रैल 2015 को तत्कालीन संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री डॉ. महेश चन्द्र शर्मा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल की उपस्थिति में लोकार्पित अपने विवादास्पद नाटक "सम्राट अशोक" के लिए पहले ही चर्चा में रह चुके हैं। उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र में 8 जनवरी 2022 को प्रकाशित अपने साक्षात्कार में सम्राट अशोक के विषय में अनेक नकारात्मक और विवादित टिप्पणियां कीं।
श्री सिन्हा ने कहा-" श्रीलंका के तीन बौद्ध ग्रंथ दीपवंस, महावंस, अशोकावदान और तिब्बती लेखक तारानाथ के ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक बहुत ही बदसूरत था। उसके चेहरे पर दाग था और वह आरंभिक जीवन में बहुत ही कामुक था। बौद्ध ग्रंथ भी कहते हैं कि अशोक कामाशोक और चंडाशोक था। चंडाशोक यानी कि वह बहुत ही क्रूर था। उसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई थी।
श्री सिन्हा ने आगे कहा-" (मुझे) अशोक और मुगल बादशाह औरंगजेब के चरित्र में बहुत समानता दिखाई दी। दोनों ने अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत पाप किए थे और अपने पाप को छिपाने के लिए अतिधार्मिकता का सहारा लिया ताकि जनता का ध्यान धर्म के प्रति प्रेरित हो जाए और उनके पाप पर किसी का ध्यान न जाए। दोनों ने अपने भाई की हत्या की थी और अपने पिता को कारावास में डाल दिया था। अशोक का चरित्र बहुत ही रोचक है। उसने अपनी पत्नी को जला दिया था, क्योंकि उसने एक बौद्ध भिक्षु का अपमान किया था।"
श्री सिन्हा की इन टिप्पणियों के बाद सुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रो राजेन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य विद्वानों ने जब जनता के सम्मुख यह सच उजागर किया कि दीपवंस, महावंस और अशोकावदान, दिव्यावदान आदि परवर्ती ग्रंथों में अशोक से संबंधित अनेक मनगढ़ंत और कपोल कल्पित कथाएं हैं जिनका कोई पुरातत्विक आधार नहीं है और इनकी बुनियाद पर अशोक को कुरूप, हीनभावना से ग्रस्त, अपने परिवार जनों और अन्य स्त्रियों का हत्यारा कहना सर्वथा अनुचित है तो श्री सिन्हा इन प्रतिप्रश्नों से बचते नजर आए।
बहरहाल इस विवाद के परिणामस्वरूप अशोक द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार के क्षेत्र में उठाए गए कदमों, उनके द्वारा आम जन के कल्याण लिए चलाए गए कार्यक्रमों, अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु रहने और उनका सम्मान करने के उनके सिद्धांत,मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उनके द्वारा की गई पहलकदमी तथा प्राणिमात्र के संरक्षण की उनकी उदार दृष्टि की जमकर चर्चा हुई और जो नई पीढ़ी अशोक के विषय में अनभिज्ञ थी उसने भी उनकी महानता को जाना।
सेंट्रल विस्टा के शिखर पर विराजमान हिंसक और भयोत्पादक शेरों के साथ मुदित भाव से अकेले खड़े माननीय प्रधानमंत्रीजी की तस्वीर आश्वासन कम देती है, चिंता और भय अधिक उत्पन्न करती है। शायद इस तस्वीर में प्रधानमंत्री जी के साथ विपक्ष का होना उनकी अद्वितीयता को कम कर देता किंतु कम से कम उनके सहयोगियों को तो इस बात का अवसर मिलना था कि वे अपने बौनेपन और असहायता का अनुभव कर सकें। इस दौरान घटित घटनाक्रम बहुत प्रतीकात्मक रहा, लोकसभा अध्यक्ष (जिन्हें वास्तव में अनावरण का यह कार्य सम्पन्न करना था) उपेक्षित से बस उपस्थित थे, उसी वैदिक रीति से पूजा पाठ भी हुआ जिससे विद्रोह कर बुद्ध धर्म अस्तित्व में आया था। हमारे देश से हिन्दू धर्म के अतिरिक्त अन्य अनेक धर्मों के अनुयायियों का अटूट रिश्ता है, किंतु संसद शायद अब उनसे दूर होती जा रही है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख पर व्याप्त संतोष और आनंद की व्याख्या करना कठिन है। क्या यह प्रसन्नता इस बात की है कि हमारी उदार राष्ट्रीय पहचान से जुड़े एक और चिह्न को उन्होंने असमावेशी हिंदुत्व के रंग में रंगने में सफलता अर्जित कर ली है?
क्या उनका आनंद इस बात को लेकर है कि नए कीर्तिमान स्थापित करती महंगाई और बेरोजगारी के बीच जब देश में आर्थिक संकट की आहट स्पष्ट सुनाई दे रही है, उन्होंने अपनी अति महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को हठपूर्वक पूर्णता तक पहुंचा ही लिया है?
अभी ही जब आलोचना, समीक्षा और बहस में सहज प्रयुक्त होने वाले अति प्रचलित शब्दों को असंसदीय घोषित करने वाली सूची चर्चा में है तब शायद उनकी खुशी इस बात को लेकर होगी कि सेंट्रल विस्टा के भव्य गलियारों में असहमत स्वरों को गूँजने न देने का एक और रास्ता तलाश कर लिया गया है।
यह भी विचारणीय प्रश्न है कि इन हिंसक शेरों का गुस्सा आखिर किस पर टूटेगा? कर्ज में डूबा, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाले संगठनों के आदेश का अनुपालन करने को लालायित भारत विश्व को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले ताकतवर देशों से तो लड़ नहीं सकता। ढीठ चीन के आक्रामक व्यवहार और उकसाने वाले कदमों पर हम कोई ठोस रणनीति बनाने के बजाए देश की जनता को भ्रम में रखने की विधियां तलाश रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेरों की यह गुर्राहट अपनी अकर्मण्यता, अक्षमता और शक्तिहीनता को छिपाने की रणनीति है। शायद अपने पौरुष के छद्म को कायम रखने के लिए नए भारत के ये शेर अपने ही देश के उन निरीह लोगों पर आक्रमण करेंगे जिन्हें देश की दुरावस्था के लिए उत्तरदायी काल्पनिक शत्रुओं के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
(रायगढ़, छत्तीसगढ़)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
भारत में आदिवासियों को कितना महत्व दिया जाता है, इसे आप इसी तथ्य से समझ सकते हैं कि इस समय भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी, वह भी महिला द्रौपदी मुर्मू हैं और तीन राज्यपाल आज भी आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसूय्या उइके ने जो मूलत: मध्यप्रदेश की हैं, आदिवासियों के लिए कई नई पहल की हैं। भारत में कई आदिवासी मुख्यमंत्री और मंत्री हैं और पहले भी रहे हैं। संसद में भी भारत के लगभग 50 सदस्य आदिवासी ही होते हैं। कई विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति और प्रोफेसर भी आदिवासी हैं।
भारत के कई डाक्टर और वकील भी आपको आदिवासी मिल जाएंगे। सरकारी नौकरियों और संसद में उन्हें आरक्षण की भी सुविधा है लेकिन आप जरा जानें कि अमेरिका और कनाडा के आदिवासियों का क्या हाल हैं। मैं अपनी युवा अवस्था से इन देशों में पढ़ता और पढ़ाता रहा हूं। मुझे इनके कई आदिवासी इलाकों में जाने का मौका मिला है। यह संयोग है कि मेरे साथी छात्रों में कभी कोई अमेरिकी या कनीडेयन आदिवासी नहीं रहा है। वहां के आदिवासी आज भी जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं।
उनसे माफी मांगने के लिए पोप फ्रांसिस, जो कि 86 साल के हैं, आजकल कनाडा गए हैं। व्हीलचेयर में बैठे पोप वहां क्यों गए हैं? ईसाई पादरियों और गोरे प्रवासियों द्वारा वहां के आदिवासियों पर किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगने के लिए गए हैं। पिछले 80-90 साल में आदिवासियों के लगभग डेढ़ लाख बच्चे लापता हो चुके हैं। इन बच्चों को उनके घर से जबरन उठाकर ईसाई स्कूल में भर्ती कर दिया जाता था।
उन पर हुए अत्याचारों की कहानी रौंगटे खड़े कर देती है। हजारों बच्चे भूख से तडफ़-तडफ़ कर मर गए, हजारों के साथ बलात्कार हुए और हजारों की हत्या कर दी गई। उनके ईसाई स्कूल उनके गांवों से इतने दूर बनाए जाते थे कि उनके माँ-बाप उन तक नहीं पहुंच सकें। कनाडा सरकार ने जांच आयोग बिठाकर जो तथ्य उजागर किए हैं, उनसे पोप मर्माहत हुए और कनाडा जाकर उन आदिवासियों से माफी मांगने का संकल्प किया।
कनाडा सरकार ने उनके पुनरोद्धार के लिए 40 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। अमेरिका और केनाडा के आदिवासियों को ‘रेड इंडियन’ और ‘इंडियन’ कहा जाता है लेकिन जऱा देखिए कि उन देशों और भारत के आदिवासियों में कितना फर्क है। (नया इंडिया की अनुमति से)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
आजादी के 75 वें साल में मैकाले की गुलामगीरी वाली शिक्षा पद्धति बदलने की शुरुआत अब मध्यप्रदेश से हो रही है। इसका श्रेय मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को है। मैंने पिछले साठ साल में म.प्र. के हर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मेडिकल और कानून की पढ़ाई वे हिंदी में शुरु करवाएं लेकिन मप्र की वर्तमान सरकार भारत की ऐसी पहली सरकार है, भारत की शिक्षा के इतिहास में जिसका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।
भारत के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री म.प्र. से प्रेरणा ग्रहण करें और समस्त विषयों की उच्चतम पढ़ाई का माध्यम भारतीय भाषाओं को करवा दें तो भारत को अगले एक दशक में ही विश्व की महाशक्ति बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। विश्व की जितनी भी महाशक्तियाँ हैं, उनमें उच्चतम अध्ययन और अध्यापन स्वभाषा में होता है। डाक्टरी की पढ़ाई मप्र में हिंदी माध्यम से होने के कई फायदे हैं। पहला तो यही कि फेल होनेवालों की संख्या एकदम घटेगी। दूसरा, छात्रों की दक्षता बढ़ेगी।
70-80 प्रतिशत छात्र हिंदी माध्यम से पढक़र ही मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होते हैं। इन्हें चिकित्सा-पद्धति को समझने में आसानी होगी। तीसरा, मरीज़ों की ठगाई कम होगी। चिकित्सा जादू-टोना नहीं बनी रहेगी। चौथा, मरीज़ों और डाक्टरों की बीच संवाद आसान हो जाएगा। पांचवा, सबसे ज्यादा फायदा उन गरीबों, पिछड़ों, अनुसूचितों के बच्चों को होगा, जो अंग्रेजी के चलते डॉक्टर नहीं बन पातें। मप्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास नारंग ने मेडिकल शिक्षा की किताबें हिंदी में तैयार करवाने के लिए जो कमेटी बनाई है, उससे मेरा सतत संपर्क बना रहता है।
कुछ पुस्तकें मूल रूप से हिंदी में तैयार हो गई हैं और कुछ के अनुवाद भी हो गए हैं। सितंबर के आखिर में शुरु होने वाले नए सत्र से छात्रों को हिंदी माध्यम की छूट मिल जाएगी। हिंदी की पुस्तकों में अंग्रेजी मूल तकनीकी शब्दों से परहेज नहीं किया जाएगा। जो छात्र अंग्रेजी माध्यम से पढऩा चाहेंगे, उन्हें छूट रहेगी। मप्र के चार हजार मेडिकल छात्रों में से अब लगभग सभी स्वभाषा के माध्यम से पढऩा चाहेंगे। यदि ऐसा होगा तो हिंदी में कई नए-नए मौलिक ग्रंथ भी हर साल प्रकाशित होते रहेंगे।
यदि इस मेडिकल की पढ़ाई को और भी अधिक उपयोगी बनाना हो तो मेरा सुझाव यह भी है कि एक ऐसी नई चिकित्सा-उपाधि तैयार की जाए, जिसमें एलोपेथी, आयुर्वेद, हकीमी, होमियोपेथी और प्राकृतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम मिले-जुले हों ताकि मरीजों का यदि एक दवा से इलाज न हो तो दूसरी दवा से होने लगे। यदि हमारी चिकित्सा में ऐसा कोई क्रांतिकारी परिवर्तन मध्यप्रदेश की सरकार करवा सके तो अन्य प्रदेशों की सरकारें और केंद्र सरकार भी पीछे नहीं रहेगी।
यह विश्व को भारत की अनुपम देन होगी। यह चिकित्सा पद्धति इतनी सुलभ और सस्ती होगी कि भारत और पड़ौसी देशों के गरीब से गरीब लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। एक बार फिर दुनिया भर के छात्र डाक्टरी की पढ़ाई के लिए भारत आने लगेंगे, जैसे कि वे सदियों पहले विदेशों से आया करते थे। (नया इंडिया की अनुमति से)
-गिरीश मालवीय
स्मृति ईरानी जी के पास फिलहाल महिला एवं बाल विकास का पोर्टफोलियो है तो उन्होंने अपनी 18 साल की पुत्री ज़ोइश ईरानी के रेस्टोरेंट के लिए एक मरे हुए व्यक्ति के नाम से बार लाइसेंस बनवाया तो क्या गलत किया? बाल विकास और महिला यानि कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल परफेक्ट है।
अब यहां सारी गलती गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण एम गाड की है उन्होंने ही अवैध रूप से प्राप्त शराब लाइसेंस को लेकर सिली सोल्स कैफे और बार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
लेकिन बेचारे नारायण एम गाड भी क्या करते ?
उन्हे भी गोवा के एक्साइज कमिश्नर के पद पर 2 महीने पहले ही जॉइनिंग मिली, वो समझ ही नहीं पाए कि मामला कितना बडा हो सकता है और वे फंस गए उन्होंने एडव रॉड्रिक्स जो गोवा में एक वकील है उनकी एक शिकायत के आधार पर यह कार्यवाही की!
सारी गलती रॉड्रिक्स की ही है उन्होंने ही यह केस खोला उन्होंने ही सबसे पहले आरटीआई के जरिए इसके दस्तावेज हासिल किए तो पता चला कि आबकारी विभाग ने सिली सोल्स कैफे और बार का लाइसेंस एंथनी द गामा के नाम पर जारी किया, और उसके साथ जमा किए गए आधार कार्ड के अनुसार वह मुंबई का निवासी था।
अब वकील साब एंथनी द गामा को ढूंढने मुम्बई पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि जो एंथनी द गामा कुछ महीने पहले गोवा में बार लाइसेंस मांगने आया था वो तो 13 महीने पहले ही मर चुका है वकील साहब मुंबई नगर निगम का एंथनी द गामा का मृत्यु प्रमाण पत्र साथ ले आए जो मुंबई नगर निगम ने 17 मई, 2021 को जारी किया था।
केस तो अब बनता ही था क्योंकि साफ-साफ धोखाधड़ी की जा रही थी तो एक्साइज कमिश्नर को मजबूरन सिली सोल्स कैफे और बार के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा कि आपने एक मृत व्यक्ति के नाम पर कैसे लाइसेंस मांग लिया? अब आप 29 जुलाई को हमारे सामने हाजिर हो और इसका जवाब दे।
जब स्थानीय स्तर पर यह खबर सामने आई तो कांग्रेस पार्टी इसे ले उड़ी और उसने सुबह प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाए कि संस्कारी स्मृति ईरानी जी की पुत्री जोइश ईरानी गोवा में बार तो चला ही रही है बल्कि मृत व्यक्ति के नाम पर बार लाइसेंस भी बनवा रही है। शाम को अपने घर पर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए सफेद कपड़े पहने स्मृति ईरानी बिफर पड़ी कि मेरी बेटी का इससे तो कोई संबंध ही नहीं है यह रेस्टोरेंट और बार उसका नहीं है मेरी 18 साल की बेटी जोइश ईरानी ब्ला ब्ला ब्ला और मेरी 18 साल की बेटी ब्ला ब्ला ब्ला और मेरी 18 साल की बेटी ब्ला ब्ला ब्ला।
प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद पत्रकारों में तो यह हौसला ही नहीं था कि वे स्मृति ईरानी से पूछ लेते कि यदि सिली सोल्स कैफे और बार का मालिकाना हक आपके परिवार का नहीं है तो किसका है ?
इस प्रेस कांफ्रेंस के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक फूड ब्लॉगर से ज़ोइश ईरानी को यह कहते हुए देखा गया कि वह रेस्तरां सिली सोल्स कैफे और बार की मालिक है। बाद में उस फूड ब्लॉगर को उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में बना पोर्क भी टेस्ट करवाया।
यह वीडियो आने के बाद स्मृति ईरानी जी की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई वैसे अब 29 जुलाई को स्थिति साफ हो जाएगी कि यह सिली सोल्स कैफे और बार किसका है ?
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत अंदर तक खुदाई करने से पता चला है कि स्मृति ईरानी के पति जुबिन फरदून ईरानी के नाम गोवा में रजिस्टर्ड एक कम्पनी है जिसका नाम है VILLANIX REALTORS AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED, देखते हैं 29 जुलाई को कौन सा खेल खेला जाता हैं।
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
इसमें जरा भी शक नहीं है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई नई और अच्छी पहल की हैं। उसकी नई शिक्षा पद्धति को देखकर कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियां भी काफी प्रभावित हुई हैं। अब दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह 50 केंद्रों में एक लाख ऐसे बच्चे तैयार करेगी, जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकें। अंग्रेजी की अनिवार्य पढ़ाई तो भारत के सभी विद्यालयों में होती है लेकिन अंग्रेजी में संभाषण करने की निपुणता कम ही छात्रों में होती है।
इसी वजह से वे न तो अच्छी नौकरियां ले पाते हैं और वे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हीनता-ग्रंथि से ग्रस्त रहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब और पिछड़े परिवारों के छात्रों को होता है। उन्हें घटिया पदों और कम वेतन वाली नौकरियों से ही संतोष करना पड़ता है। ऐसे छात्रों को जीवन में आगे बढऩे का मौका मिले, इसीलिए दिल्ली सरकार अब 12 वीं पास छात्रों को अंग्रेजी बोलने का अभ्यास मुफ्त में करवाएगी। शुरु में वह उनसे 950 रुपए जमा करवाएगी ताकि वे पाठ्यक्रम के प्रति गंभीर रहें।
यह राशि उन्हें अंत में लौटा दी जाएगी। यह पाठ्यक्रम सिर्फ 3-4 माह का ही होगा। 18 से 35 साल के युवकों के लिए यह अंग्रेजी बढिय़ा बोलो अभियान खुला रहेगा। मोटे तौर पर दिल्ली सरकार की इस योजना के पीछे उसकी मन्शा पूरी तरह सराहनीय है लेकिन दिल्ली की ही नहीं, हमारे सभी राज्यों और केंद्र की सरकार ने क्या कभी सोचा कि हमारी शिक्षा और नौकरियों में अंग्रेजी की अनिवार्यता ने भारत का कितना बड़ा नुकसान किया है? यदि सरकारी नौकरियों से अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा दी जाए तो कौन माता-पिता अपने हिरण-जैसे बच्चों पर घांस लादने की गलती करेंगे?
चीनी भाषा के अलावा किसी भी विदेशी भाषा को सीखने के लिए साल-दो साल काफी होते हैं लेकिन भारत में बच्चों पर यह घांस दस-बारह साल तक लाद दी जाती है। अपने छात्र-काल में मैंने अंग्रेजी के अलावा जर्मन, रूसी और फारसी भाषाएं साल-साल भर में आसानी से सीख ली थीं। अंग्रेजी से कुश्ती लडऩे में छात्रों का सबसे ज्यादा समय नष्ट हो जाता है। अन्य विषयों की उपेक्षा होती है। मौलिकता नष्ट होती है। हीनता ग्रंथि पनपने लगती है। अहंकार और ढोंग पैदा हो जाता है। हमारी शिक्षा-व्यवस्था चौपट हो जाती है।
आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं लेकिन अभी भी हम भाषाई और बौद्धिक गुलामी में जी रहे हैं। महात्मा गांधी और लोहिया- जैसा एक भी नेता आज तक देश में इतना साहसी नहीं हुआ कि वह मैकाले की इस गुलामगीरी को चुनौती दे सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री मनीष सिसोदिया से मैं आशा करता हूं कि वे अन्य मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की तरह पिटेपिटाए रास्ते पर तेज रफ्तार से चलने की बजाय ऐसा जबर्दस्त अभियान चलाएं कि भारत में नौकरियों और शिक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म हो जाए। जिन्हें उच्च शोध, विदेश व्यापार और कूटनीति के लिए विदेशी भाषाएं सीखनी हों, वे जरुर सीखें। उन्हें पूर्ण सुविधाएं दी जाएं। (नया इंडिया की अनुमति से)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
इस समय केंद्र सरकार कई सेठों और नेताओं के यहाँ छापे डलवा रही है। इसमें सामान्यतया कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब से लगभग तीन सौ साल पहले फ्रांसीसी विद्वान सेंट साइमाँ ने जो कहा था, वह आज भी बहुत हद तक सच है। उन्होंने कहा था कि समस्त संपत्ति चोरी का माल होती है।’ फिलहाल उनके इस दार्शनिक कथन की गहराई में उतरे बिना हम यह मानकर चल सकते हैं कि कुछ हेरा-फेरी किए बिना बड़ा माल-ताल कमाना मुश्किल ही है।
उद्योग और व्यापार में तो पैसा बनाने के लिए कई वैध और अवैध तरीके अपनाने ही पड़ते हैं लेकिन राजनीति में भ्रष्टाचार किए बिना पैसा बनाना असंभव है और लोकतंत्र की चुनावी राजनीति तो मोटे पैसे के बिना साँस भी नहीं ले सकती। पिछले 77-75 साल में मैं ऐसे कई नेताओं को जानता रहा हूँ, जिसके पास खाने और पहनने की भी ठीक-ठाक व्यवस्था नहीं थी लेकिन आज वे करोड़ों के मालिक हैं। पैसे के खेल ने दुनिया के सारे लोकतंत्रों को खोखला कर दिया है।
भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी साफ-सफाई के लिए मोदी सरकार जो कार्रवाइयां कर रही है, वह सराहनीय है लेकिन सवाल यह है कि ये सब कार्रवाइयाँ विरोधी दलों के नेताओं और सिर्फ उन सेठों के खिलाफ क्यों हो रही हैं, जो कुछ विरोधी दलों के साथ नत्थी रहे हैं? यदि सोनिया गांधी के खिलाफ जाँच हो रही है तो क्या अन्य सभी दलों के नेता दूध के धुले हुए हैं? सभी दलों के नेताओं के यहाँ छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं?
यदि नरेंद्र मोदी कुछ भाजपा के नेताओं के यहाँ भी छापे डलवाने की हिम्मत कर लें तो वे भारत के विलक्षण और एतिहासिक प्रधानमंत्री माने जाएंगे। भाजपा के कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को उनके पद से हटाया जाना काफी नहीं है। उनकी जाँच करवाना और दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा दिलवा दी जाए तो भारतीय राजनीति में स्वच्छता का शुभारंभ हो सकता है। कहते हैं कि मालवा की महारानी अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को ही दोषी पाए जाने पर हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा दिया था।
मेरे मित्र एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा कि चुनाव जीतने के लिए कोई मंत्र बताइए। मैंने तीन मंत्र बताए। उसमें पहला मंत्र यही था कि भ्रष्ट कांग्रेसियों के यहाँ आप छापे डलवा दीजिए। आप भारत के महानायक बन जाएँगे। लेकिन जो सरकार सिर्फ अपने विरोधियों के यहाँ ही छापे डलवाती है और उन नेताओं और सेठों को छुट्टा छोड़ देती है, जो उसके अपने माने जाते हैं, उस सरकार की छवि चुपचाप पैदे में बैठती चली जाती है।
इसका एक बुरा असर सत्तारुढ़ दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी होता रहता है। वे बेखौफ पैसा बनाने में जुट जाते हैं। अपने विरोधियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयाँ कानूनी दृष्टि से तो ठीक हैं लेकिन उनका नैतिक औचित्य तभी मान्य होगा, जब वे सबके विरुद्ध एक-जैसी हों। (नया इंडिया की अनुमति से)
-रेहान फ़ज़ल
एक विधायक ने मशहूर चुनाव विश्लेषक प्रणय रॉय को बताया था, "भारत में चुनाव एक परीक्षा की तरह हो गए हैं. इसमें कई विषय होते हैं जिन्हें आपको पास करना होता है. ज़रूरी नहीं कि हर विषय में आपके नंबर अच्छे ही आएँ. लेकिन चुने जाने के लिए आपके औसत नंबर 75 फ़ीसदी के आसपास होने चाहिए. वोटरों को सिर्फ़ पासिंग नंबर स्वीकार नहीं हैं. पासिंग नंबर लाने का मतलब है आपका सत्ता से बाहर होना."
बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले दस सालों में इस तरह के कई इम्तिहानों में बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के मुक़ाबले बेहतर स्कोर किया है.
1980 में जब भारतीय जनता पार्टी ने जन्म लिया था तो टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपे एक लेख की बहुत दिलचस्प हेडलाइन थी, 'वेजिटेरियन बट टेस्टी पार्टी'.
तब की बीजेपी और आज की बीजेपी में काफ़ी फ़र्क आया है. एक ज़माने में 'ब्राह्मण-बनियों की पार्टी' कही जाने वाली बीजेपी ने अपने संगठनात्मक ढाँचे में जिस तरह का बदलाव किया है उसको नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है.
हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 'द आर्किटेक्ट ऑफ़ न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रासफॉर्म्ड द पार्टी' के लेखक अजय सिंह इस बदलाव का श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं.
एक संगठन कार्यकर्ता के रूप में मोदी को सबसे पहले पहचान मिली 11 अगस्त 1979 को जब सौराष्ट्र के एक कस्बे मोरवी में मच्छू नदी का बाँध टूट गया और कुछ मिनटों में ही पूरे इलाके में पानी भर गया. ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि लोगों को बच निकलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला और 25 हज़ार लोग बह गए थे.
अजय सिंह बताते हैं, "उस समय बीजेपी के नेता केशूभाई पटेल, बाबू लाल पटेल मंत्रिमंडल में सिंचाई मंत्री थे. जब बाँध टूटा तो नरेंद्र मोदी नानाजी देशमुख के साथ चेन्नई में थे. इस बर्बादी की ख़बर सुनते ही मोदी गुजरात लौटे और उन्होंने बड़े पैमाने पर चल रहे राहत कार्य में हिस्सा लिया.
आडवाणी की रथ यात्रा में मोदी की भूमिका
वर्ष 1984 में जब गुजरात के किसानों ने आंदोलन छेड़ा तो आरएसएस प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ ने इसका ज़ोर-शोर से समर्थन किया. नरेंद्र मोदी ने पर्दे के पीछे रहकर इस आंदोलन के स्वरूप को अंतिम रूप दिया.
वर्ष 1991 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथयात्रा शुरू की तो मोदी को यात्रा के गुजरात चरण की तैयारी करने की ज़िम्मेदारी दी गई.
अजय सिंह बताते हैं, "जब आडवाणी और प्रमोद महाजन सोमनाथ मंदिर के पास वेरावल पहुँचे तो उन्हें वहाँ न तो पार्टी के पोस्टर दिखाई दिए और न ही झंडे. पार्टी हल्कों में इस बात पर चिंता भी प्रकट की गई कि शायद यात्रा के लिए ढंग से तैयारी नहीं की गई है. लेकिन जब अगले दिन यात्रा शुरू हुई तो हज़ारों लोगों की भीड़ सड़कों पर थी. समाज के हर तबके के लोग इसमें शामिल हुए. पहली बार बीजेपी ने उन लोगों तक अपनी पहुँच बनाई जिनसे जुड़ने का प्रयास संघ परिवार ने अभी तक नहीं किया था."
1996 में गुजरात में केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के बीच अंतर्कलह के कारण नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर दिल्ली भेज दिया गया जहाँ पार्टी सचिव के रूप में उन्हें पहले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की ज़िम्मेदारी दी गई. यहाँ पर संगठन के विस्तार के लिए नरेंद्र मोदी ने परंपराओं की जगह व्यवहारिकता को अधिक तरजीह दी.
हरियाणा में उन्होंने इमरजेंसी के दौर में ख़ासे बदनाम हुए बंसीलाल की पार्टी 'हरियाणा विकास पार्टी' से समझौता किया और पहली बार बीजेपी हरियाणा में सत्ता में आई. बाद में जब बंसीलाल से पार्टी ने दूरी बनाई तो नरेंद्र मोदी बीजेपी को ओमप्रकाश चौटाला की पार्टी के नज़दीक ले गए जिन पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप थे.
पार्टी में आम राय के ख़िलाफ़ उन्होंने लोकसभा चुनाव में कारगिल में शहीद हुए सैनिक की पत्नी सुधा यादव को पार्टी का टिकट देने का फ़ैसला लिया.
अजय सिंह बताते हैं, "हिमाचल प्रदेश में उन्होंने शांता कुमार के विकल्प के तौर पर प्रेम कुमार धूमल को खड़ा किया और उनकी सरकार को मज़बूती देने के लिए एक ऐसे नेता का साथ लिया जो भ्रष्टाचार के लिए काफ़ी बदनाम हो चुके थे, नरेंद्र मोदी ने सुखराम का सहयोग लेने में भी कोई झिझक नहीं दिखाई. सुखराम तब तक कांग्रेस छोड़ चुके थे और उन्होंने अपनी पार्टी 'हिमाचल विकास कांग्रेस' बना ली थी. तब तक सुखराम हर किसी के लिए अस्वीकार्य बन गए थे, केवल नरेंद्र मोदी को छोड़कर."
गुजरात दंगों पर हुई आलोचना को गुजरात की अस्मिता से जोड़ा
वर्ष 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था. मुख्यमंत्री बनते समय वो राज्य में विधायक भी नहीं थे. जब गुजरात में दंगे हुए तो शासन में उनकी अनुभवहीनता साफ़ दिखाई दी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने चारों ओर हो रही अपनी आलोचना को गुजरात की पहचान से काउंटर किया.
अजय सिंह बताते हैं, "विपक्ष, मीडिया और धर्मनिरपेक्ष ताकतों की तरफ़ से हो रही आलोचना को मोदी ने गुजराती लोगों की आलोचना से जोड़ दिया. उन्होंने अगले चुनाव में गुजराती अस्मिता के नाम पर वोट माँगे. इस शब्द को सबसे पहले संविधान सभा के सदस्य रहे लेखक केएम मुंशी ने लोकप्रिय बनाया था. उस समय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने 'गुजराती गौरव' को भुनाने के मोदी के प्रयास को पसंद नहीं किया था. उनका मानना था कि गौरव को नाम पर मतदाताओं से की गई अपील शायद सत्ता में होने के नुकसान की भरपाई न कर पाए. लेकिन नरेंद्र मोदी को पूरा विश्वास था कि वो लोगों के मूड को सही ढंग से पढ़ पा रहे हैं. "
गुजरात में आर्थिक निवेश पर बल
गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने सबसे अधिक तवज्जो राज्य में आर्थिक निवेश पर दी. उन्होंने गुजरात को निवेश के लिए सबसे बेहतरीन जगह के तौर पर पूरी दुनिया में पेश किया. मोदी ने गुजरात में 'ज्योति ग्राम योजना' शुरू की जिसके तहत हर घर को 24 घंटे एक फ़ेस बिजली आपूर्ति की गारंटी दी गई. निवेश के लिए नरेंद्र मोदी ने जो माहौल बनाया, रतन टाटा ने उस पर टिप्पणी की थी, "अगर आप गुजरात में निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं."
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रेस में मोदी पर 'सांप्रदायिक पूर्वाग्रह' का आरोप लगने के बावजूद गुजरात में उनकी छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर बनी जिसने विकास को सबसे अधिक तरजीह दी.
सवालों का सामना करना पसंद नहीं?
मैंने अजय सिंह से पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ़ इसलिए कोई संवाददाता सम्मेलन नहीं किया, क्योंकि वो कठिन सवालों से बचते हैं?
इसके जवाब में वे कहते हैं, "आप क्यों मान लेते हैं कि संवाददाता सम्मेलन करने से ही आम लोगों से संवाद स्थापित किया जाता है? उन्होंने चुनाव से पहले कई पत्रकारों से बात की है. हर महीने वो 'मन की बात' कार्यक्रम के ज़रिए देश को संबोधित करते हैं और सोशल मीडिया, ट्विटर और फ़ेसबुक का जितना इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया है उतना शायद किसी भी भारतीय राजनेता ने नहीं. दूसरे, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मोदी से पहले यूपीए की प्रमुख रहीं सोनिया गांधी ने कितने संवाददाता सम्मेलन किए हैं और कितने पत्रकारों को इंटरव्यू दिए हैं? "
सरदार पटेल की मूर्ति बनाने की राजनीतिक चतुराई
अजय सिंह नरेंद्र मोदी के लिए 'राजनीतिक रूप से चतुर' शब्द का इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए वो नर्मदा बांध के पास सरदार पटेल की 'स्टैचू ऑफ़ लिबर्टी' से ऊँची मूर्ति बनाने का उदाहरण देते हैं.
अजय सिंह की नज़रों में वो एक मज़बूत 'पॉलिटिकल स्टेटमेंट' था. जिस तरह से उन्होंने इसके लिए किसानों से अपने कृषि उपकरण दान देने का अनुरोध किया ताकि उन्हें पिघला कर उस लोहे से 182 मीटर ऊँची मूर्ति बनाई जा सके, उसके पीछे भी एक चतुर राजनीतिक सोच थी.
इसे मोदी का चातुर्य कहा जाएगा कि उन्होंने कांग्रेस के महान नेता को 'उपेक्षित गुजराती महानायक' के तौर पर अपनाते हुए आम लोगों के सामने पेश किया. उन्होंने ये भी घोषणा की कि इस मूर्ति को बनाने में पाँच लाख ग्रामीणों के प्रयास को एक टाइम कैप्सूल में रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इससे प्रेरणा ले सकें.
मोदी का वैचारिक लचीलापन
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को कई वैचारिक मुद्दों पर संघ परिवार के घटकों की कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा था. भारतीय मज़दूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच की ओर से वाजपेयी सरकार की तीखी आलोचना आम बात थी.
उसके विपरीत नरेंद्र मोदी का संघ परिवार से सामंजस्य बेहतरीन है. इसकी वजह पूछे जाने पर अजय सिंह बताते हैं, "वाजपेयी का स्वभाव मोदी से बिल्कुल अलग था और दूसरे उनकी अपनी पार्टी का बहुमत नहीं था. मोदी ने क्लासिकल संगठनवादी के रोल में अपने-आप को पूरी तरह से ढाल लिया है जिसके उठाए गए रणनीतिक कदम आगे जाकर विचारधारा को ही फ़ायदा पहुंचाते हैं."
अजय सिंह कहते हैं, "मोदी को इस बात का अंदाज़ा है कि राजनीतिक समझबूझ की परतें समय के साथ बदलती रहती हैं. दक्षिण के मुख्यद्वार और तकनीक के केंद्र रहे हैदराबाद में जब उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया तो उन्होंने बराक ओबामा के अंग्रेज़ी जुमले 'यस वी कैन' का इस्तेमाल किया. उसके कुछ दिनों बाद जब उन्होंने दिल्ली में श्रीराम कालेज ऑफ़ कॉमर्स में छात्रों को संबोधित किया तो उन्होंने उनके सामने प्रबंधन और वाणिज्य की भाषा बोली."
जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में साउथ एशिया स्टडीज़ के प्रमुख वॉल्टर एंडरसन का मानना है, "मोदी ने संघ के संकीर्ण संगठन के दायरे से बाहर आकर मतदाताओं का समर्थन लेने की कोशिश की है. अपने मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने हर गाँव और शहर में प्रभावशाली लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है चाहे उनका पुराना इतिहास जैसा भी रहा हो. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसका भी ध्यान रखा है कि उनके दल के हिंदू विचारधारा के प्रति झुकाव को कमज़ोर न किया जाए. उन्होने ऊँची जातियों के समर्थन बेस को बरकरार रखते हुए हर सामाजिक वर्ग को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की है चाहे वो यादव रहित पिछड़ी जातियों के लोग हों या जाटव रहित अनुसूचित जाति के लोग."
लेकिन उनकी इस योजना में मुसलमान अभी तक नहीं आ पाए हैं. इस समय स्थिति ये है कि न तो उनके मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान है और न ही उनकी पार्टी के संसदीय दल में. अजय सिंह कहते हैं कि शायद इसकी वजह ये है कि मुसलमानों में न सिर्फ़ बीजेपी का समर्थन करने के प्रति झिझक है, बल्कि पार्टी के प्रति उनका रवैया सक्रिय विरोध का रहा है.
हाल के दिनों में बीजेपी ने पिछड़े मुसलमानों से संपर्क साधने का अभियान शुरू किया है.
आठ नवंबर, 2016 को जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा की थी और इसकी वजह से आम लोगों को बहुत अधिक परेशानी झेलनी पड़ी थी, उम्मीद लगाई जा रही थी कि उसके बाद हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.
नोटबंदी की दिक्कतों और उसके उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिलने के बावजूद, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई. शायद इसकी वजह ये थी कि कहीं न कहीं मोदी आम लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हो गए कि उनकी इस कार्रवाई के अपेक्षित परिणाम न निकलें हों, लेकिन उनकी नीयत में कोई खोट नहीं था.
वॉल्टर एंडरसन लिखते हैं, "इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले दिनों संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने एंटी इनकंबेंसी के बावजूद 402 में से 273 सीटें जीतने में सफलता हासिल की है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ख़िलाफ़ कोविड के प्रसार, किसान आंदोलन और बेरोज़गारी जैसे कई मुद्दे काम कर रहे थे. विपक्ष के तीखे प्रचार के बावजूद पार्टी का दोबारा सत्ता में आना बताता है कि मोदी और शाह का जोड़ा चुनाव के माइक्रो प्रबंधन में पारंगत हो चुका है. जहाँ सारा ज़ोर इस बात पर है कि उनके अधिक से अधिक मतदाता चुनाव बूथ तक पहुंचें."
जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में साउथ एशिया स्टडीज़ के प्रमुख वॉल्टर एंडरसन
इमेज कैप्शन,
जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में साउथ एशिया स्टडीज़ के प्रमुख वॉल्टर एंडरसन
मोदी ने इसके महत्व पर रोशनी डालते हुए कहा था, 'मेरे लिए सबसे अधिक ज़रूरी है बूथ जीतना.. अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें चुनाव जीतने से नहीं रोक सकती.'
कर्नाटक बीजेपी के महासचिव एन रवि कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, "दस साल पहले किसी को बूथ स्थर के कार्यकर्ता की फ़िक्र नहीं थी. पार्टी में सिर्फ़ विधायक, सांसद या ज़िला पंचायत अध्यक्ष की ही पूछ हुआ करती थी. कर्नाटक में इस समय 58 हज़ार बूथ हैं. इस तरह हमारे पास 58 हज़ार बूथ अध्यक्ष हैं. हमारे पास हर बूथ पर दो सचिव हैं. इस तरह पूरे प्रदेश में सचिवों की संख्या एक लाख 16 हज़ार हो गई. हर बूथ पर 13 सदस्यों की समिति अलग से बनाई गई है. इसका अर्थ हुआ कि पूरे प्रदेश में सात लाख 54 हज़ार लोग बूथ स्तर पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं."
मीडिया को दबाने की शिकायतें
इस सबके वावजूद मोदी सरकार को अक्सर इसलिए कटघरे में खड़ा किया जाता है कि उनकी सरकार ने चारों तरफ़ भय का माहौल बना रखा है और सरकार की विभिन्न एजेंसियों को राजनीतिक मक़सद से इस्तेमाल किया जा रहा है.
मीडिया को भी दबाने की कई शिकायतें मिली हैं लेकिन मशहूर पत्रकार वीर सांघवी का मानना है कि "ऐसी चीज़े भारत में पहली बार नहीं हुई हैं. इससे पहले भी सरकारों ने राजनीतिक कारणों से एजेंसियों को अपने राजनीतिक विरोधियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है. राजीव गाँधी के समय में इंडियन एक्सप्रेस के ख़िलाफ़ मामले खोले गए और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उनके खिलाफ़ लिखने वाली पत्रिका 'आउटलुक' के मालिकों के दफ़्तर पर रेड की गई थी."
दुनिया के कई नेताओं से मोदी के संबंध बहुत अच्छे हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रेस और संचार माध्यमों में मोदी अपनी आदर्श छवि पेश करने में कामयाब नहीं रहे हैं. चाहे टाइम पत्रिका का दिया गया 'इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ़' का तमग़ा हो या न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, इकॉनॉमिस्ट और ग्लोबल टाइम्स की कई हेडलाइनें. हाल ही में जर्मन विदेश मंत्री ने भारत में प्रजातांत्रिक मूल्यों के हनन के मामलों की आलोचना की. (bbc.com)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू के चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि भारत के विरोधी दल भाजपा को टक्कर देने में आज भी असमर्थ हैं और 2024 के चुनाव में भी भाजपा के सामने वे बौने सिद्ध होंगे। अब उप—राष्ट्रपति के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गेरेट अल्वा के समर्थन से इंकार कर दिया है। याने विपक्ष की उम्मीदवार उप-राष्ट्रपति के चुनाव में भी बुरी तरह से हारेंगी। अल्वा कांग्रेसी हैं। तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस से बहुत आपत्ति है, हालांकि उसकी नेता ममता बेनर्जी खुद कांग्रेसी नेता रही हैं और अपनी पार्टी के नाम में उन्होंने कांग्रेस का नाम भी जोड़ रखा है।
ममता बेनर्जी ने राष्ट्रपति के लिए यशवंत सिंहा का भी डटकर समर्थन नहीं किया, हालांकि सिंहा उन्हीं की पार्टी के सदस्य थे। अब पता चला है कि ममता बनर्जी द्रौपदी मुर्मू की टक्कर में ओडिशा के ही एक आदिवासी नेता तुलसी मुंडा को खड़ा करना चाहती थीं। ममता ने यशवंत सिंह को अपने प्रचार के लिए पं. बंगाल आने का भी आग्रह नहीं किया। इसी का नतीजा है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों और सांसदों ने भाजपा की उम्मीदवार मुर्मू को अपना वोट दे दिया। इससे यही प्रकट होता है कि विभिन्न विपक्षी दलों की एकता तो खटाई में पड़ी ही हुई है, इन दलों के अंदर भी असंतुष्ट तत्वों की भरमार है।
इसी का प्रमाण यह तथ्य है कि मुर्मू के पक्ष में कई दलों के विधायकों और सांसदों ने अपने वोट डाल दिए। कुछ गैर-भाजपा पार्टियों ने भी मुर्मू का समर्थन किया है। इसी का परिणाम है कि जिस भाजपा की उम्मीदवार मुर्मू को 49 प्रतिशत वोट पक्के थे, उन्हें लगभग 65 प्रतिशत वोट मिल गए। द्रौपदी मुर्मू के चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के विपक्षी दलों के पास न तो कोई ऐसा नेता है और न ही ऐसी नीति है, जो सबको एकसूत्र में बांध सके। देश में पिछले दिनों दो-तीन बड़े आंदोलन चले लेकिन सारे विरोधी दल बगलें झांकते रहे। उनकी भूमिका नगण्य रही।
वे संसद की गतिविधियां जरुर ठप्प कर सकते हैं और अपने नेताओं के खातिर जन-प्रदर्शन भी आयोजित कर सकते हैं लेकिन देश के आम नागरिकों पर उनकी गतिविधियां का असर उल्टा ही होता है। यह ठीक है कि यदि वे राष्ट्रपति के लिए किसी प्रमुख विरोधी नेता को तैयार कर लेते तो वह भी हार जाता लेकिन विपक्ष की एकता को वह मजबूत बना सकता था। लेकिन भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिंहा को अपना उम्मीदवार बनाकर विपक्ष ने यह संदेश दिया कि उसके पास योग्य नेताओं का अभाव है।
मार्गेरेट अल्वा भी विपक्ष की मजबूरी का प्रतीक मालूम पड़ती हैं। सोनिया गांधी की तीव्र आलोचक रहीं 80 वर्षीय अल्वा को उप-राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने आगे करके अपने आप को पीछे कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि उप-राष्ट्रपति के लिए जगदीप धनकड़ के पक्ष में प्रतिशत के हिसाब से राष्ट्रपति को मिले वोटों से भी ज्यादा वोट पड़ेंगे याने विपक्ष की दुर्दशा अब और भी अधिक कर्कश होगी। (नया इंडिया की अनुमति से)
-जुबैर अहमद
भारत में डिजिटल यानी ऑनलाइन न्यूज मीडिया के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि जल्द ही सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने जा रही है।
केंद्र सरकार ने इसी मुद्दे पर एक नया विधेयक तैयार किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये विधेयक इस समय जारी संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है।
सरकार साल 2019 में ही प्रेस और पत्रिका के पंजीकरण विधेयक, 2019 को नया स्वरूप दे चुकी है। अब जिस विधेयक को लाने की तैयारी है, उसके दायरे में पहली बार डिजिटल समाचार मीडिया इंडस्ट्री को शामिल करने की तैयारी है।
हालांकि, इस विधेयक का कोई मसौदा सामने नहीं है, लेकिन आ रही खबरों से पता चला है कि अब सभी डिजिटल मीडिया पोर्टल और वेबसाइट को अपना पंजीकरण करवाना होगा।
इसके बाद डिजिटल न्यूज मीडिया को सरकार द्वारा रेगुलेट किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि ये नया अधिनियम 155 साल से लागू च्प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की जगह लेगा।
यह कानून 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश इंडिया में लागू किया गया था।

उस वक्त इस कानून को प्रेस के माध्यम से, विद्रोह के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था।
बीते कुछ सालों में भारत में डिजिटल मीडिया के जरिए समाचारों के प्रकाशन में बहुत इजाफा हुआ है। इन माध्यमों के जरिए न्यूज देने वाले संस्थानों की संख्या भी काफी बढ़ी है।
लेकिन तमाम परिवर्तनों के बावजूद अब तक 155 साल पुराने कानून में किसी ने संशोधन करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अब मौजूदा सरकार ने इस नए विधेयक को तैयार किया है जिसके पारित होने पर 1867 वाले कानून का अंत हो जाएगा।
लेकिन कई लोगों का तर्क है कि केंद्र सरकार डिजिटल न्यूज मीडिया को ‘नियंत्रित’ करने का प्रयास कर रही है।
कुछ विश्लेषक कहते हैं कि मोदी सरकार असहमति की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।
पत्रकार और एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संस्था के आकार पटेल ने अपने एक लेख में इस विधेयक को प्रेस की आजादी के लिए खतरा बताया है।
आकार पटेल ने लिखा, ये भारत के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं हैं। सरकार बेहद शक्तिशाली है और प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं। विपक्ष फिलहाल अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहा है।
मशहूर लेखक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर सुधीश पचौरी कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त डिजिटल मीडिया पर हमले नहीं होते। कोई मामला हुआ तो पुलिस जाती है, मीडिया वाले को गिरफ्तार कर लेती है। अब तक तो ऐसे मामलों को आईटी कानून के तहत दर्ज किया जा रहा है। लेकिन ये किसी सीधे कानून के अभाव के कारण ही था। डिजिटल मीडिया के लिए अलग से एक नया कानून तो आना ही था।
उनके मुताबिक ऐसा कानून आज नहीं तो कल, कोई न कोई सरकार हो लाएगी ही।

सुधीश पचौरी कहते हैं कि तानाशाही का खतरा सिर्फ सरकार की तरफ से ही नहीं है, अब तो विभिन्न गुटों की तरफ से भी उतनी ही तानाशाहियां हैं।
लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि इस विधेयक में बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने जैसी कोई बात नहीं है।
प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन सूर्य प्रकाश इस तर्क को बेबुनियाद मानते हैं।
वे कहते हैं, मैंने इस पर मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, मुझे वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को कम कर देगा।
सूर्य प्रकाश का कहना है कि जमाने के हिसाब से पुराने कानूनों को बदलना सराहनीय काम है।
उन्होंने बीबीसी को बताया, प्रस्तावित विधेयक मीडिया को आधुनिक युग में लाने के लिए है। मैंने हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट देखी जिसमें कहा गया है कि 63 प्रतिशत भारतीय युवा डिजिटल मीडिया पर ही न्यूज देखते, सुनते या पढ़ते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कानून में बदलाव के साथ-साथ, समय के साथ तकनीक में भी तालमेल बिठाया जाना चाहिए। (bbc.com/hindi)
-अल्पयु सिंह
क्रिस्टोफर की अपनी डायरी में ये आखिरी एंट्री थी। शायद अपनी मौत से कुछेक घंटे पहले उसने ये बात लिखी। जिस दिन उसने दम तोड़ा वो दिन बेहद हसीन था। नीले आसमान में बादल सफेद दुपट्टों की मानिंद इधर-उधर तैर रहे थे। अलास्का के जंगल में उसका आशियाना बनी नीले रंग की वैन में हरियाली खिली थी। लेकिन उसे ये सब छोडऩा था, वो जानता था।
कांपती कमजोर उंगलियों से उसने किसी तरह ये लाइन लिखी और खुली आंखों से ही दम तोड़ दिया जैसे इतने खूबसूरत नजारों को वो आखिरी वक्त तक नजरों के सामने रखना चाहता था। अगस्त 1992 में उसकी मौत की खबर न्यूज के जरिए लोगों तक पहुंची और तब हर कोई समझना चाहता था कि आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा, एक अमीर खानदान का 22 साल का लडक़ा, जो Bright ¥õÚU Sensitive दोनों था, जिसने ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से की थी और जिसके आगे एक सुनहरा कल सामने खड़ा था। वो तो अमेरिकन ड्रीम का पोस्टर ब्वॉय बन सकता था। लेकिन उसने जो कुछ किया, वो सबकी समझ से परे था।
ग्रेजुएट होते ही वो घर वालों को बताए बगैर खुद की खोज पर निकल गया। उसने एक-एक कर अपनी सारी मैटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ दी। कार कहीं छोड़ दी। डॉलर जला दिए और दो-चार कपड़ों में दो साल अमेरिका के कई जंगलों में बिना किसी प्लान या पैसे के दो साल बिताए। रास्ते में कई लोग मिले, कुछ खराब लेकिन ज्यादातर अच्छे, लेकिन आदमी, सोसायटी, रिवाज जैसे शब्दों से उकताया क्रिस चीजों की ही तरह रिश्तों का या भावनाओं का भी आदी नहीं होना चाहता। उसे जब लगता रास्ते में मिलने वाले लोग उससे मन जोडऩे लगे हैं वो बिना किसी को कुछ कहे वहां से चुपचाप चल देता।
फिल्म बताती है कि 75 साल के रॉन के मामले में क्रिस भी खासा पिघला। वो बुजुर्ग उसे पोते जैसा मानने लगे थे। लेकिन अलास्का के लिए अकेले निकलने से पहले वो उनसे कहता है कि आपको लगता है कि जीवन की सच्ची खुशी सिर्फ रिश्तों से मिलती है, तो आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। डॉलर, स्टॉक, अपार्टमेंट, वीकेंड, मल्टीनेशनल के इर्द-गिर्द चक्कर लगाने वाले खाए-अघाए अमेरिकन समाज की एक टिपिकल अमेरिकन फैमिली से निकला ये लडक़ा आखिर क्या चाहता था? क्यों इंसान और उससे जुड़ी हर रवायत से वो दूर रहना चाहता? क्या ये सिर्फ वहां के हिप्पी कल्चर की ही झलक थी? या तरूणाई की बागीपन या खुद की खोज का सफर।
सवालों के जवाब तो क्रिस के साथ ही चले गए लेकिन शायद एक सवाल का जवाब वो साफ साफ दे गया। जो शख्स भावनाओं और जुड़ाव से भी हमेशा बचने की कोशिश करता रहा, उसने मरने से पहले आखिर ऐसा क्यों लिखा - Happiness only real when shared। वैसे ये सच्ची कहानी है, जिस पर किताब और फिल्म दोनों बनी हैं।
सिंडीकेट तो इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति बनवाकर निपटाना चाहता था..!
मोरारजी देसाई को बाहर कर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का धमाका किया इंदिरा ने।
देश में पहली बार चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यकारी राष्ट्रपति बने।
-डॉ. राकेश पाठक
देश के अगले राष्ट्रपति के लिए मतदान हो चुका है। तय है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम नागरिक होंगीं।
इस अवसर पर हम आपको इतिहास के सबसे रोचक राष्ट्रपति चुनाव के किस्से सुना रहे हैं।
अब तक दो किस्तों में आप पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ‘अंतरात्मा की आवाज’ पर कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को पटखनी दिलवा कर अपने उम्मीदवार वी वी गिरि को राष्ट्रपति बनवाया। इसके बाद इंदिरा को कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया गया और पार्टी दो फाड़ हो गई।
सन् 1969 का यह चुनाव बहुतेरी सियासी कथाओं से भरा हुआ है।
आइए अब आपको कुछ और दिलचस्प वाकयात से रूबरू करवाते हैं।
कामराज ने इंदिरा को राष्ट्रपति बनाने का दांव फेंका
पूर्व में हम बता चुके हैं कि इंदिरा गांधी को ‘गूंगी गुडिय़ा’ कहने वाले कांग्रेस के खांटी दिग्गजों से उनका संघर्ष शुरू हो चुका था। कामराज,निजलिंगप्पा,अतुल्य घोष, एस के पाटिल, मोरारजी देसाई,नीलम संजीव रेड्डी आदि का खेमा ‘सिंडीकेट’कहलाने लगा था। सिंडीकेट कदम कदम पर इंदिरा गांधी की राह में कांटे बिछाता रहता था।
मजे की बात यह है कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडीकेट के दो दिग्गजों कामराज और निजलिंगप्पा का बहुत बड़ा हाथ था लेकिन जल्द ही उनके बीच तलवारें खिंच गईं थीं।
डॉ.जाकिर हुसैन के अचानक निधन से समय से पहले राष्ट्रपति चुनाव की नौबत आ गई। इस मौके पर सिंडीकेट ने इंदिरा गांधी को धूल चटाने के लिए जाजम बिछाना शुरू कर दिया।
चुनाव से पहले बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। इस समय पार्टी अध्यक्ष सिंडीकेट के ही सूरमा एस निजलिंगप्पा थे। निजलिंगप्पा मैसूर के पहले मुख्यमंत्री रहे थे।
इसमें पार्टी की ओर से उम्मीदवार तय होना था। इंदिरा गांधी ने बाबू जगजीवन राम का नाम आगे बढ़ाया लेकिन सिंडीकेट अपनी मनमर्जी पर उतारू था। उसने नीलम संजीव रेड्डी का नाम रख दिया। कार्यसमिति में इंदिरा गांधी मात खा गईं। बहुमत से सिंडीकेट के प्रत्याशी रेड्डी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए तय हो गया।
लेकिन सिंडीकेट का असल दांव अभी बाकी था। रेड्डी का नाम तय होने के बावजूद के.कामराज ने अपने भाषण में इंदिरा गांधी के कसीदे पढ़े और कहा कि हम चाहते हैं कि इंदिरा जी स्वयं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें।
इंदिरा गांधी के लिए यह समझना कठिन नहीं था कि सिंडीकेट उनके राजनीतिक जीवन की भ्रूण हत्या करने के लिए जाल बिछा रहा है।
इंदिरा गांधी ने कामराज के प्रस्ताव पर कान नहीं धरे लेकिन सिंडीकेट से निपटने की कसम खा कर बैंगलुरु से दिल्ली लौटीं।
मोरारजी को बाहर करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण
बुजुर्ग नेताओं के सिंडीकेट से मुकाबला करने में इंदिरा गांधी को पार्टी के ‘युवा तुर्क’ नेताओं का साथ मिल रहा था। ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग टर्क के इस मौसम में इंदिरा गांधी ने युवा तुर्कों की बहु प्रतीक्षित मांग को पूरा करने का फैसला किया।
ये मांग थी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्ण कांत जैसे युवा तुर्क इसके लिए आवाज उठाते रहे थे जबकि सिंडीकेट के बुढ़ऊ इसके लिए तैयार नहीं थे।
खासतौर पर इंदिरा गांधी सरकार में वित्तमंत्री मोरारजी देसाई इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थे।
इंदिरा गांधी ने सबसे पहले मोराराजी को मंत्री पद से हटाया। चौबीस घंटे में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश तैयार करवाया और 19 जुलाई 1969 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी।
(यह संयोग ही है कि अभी-अभी 19 जुलाई गई है।)
राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और इंदिरा गांधी के इस ऐतिहासिक फैसले ने सिंडीकेट को भौंचक कर दिया। देश में इस फैसले की अच्छी प्रतिक्रिया हुई थी।
दोनों पद खाली हो रहे थे इसलिए सीजेआई बने राष्ट्रपति
इस चुनाव में एक और रोचक घटना हुई थी।
जिस समय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई उस समय वी वी गिरि उपराष्ट्रपति थे। परंपरा अनुसार वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
लेकिन जब वे इंदिरा गांधी के इशारे पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए तब उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा देना पड़ा।
इस बीच जब इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश तैयार करवा लिया तो वी वी गिरि ने इस पर बतौर राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए और अगले दिन त्यागपत्र दे दिया।
अब एक और संकट सामने आ गया।
गिरि उपराष्ट्रपति पद पहले ही छोड़ चुके थे और अब चुनाव मैदान में आने पर राष्ट्रपति के कार्यवाहक दायित्व से भी मुक्त हो गए।
दोनों पद खाली नहीं रह सकते थे। तब तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्ला को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया।
आजादी के बाद यह पहला मौका था जब देश के प्रधान न्यायाधीश को राष्ट्रपति का दायित्व सम्हालना पड़ा।
(डॉ राकेश पाठक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वर्तमान करमवीर न्यूज के प्रधान संपादक हैं।)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
सर्वोच्च न्यायालय ने नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर के साथ पूरा न्याय किया है। उसने दोनों के खिलाफ की गई दर्जनों पुलिसिया शिकायतों (एफआईआर) को रद्द करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ जो भी मुकदमे चलें, वे किसी एक ही शहर में चलें। कई शहरों में अगर उन पर मुकदमे चलते रहे तो कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सबसे पहली तो यही कि कई फैसले परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। दूसरी समस्या यह कि आरोपी व्यक्ति कितने शहरों की अदालतों का चक्कर लगाता रहेगा? तीसरी समस्या उसकी अपनी सुरक्षा की है।
वैसे जुबैर को उनके विवादास्पद ट्वीट पर वैसी धमकियां नहीं मिल रही हैं जैसी कि नुपुर शर्मा को मिल रही है। कानून की जिन लोगों को थोड़ी भी समझ है, उन्हें पता है कि जुबैर और नुपुर दोनों को ही अदालत निर्दोष घोषित करने वाली हैं। नुपुर की गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हुई है लेकिन जुबैर को हफ्तों जेल में डाले रखा गया है। उन्हें जमानत भी नहीं मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें तुरंत रिहा किया और उसने उ. प्र. की सरकार और पुलिस की भी कड़ी आलोचना की है।
सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने कहा है कि किसी भी पत्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई भी बाधक कैसे बन सकता है? यदि जुबैर ने 2018 में किसी फिल्म के संवाद को ट्वीट कर दिया तो क्या उसने इतना खतरनाक काम कर दिया है कि उसे जेल में बंद कर दिया जाए, उसे जमानत भी नहीं दी जाए और उसे दंगे भडक़ाने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? जजों ने इस तथ्य पर भी एतराज जाहिर किया है कि जुबैर के खिलाफ कई एजेन्सियां जांच-पड़ताल में जुट गई हैं।
जुबैर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तरह-तरह के आरोप लगाए हैं। उसका तर्क था कि जुबैर पत्रकार नहीं है। वह ‘अल्टन्यूज’ नामक संस्था चलाता है और उसके जरिए वह दो करोड़ रु. सालाना कमाता है। 2018 में उसने एक फिल्म के एक चित्र को फिर से ट्वीट करके लिख दिया था- ‘2014 से पहले हनीमूल होटल, 2014 के बाद हनुमान होटल’। इसी तरह के अन्य कई आरोप जुबैर पर लगाए गए थे। इन सब आरोपों की जांच अब दिल्ली की अदालत करेगी।
इससे भी अधिक दयनीय मामला नुपुर शर्मा का है। एक टीवी संवाद में जब एक वक्ता ने शिवलिंगों का मजाक उड़ाया तो नुपुर ने जवाब में एक हदीस को उद्धृत कर दिया। इसे पैगंबर की शान में गुस्ताखी माना गया और उसके चलते दो लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई, नुपुर की हत्या की धमकियां दी गईं और उस पर मुकदमे दायर हो गए। जुबैर के खिलाफ सरकारी रवैए और नुपुर के खिलाफ कुछ लोगों के रवैए से ऊपर उठकर सर्वोच्च न्यायालय ने जो निष्पक्ष रवैया अपनाया है, वही धर्म-निरपेक्ष भारत में उचित और शोभनीय है। (नया इंडिया की अनुमति से)