श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों में दाखिल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो तब तक वहां बने रहेंगे जब तक दोनों नेता आधिकारिक रूप से इस्तीफ़ा नहीं दे देते.
संसद के स्पीकर के शनिवार को दिए गए बयान के मुताबिक राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि वो 13 जुलाई इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन राष्ट्रपति ने अब तक इस बारे में ख़ुद कोई बयान नहीं दिया है.
वहीं प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को विरोध के बाद कहा कि वो अपना पद छोड़ देंगे. उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया.
छात्र प्रदर्शनकारियों के नेता लाहिरु वीरासेकरा ने न्यूज़ एजेंसी एएफ़पी से कहा, "हमारा संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है. हम तब तक इस संघर्ष को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक वो (राष्ट्रपति राजपक्षे) जाते नहीं हैं."
राजनीतिक समीक्षक और मानवाधिकार वकील भवानी फोन्सेका ने रॉयटर्स से कहा, "अगले कुछ दिन बहुत अहम हैं क्योंकि इस दौरान ये देखने को मिलेगा कि यहां कि राजनीति में क्या होता है."
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों नेता वास्तव में इस्तीफ़ा दे देंगे.
बीते कई महीनों के विरोध प्रदर्शन और दोनों नेताओं से इस्तीफ़े की मांग के बाद श्रीलंका में शनिवार को बड़ी संख्या में लोग ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों में घुस गए.
राष्ट्रपति को देश के आर्थिक दुर्व्यवस्था के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसकी वजह से देश में महीनों से खाद्य पदार्थों, ईंधन और दवाओं की कमी हो रही है.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने मीडिया में पूछे जा रहे सवालों के जवाब में बताया है कि नकदी की समस्या से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने इस साल 3.8 बिलियन डॉलर की मदद पहुंचाई है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि, हम उन कई चुनौतियों से अवगत हैं जिसका सामना श्रीलंका और वहां के लोग कर रहे हैं. इस कठिन दौर से उबरने की कोशिश में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं.
अरिंदम बागची ने कहा, "नेबरहुड फर्स्ट नीति की केंद्र में श्रीलंका है और इसे देखते हुए भारत ने इस साल श्रीलंका में गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने को लेकर 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का अभूतपूर्व समर्थन दिया है."
अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहा है. वो पहले से ही कर्ज़ में डूबा हुआ है. वो कर्ज़ की किस्तों को भी नहीं चुका पा रहा है. वो अपने पड़ोसी देशों भारत, चीन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी आर्थिक मदद मांग रहा है.
श्रीलंकाई सेना के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ जनरल शवेंद्रा सिल्वा ने रविवार को लोगों से अपील की कि वो देश के सामने मौजूद संकट के शांतिपूर्ण समाधान में मदद करें.
प्रदर्शनकारी शनिवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास में घुस गए थे. बाद में कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में आग लगा दी थी. इन घटनाओं के बाद से राजधानी कोलंबो में तनाव बना हुआ है. राष्ट्रपति राजपक्षे अभी कहां हैं, इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.
इस बीच, श्रीलंका पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि रनिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगाने के मामले में रविवार को तीन संदिग्धों को गिरफ़्तार किया गया है. गिरफ़्तार किए गए लोगों की पहचान जाहिर नहीं की गई है.
श्रीलंका में सरकार के ख़िलाफ़ जारी विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे कई लोगों ने सोशल मीडिया पर हिंसा की निंदा की है. इनमें कई पूर्व क्रिकेटर भी शामिल हैं.
इस बीच कोलंबो की सड़कों पर तैनात पुलिस और सेना के जवाब अपने कैंप और स्टेशनों में लौट गए हैं. शनिवार के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया था. रविवार को बहुत कम पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर नज़र आए.
इस बीच श्रीलंका सरकार के मंत्री धम्मिका परेरा ने इस्तीफ़ा दे दिया है. उन्हें हाल में निवेश संवर्धन मंत्री बनाया गया था. रविवार को राष्ट्रपति के नाम लिखे पत्र में परेरा ने कहा कि उन्होंने ये पद मौजूदा संकट को देखते हुए और देश के प्रति अपने प्यार की वजह से स्वीकार किया था.
परेरा को मिलाकर अब तक चार मंत्री इस्तीफ़ा दे चुके हैं. इनमें हैरिन फर्नांडो, मनुषा नानायकारा और बंधुला गुणावर्धने शामिल हैं.
इस बीच राष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी कि देश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आ रही है. श्रीलंका में बीते काफी समय से गैस और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों की कमी है.
सचिवालय ने बताया कि 37सौ मीट्रिक टन गैस लेकर कार्गो शिप रविवार को पहुंचेगा. पत्र में जानकारी दी गई है कि गैस पहुंचते ही सिलेंडर की डिलेवरी शुरू हो जाएगी. दूसरी खेप 11 जुलाई यानी सोमवार को पहुंचेगी.
श्रीलंका में चल रहे वर्तमान संकट के दरम्यान कांग्रेस पार्टी ने रविवार को श्रीलंकाई लोगों के साथ अपनी एकजुटता ज़ाहिर की है और उम्मीद जताई है कि वो इस संकट से उबरने में सक्षम होंगे.
साथ ही कांग्रेस ने ये उम्मीद भी जताई कि भारत मौजूदा हालात से निपटने में अपने पड़ोसी देश की मदद करता रहेगा.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक संदेश में कहा कि कांग्रेस पार्टी श्रीलंका में उभरती राजनीतिक स्थिति पर चिंता ज़ाहिर करती है और लगातार वहां की स्थिति पर नज़र बनाए है.
उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौती, बढ़ती कीमतें और खाद्य पदार्थों, इंधन और आवश्यक वस्तुओं की कमी ने वहां लोगों के बीच कठिनाई और भारी संकट पैदा किया है.
सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा, "कांग्रेस पार्टी संकट की घड़ी में श्रीलंका और उसके लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती है और उम्मीद करती है कि वो इससे उबरने में सक्षम होंगे."
उन्होंने ये भी कहा कि, "हमें उम्मीद है कि वर्तमान मुश्किल के दौर में भारत, श्रीलंका की सरकार और वहां के लोगों की सहायता करना जारी रखेगा."
श्रीलंका संकट पर यूरोपीय यूनियन का बयान
यूरोपीय यूनियन (ईयू) ने कहा है कि श्रीलंका संकट पर उसकी नज़र है और वो श्रीलंका के लोगों को और मदद मुहैया कराने के लिए उपलब्ध विकल्पों का जायजा ले रहा है.
ईयू प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि श्रीलंका के घटनाक्रम पर उनकी क़रीबी नज़र है.
ईयू ने श्रीलंका के सभी दलों से अपील की है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता तलाशें.
बयान में कहा गया है, " हम सभी पार्टियों से अपील करते हैं कि वो आपस में सहयोग करें और शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और व्यवस्थित हस्तांतरण पर ध्यान लगाएं. "
श्रीलंका संकट पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर
उधर भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आर्थिक संकट से ग़ुजर रहे श्रीलंका की मदद कर रहा है.
रविवार को केरल पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा श्रीलंका का समर्थन करता रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल अभी कोई शरणार्थी संकट नहीं है.
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचे एस जयशंकर ने हवाई अड्डे के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हम श्रीलंका का समर्थन करते रहे हैं. हम इस वक़्त भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं."
श्रीलंका में ताज़ा आर्थिक संकट पर पूछे गए एक सवाल पर जयशंकर ने कहा, "फिलहाल वो अभी अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, लिहाजा हमें इंतज़ार करना होगा और ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं."
इस दौरान शरणार्थी संकट पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, "फिलहाल कोई शरणार्थी संकट नहीं है."
अभूतपूर्व आर्थिक संकट के जूझ रहे श्रीलंका में लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफ़े की मांग को लेकर बीते कुछ महीनों से सड़कों पर ज़ोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं. शनिवार को यह प्रदर्शन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गया जिसके बाद देर शाम तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए.
पीएम के घर में आग लगाने के मामले में तीन गिरफ़्तार
श्रीलंका पुलिस के मुताबिक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगाने के मामले में तीन संदिग्ध लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
श्रीलंका में शनिवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के घर में आग लगा दी गई थी. रिपोर्टों के मुताबिक उस समय विक्रमसिंघे अपने घर में मौजूद नहीं थे.
श्रीलंका पुलिस के प्रवक्ता ने गिरफ़्तारी की जानकारी दी है.
शनिवार को प्रदर्शनकारी पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर में घुसे. रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रपति उसके पहले सुरक्षित जगह चले गए थे. बाद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की ओर से बताया गया कि वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं.
प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन से लाखों रुपये मिलने का दावा
श्रीलंका में शनिवार को बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुस गए और तोड़फोड़ की. मीडिया रिपोर्टों में ये दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन से लाखों रुपये मिले हैं.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें राष्ट्रपति आवास में घुसे लोग नोटों की गिनती कर रहे हैं. श्रीलंका के मीडिया आउटलेट डेली मिरर की रिपोर्ट कहती है कि इस पैसे को सिक्योरिटी यूनिट्स को सौंप दिया गया है.
प्रशासन का कहना है कि वो मामले की जांच के बाद मौजूदा स्थिति की जानकारी देंगे.
शनिवार को कोलंबो में हज़ारों लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफ़े की मांग करते हुए राजधानी कोलंबो में इक्ट्ठा हुए थे. देश के ख़राब आर्थिक हालात से जूझ रहे लोगों का प्रदर्शन हिंसक हो उठा और वो राष्ट्रपति आवास में घुस गए. सामने आ रहे वीडियो और तस्वीरों में लोग राष्ट्रपति आवास की रसोई, बिस्तर और टॉयलेट का इस्तेमाल भी करते दिख रहे हैं.
प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के निज़ी आवास को भी आग लगा दी. हालांकि, प्रदर्शनकारियों के हल्लाबोल के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही अपने आवासों में मौजूद नहीं थे.
शनिवार रात को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने ही इस्तीफ़े की घोषणा कर दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.
सेना ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने के लिए की अपील
श्रीलंका में शनिवार को हुए बेहद हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने के लिए सुरक्ष बलों के साथ सहयोग करने की अपील की है.
श्रीलंका के चीफ़ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ़ ने कहा है कि राजनीतिक संकट के शांतिपूर्ण तरीक़े से समाधान के लिए एक मौका आया है.
शनिवार को गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर हमला बोल दिया था. वहीं, हज़ारों की भीड़ ने प्रधानमंत्री के निजी आवास पर आग लगी दी थी.
लोगों को हिंसा से रोकने के लिए सेना और पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें भी छोड़ीं लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा.
श्रीलंका में लोग खाने के समाने, पेट्रोल और दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं. सरकार के पास इन आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची है. वहीं, देश में महंगाई आसमान छू रही है.
देश के खराब आर्थिक हालात से नाराज लोग महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं.
शनिवार को विरोध प्रदर्शन के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा देने की घोषणा की है.
प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों की कार्रवाई बना मानवाधिकार हनन का मुद्दा
शनिवार को लगे कर्फ़्यू और पिछले कुछ दिनों से श्रीलंका में आ रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया आई है. श्रीलंका की मानवाधिकार परिषद ने भी शनिवार रात एक बयान जारी कर कहा है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस का शनिवार को कर्फ़्यू लगाना अवैध था.
इस बयान को शीर्षक दिया गया है, "जो आप प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कर सकते उसे अप्रत्यक्ष तौर पर ना करें. किसी मार्च को रोकने के लिए कोर्ट का आदेश ना मिलने पर सरकार अवैध तरीक़े से मार्च रोकने की कोशिश कर रही है."
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने भी सरकार और लोगों के बीच चल रहे टकराव को लेकर एक बयान जारी कर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए संयम बरतने की सलाह दी थी.
संयुक्त राष्ट्र ने कहा, "हम शनिवार को कोलंबो में बड़े स्तर पर हुए प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन से जनसभाओं को संभालने और हिंसा रोकने के लिए संयम बरतने की अपील करते हैं."
इसके अलावा मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक वीडियो जारी कर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों और पुलिस के हमले की निंदा की है. एमनेस्टी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक मानवाधिकार है.
श्रीलंका में शनिवार को राजधानी कोलंबो में जनसैलाब उमड़ आया और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास पर हमला बोल दिया. इसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को इस्तीफ़े की घोषणा करनी पड़ी.
लेकिन, इससे पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन को ख़त्म करने और हज़ारों की संख्या पहुंचे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने इलाक़े में कर्फ़्यू लगा दिया लेकिन उसका खास फ़ायदा नहीं हुआ. पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें भी छोड़ीं.
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही प्रदर्शनकारियों के हल्लाबोल के समय अपने घर से थे नदारद
श्रीलंका में शनिवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी. वो 13 जुलाई को इस्तीफ़ा देने वाले हैं.
इससे पहले शनिवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास के अंदर घुस गए थे. उन्होंने प्रधानमंत्री के निजी आवास में भी आग लगा दी थी.लेकिन, उस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही अपने आवास पर मौजूद नहीं थे.श्रीलंका में खराब आर्थिक हालात के चलते लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. प्रदर्शनकारी लगातार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं.फिलहाल राष्ट्रपति के साथ-साथ प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी है.शनिवार को संसद के स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रपति ने ''सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करने'' के लिए अपने पद से हटने का फ़ैसला किया है. साथ ही उन्होंने लोगों से ''क़ानून का सम्मान'' करने की अपील की है.इस घोषण के बाद शहर में जश्न का माहौल बन गया और लोग आतिशबाजियां करने लगे.
श्रीलंका के राजनीतिक संकट के समाधान पर आईएमएफ़ ने क्या कहा
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वो श्रीलंका के राजनीतिक संकट के समाधान की उम्मीद कर रहा है जिससे बेल आउट पैकेज को लेकर बातचीत फिर से शुरू की जा सके.
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शनिवार को इस्तीफ़े की घोषणा कर दी है. वो 13 जुलाई को इस्तीफ़ा देने वाले हैं.
इससे पहले शनिवार को श्रीलंका में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुस आए.
प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के निजी आवास में भी आग लगा दी.
आईएमएफ़ ने एक बयान जारी कर कहा, "हम मौजूदा स्थिति के समाधान की उम्मीद करते हैं जिससे आईएमएफ से सहयोग वाले कार्यक्रम को लेकर बातचीत शुरू हो सके."
श्रीलंका के हालात पर अमेरिका ने दी चेतावनी
अमेरिका ने रविवार को श्रीलंका के नेताओं से संकट के दीर्घकालीन हल के लिए जल्द कदम उठाने की अपील की है. शनिवार को राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे को अपना सरकारी आवास छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़े का एलान कर दिया है. अमेरिका का ये संदेश श्रीलंका में शनिवार को हुए घटनाक्रम के बाद आया है. समाचार एजेंसी एएफ़पी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन इस समय थाईलैंड के दौरे पर हैं.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "श्रीलंका की संसद को इन हालात में देश की बेहतरी के लिए, न कि किसी राजनीतिक दल के लिए प्रतिबद्धता लेकर कदम उठाना चाहिए. हम इस सरकार या संवैधानिक रूप से चुनी गई किसी नई सरकार से तेज़ी से काम करने की अपील करते हैं ताकि संकट का हल तलाशा जा सके और उस पर अमल हो. इससे श्रीलंका में लंबे समय के लिए आर्थिक स्थिरता आएगी और बिगड़ती आर्थिक स्थिति, भोजन और ईंधन की कमी को लेकर श्रीलंका के लोगों का जो असंतोष है, उसका हल निकाला जा सकेगा."
अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों या पत्रकारों पर किसी हमले को लेकर चेतावनी भी दी है. हालांकि शनिवार को हुई हिंसा को लेकर अमेरिका ने उसकी आलोचना भी की है. शनिवार को नाराज़ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे का घर जला दिया था.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "श्रीलंका के लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है. हम प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की किसी भी घटना की पूरी जांच और जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी और उनपर कार्रवाई की मांग करते हैं."
अमेरिका श्रीलंका के गृह युद्ध को लेकर राजपक्षे सरकार की नीतियों और चीन के साथ उसकी नजदीकी का कटु आलोचक रहा है. (bbc.com)





.jpg)


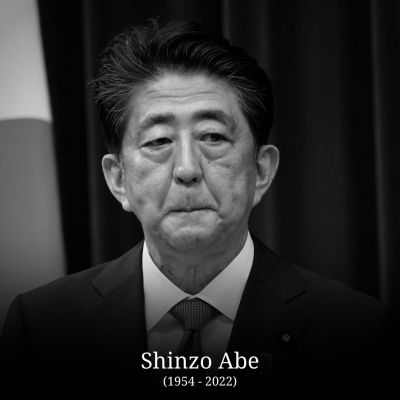
.jpg)
.jpg)









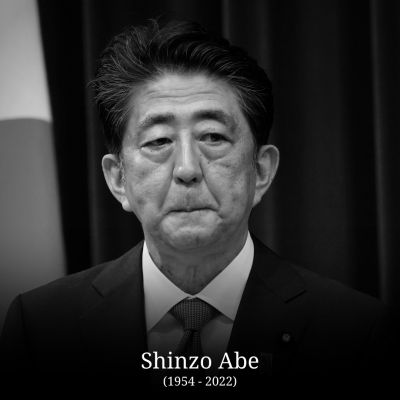

.jpg)

.jpg)

.jpg)







