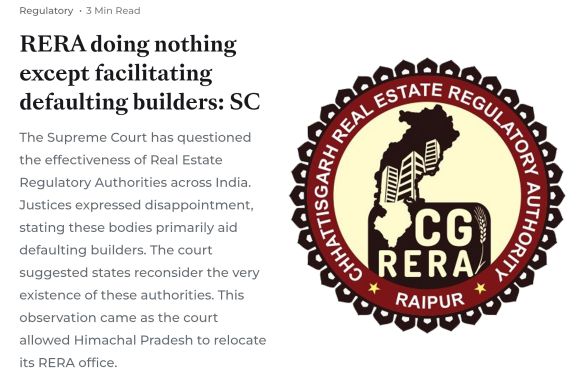संपादकीय

दिल्ली में शहरी बेघरों के लिए सिर पर छत की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस बी.आर.गवई ने सवाल किया कि क्या चुनावों के पहले जिन रेवडिय़ों की घोषणा की जाती है, क्या उनकी बजाय बेघरों को समाज की मूलधारा में लाने की बात नहीं करनी चाहिए ताकि वे भी राष्ट्र की मूलधारा में योगदान कर सकें? जज ने सरकार की तरफ से दाखिल जवाब में इस बात के जिक्र पर भी अफसोस किया कि उसमें बेघरों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र है बजाय इसके कि उन्हें किसी काम से लगाया जाए। जज ने पूछा कि क्या हम परजीवियों के एक तबके का निर्माण नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इन्हीं चुनावी-रेवडिय़ों की वजह से लोग अब काम करना नहीं चाहते हैं। उन्हें मुफ्त का राशन मिल रहा है जो कि बिना काम किए दिया जा रहा है। उन्होंने अपने निजी अनुभव गिनाते हुए कहा कि उनके किसान परिवार में अब महाराष्ट्र में इन्हीं चुनावी फ्रीबीज की वजह से खेतों में मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सबको घर बैठे बहुत कुछ मुफ्त मिल रहा है। जनहित याचिका की तरफ से नामी वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि दिल्ली सरकार के चलाए जा रहे शेल्टरों की हालत इतनी खराब है कि उस वजह से भी बेघर लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं। इस पर जज ने पूछा कि क्या ऐसे शेल्टर की हालत सडक़ पर सोने से भी ज्यादा खराब है, लोग इन दोनों में से किसे पसंद करेंगे? जस्टिस गवई ने अपना विचार रखा कि लोगों को मुफ्त में चीजें मिलती हैं तो वे अलाल होते जा रहे हैं लेकिन उन्होंने साथ-साथ यह भी माना कि सिर छुपाने का हक लोगों का बुनियादी हक है, और जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे पर तो विचार करना ही है।
चुनावों में किस तरह की लुभावनी घोषणाएं की जाएं, और कैसी न की जाएं इस पर कुछ जनहित याचिकाएं पहले से सुप्रीम कोर्ट में चली आ रही हैं, और पिछले मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड़ की अगुवाई में एक बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी लेकिन यह मामला उनके रिटायर होने तक पूरा नहीं हो पाया था इसलिए इसे अगले मुख्य न्यायाधीश के आने के बाद किसी नई बेंच के सामने पेश करने की बात कहते हुए जस्टिस चन्द्रचूड़ ने इसे रोक दिया था। लेकिन लोकसभा का आम चुनाव निपट जाने की वजह से इसे अधिक प्राथमिकता नहीं मिल पाई, और सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों मामले दस-दस, बीस-बीस बरस से चले आ रहे हैं, और कई मामले व्यापक और तात्कालिक महत्व के रहते हैं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश की निजी पसंद-नापसंद पर भी यह रहता है कि वे किन मामलों को पहले देखें। फिलहाल चुनावों में फ्रीबीज का मामला अभी तक किसी किनारे पहुंचा नहीं है, और जस्टिस गवई ने एक दूसरी जनहित याचिका के दौरान वकीलों से चर्चा में यह मौखिक विचार सामने रखा था कि चुनावी तोहफों के बजाय लोगों को स्थाई रूप से देश के कामकाज की मूलधारा में लाया जाना बेहतर होगा।
हम इसी पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं कि मध्यप्रदेश से शुरू हुई लाड़ली बहना, छत्तीसगढ़ में चाउर वाले बाबा रमन सिंह की भारी कामयाब पीडीएस प्रणाली, तमिलनाडु में शुरू स्कूलों में सुबह का नाश्ता, और एक-एक करके देश के दर्जन भर राज्यों में अब चल निकली उन राज्यों की महतारियों के लिए सीधे नगदी की योजना का कोई अंत नहीं है। केन्द्र सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5-5 किलो अनाज दे रही है, जिन ग्रामीण इलाकों में रोजगार नहीं रहता, वहां पर मनरेगा जैसी रोजगार योजना ने लोगों को भूखों मरने से बचाया है। इसके अलावा गरीब जोड़ों की शादियां, मुफ्त बिजली, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त इलाज जैसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनके मुफ्त शब्द पर कई लोगों को आपत्ति भी होती है कि ये जनता के अपने पैसों पर चल रही हैं, और इन्हें मुफ्त कहना एक गलत शब्दावली है। हम भाषा की बारीकी पर गए बिना यह जरूर सोचते हैं कि वोट पाने के लिए चुनावी तोहफों की शक्ल में राजनीतिक दल जितने वायदे करते हैं, उनके बाद सरकार के बजट में अधिक लचीलापन नहीं बचता है। और जब एक-एक योजना एक-एक राज्य में करोड़ों लोगों को फायदा देने वाली रहती है, तो यह बात तो जाहिर रहती ही है कि इसमें लोगों की बारीक शिनाख्त नहीं हो पाती, और इनमें एक पर्याप्त बड़ा हिस्सा अपात्र लोगों का भी रहता है। अब एक तरफ सरकारें लोगों को रोजगार देने, या किसी उत्पादक और मुनाफे वाले कामकाज में लगाने से कतराती हैं, और उन्हें सीधे फायदा पहुंचाकर उनसे वोट पाकर किसी तरह पांच साल की सरकार बना लेना चाहती हैं। अर्थशास्त्र के हिसाब से इसमें दो खराबियां हैं। एक तो यह जब इतने व्यापक तबके को किसी योजना में हितग्राही बनाया जाता है, तो उसमें अपात्र लोगों की शिनाख्त मुमकिन नहीं हो पाती। दूसरी बात यह रहती है कि बजट का इतना बड़ा हिस्सा गैररोजगारोन्मूलक कामों में चले जाता है कि देश को इन रेवडिय़ों के एवज में आर्थिक उत्पादकता कुछ नहीं मिलती। अधिक से अधिक गरीब तबकों का पेट भर जाता है, उन्हें दारू पीने को हजार-दो हजार रूपए महीने मिल जाते हैं, राजनीतिक दलों को इसके एवज में वोट मिल जाते हैं, लेकिन यह कीमत खासी महंगी पड़ती है। सरकार बनाने के कुछ अधिक गंभीर तरीके होने चाहिए, बजाय महज लुभावनी योजनाओं से वोटरों को फांसने के, और फिर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उन वायदों को पूरा करने में खर्च करने के।
लोकतंत्र में सरकारों को अपनी कमाई अपनी मर्जी से खर्च करने की तकरीबन पूरी छूट है। और अब तो देश में योजना आयोग भी नहीं रह गया है जहां राज्यों को कमाई और खर्च के अपने आंकड़ों को पेश करना होता था। अब सब कुछ अधिक मनमर्जी से अधिक दूर तक चलने वाला सिलसिला हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को आगे बढऩा चाहिए, चुनाव आयोग में तो एक किस्म से अपने हाथ झाड़ लिए हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, और सरकारों को जवाब देना चाहिए कि क्या रेवडिय़ों की बोलियों के बीच मेहनत से कमाने-खाने की चर्चा की कोई गुंजाइश रहनी चाहिए, या फिर देश की जनता को निकम्मा बनाने की कुछ और योजनाओं के बारे में कुछ सोचा जाए? अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ सरकारी मदद और रियायतों की वजह से सामाजिक-मानवीय पैमानों पर एक ठीकठाक जिंदगी जी रही है, तो क्या इसे उस समाज की आर्थिक उत्पादकता भी माना जा सकता है? ये सवाल बड़े अलोकप्रिय, गरीब-विरोधी, और पूंजीवादी लग सकते हैं, लेकिन देश की पूरी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होने के साथ-साथ चुनावी रेवडिय़ों पर आधारित अर्थव्यवस्था भी हो गई है। इस नौबत को सुधारने के रास्ते सुप्रीम कोर्ट में इस बहस के दौरान सामने आ सकते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)