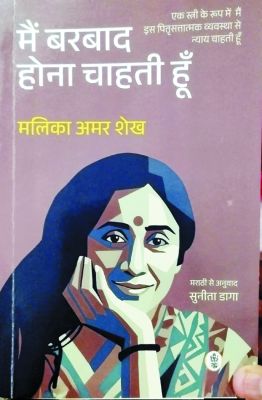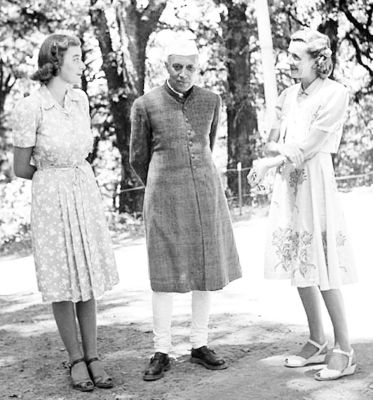विचार / लेख

-प्रमोद भार्गव
संदर्भ: जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की पिछले एक दषक के जारी आंकड़ों के अनुसार बेघर हुए लोग
दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के कारण पिछले एक दषक 2015 से 2024 के दौरान आंतरिक विस्थापन के कारण पर्यावरण शरणार्थियों की संख्या में बढ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। इस कारण कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अनेक बार प्राकृतिक आपदा के तीव्र और व्यापक खतरे उत्पन्न हुए। परिणामस्वरूप 210 देषों में 26.48 करोड़ लोगों को आंतरिक विस्थापन झेलना पड़ा है। जो न केवल एक रिकॉर्ड के रूप में सर्वाधिक है, बल्कि 2.65 करोड़ के दषकीय औसत से कहीं अधिक है। इस मामले में पूर्व और दक्षिण एशिया सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्र रहे। देशों के स्तर पर बीते एक दशक में चीन, फिलीपींस, भारत, बांग्लादेश और अमेरिका में दर्ज विस्थापन के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। चीन में 4.69 और फिलीपींस में 4.61 करोड़ लोगों को अपने ही देष में विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा है। इसी कालखंड में भारत में बाढ़, तूफान और भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते 3.23 करोड़ लोगों को आंतरिक विस्थापन का संकट उठाना पड़ा है। किसी देश के अंदर विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से चीन और फिलीपींस के बाद भारत विष्व में तीसरे स्थान पर हैं। जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (आईडीएमसी) की एक नई रपट में यह दावा किया गया है।
रपट के मुताबिक वैष्विक स्तर पर 90 फीसदी आपदा जनित विस्थापन बाढ़ और तूफान का परिणाम रहा है। सबसे ज्यादा तूफान के कारण 12.09 करोड़ लोगों को विस्थापन की परेषानी उठानी पड़ी है। इसी अवधि में बाढ़ के कारण 11.48 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर समुद्री तूफान से हुए लोगों के विस्थापन में ‘अंफान’ सहित अन्य चक्रवातों की हिस्सेदारी 92 प्रतिशत रही। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीब और निर्बल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्हें बार-बार और लंबे समय तक पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। सामाजिक असमानता और आर्थिक विसंगति के कारण इन लोगों को इन प्राकृतिक आपदाओं का भीशण संकट झेलना पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनियाभर में हर साल औसतन 3 करोड़ लोगों को समुद्र और नदी तटीय बाढ़, सूखा और चक्रवती तूफानों के चलते भविश्य में भी ऐसी आपदाओं से विस्थापन का संकट झेलना होगा। यानी पर्यावरण शरणार्थियों की संख्या भविष्य में और विकराल रूप में पेश आएगी।
जलवायु विषेशज्ञों का मानना है कि इस विराट व भयानक संकट के चलते यूरोप, एशिया और अफ्रीका का एक बड़ा भूभाग इंसानों के लिए रहने लायक ही नहीं रह जाएगा। तब लोगों को अपने मूल निवास स्थलों से जिस पैमाने पर विस्थापन या पलायन करना होगा,वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व होगा। इस व्यापक परिवर्तन के चलते खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी आएगी। अकेले एशिया में कृषि को बहाल करने के लिए हर साल पांच अरब डॉलर का अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। बावजूद इसके दुनिया के करोड़ों लोगों को भूख का अभिशाप झेलना होगा। प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के दुष्परिणामस्वरूप दुनियाभर में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं।
विज्ञान पत्रिका ‘साइंस‘ में प्रकाषित अध्ययन में कहा गया है कि यदि वैष्विक तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो हिंदू कुष हिमालय के हिमखंडो की बर्फ इस सदी के अंत तक 75 प्रतिषत तक पिघल जाएगी। हिंदू कुश पर्वत के ये ग्लेशियर कई नदियों के उद्गम स्थल हैं और ये नदियां 2 अरब लोगों की आजीविका का साधन बनती हैं। यदि दुनिया के देश इस तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर सकें तो हिमालय और काकेशस पर्वत में स्थित हिमनदों की बर्फ 40 से 45 प्रतिशत सुरक्षित रह सकती है। इसके विपरीत यदि इस सदी के अंत तक दुनिया 2.60 डिग्री सेल्सियस गर्म होती है तो वैश्विक स्तर पर ग्लेशियर की बर्फ का केवल एक चौथाई हिस्सा ही बचेगा।
अध्ययन में कहा है कि मानव समुदायों के लिए सबसे अहम ग्लेशियर क्षेत्र जैसे कि यूरोपियन आल्प्स, पश्चिमी अमेरिका और कनाडा की पर्वत श्रृंखलाएं एवं आइसलैंड बुरी तरह से प्रभावित होंगे। दो डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर यह क्षेत्र अपनी समूची बर्फ खो सकते हैं और 2020 के स्तर पर केवल 10-15 प्रतिशत ही बर्फ बची रह पाएगी। स्कैंडिनेविया पर्वत का भविष्य और भी भयावह हो सकता है, क्योंकि इस स्तर के तापमान में वहां के ग्लेशियरों पर बर्फ बचेगी ही नहीं। 2015 के पेरिस समझौते के द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य तक तापमान को सीमित करने से सभी क्षेत्रों में कुछ ग्लेशियर पर बर्फ को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। ये हालात मानव जीवन को अभूतपूर्व रूप में प्रभावित कर खतरे में डाल देंगे। इस कारण अकेले एशिया में 2 अरब लोगों को आजीविका का संकट झेलना पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि 2050 तक दुनिया भर में 25 करोड़ लोगों को अपने मूल निवास स्थलों से पलायन को मजबूर होना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन की मार मालदीव और प्रषांत महासगर क्षेत्र के कई द्वीपों के वजूद को पूरी तरह लील होगी। इन्हीं आशंकाओं के चलते मालदीव की सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए चर्चा के लिए समुद्र की गहराई में बैठकर औद्योगिक देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा था ताकि ये देष कार्बन उत्सर्जन में जरूरी कटौती कर दुनिया को बचाने के लिए आगे आएं।
इस बदलाव का बांग्लादेश को बड़ा संकट झेलना होगा, क्योंकि यहां आबादी का धनत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए बांग्लादेष के लोग बड़ी संख्या में इस परिवर्तन की चपेट में आएंगे। यहां तबाही का तांडव इतना भयानक होगा कि सामना करना नामुमकिन होगा। भारत की सीमा से लगा बांग्लादेश तीन नदियों के डेल्टा में आबाद है। इसके दुर्भाग्य की वजह भी यही है। इस देश के ज्यादातर भूखण्ड समुद्र तल से बमुश्किल 20 फीट की ऊंचाई पर आबाद हैं। इसलिए धरती के बढ़ते तापमान के कारण जलस्तर ऊपर उठेगा तो सबसे ज्यादा जलमग्न भूमि बांग्लादेश की होगी। जलस्तर बढऩे से कृषि का रकबा घटेगा। नतीजतन 2050 तक बांग्लादेश की धान की पैदावार में 10 प्रतिशत और गेहूं की पैदावार में 30 प्रतिशत तक की कमी आएगी। इक्कीसवीं सदी के अंत तक बांग्लादेश का एक चौथाई हिस्सा पानी में डूब जाएगा। वैसे तो मोजांबिक से तवालु और मिश्र से वियतनाम के बीच कई देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन होगा,लेकिन सबसे ज्यादा पर्यावरण शरणार्थी बांग्लादेश के होंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस देश से दो से तीन करोड़ लोगों को पलायन कर मजबूर होना पड़ेगा।
बांग्लादेष पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने वाले जेम्स पेंडर का मानना है कि 2080 तक बांग्लादेश के तटीय इलाकों में रहने वाले पांच से दस करोड़ लोगों को अपना मूल क्षेत्र छोडऩा पड़ सकता है। देश के तटीय इलाकों से ढाका आने वाले लोगों की तादद लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका की प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन ने बांग्लादेश के पर्यावरण षरणार्थीयों पर एक विषेश रपट में कहा है कि बूढ़ी गंगा किनारे बसे ढाका शहर में हर साल पांच लाख लोग आते हैं। इनमें से ज्यादातर तटीय और ग्रामीण इलाकों से होते हैं। यह संख्या वाशिंगटन डीसी के बराबर है।
इस व्यापक बदलाव का असर कृषि पर दिखाई देगा। खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी आएगी। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति षोध संस्थान के मुताबिक अगर ऐसे ही हालात रहे तो एषिया में एक करोड़ दस लाख, अफ्रीका में एक करोड़ और बाकी दुनिया में चालीस लाख बच्चों को भूखा रहना होगा। संयुक्त राष्ट्र के एक आंकलन के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी 9 अरब 20 करोड़ हो जाएगी। उभरते जलवायु संकट और बढ़ते पर्यावरण शरणार्थियों के चलते इतने शरणार्थियों को अनाज उत्पादन के लिए कृषि लायक भूमि उपलब्ध कराना असंभव होगा। अतएव पर्यावरण शरणार्थियों के इस संकट से निपटना तब और मुश्किल होगा, जब अमेरिका जैसे पूंजीपति देष राहत कोष घटाकर इन शरणार्थियों को भगवान भरोसे छोड़ देने का काम कर रहे हैं।
(लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं।)