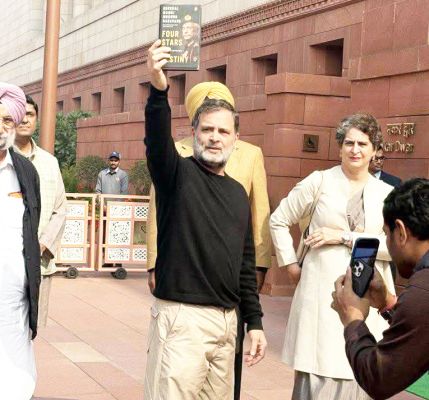विचार / लेख
- एकलव्य
यह आम लोगों का पर्व है, इस आयोजन की आत्मा आम लोग हैं। वो आम लोग जिन्हें हम 'अमौसा के मेला' कविता में देखते हैं। हजारों हजार लोग बीस बीस किमी पैदल चल रहे हैं ताकि स्नान कर पाएं, हिलने की जगह नहीं है तभी बीच में हूटर बजाती गाडिय़ां आ जाती हैं और उन्हें जगह देना है।
ये तथाकथित वीआईपी लोग यदि पुण्य अर्जित करने की लालसा से आ रहे हैं तो यकीनन आम लोगों के कष्ट की कीमत पर तो उन्हें उनका पुण्य' नहीं मिलने वाला।
वृद्धि- विकास को लेकर मेरी अपनी समझ है जिसे सुनकर बाज दफ़ा सतही रूप से मेरे विचार प्रगति विरोधी भी लग सकते हैं पर मेरा मानना है कि विकास के नाम पर किसी भी चीज की मूल आत्मा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
प्रत्येक स्थान का अपना महत्व होता है उसकी स्थानीय विशेषताएं होती हैं जो उसे बाकियों से अलग करती हैं। बनारस में तोड़ फोड़ मचाकर आप उसे लखनऊ नहीं बना सकते और यदि बनाना चाहें तो उसकी कीमत होगी बनारस की मृत्यु।
हमेशा से यह मेला दो वर्ग से बनता आया है- साधु संत नागा सन्यासी और आम लोग, जो दूर दूर से स्नान करने आते हैं या वो जो महीने भर का कल्पवास किये होते हैं। इन सबके बीच बाजार की उतनी ही जगह बचती है जितनी कि उसकी आवश्यकता होती है।
लगातार मेला घूमते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ कि अबकी बार आम लोग हाशिये पर हैं जो इस मेला और इस जुटान के श्रृंगार हैं वही लोग कहीं पीछे छूट रहे हैं। बाजार जबरिया घुसा हुआ है। तमाम दावों के बावजूद आम जन के लिए कोई विशेष सुविधा नजऱ नहीं आ रही सिवाय कि उन्हें पैदल चलने दिया जा रहा है।
सबसे पहले तो इस वीआईपी मूवमेंट को तुरन्त रोकना चाहिए। यदि जज साहब और उनकी मेहरारू को श्रद्धा है तो वो भी पैदल चलें और दूसरी बात कि मेला क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यालयों के अलावे केवल साधुओं और कल्पवासियों के लिए ही जमीन आवंटित होनी चाहिए। एक-एक लाख रुपये की टेंट सिटी ऐसी जगहों पर न केवल अश्लील लगती हैं बल्कि वो संसाधनों का भी अत्यधिक उपभोग करते हैं।
सरकार और मेला प्रशासन को यह याद तो रहना ही चाहिए कि सर पर गठरी लादे चना चबेना खाते लोग ही कुम्भ को दिव्यता और भव्यता प्रदान करते हैं न कि ये सस्ती चाइनीज झालरें।