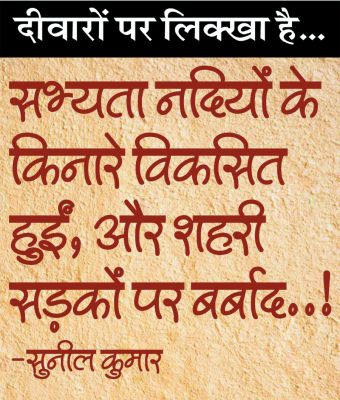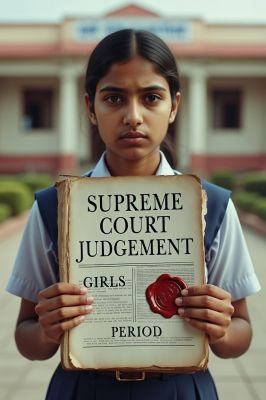ताजा खबर

झारखंड में आदिवासी महिलाएं महुआ से लड्डू बनाकर आजीविका बढ़ा रही हैं। फोटो: शुभम
-वर्षा सिंह
मखाना बोर्ड की तर्ज पर महुआ जैसे वन उत्पादों और दूसरे स्थानीय संसाधनों को संस्थागत समर्थन देने के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड बनाने की मांग उठ रही है।
मांग है कि ऐसा बोर्ड शोध, नवाचार, बीज संरक्षण, बुनियादी ढांचा, क्षमता निर्माण और मूल्य संवर्धन पर साथ-साथ काम करे।
जानकार मानते हैं कि इससे स्थानीय संसाधनों पर आधारित एक टिकाऊ खाद्य व्यवस्था बनाने में मदद मिल सकती है।
“हम लोग महुआ के वृक्ष से फूल गिरने के समय का अनुमान लगाकर चुनने जाते हैं। कोई पेड़ रात में ही अपने फूल गिरा देता है और सुबह के समय पेड़ के नीचे महुआ फैला हुआ मिलता है। कुछ पेड़ों में एक-आध फूल टिप-टप करके गिरते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए। वे सूर्य की रोशनी और उसके ताप से फूल गिराते हैं”।
रोनी उरांव झारखंड के रांची जिले के अंगड़ा ब्लॉक के रामपुर टोली गांव में रहती हैं। वह बताती हैं कि फरवरी के आखिरी हफ्ते से मार्च-अप्रैल तक उनका पूरा गांव महुआ फूल चुनने में दिन-रात लगा रहता है।
रोनी आगे कहती हैं, “जब रात में महुआ गिरता है तो हमें सहूलियत होती है। हम पहले फूल चुनते हैं, फिर घर का काम करते हैं। लेकिन जहां देर से फूल गिरता है, हमें नजर रखनी पड़ती है कि फूलों को पशु न खा जाएं। क्योंकि महुआ हमारी आय का एक स्रोत है।”
“जंगल में कुछ महुआ पेड़ों में कली बननी शुरू हो गई है। लेकिन हमारे पेड़ थोड़ी देर से फूल देते हैं”। रोनी और गांव की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया जब महुआ को इकट्ठा करने के लिए पेड़ों के चारों ओर जाल लगाने की तकनीक का पता चला।
झारखंड के आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर कार्य कर रही वाइल्ड हार्वेस्ट संस्था ने फूड-ग्रेड महुआ इकट्ठा करने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया। इसके संस्थापक ऋषभ लोहिया बताते हैं, “महुआ के फूल बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हैं। यह एक तरह का सुपरफूड है। लेकिन इसे सही तरह से इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। अभी महुआ चुनने के लिए लोग पेड़ों के नीचे गिरी सूखी पत्तियों में आग लगा देते हैं। इससे जंगल जलने का भी खतरा होता है। महुआ फूल ज़मीन पर गिरते हैं तो उसमें राख लग जाती है। वे इसे ज़मीन पर, आंगन में, या सड़क पर सुखाते हैं। कई बार उसमें फंगस भी लग जाता है”।
“हमने उन्हें पेड़ के चारों ओर जाल लगाने के बारे में बताया। इससे एक-दो घंटे में ही जाल पर सारे फूल इकट्ठा हो जाते हैं। उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर होते हैं और लोगों को कम मेहनत में अच्छी कीमत भी मिल जाती है।”
शराब के लिए बदनाम महुआ को शहरी थाली में एक पौष्टिक आहार के तौर पर लाने का सपना देखने वाले ऋषभ ने वर्ष 2024 में 40 ग्रामीण परिवार और उनके 100 पेड़ों के साथ काम करना शुरू किया। वर्ष 2025 में 200 पेड़ों से जाल लगाकर महुआ चुनने के काम का विस्तार हुआ।
वह कहते हैं, “ये बेहद महत्वपूर्ण वनोपज है। हम इसका मूल्य-संवर्धन कर इसके लड्डू और अचार जैसे उत्पाद बना रहे हैं। इससे ग्रामीणों की आय बेहतर हो रही है। लेकिन अभी ये काम असंगठित तौर पर हो रहा है। इसके मानक तय नहीं हैं। लोगों की बाजार तक पहुंच सीमित है। महुआ जैसे वनोपज पर संगठित और व्यवस्थित तौर पर काम किया जाए तो इसके कई फायदे हैं। इन पर शोध और बेहतर तकनीक के साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार हो सकें”।
ऋषभ इसके लिए बिहार के मखाना बोर्ड की तर्ज़ पर वनोपज आधारित बोर्ड की मांग करते हैं। “भारत सरकार ने पिछले बजट में जिस तरह मखाना बोर्ड बनाया, वैसे ही महुआ जैसे महत्वपूर्ण लघु वनोपज आधारित बोर्ड का बनना बहुत जरूरी है। देश के करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी समुदाय वनोपज से सीधे तौर पर जुड़े हैं। ये उनकी खाद्य सुरक्षा, आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है”।
रोनी उरांव पहले महुआ फूलों को स्थानीय बाज़ार में बेचती थीं,, “मैं किसी साल एक क्विंटल तो कभी 50-60 किलो ही महुआ चुन पाती थी। तकरीबन पांच-सात हजार रुपए तक कमा लेती थी। लेकिन अब हम इसके लड्डू बना रहे हैं तो कमाई बढ़ गई है। हम 20 रुपए का एक लड्डू बेचते हैं। गांव की पांच अन्य महिलाओं के साथ मिलकर हम एक महीने में 300-350 लड्डू बना लेते हैं”।
मखाना-महुआ जैसे स्थानीय संसाधन
रोनी की तरह ही देश में, लगभग 300 मिलियन आदिवासी और अन्य स्थानीय लोग अपने निर्वाह और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। भारत में 3,000 पौधों की प्रजातियों की अनुमानित विविधता है। इन्हें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (एमएफपी) के रूप में जाना जाता है।
ट्राइफेड (भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ) के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत, लघु वन उपज में बांस, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू/केंदू के पत्ते, औषधीय पौधे, जड़ी-बूटियाँ, जड़ें और कंद सहित सभी गैर-लकड़ी वन उत्पाद शामिल हैं।
देश में तकरीबन 87 लघु वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। महुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति किलो है। हालांकि बाज़ार में ये 40-45 रुपए प्रति किलो तक मिलता है।
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, स्थानीय लोगों को “लघु वन उपज के पारंपरिक स्वामित्व, उपयोग और निपटान का अधिकार” देता है, चाहे उन्हें गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्र किया गया हो। यह अधिनियम सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर जी रहे समुदाय की सुरक्षा, उनके जीवन और आजीविका के अधिकार को जंगलों के पर्यावरणीय संरक्षण के साथ संतुलित करने के उद्देश्य से बनाया गया।
ट्राइफेड अपनी वेबसाइट पर लिखता है, “फिर भी जंगलों पर निर्भर आदिवासी और अन्य स्थानीय समुदाय अक्सर वंचित रहते हैं और इस अधिनियम से मिलने वाले अपेक्षित लाभ का पूरा फायदा नहीं उठा पाते”।
झारखंड में ट्राइफेड के क्षेत्रीय प्रबंधक शैलेंद्र कुमार राजू कहते हैं, “वंदन विकास केंद्रों, वैल्यू एडिशन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिये ट्राइफेड आदिवासी समुदाय के साथ काम करता है। इसके अलावा अपने आउटलेट्स, मेलों और विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देता है और उन्हें बाज़ार उपलब्ध कराता है।”
“पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह मिलेट्स के लिए कार्य किया गया, हम महुआ समेत अन्य वनोपज को भी इसी तरह बढ़ावा दें तो स्थानीय समुदाय को इनका लाभ मिल सकता है”। इसके लिए वह एक ठोस नीति और समग्र व्यवस्था की जरूरत पर ज़ोर देते हैं। “ऐसा तंत्र जो महुआ समेत सभी उत्पादों पर लागू हो। यह व्यवस्था मूल्य संवर्धन, तकनीक और बाजार तक पहुंच की पूरी श्रृंखला को कवर करे”।
स्थानीय संसाधनों पर आधारित राष्ट्रीय बोर्ड की मांग
खेती की मुख्य धारा में शामिल फसलों से अलग, मखाना जैसी जल-आधारित स्थानीय उपज और महुआ जैसी वनोपज आदिवासी और स्थानीय समुदायों की पारंपरिक खाद्य प्रणालियों का हिस्सा रही हैं।
मखाना क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की बनाया। इसका उद्देश्य मखाना मूल्य श्रृंखला में प्रशिक्षण, खेती और प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी विकास, ग्रेडिंग, ड्राइंग, पॉपिंग और पैकेजिंग के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, खेती के नए तरीके, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, मार्केट लिंक और निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके लिए 476 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। दिसंबर 2025 में बोर्ड की पहली बैठक में इस केंद्रीय योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
इनवायरमेंट एक्शन ग्रुप कल्पवृक्ष से जुड़ी और संगठन में संरक्षण और आजीविका कार्यक्रमों का समन्वय कर रही नीमा पाठक ब्रूम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में महुआ, बांस, तेंदुपत्ता, शहद, जंगली सीताफल जैसे लघु वनोपज का स्वतंत्र तौर पर प्रबंधन कर रही ग्रामसभाओं का उदाहरण देती हैं।
“लोगों ने सामूहिक रूप से सहकारी समितियां और ग्रामसभाओं का महासंघ बनाकर विपणन, संग्रहण और नियामक प्रणाली बनाने की पहल की है। सामूहिक तौर पर काम कर रहे इन मॉडल को देखें और इन्हें समर्थन देने का एक ढांचा तैयार करें तो यह बहुत प्रभावी होगा। इससे अनौपचारिक रूप से बिखरी हुई व्यवस्था में काम कर रहे लोगों को एक बोर्ड के तहत लाया जा सकता है।”
हिमालयी क्षेत्रों के संरक्षण और ग्रामीण विकास पर काम करने वाले पर्यावरणविद् अनिल जोशी भी क्षेत्रीय संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक बोर्ड की मांग का समर्थन करते हैं। “इससे क्षेत्रीय संसाधनों की पहचान मजबूत होगी। उससे जुड़े पूरे इको-सिस्टम की भी ब्रांडिंग होगी।” वह उत्तराखंड के माल्टा और बुरांस का उदाहरण देते हैं।
वन और स्थानीय उपज पर आधारित खानपान जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। आदिवासी खाद्य और आर्थिक नीतियों की विशेषज्ञ और नासिक स्थित सिविल सोसाइटी संगठन ‘प्रगति अभियान’ से जुड़ी अश्विनी कुलकर्णी कहती हैं, “देश में गिनी-चुनी 50 से भी कम फसलों पर शोध और विकास कार्य किया जा रहा है। खाद्य विविधता जितनी अधिक होगी, इनका जीन पूल जितना बड़ा होगा, जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने में उतनी ही मदद मिलेगी।”
वे वनोपज पर शोध और विकास, बीज संरक्षण और जीन पूल को समझने जैसे कामों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाने का समर्थन करती हैं। ताकि जलवायु परिवर्तन के चलते भयंकर सूखे, बेमौसमी या भारी बारिश की परिस्थितियों में स्थानीय जलवायु पर निर्भर खाद्य विविधता हमारे मजबूत विकल्प के तौर पर मौजूद हो।
“भारी उपेक्षा के बावजूद महुआ, रागी, कौनी जैसी उपज हमारे बीच मौजूद हैं। इनका संरक्षण करने वाले स्थानीय किसानों को नीतिगत मुद्दों से जुड़ी बातचीत में शामिल कर ज़मीन से उभरा हुआ एक मॉडल तैयार करना होगा। ताकि स्थानीय उत्पाद, स्थानीय खरीद और स्थानीय वितरण को बढ़ावा मिले। यही भविष्य की राह है”।
जलवायु और भोजन से जुड़े मुद्दों पर संवाद का एक मंच मुंबई क्लाइमेट वीक है। महाराष्ट्र सरकार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका और न्यूयॉर्क स्थित क्लाइमेट ग्रुप के सहयोग से हो रहे इस आयोजन के संस्थापक शिशिर जोशी कहते हैं कि जलवायु से जुड़ी बातचीत को आम नागरिकों तक ले जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके असर को सीधे वही झेल रहे हैं या भविष्य में झेल सकते हैं।
उनके मुताबिक, “पर्यावरणीय नुकसान को पूरी तरह पलटना संभव नहीं है, लेकिन नागरिक-केन्द्रित और नीति स्तर पर गंभीर हस्तक्षेप समय की जरूरत है। खाद्य प्रणाली ऐसा ही एक क्षेत्र है, जिसमें नागरिक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। समुदाय स्तर पर खानपान की आदतों में बदलाव या टिकाऊ खेती के लिए छोटे नीतिगत प्रोत्साहन भी किसानों के लिए बड़ा सहारा बन सकते हैं। ऐसी नीतियों और नागरिक भागीदारी से जुड़े जलवायु-अनुकूल तरीकों को मुंबई क्लाइमेट वीक में एक साझा मंच मिलेगा।”
स्थानीय उपज अब भी आदिवासी-ग्रामीण समुदाय की थाली का हिस्सा हैं।
रोनी उरांव महुआ से बनने वाले स्थानीय व्यंजन जैसे मिठाइयां, पूड़ियां, ठेकुआ, जलेबी, चटनी, अरसे का स्वाद याद करती हैं, “लोग तो महुआ का शराब ही जानते हैं लेकिन हमारी दादी इससे कई पकवान बनाती थीं। इसके तेल का इस्तेमाल होता था। इसको सुखाकर इसका किशमिश बनाया जाता था। हम इसमें मेवे मिलाकर लड्डू बना रहे हैं। जब किसी मेले में हम अपना स्टॉल लगाते हैं तो हमारा पूरा स्टॉक बिक जाता है।” (downtoearth.org.in)