ताजा खबर

एक वक्त था जब आज के मीडिया के तहत सिर्फ अखबार ही आया करते थे। उन दिनों अखबारों का वजन रद्दी से तय नहीं होता था, बल्कि उसकी प्रसार संख्या से तय होता था, और उसकी साख से भी। कुछ अखबार कम छपते-बिकते थे, लेकिन उनकी बात का वजन अधिक रहता था। बाद में टीवी चैनल आए, और उनकी दर्शक संख्या गिनने के सच्चे-झूठे जैसे भी हो, कुछ पैमाने बनाए गए। इस दौर में भी यह कुछ हद तक कायम रहा कि सबसे अधिक देखे जाने वाले चैनलों की साख भी सबसे अधिक हो, यह जरूरी नहीं था। दर्शक संख्या की लिस्ट में नीचे आने वाले कुछ चैनलों का नाम भी साख की लिस्ट में ऊपर रहता था, ठीक वैसे ही जैसे कुछ अखबार बिकते-दिखते तो कम थे, लेकिन उनकी बात को अधिक गंभीरता से लिया जाता था।
अखबार के बिकने को उसके अलग-अलग पन्नों से नहीं तौला जा सकता था। पूरे का पूरा अखबार एक ही रहता था, उसकी सामग्री किसी वेबसाईट पर भी नहीं रहती थी जिससे कि यह देखा जा सके कि उसके अलग-अलग पन्नों पर छपी सामग्री में से किसे कम देखा जा रहा है, और किसे अधिक। लेकिन टीवी के आने के साथ ही यह भी हिसाब-किताब लगने लगा कि किस चैनल के कितने बजे के कार्यक्रम में दर्शक संख्या कितनी है, और दर्शक कितनी देर वहां पर रूकते हैं। फिर धीरे-धीरे अखबारों और टीवी चैनलों की वेबसाइटें बननी लगीं, और बहुत सी समाचार वेबसाइटें खुद की भी थीं। इनमें किस लेख या समाचार, किस वीडियो या ऑडियो को कितने लोगों ने देखा, यह अलग-अलग दिखने लगा, और इसी से यह तय होने लगा कि वेबसाइट पर, या उसके पीछे के अखबार में क्या छापा जाए, और क्या नहीं।
अब जब सोशल मीडिया पर फॉलोअर, लाईक्स, रीपोस्ट, और कमेंट जैसे कई पैमाने लोकप्रियता को तय करने लगे, तो उत्कृष्टता सौतेले बच्चे सरीखी हो गई। उसी घर में उसे ऐसे कोने पर रखा गया कि वह मेहमानों को न दिखे। आज पल-पल यह तय होता है कि किसी रिपोर्टर, स्तंभकार, या संपादक के लिखे हुए पर कितने दर्शक, श्रोता, या पाठक जुटे। यूट्यूब पर यह दिखने लगा कि किस उम्र के औरत या मर्द, देश और दुनिया के किन इलाकों से कितनी देर देख रहे हैं, उनकी उम्र क्या है, और कितने फीसदी लोग कितने सेकेंड के बाद देखना बंद कर देते हैं।
किसी देश में लोकतांत्रिक चुनावों में चुनी गईं सरकारें जिस तरह उत्कृष्टता की कोई गारंटी नहीं होतीं, ठीक उसी तरह आज के मीडिया पर किसी सामग्री को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से उसकी उत्कृष्टता का कुछ भी लेना-देना नहीं रहता, इससे जरूर लेना-देना रहता है कि उसे कितने लोग देखने वाले हैं। अब किसी भी तरह के मीडिया संस्थान में महत्व का यही एक पैमाना रह गया है कि उसे कितने लोग देखेंगे, सुनेंगे, या पढ़ेंगे। नतीजा यह हुआ है कि आज के मीडिया में काम करने वाले लोग, चाहे वे वहां के कर्मचारी हों, या बाहर बैठे हुए लेखक हों, उनके ऊपर विश्लेषकों का लगातार यह दबाव रहता है कि उन्हें किस विषय पर लिखना है, क्या लिखना है, क्या बोलना है, और कितनी देर यह काम करना है।
हमारा अपना तजुर्बा यह है कि हम अपने अखबार के यूट्यूब चैनल पर अगर रूस और यूक्रेन के बारे में कुछ कहते हैं, या गाजा पर इजराइली ज्यादतियों के बारे में कुछ कहते हैं, तो उसे बड़ी सीमित संख्या में लोग देखते हैं। दूसरी तरफ हम किसी बहुत ही सतही राजनीतिक विवाद के बारे में कोई गंभीर टिप्पणी करते हैं, तो उसके सतही पहलू की वजह से उसे देखने वालों की कतार लग जाती है। अब अगर हमारी अर्थव्यवस्था यूट्यूब से मिलने वाली कमाई की मोहताज रहती, तो दुनिया के जरूरी मुद्दों पर कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता, और ओछी बातों को बोलने के बाद किसी और बात पर बोलने को समय ही नहीं रहता। गनीमत यही है कि हम अभी तक इस अंधी दौड़ में शामिल हुए बिना काम कर रहे हैं। अखबार की वेबसाइट पर भी अगर हमने अलग-अलग सामग्री को देखने वाले लोगों की गिनती देखना शुरू किया होता, तो कोई गंभीर और ईमानदार बात लिखना मुश्किल हो गया रहता।
डिजिटल टेक्नॉलॉजी और उसकी वजह से मिलने वाले दर्शक-पाठक की संख्या के आंकड़े, लोगों के किसी सामग्री पर कितनी देर रूकने का हिसाब-किताब यह सब आज जिंदा रहने की मजबूरी के लिए तो जरूरी है, लेकिन यह उत्कृष्टता की कीमत पर ही हो पाता है। एक वक्त अखबार सबसे महत्वपूर्ण जानकारी समाचार के शीर्षक में दे देता था, अब डिजिटल मीडिया में इस जानकारी को छुपाकर एक सनसनीखेज तरीके से आधी-अधूरी जानकारी देने का चलन है, जो कि कई बार सोच-समझकर झूठी, या गलतफहमी पैदा करने वाली बनाई जाती है। इस तरह का एक बड़ा फर्क कुछ तो टेक्नॉलॉजी की वजह से आया है, और कुछ कारोबारी दबाव ने उत्कृष्टता का गला घोंट दिया है।
एक वक्त था जब कहा जाता था कि बीबीसी में अपने संवाददाताओं या दूसरे विश्लेषकों को श्रोताओं या दर्शकों की तरफ से आने वाली प्रतिक्रियाओं से अलग रखा जाता है ताकि वे प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न हों। आज हालत यह है कि कोई भी सामग्री पोस्ट होते ही हर कुछ मिनटों में देखा जाता है कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, कितने लागे पढ़ रहे हैं, प्रतिक्रिया कैसी आ रही है, और टिप्पणियों में क्या लिखा जा रहा है। टेक्नॉलॉजी ने टाइपिंग आसान कर दी, फोटो बेहतर कर दी, वक्त बचा दिया, लेकिन उत्कृष्टता की कुर्बानी ले ली!



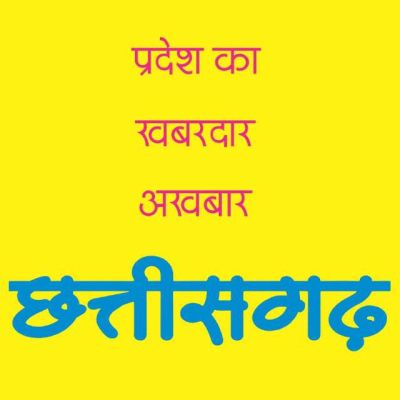

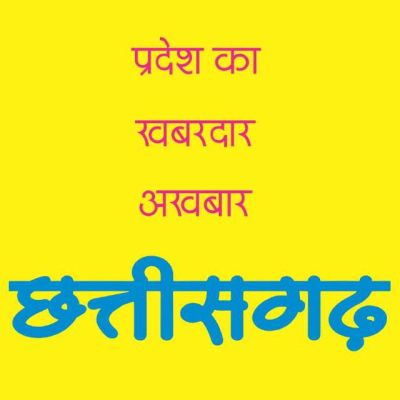
.jpg)
.jpg)



.jpg)







