संपादकीय

छत्तीसगढ़ में इन दिनों सब्जी उगाने वाले किसानों की एक मुसीबत आई हुई है कि टमाटर की फसल खेतों से तोडऩे में जो पैसा लगता है और बाजार तक पहुंचाने में उतना खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। टमाटर इतने सस्ते हो गए हैं कि उनके खरीदार नहीं रह गए, और किसान उन्हें तोडक़र बाजार लाकर बेच नहीं पा रहे। यह नौबत हर बरस कुछ महीनों के लिए सुनाई देती है जब छत्तीसगढ़ के कई इलाक़े परंपरागत रूप से टमाटर की फसल सडऩे के लिए खेतों में छोड़ देते हैं, कई जगह विरोध करने के लिए और अपना तेवर दिखाने के लिए उन्हें सडक़ों पर फेंक देते हैं। हमारी पूरी जिंदगी यह देखते हुए गुजर गई कि फल-सब्जियों के लिए, प्रदेश की दूसरी वनोपज के लिए, ऐसी फूड इंडस्ट्री लगाई जाए जो कि लोगों को रोजगार भी दे सके और छत्तीसगढ़ में होने वाली, खेतों या जंगलों की फसल का बेहतर इस्तेमाल भी कर सके अभी जैसे बस्तर इमली के लिए जाना जाता है। इस प्रदेश के बहुत से इलाकों में महुआ बहुत अधिक होता है लेकिन इन सबका इस्तेमाल यहां से बाहर जाकर होता है। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के कुछ स्वसहायता समूह कुछ छोटे-मोटे सामान बनाते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग का इंतज़ाम ठीक से नहीं होता और उनके ब्रांड की साख नहीं बन पाई है इसलिए भी उनके सामान को ग्राहक नहीं मिल पाते। अभी आईएस प्रदेश को अपनी सीमाएं मालूम हैं कि खेत क्या उगा सकते हैं और वनोपज से क्या-क्या मिल सकता है। लेकिन इन सीमाओं का अपार विस्तार हो सकता है, अगर प्रदेश में जगह-जगह अलग-अलग इलाक़ों में ऐसी फूड इंडस्ट्री लगे जो कि इमली के तरह-तरह के सामान बना सके मशरूम के सामान बना सके जो टमाटर के कैचअप बना सके या टमाटर प्यूरी बनाकर टमाटर केचप और सॉस बनाने वाले करखानों को बेच सके। महुआ में कई तरह का वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। यह भी कुछ साल पहले पता लगा कि छत्तीसगढ़ का महुआ दूसरे कुछ देशों में जाकर वहाँ पर उससे शराब बनाई जा रही है जो कि महंगे दामों पर बिकती है। अभी सवाल यह भी उठता है कि महुआ के पेड़ के नीचे एक जाली लगा दी जाती है जिससे कि महुआ मिट्टी और कंकड़ से टकराकर खराब नहीं होता। तो इसमें कौन सी ऐसी हाईटेक की बात है या कौन सा बड़ा पूंजी निवेश इसमें लगता है कि यह काम नहीं किया जा सकता सरकार को यह बात सोचना चाहिए की प्रदेश की उपज जो है उसमें क्या-क्या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है और ऐसा भी नहीं है कि इनसे जो सामान बनाया जा सकता है उनकी स्थानीय खपत नहीं है आज भी प्रदेश के बाहर से इमली की चटनी, टमाटर का सॉस कई तरह की चीजें मशरूम का पाउडर कई तरह की चीजें प्रदेश के बाहर से यहां आती ही है और इनकी यहां उपज भी बढऩे लगेगी अगर छत्तीसगढ़ में इन चीजों की प्रोसेसिंग इकाईयां लगने लगेंगी और हो सकता है कि यह प्रोसेसिंग इकाइयां अपने खुद के ब्रांड विकसित न कर सके, लेकिन देश के जो स्थापित ब्रांड हैं वे भी कच्चा माल अलग-अलग प्रदेशों से इसी तरह खरीदते हैं।
इन दिनों ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मिलेट्स का चलन बहुत बढ़ा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है की यह आम अनाज के मुक़ाबले अधिक सेहतमंद है। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स की ढेरों संभावनाएं हैं, यहां पर कांकेर जैसी कुछ जगहों पर मिलेट्स की प्रोसेसिंग यूनिट लगी हैं। इसका स्थानीय बाजार है, ऑनलाइन बाजार भी बहुत विकसित हो चुका है। अब यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह मिलेट्स की फसल को, उसकी प्रोसेसिंग को पैकिंग और मार्केटिंग को कामयाब कैसे करें। इससे असंगठित कृषक वर्ग जो है उसका रोजगार बढ़ेगा उसकी कमाई बढ़ेगी, वरना आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में पूरी की पूरी कृषि, सिर्फ धान की फसल पर टिक गई है क्योंकि सरकार बहुत महंगा दाम देकर उस धान को खरीद लेती है। अभी इसके साथ-साथ एक एक दो और बातों पर चर्चा जरूरी है। छत्तीसगढ़ से कोसे के कपड़ों का पूरी दुनिया में बाजार बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो यह विख्यात है ही, यहां इसका घरेलू बाजार भी बहुत है, लेकिन महानगरों में जाकर भी यहाँ का कोसा बिकता है और दुनिया के बाकी देशों में भी इसके दाम बहुत अच्छे मिलते हैं। यह पूरा का पूरा काम बिना किसी हाईटेक के, बिना अधिक बिजली या रसायन के इस्तेमाल के, कोसे के, रेशम के, ककून पेड़ों पर कीड़ों को पालकर तैयार किए जाते हैं। रेशम के कीड़ों से और घरों में महिला, बच्चे, बूढ़े सब लोग मिलकर इन ककून से कोसा बनाने का काम करते हैं। बुनकर गांव गांव में हैं। प्रदेश के कुछ इलाक़े इसके लिए विख्यात हैं और परंपरागत, पारिवारिक बुनकरों की बहुत बस्तियाँ भी हैं। छत्तीसगढ़ के बने हुए कोसा टसर का बाजार बहुत बड़ा है पहनाने के कपड़ों के अलावा जो बहुत रईस तबका जिस तरह से सोफे के कपड़े, परदे के कपड़े, सिल्क, टसर, कोसे के लेने लगे हैं, उसका भी बाजार बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़ को एक टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट की तरह हैंडलूम के कपड़ों को बनाने वाले राज्य की तरह विकसित करने की अपार संभावना है यहां लोगों के पास परंपरागत रूप से यह होना रहे यहां का बाजार बाहर बना हुआ है यहां का ब्रांड भी बाहर छत्तीसगढ़ का कोसा चला हुआ है अभी यह सरकार पर निर्भर करता है और इन सबसे चाहे जो बात से हमने शुरू की है, वनोपज हो या सब्जियों की प्रोसेसिंग हो, वाहन से लेकर सिल्क और कोसे के कपड़ों तक, इन सबसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मदद मिलेगी और इन दिनों दुनिया भर में लगातार यह चलन बढ़ते चल रहा है कि किस तरह से रसायन फ्री कपड़ों का उत्पादन हो, किस तरह से लोग अभी ऑर्गेनिक सब्जिय़ाँ या ऑर्गेनिक फल खाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में धान से परे भी, सरकारी मदद से अनुदान से परे भी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बहुत जरूरत है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)







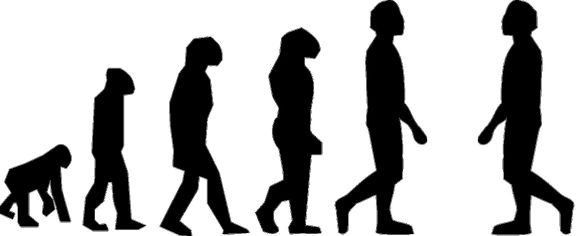




.jpg)

.jpg)


