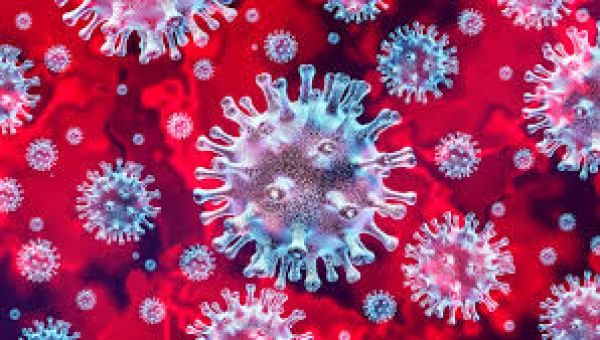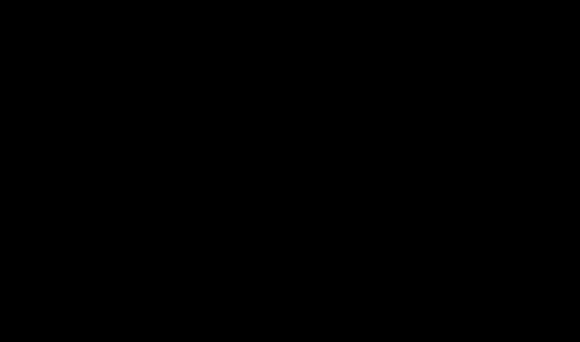बेंगलुरु, 7 अप्रैल कर्नाटक में हर राजनीतिक दल का अलग-अलग क्षेत्र में खासा प्रभाव है लेकिन हर हिस्से की "सूक्ष्म स्थिति" को समझना महत्वपूर्ण है। ऐसे में, प्रदेश का कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र एक अहम क्षेत्र है जहां से 50 विधायक चुने जाते हैं।
इस क्षेत्र को पहले बंबई (मुंबई) कर्नाटक क्षेत्र कहा जाता था। इस क्षेत्र में सात जिले आते हैं जिनमें बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, हावेरी, गडग, बागलकोट और उत्तर कन्नड़ शामिल हैं। इस क्षेत्र में, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है और माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में जनता दल (सेक्युलर) कमजोर स्थिति में है।
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं।
राज्य सरकार ने 2021 में इस क्षेत्र का नाम बदल दिया था। आजादी से पहले यह क्षेत्र तत्कालीन बंबई ‘प्रेसीडेंसी’ के तहत था और सरकार ने इसका नाम मुंबई-कर्नाटक से बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया।
कित्तूर नाम बेलगावी जिले के एक ऐतिहासिक तालुक के नाम पर रखा गया है जहां एक समय रानी चेन्नम्मा (1778-1829) का शासन था और उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से पहले अंग्रेजों से मुकाबला किया था।
यह क्षेत्र मुख्य रूप से एक लिंगायत बहुल क्षेत्र है और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित कई वरिष्ठ नेता इसी क्षेत्र से आते हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की कुल 50 सीट में से 30 सीट भाजपा को मिली थी जबकि कांग्रेस को 17 और जद (एस) को दो सीट मिली थी।
इस क्षेत्र में एक समय कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में होती थी लेकिन बाद में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत समुदाय के समर्थन से भाजपा इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन गई।
इस क्षेत्र में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा के समर्थन में वृद्धि 1990 के दशक में हुई। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को पद से हटा दिया था। लिंगायत पाटिल उस समय ‘स्ट्रोक’ बीमारी से उबर रहे थे। उसके बाद समुदाय कांग्रेस के खिलाफ हो गया।
बाद में भाजपा के बी एस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के प्रमुख नेता बन कर उभरे और यह क्षेत्र कुछ समय तक भाजपा का गढ़ बना रहा। लेकिन येदियुरप्पा के भाजपा से अलग होने तथा तत्कालीन राज्य सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझानों के बीच 2013 में कांग्रेस ने शानदार वापसी की और क्षेत्र की 50 में से 31 सीट पर कामयाबी हासिल की।
वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले, येदियुरप्पा वापस भाजपा में आ गए जिससे पार्टी को पुन: अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल गया। हालांकि अब येदियुरप्पा के चुनावी राजनीति से अलग हो जाने के बाद कांग्रेस लिंगायत समुदाय का समर्थन पुन: पाने की कोशिश कर रही है।
इस क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की भी खासी संख्या है। (भाषा)