अफ्रीकी देशों में भूख और कुपोषण की समस्या विकराल होती जा रही है. जलवायु से लेकर युद्ध, महामारी और तमाम देशों की सरकारों की नाकामी ने दुनिया के लिए एक बड़ा मानवीय संकट पैदा कर दिया है.
 (dw.com)
(dw.com)
अक्टूबर में नादिफा आबदी जब अपनी कुपोषित बेटियों को मोगादिशु के अस्पताल ले गईं तो नर्स ने बताया कि 42 और बच्चे उस दिन भूख से बीमार हो कर इमर्जेंसी वार्ड में भर्ती हुए हैं. उसके एक दिन पहले यह संख्या 57 थी.
बेनादिर मैटर्निटी एंड पेड्रियाटिक हॉस्पिटल का कहना है कि कुपोषित बच्चों की संख्या बीते एक साल में दोगुनी हो गई है. वो अब हर महीने एक हजार से ज्यादा बच्चों का इलाज कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सोमालिया में अकाल के कारण पांच लाख से ज्यादा बच्चों का जीवन संकट में है. यह इस शताब्दी में दुनिया के किसी भी एक देश के लिए सबसे बड़ी संख्या है.
पूरे अफ्रीका में पूरब से लेकर पश्चिम तक लोग भोजन के संकट का सामना कर रहे हैं. राजनयिकों और मानवीय सहायता पहुंचाने में जुटे लोगों के मुताबिक इस महादेश ने इतना जटिल और बड़ा भोजन संकट इससे पहले कभी नहीं देखा.
संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (एफएओ) के मुताबिक अफ्रीका में हर पांचवां आदमी यानी करीब 27.8 करोड़ लोग 2021 में ही भूख का सामना कर रहे थे. एफएओ का कहना है कि यह स्थिति अब और ज्यादा बिगड़ गई है.
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक पूर्वी अफ्रीका में भोजन की अत्यधिक कमी है यानी वो स्थिति जब इसकी वजह से जीवन या रोजगार पर तुरंत खतरा हो. पिछले एक साल में ही वहां यह 60 फीसदी बढ़ गई जबकि पश्चिमी अफ्रीका में करीब 40 फीसदी.
संघर्ष और जलवायु परिवर्तन इसके दीर्घकालीन कारण हैं. कोविड-19 की महामारी के बाद कर्ज का बोझ, बढ़ती कीमतें और यूक्रेन की जंग ने स्थिति को ज्यादा बिगाड़ दिया है. यूरोपीय सहायता फंस गयी है और दूसरी जगहों हाल भी कुछ अच्छा नहीं है.
बेनादिर हॉस्पिटल के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉ अवैस ओलोव बताते हैं कि दूसरे क्लिनिकों से आ रहे मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, "बाकी दुनिया से मदद के बगैर यहां की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली जायेगी." वो पांच कारण जिन्होंने अफ्रीका की हालत बिगाड़ दी है.
1. जलवायु परिवर्तन
पूर्वी अफ्रीका में बरसात के लगातार चार मौसम से बारिश नहीं हुई है. डब्ल्यूएफपी के पूर्वी अफ्रीका निदेशक मिषाएल डनफोर्ड के मुताबिक बीते 40 साल का सबसे भयानक सूखा पड़ा है. अफ्रीकी देश दुनिया भर में होने वाले जलवायु परिवर्तन का कारण बने कार्बन उत्सर्जन के महज 3 फीसदी के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन किसी भी दूसरे इलाके की तुलना में उन्हें ज्यादा नुकसान हो रहा है. जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज्यादा खतरा झेल रहे 20 देशों में चार को छोड़ कर बाकी सभी अफ्रीकी देश हैं.
इथियोपिया, केन्या, सोमालिया के करीब 2.2 करोड़ लोग केवल सूखे के कारण अत्यधिक खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं. अगर बारिश फिर नहीं हुई तो फरवरी में यह संख्या 2.6 करोड़ तक चली जाएगी.
बारिश की कमी के कारण फसल पैदा नहीं हो रही है. उत्तरी केन्या में मवेशियों के लिए पानी की तलाश में गहरी से गहरी खुदाई की जा रही है. मसाई समुदाय के लोगों का जीवन उनकी गायों पर टिका है लेकिन उन्हें मरते देखने से बचने के लिए वो अपनी गायें बेच रहे हैं.
उधर पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बीते तीस सालों की सबसे ज्यादा बारिश हुई है. अक्टूबर के मध्य तक करीब 50 लाख लोग और 10 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन पर इसका असर हुआ है.
अफ्रीका में संघर्ष
संघर्ष लंबे समय से भूख का एक कारण रहा है. जंग के कारण आम लोगों को अपना घर, रोजगार, खेत और भोजन के स्रोत से दूर जाना पड़ता है. संघर्ष में सहायता पहुंचाना भी मुश्किल होता है.
पिछले एक दशक में अफ्रीका के बेघर लोगों की संख्या तीन गुनी बढ़ कर 2022 में रिकॉर्ड 3.6 करोड़ तक जा पहुंची है. वास्तव में यह पूरी दुनिया में युद्ध के कारण कुल बेघर लोगों की संख्या का आधा है.
2016 में अफ्रीका के हथियारबंद गुटों के बीच 3,682 लड़ाइयां हुईं. 2021 में इन संघर्षों की संख्या 7,418 तक जा पहुंची. सोमालिया तो 1990 के दशक से ही गृहयुद्ध में घिरा है.
यूरोप में संघर्ष
फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने अफ्रीका की समस्याएं और बढ़ा दीं. नये उभरे संकट ने अमीर सरकारों की बड़ी राहत एजेंसियों का ध्यान साल के पहले आधे हिस्से में पूरी तरह यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया. इस साल की शुरुआत में जब संकट ज्यादा बढ़ा तो अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक ने एक आपातकालीन भोजन उत्पादन कोष बनाया. 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के इस कोष का लक्ष्य अफ्रीकी किसानों को गेहूं, मक्का, चावल और सोयाबीन की खेती में मदद करना था.
हालांकि पूरे अफ्रीका में संकट केवल पिछले एक साल में ही 14 फीसदी बढ़ गई. दानदाताओं की संख्या 12 फीसदी बढ़ने के बाद भी इससे केवल आधी जरूरतें ही पूरी हो सकीं. यूरोपीय देशों ने खासतौर से अफ्रीका के लिए सहायता में कटौती की है. यूरोपीय सरकारों ने 2022 में अफ्रीकी देशों को मदद में 21 फीसदी का योगदान दिया. 2018 से यह 16 फीसदी कम है. अमेरिका जैसे कुछ देशों ने मदद बढ़ाई है लेकिन कमी अब भी पूरी नहीं हो सकी है.
सबसे ज्यादा मानवीय सहायता कोष से मदद पाने वाले पांच में से चार अफ्रीकी देश होर्न ऑफ अफ्रीका इलाके के हैं जो सूखे से जूझ रहे हैं. इसकी वजह से कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़े हैं. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कुछ मामलों में राशन की कटौती करनी पड़ी है. डब्ल्यूएफपी का कहना है कि अगर जल्द ही और धन नहीं मिला तो उसे 10 फीसदी शरणार्थियों को राशन देना बंद करना पड़ सकता है.
रूस के छेड़े युद्ध के कारण अनाज के निर्यात पर भी काफी असर हुआ है. तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में काला सागर के तीन यूक्रेनी बंदरगाहों से 1 अगस्त को अनाज का निर्यात शुरू हुआ. 13 दिसंबर तक 615 जहाज यहां से रवाना हुए लेकिन इनमें से महज 11 जहाज ही उप सहारा अफ्रीका में गये.
युद्ध के कारण उर्वरकों की भी कमी हो गई है. जहां स्टॉक मौजूद है वहां भी कीमत इतनी ज्यादा है कि किसान खरीद नहीं सकते. इसकी वजह से अगले साल की पैदावार में 20 फीसदी तक की कटौती करनी पड़ सकती है.
कर्ज
कोविड-19 की महामारी ने अफ्रीका को अगले कई सालों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है. कई सालों तक कर्ज लेने के बाद देशों को अब उन्हें चुकाने की मुश्किल से जूझना पड़ रहा है. आईएमएफ के मुताबिक उप सहारा के 35 में से 19 देश कर्ज का तनाव झेल रहे हैं. इन देशों में सरकारें अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में अक्षम हैं और कर्ज की पुनर्संरचना बहुत जरूरी है.
चाड का उदाहरण देखिए. देश के 3.2 करोड़ लोगों पर सितंबर में 42 अरब डॉलर का कर्ज है. इसका मतलब है कि हर नागरिक पर करीब 13,000 डॉलर. इसी तरह दिसंबर में घाना का कर्ज उसकी जीडीपी के 100 फीसदी से ऊपर चला गया.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनाज, डेयरी, मांस, खाद्य तेल और चीनी की कीमतें 2021 में 23 फीसदी बढ़ गईं. इसकी वजह से उप सहारा अफ्रीका में लोगों के घर में सिर्फ खाने का खर्च ही उनकी आमदनी के 40 फीसदी हिस्से तक चला गया.
सरकारें
अफ्रीकी सरकारों ने भोजन संकट के बार बार आने से बचने के लिए बहुत कम काम किया है. उत्पादन बढ़ाने, आयात घटाने और खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने के लिए 2003 में अफ्रीकी नेताओं ने पांच साल के भीतर अपने राष्ट्रीय बजट का 10 फीसदी कृषि और ग्रामीण विकास पर खर्च करने की शपथ ली थी.
2021 में जब लगभग दो दशक बीत चुके हैं, माली और जिम्बाब्वे ही सिर्फ ऐसा कर सके हैं. ब्रिटेन की चैरिटी संस्था ऑक्सफैम के मुताबिक अफ्रीका के 39 देश में 2019 से 2021 के बीच सर्वेक्षण से पता चला कि उनका कृषि खर्च और कम हो गया है.
कृषि अफ्रीका की जीडीपी में करीब 20 फीसदी का योगदान देता है और आधे से ज्यादा अफ्रीकी लोग इसी सेक्टर में काम करते हैं. हालांकि इनमें से ज्यादातर खेती छोटे स्तर पर गुजारा करने वाली खेती है इसलिए अफ्रीका को गेहूं, खजूर का तेल और चावल जैसी बुनियादी चीजें भी आयात करनी पड़ती हैं.
बीते सालों में फसलों की उत्पादकता बढ़ी है लेकिन वो अब भी दुनिया में सबसे निचले स्तर पर हैं. बढ़ती आबादी के मुकाबले उनका हाल बहुत बुरा है.
एनआर/एए (रॉयटर्स)






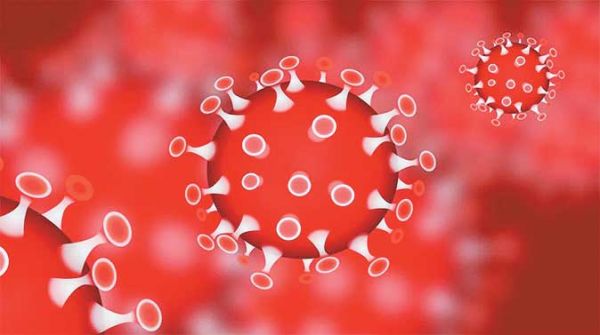

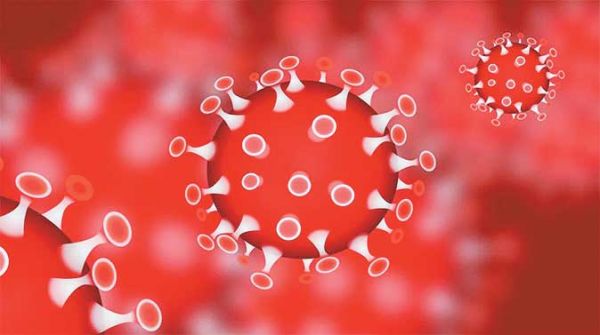








.jpg)















