संपादकीय

दुनिया के अलग-अलग देशों, शहरों, और संस्कृतियों में तमाम चीजें एक सरीखी नहीं रहतीं, फिर भी एक-दूसरे से सीखने के लिए कई चीजें रहती हैं। भारत जैसे देश के भीतर भी किसी एक जिले में कलेक्टर की की गई कोई मौलिक पहल बाकी देश में भी जगह-जगह इस्तेमाल होने की मिसालें ताजा इतिहास में दर्ज हैं। इसलिए अच्छे प्रयोगों, अच्छी चीजों, और अच्छी सोच का इस्तेमाल दूर-दूर तक किया जा सकता है। अब दो दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने मिला कि किस तरह अमरीका के न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच सामानों की अदला-बदली, उसके दान, या बहुत मामूली दाम पर खरीदी का एक बड़ा ही अच्छा सिलसिला चले आ रहा है। फिर इस बारे में और जानकारी ढूंढने पर पता लगा कि यह अमरीका के कई विश्वविद्यालयों में चलने वाला एक सिलसिला है जिसमें वहां पढ़ रहे, या खासकर पढ़ाई पूरी करके जा रहे छात्र-छात्राओं में यह परंपरा है कि वे अपने अधिकतर सामान छोड़ जाते हैं। फिर इन्हीं सामानों को किसी बड़े स्टोर की तरह जमाकर, सजाकर विश्वविद्यालय नए, या दूसरे छात्र-छात्राओं को अदला-बदली में, मुफ्त, या बहुत मामूली दाम पर मुहैया कराते हैं। अलग-अलग विश्वविद्यालयों का हर बरस का यह आंकड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने कितना टन कबाड़ कचरे के पहाड़ पर जाने से रोका। अब यह अमरीका या अधिक विकसित देशों के लिए तो एक अधिक काम की बात है जहां लोग बहुत सारा सामान इस्तेमाल करते हैं, और अच्छी-खासी हालत में अपने पुराने सामान दूसरों के लिए छोड़ भी जाते हैं। योरप जैसे विकसित इलाके में बहुत से देशों में शहरों के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग दिन बंटे रहते हैं जब लोग अपने घर का गैरजरूरी सामान निकालकर बाहर रख देते हैं, और दूसरे जरूरतमंद लोग सामान उठाकर ले जाते हैं। एक या दो दिन इंतजार के बाद म्युनिसिपल बचे सारे सामान को कबाड़ मानकर घूरे पर ले जाता है, और फिर जैसा चाहे उसका निपटारा हो।
अधिक संपन्न देशों में ऐसा कबाड़ अधिक निकलता होगा, लेकिन भारत जैसे देश में भी ऐसे बहुत से संपन्न तबके रहते हैं जिनके पास बहुत सा गैरजरूरी सामान इकट्ठा होते रहता है। वह उनके घर, और उनकी छाती पर बोझ भी बना रहता है, और दूसरी तरफ जरूरतमंद लोग वैसे ही सामान बाजार से खरीदते हैं जिससे कि धरती पर प्रदूषण का बोझ बढ़ता है। बहुत से जरूरतमंद तो ऐसे रहते हैं जिनकी ऐसे सामानों को खरीदने की ताकत नहीं रहती, और वे बिना सामानों के गुजारा कर लेते हैं। कबाड़ और जुगाड़ के बीच एक छोटे से पुल की जरूरत रहती है जिससे कि धरती को अधिक नुकसान होना बच सकता है। यह नुकसान दो तरीके से होता है, सामानों के कबाड़ का निपटारा कभी भी सौ फीसदी नहीं हो पाता, और बहुत से सामान हजारों बरस के लिए कचरा-पटी खदानों, या कचरे के पहाड़ों की शक्ल में धरती पर बोझ बन जाते हैं। दूसरी तरफ जरूरतमंद लोगों के लिए वैसे ही सामान और बनाने के लिए धरती की चीजों का इस्तेमाल होता है, और ऊर्जा लगती है, प्रदूषण होता है, धरती पर कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है।
हमने कई बरस पहले इसी कॉलम में उस वक्त के अपने अतिउत्साह में यह लिखा था कि संपन्न या मध्यमवर्गीय तबकों के लोगों को छोटे-छोटे समूह बनाने चाहिए जिसमें वे अपने आसपास के लोगों के पास इकट्ठा फिजूल के सामान उनसे दान की शक्ल की मांगें, फिर कहीं गोदाम या बड़े स्टोर जैसी जगह जुटाकर वहां पर इन सामानों को दूसरे जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त, या मुफ्त जैसे दाम पर मुहैया कराएं। उस वक्त हमें लगा था कि दस लोगों का समूह इस काम को शुरू कर सकता है, और इनमें से हर व्यक्ति दस-दस अलग-अलग लोगों को जोड़ सकते हैं, जो कि दस घरों से कबाड़ जुगाड़ करने का जिम्मा लें। फिर वे किसी छुट्टी या त्यौहार के दिन अपने संपर्क के दस परिवारों से पहले से बात करके जाएं, और उनके गैरजरूरी सामान लाकर किसी एक जगह इकट्ठा करें। इसके बाद वालंटियरों का एक समूह इन सामानों को छांटकर, जांचकर, अलग-अलग जमाकर, जरूरतमंद लोगों के लिए रख दे, जिन्हें मामूली दाम पर दिया जाए। मामूली दाम इसलिए जरूरी है कि मुफ्त का सामान लोगों के मिजाज को पचता नहीं है, और वे यहां से मुफ्त में उठाकर सबसे पास के घूरे पर फेंक भी सकते हैं। इसलिए थोड़े-बहुत दाम लेना जरूरी रहता है। मुफ्त के सामान को देना, और लेना, इन दोनों के लिए समाज में सभ्यता का एक विकास जरूरी होता है, किसी देश का अपमान किए बिना भी यह आसानी से समझा जा सकता है कि वहां के लोग कितने जिम्मेदार हैं। हमें याद है कि 1971 के बांग्लादेश निर्माण के वक्त जो लाखों शरणार्थी भारत आए थे, और उनमें से दसियों हजार को छत्तीसगढ़ भी भेजा गया था, उस वक्त विकसित पश्चिमी देशों ने उनके लिए मदद करने को नए, या तकरीबन नए कंबल भेजे थे। उस वक्त तक भारत में ऐसे विदेशी रंगारंग कंबलों का चलन बड़ा कम था। शरणार्थियों की मदद के लिए आए हुए इन कंबलों से हमारे शहर के फुटपाथ पट गए थे, और लोगों के बीच रस्ते का माल सस्ते में के अंदाज में बिकने वाले विदेशी कंबलों को खरीदने के लिए होड़ लग गई थी। अब ये कंबल संगठित रूप से शरणार्थियों से बाजार में आए थे, या सरकार में से ही किसी ने इन्हें बाजार की तरफ मोड़ दिया था, यह ठीक से याद नहीं है।
दुनिया के बहुत से देशों में सामान दान करने की परंपरा विश्वविद्यालयों के बाहर भी है। और ऐसे सामान कहीं मुफ्त बांटे जाते हैं, तो कहीं मामूली दाम पर बेचे भी जाते हैं ताकि ले जाने वाले लोगों को उनकी अहमियत मालूम हो। भारत में कई तरह के राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली रोटरी या लॉयंस जैसी संस्थाएं हैं, उद्योग और व्यापार की संस्थाएं भी सब जगह हैं। राजनीतिक दल भी पूरे देश में हैं, धर्म और जाति के संगठन भी खासे सक्रिय हैं। हमने कई बरस पहले ‘दस का दम’ नाम की जो सोच सामने रखी थी, उस पर तो इनमें से कोई भी अमल कर सकते हैं, और धरती पर बोझ बढऩे से थम सकता है, लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है। हर समाज में, शहर में, कई ऐसे उत्साही लोग मिल सकते हैं जो विश्वसनीयता की अपनी साख के साथ ऐसा बीड़ा उठा सकें। इससे लोगों के घरों में भरा हुआ कबाड़ भी घटेगा, सामानों का अधिकतम इस्तेमाल भी हो सकेगा, और नए सामान बचना कुछ थमेगा। पर्यावरण के संदर्भ में एक शब्द, री-साइकिलिंग, अक्सर इस्तेमाल होता है। यह कबाड़ की प्रोसेसिंग करके उससे कुछ बनाने के बारे में अधिक कहा जाता है। लेकिन कबाड़ में जाने से पहले ही चीजों को रोककर, उनकी बाकी जिंदगी का इस्तेमाल करने का सिलसिला एक बेहतर री-साइकिलिंग होगा। अमरीकी विश्वविद्यालयों के एक ताजा वीडियो ने हमारी अपनी एक बासी हो चुकी सोच पर लिखने का मौका दिया है, हम तो अपनी पहल से यह काम शुरू नहीं कर पाए, लेकिन हमसे अधिक काबिल कुछ लोग यह जरूर कर सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, आप धरती को एक बेहतर जगह, और समाज को एक बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)



.jpg)





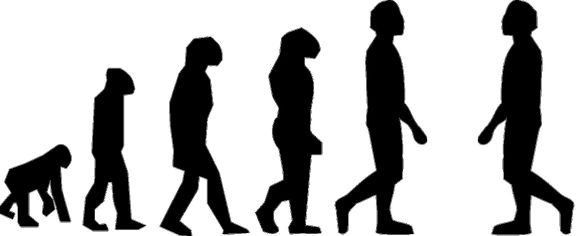




.jpg)

