साहित्य/मीडिया

-रमाकांत श्रीवास्तव
करोना काल में पढऩे और मनपसंद फिल्में देखकर समय अधिक गुजारा। सत्यजीत राय मेरे सर्वाधिक प्रिय फिल्मकार हैं। उनकी अधिकांश फिल्में मेरी देखी हुईं हैं। उन्हें दुबारा देखकर उनकी अद्भुत दृष्टि और जीवन सौंदर्य को चित्रित करने की उनकी क्षमता को और बेहतर समझने की कोशिश की। कल एक बार फिर अपनी पसंदीदा फिल्म ‘महानगर’ देखकर आंनद लिया। इस फिल्म पर दो शब्द कहने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूं।
नरेंद्र नाथ की रचना पर आधारित ‘महानगर’ फिल्म सत्यजीत राय की ही पटकथा, संगीत और उनके निर्देशन में पूर्णता प्राप्त करती है। राय ने अपनी अधिकांश फिल्मों में यह पद्धति अपनाई है। 1963 में बनी इस फिल्म को 1964 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सिलवर बियर पुरस्कार से अलंकृत किया गया था।
राय ने हमेशा अपने समकाल और अपने परिचित परिवेश को अपनी रचना का आधार बनाया। महानगर कलकत्ता के मध्य वर्ग को केंद्र में रख कर बनाई गई महान कृति है। अनिल चटर्जी और माधवी मुखर्जी अभिनीत फिल्म मजूमदार परिवार की आर्थिक मुश्किलों, अंतद्र्वंंद्व, रिश्तों की खूबसूरती को बेहद सहजता और सूक्ष्मता से चित्रित करती है। राय की अपनी कृति पर अद्भुत पकड़ आश्चर्य में डालने के साथ ही विभोर करती है। फिल्म की कहानी में घर की हालत को बेहतर बनाने में सहायक होने के लिए पत्नी एक कम्पनी में सेल्स गर्ल की नौकरी करती है। इसी बीच पति की नौकरी भी छूट जाती है। जिस बैंक में उसकी नौकरी थी वह दिवालिया हो जाता है।
घटनाओं को बेहद संक्षिप्त संकेतों में समेटते हुए दो बिंदुओं को मैं रेखांकित करना चाहता हूं। फिल्म बिना किसी अतिरिक्त सैद्धांतिक आवेग के स्त्री के साहस और सत्यनिष्ठा का चित्रण करती है। श्रीमती मजूमदार (नायिका माधवी मुखर्जी) अपनी सहयोगी एक एंग्लो इंडियन सेल्स गर्ल के प्रति बॉस के दुव्र्यवहार के विरोध में खड़ी होती है। बॉस एंग्लो इंडियन गर्ल को नापसंद करता है क्योंकि वह बंगाली नहीं है। श्रीमती मजूमदार से वह कहता भी है कि आप बंगाली होकर मेरे विरोध में उसका समर्थन कर रही हो? जब नायिका कहती है कि आप उससे माफी मांगे तब बॉस का कथन है- ऐसे सवाल टेबल के उधर से नहीं टेबल के इस तरफ से किए जाते है। श्रीमती मजूमदार अपना त्याग पत्र देकर आफिस से निकल जाती है।
फिल्म का आखरी दृश्य अनोखा हैं। नायिका जब सीढिय़ों से उतरने के लिए आफिस से बाहर आती है तब उसे लगता है कि घर की गंभीर आर्थिक स्थिति में उसकी आय ही एक मात्र संबल थी अब उसका पति नाराज होगा। वह रोती हुई नीचे उतरती है। उसका पति उसे लेने आता है। वह रोने का कारण पूछता है। पत्नी कहती है तुम जरूर मुझसे नाराज होंगे। किन्तु कारण सुनने के बाद पति कहता है कि तुमने सत्य का पक्ष लेकर विरोध किया। सही किया है इसलिए दुख मत करो। फिर महानगर की ओर देख कर कहता है- क्या इतने बड़े महानगर में हमें कोई दूसरा काम नहीं मिलेगा।
पति-पत्नी साथ-साथ भीड़ भरी सडक़ की ओर बढ़ते है। कैमरा पीछे सरकता है और लांग शॉट में वे दोनों भीड़ में समा जाते है। फिल्म संवेदनशील दर्शक के मन में सवाल छोड़ जाती है कि क्या उन्हें दूसरी नौकरी मिलेगी? क्या साहस का कोई प्रभाव होता है? क्या टेबल के इधर और उधर की स्थिति यही बनी रहेगी?
50 साल के बाद भी ये सवाल जस के तस हैं। फिल्म के और भी कई महत्व पूर्ण पहलू हैं। मैंने केवल उसके केंद्रीय भाव को सामने रखा है। इतने वर्षों के बाद इस फिल्म को शायद तीसरी बार देख कर मन में यह ख्याल आया कि हमारा समाज आज भी कहां खड़ा है! महानगर तो छोडि़ए कस्बों, गांवों तक का आसमान इन प्रश्नों से आक्रांत है।
अंत में एक दिलचस्प बात। सत्यजीत राय ने इसका जिक्र किया है कि उनके एक प्रशंसक ने उन्हें लिखा कि अंतिम दृश्य में आपने एक अनोखा संकेत दिया है। लॉन्ग शॉट में दिखलाया गया है कि बिजली के एक खंबे के दो लाइट में एक जल रही है और एक बुझी है। राय ने मजा लेते हुए बतलाया है कि दरअसल यह तो महानगर का बिजली विभाग ही बतला सकता है कि ऐसा क्यों हुआ था।





.jpg)
.jpg)
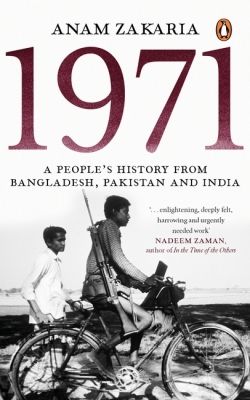
.jpg)
.jpg)
.jpg)








