साहित्य/मीडिया

22 मार्च को भारत में हुए जनता कर्फ्यू और 24 मार्च से लगातार चल रहे लॉकडाऊन के बीच साहित्य के पाठकों की एक सेवा के लिए देश के एक सबसे प्रतिष्ठित साहित्य-प्रकाशक राजकमल, ने लोगों के लिए एक मुफ्त वॉट्सऐप बुक निकालना शुरू किया जिसमें रोज सौ-पचास पेज की उत्कृष्ट और चुनिंदा साहित्य-सामग्री रहती थी। उन्होंने इसका नाम ‘पाठ-पुन: पाठ, लॉकडाऊन का पाठाहार’ दिया था। अब इसे साप्ताहिक कर दिया गया है। इन्हें साहित्य के इच्छुक पाठक राजकमल प्रकाशन समूह के वॉट्सऐप नंबर 98108 02875 पर एक संदेश भेजकर पा सकते हैं। राजकमल प्रकाशन की विशेष अनुमति से हम यहां इन वॉट्सऐप बुक में से कोई एक सामग्री लेकर ‘छत्तीसगढ़’ के पाठकों के लिए सप्ताह में दो दिन प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले दिनों से हमने यह सिलसिला शुरू किया है।
यह सामग्री सिर्फ ‘छत्तीसगढ़’ के लिए वेबक्लूजिव है, इसे कृपया यहां से आगे न बढ़ाएं।
-संपादक
‘सच्ची रामायण’ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
-अनुवादक
देविना अक्षयवर
देविना अक्षयवर का जन्म 22 जून, 1985। मॉरीशस में जन्मीं देविना अक्षयवर ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से ‘समकालीन स्त्री उपन्यास-लेखन में राजनीतिक चेतना (1990-2010)’ विषय पर पीएच.डी. की उपाधि हासिल की है। डॉ. गणपत तेली के साथ ‘आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के कुछ साहित्यिक स्रोत’ (2016) पुस्तकों का सह-सम्पादन किया है। विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में इनकी समीक्षात्मक रचनाएँ एवं लेख प्रकाशित होते हैं।
(9 दिसम्बर, 1969 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ई.वी. रामासामी नायकर ‘पेरियार’ की अंग्रेजी पुस्तक ‘रामायण : अ ट्रू रीडिंग’ व उसके हिन्दी अनुवाद ‘सच्ची रामायण’ को जब्त कर लिया था, तथा इसके प्रकाशक पर मुकदमा कर दिया था। इसके हिन्दी अनुवाद के प्रकाशक उत्तर प्रदेश-बिहार के प्रसिद्ध मानवतावादी संगठन अर्जक संघ से जुड़े लोकप्रिय सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता ललई सिंह यादव थे। उन्होंने ‘सच्ची रामायण’ का प्रकाशन 1968 में किया था।
बाद में उत्तर भारत के पेरियार नाम से चर्चित हुए ललई सिंह ने जब्ती के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट मेंचुनौती दी। वे हाईकोर्ट में मुकदमा जीत गए। सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई तीन जजों की खंडपीठ ने की। खंडपीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर थे तथा दो अन्य न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और सैयद मुर्तज़ा फज़़ल अली थे।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर 16 सितम्बर, 1976 को सर्वसम्मति से फैसला देते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।
निम्नांकित सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेजी में दिए गए फैसले के प्रासंगिक अंशों का अनुवाद है।)
भारत का सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललई सिंह यादव
याचिकाकर्ता : उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रत्यर्थी : ललई सिंह यादव
निर्णय की तारीख : 16 सितम्बर, 1976
पूर्णपीठ : कृष्ण अय्यर, वी.आर. भगवती, पी.एन.फज़ल अली सैयद मुर्तज़ा
निर्णय : आपराधिक अपीली अधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या 291, 1971
(इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 1971 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति की अपील। विविध आपराधिक केस संख्या 412/70)
अपीलकर्ता की ओर सेडी.पी. उनियाल तथा ओ.पी. राणा। प्रत्यर्थी की ओर से एस.एन. सिंह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुछ मामले ऊपर से दिखने में अहानिकर लग सकते हैं; किन्तु वास्तविक रूप में ये लोगों की स्वतंत्रता के संदर्भ में अत्यधिक चिंताजनक समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। प्रस्तुत अपील उसी का एक उदाहरण है। इस तरह की समस्याओं से मुक्त होकर ही ऐसे लोकतंत्र की नींव पड़ सकती है, जो आगे चलकर फल-फूल सके।
इस न्यायालय के समक्ष यह अपील विशेष अनुमति से उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार द्वारा की गई है। अपील तमिलनाडु के दिवंगत राजनीतिक आंदोलनकर्ता तथा तर्कवादी आन्दोलन के नेता पेरियार ई.वी.आर. द्वारा अंग्रेजी में लिखित ‘रामायण : अ ट्रू रीडिंग’ नामक पुस्तक और उसके हिन्दी अनुवाद की जब्ती के आदेश के संबंध में की गई है। अपील का यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 99-ए के तहत दिया गया है। अपीलकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार [जब्ती की अधिसूचना इसलिए जारी की गई है क्योंकि], ‘यह पुस्तक पवित्रता को दूषित करने तथा अपमानजनक होने के कारण आपत्तिजनक है। भारत के नागरिकों के एक वर्ग, हिन्दुओं के धर्म और उनकी धार्मिक भावनाओं को अपमानित करते हुए जान-बूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा [इसमें] है। अत: इसका प्रकाशन धारा 295 एआईपीसी के तहत दंडनीय है।’ [उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी] अधिसूचना में सारणीबद्ध रूप में एक परिशिष्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें पुस्तक के अंग्रेज़ी और हिन्दी संस्करणों के उन प्रासंगिक पृष्ठों तथा वाक्यों का सन्दर्भ दिया गया है, जिन्हें संभवत: अपमानजनक सामग्री के रूप में देखा गया है। उत्तरप्रदेश सरकार की इस अधिसूचना के बाद प्रत्यर्थी प्रकाशक [ललई सिंह] ने धारा 99-सी के तहत [इलाहाबाद] उच्च न्यायालय को आवेदन भेजा था। उच्च न्यायालय की विशिष्ट पीठ ने उनका आवेदन स्वीकार किया तथा सच्ची रामायण पर प्रतिबंध लगाने और इसकी जब्ती करने से संबंधित उत्तरप्रदेश सरकार की अधिसूचना को खारिज कर दिया। [इलाहाबाद] उच्च न्यायालय द्वारा [उपरोक्त अधिसूचना को खारिज करना] के निर्णय से असन्तुष्ट राज्य सरकार ने विशेष अनुमति से इस न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय) में अपील दायर की है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने हमारे समक्ष जोर देकर कहा कि ‘सरकार की अधिसूचना में ऐसा कोई दोष नहीं है, जिसके कारण उच्च न्यायालय ने उसे अमान्य घोषित किया गया है।’ राज्य सरकार के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि ‘चूँकि इस विवादित पुस्तक के लेखक ने कठोर शब्दों में श्रीराम जैसे महान अवतारों की निंदा की है और सीता तथा जनक की छवि को तिरस्कारपूर्वक धूमिल किया है, इसीलिए यह पुस्तक इन समस्त दैवीय महाकाव्यात्मक चरित्रों की आराधना या पूजा करने वाले विशाल हिन्दू समुदाय की धार्मिक भावनाओं पर अनुचित प्रहार करती है। लेखक का यह कार्य निंदनीय है।’
[लेकिन] उच्च न्यायालय ने बहुमत से इन तर्कों को किनारे लगाते हुए सरकारी आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि ‘राज्य सरकार ने धारा 99-ए के अनुसार अपनी अधिसूचना में उन तथ्यों का विवरण नहीं दिया है, जिनके आधार पर उसने किताब के बारे में [उपरोक्त] राय बनाई। [राज्य सरकार का कहना है कि] सिर्फ इसी एकमात्र कारण से उसे याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए और इलाहाबाद [उच्च न्यायालय] के आदेश को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
[लेकिन धारा 99-ए से संबंधित] प्रावधान में तीन ऐसी स्थितियों [का जिक्र] है, जो नागरिकों द्वारा सृजित रचनाओं को जब्त करने का अधिकार देती हैं। इसके तीन प्रासंगिक भागों को [हम] पुन: उद्धृत कर रहे हैं:-
‘99 ए (1): कोई समाचार पत्र या पुस्तक अथवा कहीं से भी मुद्रित ऐसा दस्तावेज, जिसमें निहित सामग्री या कोई अंश राज्य सरकार को भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देता हुआ या देने की मंशा रखता हुआ प्रतीत हो, या जिसका उद्देश्य जान-बूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से किसी भी ऐसे वर्ग के धार्मिक विश्वासों का अपमान कर उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना हो। अर्थात, कोई भी सामग्री; जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए, धारा 153-ए या धारा 295-ए के तहत दंडनीय है। राज्य सरकार अपनी राय का आधार बताते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी सामग्री का प्रसार करने वाले समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज की हर प्रति को जब्त करनेका आदेश दे सकती है।’
अत: एक प्रामाणिक आदेश के त्रिपक्षीय पहलू इस प्रकार हैं:-
(1) कि पुस्तक या दस्तावेज में कोई सामग्री हो।
(2) ऐसी सामग्री या तो भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देती हो या देने का इरादा रखती हो।
(3) तथा सरकार ने [सामग्री के संबंध में अपनी] राय किन तथ्यों के आधार पर बनाई, इसका विवरण दिया जाए।
[उपरोक्त तीन पहलुओं को परखने के] पश्चात् ही राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से ऐसी सामग्री का प्रचार करने वाली पुस्तक या दस्तावेज की सभी प्रतियों को जब्त करने का आदेश देसकती है।
[इस न्यायालय के सामने प्रश्न यह है कि] क्या [उत्तर प्रदेश सरकार की उपरोक्त] अधिसूचना वैधानिक तौर पर अनिवार्य उपरोक्त तीसरी माँग (सरकार ने सच्ची रामायण की प्रतियों की जब्ती की राय किन आधारों पर बनाई, इसका विवरण दिया जाए) को पूरा करती है या फिर यह कारणों [जब्ती के कारणों] के विवरण के अभाव में अपनी वैधता खो देती है? इसी तीसरी माँग जैसे महत्वपूर्ण तत्व की कमी को देखते हुए [इलाहाबाद] उच्च न्यायालय ने [राज्य सरकार द्वारा दिए गए जब्ती के] आदेश को खारिज कर दिया [था]। परन्तु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील, मि. उनियाल ने [हमारे समक्ष] कहा है कि यद्यपि सरकार की राय के आधार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है; तथापि [राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के साथ संलग्न] परिशिष्ट द्वारा इसकी पूर्ति हो जाती है।
उनका तर्क है कि आपत्तिजनक पुस्तक के पृष्ठों तथा पंक्तियों की संख्या मामलेके ‘विषयवस्तु’ तथा ‘आधार’ दोनों पर प्रकाश डालती है; खासकर ‘आधार’ तो इतना प्रत्यक्ष है कि उसे किनारे लगाना असंगत है। राज्य के अधिवक्ता का कहना है कि यह ऐसा मामला है, जिसका पर्याप्त रूप से विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। यह विवरण चाहे विशिष्ट रूप से दिया गया हो, चाहे अन्तर्निहित अर्थ के माध्यम से अथवा निहितार्थ द्वारा, ये विवरण कानूनी आवश्यकता को पूरा करते हैं तथा इनसे सरकारी निष्कर्ष का आधार अथवा कारण प्रस्तुत करने की आवश्यकता काफी हद तक पूरी हो जाती है। हालाँकि, औपचारिक तौर पर न सही, लेकिन [उनका कहना है कि यह आवश्यकता] परिशिष्ट से पूरी हो जाती है।
उन्होंने यह भी कहा है कि परिशिष्ट भी आदेश का एक अभिन्न अंग है, जो स्वत: ही स्पष्ट सामग्री प्रस्तुत कर देता है। [उनका कहना है कि] जब कारण स्वत: स्पष्ट हों, तो चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है और कानून महज औपचारिकता की पूर्ति के लिए उनकी अलग से व्याख्या करने की माँग नहीं करता है। [उत्तरप्रदेश सरकार के अधिवक्ता की उपरोक्त दलीलों का प्रतिवाद करते हुए इस न्यायालय ने कहा कि] दंड संहिता द्वारा अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता पर रोक लगाने की शर्तों को निहितार्थ के सुविधाजनितवाद के सिद्धांत द्वारा कमजोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह शर्त बहुत सोच-समझकर लगाई गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की मूल प्रकृति के मद्देनजर विशिष्ट प्रावधानों के सख्त और प्रकट अनुपालन के बिना इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
आखिरकार एक मुक्त गणराज्य में सभी मौलिक अधिकार मौलिक होते हैं, सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के समय को छोडक़र। क्योंकि आपातकाल के समय संवैधानिक रूप से स्वीकृत कठोर प्रतिबंधों को सीमित कर दिया जाता है। हमारे विचार के केन्द्र में दंड प्रक्रिया संहिता और दंड संहिता हैं और ये कानून हर समय लागू रहते हैं। इसलिए हमें कानून की व्याख्या इस तरह से करनी होगी कि संविधान और कानूनों में निर्धारित देश की सुरक्षा-आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखा जा सके।
क्लिक करें और यह भी पढ़े : उत्कृष्ट साहित्य का सिलसिला, आज चर्चित लेखिका शोभा डे का एक उपन्यास-अंश
[लेकिन] अपीलकर्ता के वकील का तर्क है कि जब्त किताब में दिए गए संदर्भ श्री राम, सीता और जनक के इतने कठोर तरीके से प्रतिकारक हैं और इनकी ऐसी निंदा करते हैं कि न्यायालय को उत्तर प्रदेश के हिन्दुओं की अपमानित भावनाओं की कल्पना स्वयं कर लेनी चाहिए तथा यह मान लेना चाहिए कि आदेश में कारणों को अदृश्य स्याही से लिखा गया है। [सरकारी वकील के] इन तर्क की महत्ता का आंकलन करते हुए, हमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा (अ) संवैधानिक परिप्रेक्ष्य, अर्थात क्या मौलिक स्वतंत्रता को कानूनी रूप से बाधित करने की कोशिश की जा रही है; और (ब) प्रकाशित सामग्री के बारे में आमतौर पर लोग जो विचार रखते हैं, उससे भिन्न अन्य तरह के विचारों की संभावनाएँ भी मौजूद हैं। ये संभावनाएँ सरकार लिए उन परिस्थितियों और कारणों का विवरण देना अनिवार्य बना देती हैं; जिस आधार पर सरकार ने प्रकाशित सामग्री के बारे में राय कायम की और उसे जब्त करने का निर्णय लिया।
भारत में राज्य धर्मनिरपेक्ष है और उसका हमारे बहुलतावादी समाज में प्रचलित किसी एक या अन्य धर्म की आस्थाओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है। लेकिन, वह मात्र शान्ति और लोक-व्यवस्था के उल्लंघन के विरुद्ध समाज का संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही बाध्य नहीं है; बल्कि वह ऐसी स्थिति बनाए रखने के लिए भी बाध्य है, जिसमें अशिष्ट भाषा में लिखित लेख या आपत्तिजनक प्रकाशन भिन्न या विरोधी मान्यताओं के लोगों की भावनाओं को इस तरह आहत न करें, जिससे ये जनसमूह हिंसक कृत्यों की ओर प्रवृत्त हों। अच्छी सरकार को अनिवार्य रूप से शान्ति और सुरक्षा की दरकार होती है और जो कोई भी बम अथवा पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक शांति भंग करता है, वह सरकार की कानूनी कार्रवाई के निशाने पर होता है।
हमारा प्रस्ताव है कि हम अपने समक्ष आए इस मसले को विषय-वस्तु की दृष्टि से तथा व्यापक परिप्रेक्ष्य दोनों ही संदर्भ में देखें और इन दोनों के समागम से इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय गलत नहीं था और अपील नामंजूर होनी चाहिए। भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों को इस [तरह के] प्रश्न पर विचार करनेका अवसर प्राप्त हुआ है; लेकिन वे अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं।
जब कानून द्वारा एक नागरिक के अधिकार पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसके पीछे एक ठोस कारण की आवश्यकता होती है। खासकर तब, जब इसके अद्र्ध-दंडात्मक (चसी पीनल) परिणाम भी होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के माननीय रचयिताओं ने धारा 99-ए को इस प्रकार तैयार किया है, जिससे नागरिकों की चिन्ताओं का समाधान हो सके तथा सरकार द्वारा इसके प्रयोग पर सतर्क नियंत्रण बरता जा सके। इसके प्रावधानों का प्रयोग विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह धारा सरकार को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य करती है, जहाँ सरकार को नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी और घृणा की भावना को बढ़ावा देने के स्पष्ट और वर्तमान खतरे पर विचार करना हो अथवा इसकी प्रवृत्ति या मंशा नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की हो। [हालाँकि] धारा में अन्य प्रवृत्तियाँ भी व्यक्त हैं, जिनका सरोकार वर्तमान मामले से नहीं है। लेकिन, [इतना तय है कि] ऐसे मामले में सरकार अपनी राय के आधार को वर्णित करने के लिए बाध्य है। हमारा सरोकार [उपरोक्त त्रिपक्षीय पहलू के] अंतिम भाग से है।
जब [वह] धारा स्पष्टत: कहती है कि आपको यह आधार बताना होगा, तो यह कोई जवाब नहीं है कि उन्हें वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अन्तर्निहित हैं।...किसी पुस्तक को दंडनीय अपराध के अन्तर्गत जब्त करना एक गंभीर मामला है; न कि उदासीनता के साथ निष्पादित किया जाने वाला एक नियमित कार्य। दंड संहिता के अनुसार इसमें की गई उपेक्षा का परिणाम इसकी वैधानिक मान्यता का खात्म होना है। [संविधान के निर्माण में निहित] ये विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम राज से गणतंत्र में बदलाव को स्वीकारते हैं और लोगों को सौंपे गए महान अधिकारों के उच्च स्थान का सम्मान करते हैं। जहाँ बोलना एक संवैधानिक कर्तव्य है, वहाँ मौन रहना एक घातक अपराध है। यह बात [संविधान की] विभिन्न धाराओं को समन्वित रूप से देखने पर स्पष्ट होती है। मसलन, धारा 99-सी असन्तुष्ट पक्ष को निषेधात्मक आदेश को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार देती है और अदालत सरकारी आदेश में दिए गए कारणों की जाँच कर उसकी पुष्टि करती है या उसे खारिज करती है।
अदालत आदेश में निर्धारित कारणों से परे जाँच नहीं कर सकती है और यदि इन कारणों को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, तो अदालत किसकी जाँच करेगी? और, इस चूक से न्यायालय में [असन्तुष्ट पक्ष द्वारा] अपील करने का महत्वपूर्ण अधिकार अर्थहीन हो जाता है। चाहे वह चूक लापरवाही से हो या सुनियोजित रूप से। कानून जिस हद तक प्रकाशन की स्वतंत्रता देता है, यदि प्रकाशन उसी दायरे तक सीमित है; तो प्रतिबंध लगाने वाली धारा के इस्तेमाल से अदालत को असहमति जरूर प्रकट करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से इस तरह के खतरनाक नतीजे की संभावना पैदा होती है।
क्लिक करें और पढ़ें : उत्कृष्ट साहित्य : सोपान जोशी की किताब, 'जल थल मल' पुस्तक का एक अंश
...धारा 99-ए में दिए गए निर्देश के बावजूद राज्य को जब्ती के कारणों का विवरण देने के दायित्व से मुक्त करना लोगों की निश्चित स्वतंत्रता पर शक्ति के उपयोग का हिंसात्मक अवसर देना है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? निश्चित रूप से राष्ट्र की सुरक्षा और समाज की शान्ति व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबंध की माँग करती है। हम चाहे स्वतंत्र क्यों न हों, फिर भी कानून के अधीन हैं।
(1) ए.आई.आर 1961 एस.सी.1662, 1666.
विरोधी मतों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हमारे संविधान निर्माताओं की आस्था मिल्स के प्रसिद्ध कथन और वाल्तेयर की प्रेरित करने वाले इस कथन का सम्मान करती थी जो इस प्रकार है-
‘यदि एक व्यक्ति को छोडक़र सम्पूर्ण मानव जाति का एक मत हो और केवल उस एक व्यक्ति का विरोधी मत हो, तो भी मानवजाति द्वारा उसको चुप करा देना न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन, यदि उस अकेले व्यक्ति में मानव जाति को मौन करने की शक्ति हो तो यह न्यायसंगत होगा। (अपने निबंध ‘ऑन लिबर्टी’ में मिल्स, पृ. 19-20: थिंकर लाइब्रेरी सं., वाट्स)’
‘तुम जो कहते हो, मैं उसे अस्वीकार करता हूँ, परन्तु तुम्हारे यह कहने के अधिकार की रक्षा, मैं अन्तिम श्वास तक करूँगा। (वाल्तेयर, एस.जी. टालंटयर, द फ्रेंड्स ऑफ वाल्तेयर, 1907)’
अधिकार और उत्तरदायित्व ‘एक जटिल प्रणाली’ है और हमारे संविधान के रचयिताओं ने स्वतंत्रता के उदारवादी प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निर्धारित किए; क्योंकि, वे लोग अराजकता के स्वरूप से भली-भाँति अवगत थे। संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर ने तर्क दिया था कि यह कहना गलत है कि मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाना वर्जित है और उन्होंने गितलो बनाम न्यूयॉर्क के दो स्वत: स्पष्ट अनुच्छेदों को उद्धृत किया है; जो इस प्रकार हैं:
‘बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता एक लम्बे अरसे से स्थापित बुनियादी सिद्धान्त है, जो कि संविधान द्वारा सुरक्षित अधिकार हैं। लेकिन, यह वस्तुत: गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बोलने या प्रकाशित करने की पूरी छूट नहीं देते हैं। हमें चुनना होगा, या तो हमें अपने भावों को व्यक्त करने का उचित अधिकार मिले, या फिर एक अप्रतिबंधित और अनियंत्रित अधिकार; जो भाषा के हरसंभव प्रयोग को उन्मुक्तता प्रदान करे और उन लोगों को दण्डित होने से बचाए, जो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं।’
‘सरकार पुलिस के माध्यम से अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उन लोगों को दण्डित कर सकती है, जो लोक कल्याण के प्रतिकूल बातें करके अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, जो आम जनता की नैतिकता को भ्रष्ट करने में प्रवृत्त होते हैं; अपराध करने के लिए उकसाते हैं और जन-शांति को भंग करते हैं। इस पर विवाद या संदेह नहीं किया जा सकता।...’
इस संवैधानिक सारांश से सुस्पष्ट रूप से यह व्याख्यायित हो जाता है कि संहिता की धारा 99-ए हमारा स्पष्टीकरण सिद्ध करती है। लोक व्यवस्था तथा शांति के हित में जन-शक्ति की भूमिका इसलिए नहीं होती कि बहुसंख्यक रूढि़वादियों को संतुष्ट करने के लिए चन्द रूढि़-विरोधियों का दमन किया जाए; बल्कि उसकी उपस्थिति इसलिए होती है, ताकि ऐसे विचारों को समय रहते रोका जाए, जो लोगों के दिमागों में खलबली मचा सकते हैं और उन्हें उत्पात के लिए प्रेरित कर सकते हैं। विशाल जनसमूह के बीच घृणा एवं उपद्रव जैसी भावनाएँ गुप्त रूप से हिंसा भडक़ा सकती हैं और सरकार समाज की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए अपने सुविचारित आधारों पर लिए गए निर्णय के जरिये पुस्तक के प्रसार पर रोक को वरीयता दे सकती हैं।
एक प्रबुद्ध सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की इस शक्ति का उपयोग उन्नत आर्थिक विचारों, विवेकशील तथा तर्कसंगत आलोचनाओं या पुरातन रूढि़वादी सच्चाई को साहस के साथ सामने लाने के प्रयास को कुचलने के लिए नहीं करगी। सुव्यवस्थित सुरक्षा एक संवैधानिक मूल्य है। यदि प्रगतिशील तथा प्रतिगामी लोगों का शांतिपूर्वक सहअस्तित्व सुनिश्चित करना है, तो इसका संरक्षण समझदारी से किया जाना चाहिए। संहिता की धारा 99-ए का यही सार है।
मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के अधिकार का वास्तविक इस्तेमाल सैद्धान्तिक तर्क पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान पर निर्भर करेगा। जहाँ मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध पर आधारित ‘सुस्पष्ट और आसन्न खतरा’ का अमेरिकी सिद्धान्त भारत में अनिवार्य रूप से लागू नहीं भी हो सकता है, वहीं होम्स जे. के ज्ञानवर्धक विचार प्रशासक और न्यायाधीश को सीख देने में सहायक हैं। शेनेक बनाम यू.एस.(1) मामले में होम्स जे. ने इस वास्तविक परीक्षण को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है। उन्होंने कहा है—
‘हम यह मानते हैं कि कई जगहों पर और सामान्य परिस्थितियों में प्रतिवादी अपने द्वारा प्रसारित परिपत्र में जो कुछ भी कहता है, वह अपने संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रहकर ही कहता है। लेकिन, प्रत्येक व्यवहार का स्वरूप उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिनमें वैसा व्यवहार किया जाता है।...कानून द्वारा बोलने की स्वतंत्रता की कड़ी सुरक्षा ऐसे व्यक्ति का बचाव नहीं करेगी जो थिएटर में ‘आग-आग’ चिल्लाकर भगदड़ मचाएगा। यह ऐसे व्यक्ति को दी गई निषेधाज्ञा से भी नहीं बचाती है, जो अपने शब्दों के बल से समाज पर अनुचित प्रभाव डालता हो। हर मामले में उठने वाला सवाल यह होता है कि क्या प्रयुक्त शब्द ऐसी ही परिस्थितियों में प्रयोग किए गए थे और क्या वे ऐसी प्रकृति के थे, जो प्रत्यक्ष और तात्कालिक खतरा पैदा करने वाले थे। जो वास्तविक खतरा पैदा करते हों, जिन्हें रोकने का अधिकार [अमेरिकी] कांग्रेस को है? यह खतरा कितना और किस स्तर का है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है?’
क्लिक करें और पढ़ें : उत्कृष्ट साहित्य : फिल्म संगीतकार अनिल विश्वास पर पंकज राग का लिखा- 'बादल-सा निकल चला, यह दल मतवाला रे'
एब्राइन्स बनाम यू.एस. (2) मामलों में एक प्रसिद्ध परिच्छेद में भी उन्होंने इस सिद्धान्त को विकसित करते हुए कहा कि-
‘विचारों की अभिव्यक्ति पर दंड देना मुझे पूरी तरह से तर्कसंगत लगता है। यदि आपको अपने प्रत्युत्तर या अपनी शक्ति पर कोई संदेह नहीं है और तहे-दिल से कोई परिणाम चाहते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अपनी अभिव्यक्ति कानून के दायरे में रहकर करेंगे, और वह अभिव्यक्ति विपक्ष को परास्त कर देगी। विरोध को अस्वीकार करने से यह इंगित होता है कि आप कहने को प्रभावी शक्ति नहीं मानते हैं, जैसे कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसने कोई असंभव कार्य को संभव कर दिया हो, या यह कि आप परिणाम के लिए पूरे मन से परवाह नहीं करते हैं, या यह कि आपको या तो अपनी शक्ति पर या फिर अपने प्रत्युत्तर पर संदेह है। लेकिन जब मनुष्य को यह महसूस होगा कि समय के साथ कई विरोधी विचारधाराएँ औंधे मुंह गिरी हैं, तो उन्हें अपने आचरण के आधारों से भी ज्यादा विश्वास इस विचार पर हो सकेगा कि वे जिस सर्वोत्तम स्थिति की इच्छा करते हैं, वह विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के बेहतर तरीके से हासिल की जा सकती है। सत्य की उत्तम परीक्षा तब होती है, जब मनुष्य की विचार-शक्ति को दूसरों के समक्ष रखा जा सके और उनके विचारों की अभिव्यक्ति स्वीकार की जा सके और जब उन्हें यह अहसास हो कि सत्य ही वह एकमात्र आधार है, जिस पर वे अपनी इच्छाओं को निरापद रूप से पूरा कर सकते हैं। हर हाल में वही हमारे संविधान का सिद्धान्त है। यह एक प्रयोग है, क्योंकि हमारा सम्पूर्ण जीवन ही एक प्रयोग है।’
बोमेन बनाम सेकुलर सोसाइटी लिमिटेड (2) मामले में लॉर्ड समर ने एक बार फिर आलंकारिक भाषा में लिखित एक परिच्छेद में स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की गतिशीलता को रेखांकित किया था, जो कि एक साथ बोधगम्य हैऔर सुरुचिपूर्ण भी-
(1) (1918) 249 यू.एस. 47.52=63 एल.ई.डी. 470.473-474.
(2) (1919) 250 यू.एस. 616, 629=63 एल.ई.डी. 1173, 1180.
(3) (1917) ए.सी. 406, 466-7.
‘समाज को खतरे में डालने वाले शब्द तथा कृत्य समय-समय पर अनुपात में भिन्न होते हैं। क्योंकि, वास्तव में समाज स्थिर या असुरक्षित होता है, या उसके विवेकशील सदस्य यह मानते हैं कि उस पर हमला हो सकता है। वर्तमान समय में ऐसी सभाओं तथा जुलूसों को कानूनी तौर पर वैध माना जाता है, जिन्हें डेढ़ सौ साल पहले राजद्रोही माना जाता था और ऐसा इसलिए नहीं है कि कानून कमजोर पड़ गया है या बदल गया है; बल्कि इसलिए कि समय के बदलने से समाज पहले से ज्यादा सशक्त हुआ है।’
क्लिक करें और यह भी पढ़ें : उत्कृष्ट साहित्य : त्रिलोकनाथ पांडेय का लिखा- 'फर्जी खबरों का मायाजाल'
वर्तमान समय में विवेकशील मनुष्यों को समाज के विघटन या पतन का डर नहीं होता; क्योंकि धर्म पर सार्वजनिक तौर पर जिन युक्तियों से चोट की जाती है, वे अवमाननापूर्ण नहीं होतीं। इसकी कोई संभावना नहीं है कि भविष्य में हमारे समाज की महत्वपूर्ण संस्थाओं को क्षीण करने के लिए अभिकल्पित धर्म-विरोधी हमले जनसाधारण के लिए खतरा पैदा करनेके दोष से अपने आप में अपराध सिद्ध होंगे। कानून की नजर में एक दिशा में आगे बढऩे वाला विचार खुद को नए अनुभवों के आधार पर दूसरी दिशा में मुडऩे से नहीं रोकता, न ही परिस्थितियों के फिर से बदलने पर वह अपनी उत्तरवर्ती पीढिय़ों को बाँधे रखता है।
आखिर, किसी भी मत का समाज के लिए खतरा होना, समय तथा वास्तविकता पर निर्भर है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जिससे समाज का खुद को आवश्यकतानुसार खतरों से बचाव करने का कानूनी अधिकार सीमित हो जाए। लेकिन, इतना कहना चाहूँगा कि जो अनुभव कभी खतरे को वास्तविक सिद्ध करते थे, अब नगण्य हो चुके हैं; और जो खतरे कभी बहुत निकट महसूस होते थे, अब टल गए हैं। सामान्य नियमों के अनुसार ईश्वर-निन्दा और अधर्म जैसा कुछ भी नहीं होता...जो हमें अपने समय में उस अनुभव के अनुसार विशेष परिस्थितियों में उन्हें लागू करने के अलग-अलग तरीकों को अपनाने से रोक सके।’
ऐसी है हमारी संवैधानिक योजना। ऐसी विधिशास्त्र संबंधी गतिशीलता और स्वतंत्रता एवं संयम के तात्विक आधार। कानून एवं राजनीति के सूक्ष्म संगम की संवेदनशीलता को न्यायाधीशों को कर्तव्यनिष्ठा से सँभालना पड़ता है।
इस मामले समापन से पहले, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम पुस्तक की गुणवत्ता या उसकी भडक़ाऊ और अपमानसूचक शब्दावली पर कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। यह कई कारक तत्वों की मेल पर निर्भर करता है। जो विचार रूढि़वादियों को ठेस पहुँचा सकता है, वह प्रगतिशील समुदायों के लिए हास्यास्पद हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर किसी एक धर्म, सम्प्रदाय, देश या समय के लिए जो विचार या शब्द अपमानजनक हो सकता है, वह दूसरों के लिए उतना ही पवित्र हो सकता है। रूढि़वादियों को स्वामी विवेकानन्द की इस फटकार से अब भी आक्रोश पैदा हो सकता है—
‘हमारा धर्म रसोई में है, हमारा ईश्वर वह बर्तन है जिसमें हम खाना पकाते हैं और हमारा धर्म कहता है—‘मुझे मत छूना, मैं पवित्र हूँ’ (जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनकी ‘डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया’ के पृ.-339 से उद्धृत)। मानव उन्नति का सूत्र स्वतंत्र विचार और उनकी अभिव्यक्ति में निहित है। लेकिन, जहाँ जनहित का प्रश्न हो, वहाँ सामाजिक अस्तित्व यथोचित नियंत्रणों का भी विधान करता है। न्यायिक समीक्षा की देखरेख में शासकीय विवेक संतुलन बनाए रखता है। हम न तो आपातकालीन स्थितियों की बात कर रहे हैं और न ही संवैधानिक रूप से पवित्र माने गए विशेष निर्देशों की, बल्कि हम तो सामान्य समय और व्यावहारिक कानूनों का समर्थन करते हैं, जो सब के काम आएँ।’
हम अपीलकर्ता राज्य सरकार के अधिवक्ता से यह कहना चाहेंगे कि यदि सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विवादित पुस्तक के विरुद्ध धारा 99-ए लागू करने के लिए खुद को विवश महसूस करे, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है; लेकिन निश्चित रूप से उसे अपने मत के आधारों के विवरण और धारा 99-सी के तहत कार्यवाही करने के कारणों की न्यायालयीय माँग को पूरा करना होगा। हमारा विस्तृत विचार-विमर्श कानूनी प्रश्नों को हल करता है और एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में आन्तरिक या प्रत्यक्ष द्वंद्वों का समाधान प्रस्तुत करता है।
विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुकदमे निम्न हैं-
अरुण रंजन घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य।
(1) और ज्वालामुखी बनाम ए.पी. राज्य।
(2) जो अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित विचार का समर्थन करते हैं; और मोहम्मद खालिद बनाम मुख्य आयुक्त।
(3) चिन्ना अन्नामलाई बनाम राज्य।
(4) और बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य।
(5) जो अपील के तहत इलाहाबाद के निर्णय सेसहमत थे। संभवत: उपरोक्त मामलों में से प्रत्येक में अनुपात पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि इस निर्णय के पहले हिस्से में प्रत्यर्थियों के विचारों पर अमल किया जा चुका है।
विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कई मौकों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 99-ए के तहत शक्तियों के प्रयोग की माँग की संभाव्यता हमें विरोध की स्थिति में ला देती है। विविधता में एकता के अलावा, भारत सांस्कृतिक विपर्ययों, कई धर्मों तथा विधर्मों, तर्कवाद और धार्मिक कट्टरता तथा आदिम पंथों और भौतिकवादी सिद्धान्तों के सह-अस्तित्व का देश है। इतिहास और भूगोल की बाध्यताएँ और मध्ययुगीन संस्कृति के शिथिल पड़ते प्रभावों पर आधुनिक विज्ञान का प्रहार, प्रिय-अप्रिय लडिय़ों से बने एक मोजाइकनुमा चित्रपट प्रस्तुत करते हैं; जिसने उनकी आपसी आलोचना की उदारचेता सहिष्णुता को व्यापक रूप से जीवन का एक आवश्यक अंग बना दिया है; भले ही उनकी अभिव्यक्ति अनर्गल ढंग से क्यों न होती हो। हमें विश्वास है कि जब्ती के कठोर निर्देशों की कार्यवाही में सरकारें अपने अभिमान को हावी नहीं होने देंगी, बल्कि हमारे समाज की इन अटल सच्चाइयों पर गौर करेंगी।
यदि कुछ क्षण के लिए हम भारत के महान विचारकों-मनु से लेकर नेहरू तक को छोड़ भी दें, तो पाएँगे कि गैलीलियो और डार्विन, थॉरो और रस्किन से लेकर कार्ल माक्र्स, एच.जी. वेल्स, बर्नार्ड शॉ तथा बट्र्रेंड रसेल तक, कई मनीषियों के विचारों एवं कथनों पर आपत्ति जताई गई है। आज भी हमारे देश में कहीं-न-कहीं ऐसे कट्टर लोग मिल जाते हैं, जो उनके लेखन से आहत होते हैं; लेकिन कोई भी सरकार इतनी रूढि़वादी नहीं होगी कि उनके बारे में चन्द कट्टरपंथियों के दुराग्रही विचारों के मद्देनजर उनके महान लेखन को जब्त करने के अधिकार की माँग कर।
(1) आई.एल.आर (1957) कलकत्ता 396.
(2) आई.एल.आर (1973) ए.पी. 114.
(3) ए.आई.आर 1968 दिल्ली 18 (एफ.बी.)।
(4) ए.आई.आर. 1971 मद्रास 44 (एफ.बी.)।
(5) 1964 जे. एंड के.एल.आर. 591।1974.
विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के प्रति एक प्रसिद्ध माओवादी विचार उदार दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से इस प्रकार व्यक्त करता है—
‘कला और विज्ञान की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए सौ फूलों को खिलने तथा सौ विचारधाराओं के बीच वाद-विवाद का अवसर देने की नीति उपयोगी होती है।’
हेराल्ड लास्की, जिन्होंने अपनी ‘ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स’ के जरिये भारत के कई प्रगतिशील विचारकों को प्रभावित किया है। उनके निम्नांकित कथन में एक चिरकालिक सच्चाई दृष्टिगत प्रकट होती है-
‘ कोई भी सरकार सामाजिक मुद्दों को लेकर कभी-भी इतनी दृढ़ मत नहीं होती कि वह राष्ट्र के नाम पर उन्हें दंडनीय घोषित कर दे। पिछले कुछ वर्षों के अमेरिकी अनुभवों से यह दुखद रूप से स्पष्ट होता है कि सरकारी तंत्र में कभी-भी सटीक तौर पर अंतर करने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती, जिससे वह यह तय कर सके कि अक्षेपित विचार समुचित रूप सेवर्तमान अव्यवस्था को जन्म देता है।’
‘इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अव्यवस्था का महिमा मंडन किया जा रहा है। यदि हिंसात्मक विचारों का सरकार पर इतना नियंत्रण हो कि उसकी बुनियाद ही हिल जाए, तो उसकी शासन-प्रणालियों में कोई घोर गड़बड़ी है।’
क्लिक करें और यह भी पढ़ें : उत्कृष्ट साहित्य : ठोकू गोसाईं नाच रहा था, बिहार के लौंडा नाच की याद
‘लगभग हमेशा ही, ऐसे मामले कम देखने को मिलते हैं, जिनमें दमन करने वाला पक्ष जीतता है। चूँकि, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से तनावग्रस्त स्थिति में शांति बहाल की जा सकती है; इसलिए लगभग हमेशा ही उसका प्रयोग न्यायसंगत सिद्ध होता है। इसके साथ ही बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का अर्थ है—किसी आंदोलन को भूमिगत रूप से चालित होने के लिए बाध्य करना; जो अवैधानिक है। वोल्तेयर से फ्रांस को खतरा उनके अकादमी के लिए चुने जाने से नहीं था, बल्कि उनकी इंग्लैंड यात्रा से था।’
‘लेनिन रूसी जारशाही के लिए ड्यूमा में उतना खरनाक नहीं होता, जितना कि वह स्विट्जरलैंड में रूसी जारशाही व्यवस्था के लिए था। वस्तुत: बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें वैधानिक स्वीकृति अन्तर्निहित होती है, एक साथ असंतोष का भाव-विरेचन तथा यथास्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता का आह्वान है। एक सरकार अपने समर्थकों द्वारा अपने प्रशस्ति-गान की तुलना में अपने विरोधियों की आलोचना से अधिक सीख सकती है। उस आलोचना का दम घोटना अंतत: कम-से-कम स्वयं के विनाश की ही तैयारी है।’
निर्णय के अन्त में सर्वोच्च न्यायालय नेएक टिप्पणी जोड़ते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से घोषित आपातकाल [सच्ची रामायण पर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के समय देश में आपातकाल लागू था] के वर्तमान संदर्भ में, कानून को आपातकाल संबंधी प्रावधानों में अंकित परिमित दायरों में रहकर ही कार्यवाही करनी पड़ेगी और यह निर्णय पूर्व-आपातकालीन कानूनी आदेश से संबंधित है। अत: हम अपील को खारिज करते हैं।
(सच्ची रामायण पुस्तक से)





.jpg)
.jpg)
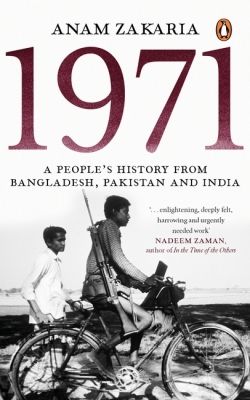
.jpg)
.jpg)
.jpg)








