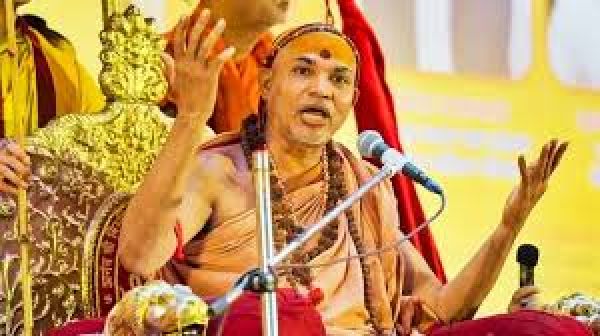राष्ट्रीय

BBC/DILIP KUMAR SHARMA
-दिलीप कुमार शर्मा
"डायन प्रथा के ख़िलाफ़ शुरुआती संग्राम में बहुत बाधाएं आईं. मुझे लाठी-डंडे और धारदार हथियार से कई बार मारने का प्रयास किया गया. मुझसे लिखित में लिया गया कि मैं गांव में दोबारा कदम नहीं रखूंगी. मुझे पकड़कर चप्पलों की माला पहनाने के प्रयास किए गए. बहुत धमकियां मिलीं. लेकिन मैंने हार नहीं मानी. आज डायन-शिकार करने वाले लोग मेरे नाम से ख़ौफ़ खाते हैं."
72 साल की बीरुबाला राभा जब ये बातें कहती हैं तो उनका चेहरा साहस और आत्मविश्वास से चमकने लगता है.
भारत सरकार ने असम की सामाजिक कार्यकर्ता बीरुबाला को इस साल पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है.
राभा जनजाति से आने वाली दुबली-पतली और छोटी कद काठी वाली बीरुबाला ने जादू-टोना करने वाले कथित अवतारों से अब तक 40 से अधिक ग्रामीणों की जान बचाई है. इनमें अधिकतर पीड़ित महिलाएँ हैं.
वह कहती हैं, "पद्मश्री मिलने से मुझे बहुत खुशी हुई है. इससे डायन हत्या जैसे अंधविश्वास के ख़िलाफ़ आगे लड़ने में और मदद मिलेगी. क्योंकि इस तरह की मान्यता के बाद प्रशासन और बाकी के लोगों का पूरा सहयोग मिलने लगता है. मैं जब 1998 में झाड़-फूंक करने वाले 'देवधोनी' अर्थात कथित अवतारों के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी उस समय प्रशासन से पूरी मदद नहीं मिलती थी. क्योंकि मैं अकेली थी और इसलिए लोग मेरी बात नहीं मानते थे. लेकिन 2005 में जब मेरा नाम नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया उसके बाद से पुलिस तथा प्रशासन के लोग मेरी मदद के लिए आगे आने लगे."

BBC/DILIP KUMAR SHARMA
आंदोलन की बदौलत बना क़ानून
डायन हत्या जैसी कुप्रथा के ख़िलाफ़ बीरुबाला के आंदोलन की बदौलत असम सरकार ने 2015 में असम डायन प्रताड़ना (प्रतिबंध, रोकथाम और संरक्षण) क़ानून बनाया.
इस क़ानून में किसी को डायन क़रार देना या फिर डायन के नाम पर किसी का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने को संज्ञेय अपराध माना जाता है और ग़ैर ज़मानती धाराएं लगाई जाती हैं. इस क़ानून में अभियुक्तों को पांच वर्ष के कारावास से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है.
क्या असम में डायन प्रथा के ख़िलाफ़ क़ानून बन जाने के बाद निर्दोष ग्रामीणों की हत्या के मामले कम हुए हैं?
इस सवाल का जवाब देते हुए बीरुबाला कहती हैं, "पहले के मुक़ाबले ग्रामीण लोगों में डायन हत्या को लेकर काफ़ी जागरुकता आई है. इसके साथ ही क़ानून बनने से कुछ लोगों में डर भी पैदा हुआ है. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ ही अब लोग ठगी करने वाले तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाना छोड़ रहे हैं."
वो कहती हैं, "लेकिन जनजातीय समाज में यह अंधविश्वास और कुप्रथा अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है. इसके लिए ख़ासकर आदिवासी महिलाओं को शिक्षित करना बेहद ज़रूरी है. यह अंधविश्वास सैकड़ों साल पुरानी प्रथा की जड़ें हैं जिसे ख़त्म करने के लिए आगे बहुत काम करना है."

BBC/DILIP KUMAR SHARMA
जब पहली बार अंधविश्वास के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई
दरअसल 1996 में बीरुबाला के बड़े बेटे धरमेश्वर को टायफाइड हो गया था और वह उसे लेकर गांव के एक वैद्य के पास गई थीं.
वैद्य ने बीरुबाला से कहा था कि उनका बेटा एक जादूगरनी के चक्कर में पड़ गया है और वह उसके बच्चे की मां बननी वाली है और जैसे ही उस बच्चे का जन्म होगा, उनका बेटा मर जाएगा. लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.
वह कहती हैं, "वैद्य की बात जब झूठी साबित हुई तो मुझे लगा कि ये लोग जादू-टोना कर हमारे आदिवासी समाज को नष्ट कर रहे हैं. महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित किया जा रहा था. मैंने उसी वक्त ठान लिया कि हमारे समाज को डायन जैसी कुप्रथा और अंधविश्वास से मुक्त करवाना है."
"फिर मैंने गांव की महिला समिति से जुड़कर डायन संबंधी जागरुकता पर अंदर ही अंदर काम करना शुरू किया. इस दौरान कई ग़ैर सरकारी संगठनों के लोगों से मुलाक़ात हुई और डायन हत्या जैसे अंधविश्वास के ख़िलाफ़ आवाज़ धीरे-धीरे बुलंद होती चली गई."

पिछड़े आदिवासी गांवों में बड़े पैमाने पर मौजूद अंधविश्वास और स्वास्थ्य सुविधाएँ बुरी हालत में होने के कारण लोग नीम हकीम पर भरोसा करते हैं. यही कारण है कि ये लोग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर फ़सल बर्बाद होने, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के लिए औरतों को ज़िम्मेवार ठहराने लगते हैं.
अकेली महिलाएं, विधवा और बुज़ुर्ग जोड़े मुख्य तौर पर इनके निशाने पर होते हैं. कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें आपसी रंजिश के कारण झाड़-फूंक करने वालों के साथ मिलकर निर्दोष लोगों को डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता है.
बीरुबाला का मानना है कि इस अंधविश्वास के ख़िलाफ़ औरतों को लड़ना होगा.
वह कहती हैं, "यह मेडिकल साइंस का युग है. जब आप बीमार पड़ जाओ, तो डॉक्टर के पास जाओ न कि किसी नीम-हकीम के पास. जिन लोगों के मन में नफ़रत और हिंसा है वही लोग ऐसे अंधविश्वास को मानते हैं. जब मैं ग्रामीणों से ये बातें कहती हूं तो वे अब मेरी बात सुनते हैं. इस कुप्रथा में विश्वास करने वाले लोग अब मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरे बुलाने पर एसपी-पुलिस पहुंच जाएगी."
असम-मेघालय सीमावर्ती ग्वालपाड़ा ज़िले के ठाकुरबिला जैसे एक छोटे से गांव में रहने वाली बीरुबाला ने डायन हत्या के ख़िलाफ़ 22 साल पहले जब यह आंदोलन शुरू किया था उस समय उनके गांव के लोगों ने उन्हें तीन साल तक समाज से बाहर कर दिया था.
लेकिन आज वह जहां भी जाती हैं, उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है. लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी और ऑटोग्राफ लेते हैं. पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं. असम के अलग-अलग हिस्सों में बीरुबाला को सम्मानित करने के लिए लोग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं.

BBC/DILIP KUMAR SHARMA
2011 से 'मिशन बीरुबाला' शुरू किया
असम के जनजातीय ग्रामीण इलाक़ों में बीरुबाला ने डायन प्रथा जैसे अंधविश्वास के ख़िलाफ़ जागरूकता के लिए 2011 से 'मिशन बीरुबाला' शुरू किया है.
इस मिशन से सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं और असम के विभिन्न ज़िलों में काम कर रहे हैं.
पद्मश्री से पहले बीरुबाला को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उद्यमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं. केवल पांचवीं तक की पढ़ाई करने वाली बीरुबाला को उनके काम के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने साल 2015 में मानद डॉक्टरेट की डिग्री से नवाज़ा था.
असम में ख़ासकर आदिवासी समाज में दशकों से डायन के नाम पर ख़ौफ़नाक कहानियां सुनाई जाती रही हैं.
नवंबर 2019 में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2011 के बाद से, डायन-शिकार के मामलों में 107 लोग मारे गए हैं. लेकिन पिछले तीन-चार सालों से डायन हत्या से जुड़ी घटनाओं में कमी आई है. (bbc.com)