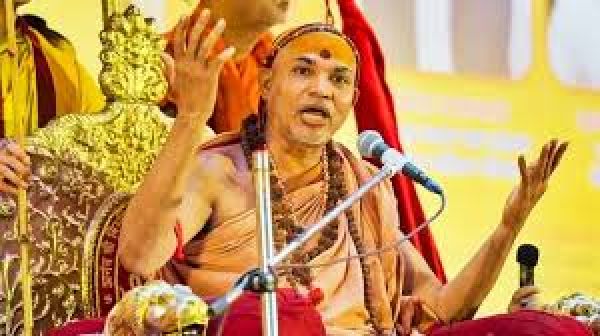राष्ट्रीय

कार्टूनइमेज स्रोत,BBC/NIKITA DESHPANDE
-पूजा छाबड़िया
तारा कौशल ने अपनी रिसर्च के सिलसिले में कई बलात्कारियों का इंटरव्यू किया और इसका उन पर गंभीर असर पड़ा है.
उन्होंने 2017 से बलात्कारियों के इंटरव्यू पर आधारित अपने रिसर्च की शुरुआत की. इसके बाद वे अवसाद की चपेट में आयीं, उनके दिमाग़ ने काम करना बंद कर दिया और कई दिन तो वह बस रोती रहीं.
एक शाम उन्होंने नोएडा के अपने फ्लैट के बेडरूम में खुद को बंद कर लिया. तारा उस शाम को याद करती हैं, "मेरे पार्टनर साहिल दरवाज़े पर खड़े थे. वह बार बार पूछ रहे थे कि ठीक तो हो, लेकिन मैं अंदर लगातार रो रही थी. तब मुझे लगा कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है."
वैसे भी रिसर्च शुरू करने से पहले तारा यौन हिंसा का आघात झेल रही थीं. वे जब 16 साल की थीं तब से इस मुद्दे पर बात कर रही हैं. उन्होंने अपने माता-पिता को बताया, "जब मैं चार साल की थी, तब माली ने मेरे साथ बलात्कार किया था."
यह सुनकर तारा के माता-पिता अवाक रह गए थे. लेकिन तारा के लिए यह अपने अंदर चल रहे तूफ़ान को बाहर निकालने जैसा था. इसके बाद से अपने साथ हुई यौन हिंसा के बारे में वह लगातार बोल रही हैं, पब्लिक डिबेट में हिस्सा ले रही हैं, दोस्तों से चर्चा कर रही हैं और अब किताब भी लिख रही हैं.
तारा ने बताया, "उस घटना की कुछ कुछ यादें हैं. मैं उसका नाम जानती हूं. वह कैसा लगता था ये जानती हूं. मुझे उसके घुंघराले बाल और मेरी ब्लू ड्रेस पर ख़ून लगना याद है." जब वह बड़ी होने लगीं तो उन्होंने हर दिन होने वाले दूसरे यौन उत्पीड़नों के बारे में सोचना शुरू किया. वह यह जानना चाहती थीं कि आख़िर ऐसा क्यों होता है?
उन्होंने बीबीसी को बताया, "मेरी किताब 'व्हाय मेन रेप' मेरी व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा का नतीजा है. इस दौरान मुझे मानसिक आघात भी सहना पड़ा है."
छिपे बलात्कारी की पहचान
दिसंबर, 2012 में दिल्ली की चलती बस में फिज़ियोथेरेपी की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद से भारत में बलात्कार और यौन हिंसा पर काफ़ी चर्चा हुई है. इस घटना के कुछ ही दिनों के भीतर आंतरिक ज़ख़्मों के चलते पीड़िता की मौत हो गई थी. मामले के चार दोषियों को मार्च, 2020 में फांसी की सज़ा हुई. यौन अपराध पर सख़्ती के बावजूद बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में भारत में कुल 33,977 बलात्कार हुए. इसका मतलब यह है कि भारत में प्रति 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना होती है. हालांकि इन मुद्दों पर काम करने वाले एक्टिविस्टों की मानें तो वास्तविक संख्या कहीं ज़्यादा होगी क्योंकि कई मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं.
तारा उनके बारे में जानना चाहती थीं जिन्हें कभी बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया गया, जिन पर कभी बलात्कार के मामले दर्ज नहीं हुए. वह इस कोशिश में देश भर में नौ लोगों से मिलीं, जिन पर बलात्कार के आरोप लगे ज़रूर लेकिन इन लोगों से कभी आधिकारिक पूछताछ नहीं हुई.
तारा ने अपनी किताब में लिखा है, "मैंने उनके घर के माहौल को समझने में समय लगाया. उनका इंटरव्यू लिया. उन्हें, उनके परिवार और दोस्तों को समझने की कोशिश की. मैं अंडरकवर अपना काम कर रही थी- इसके लिए मैंने अलग नाम, ईमेल और फेसबुक आईडी का इस्तेमाल किया."
अंडरकवर काम करने के दौरान उन्हें अपना टैटू छिपाना पड़ा और इस दौरान उन्होंने हमेशा परंपरागत कुर्ते और जीन्स ही पहने. इतना ही नहीं वह अपने साथ एक अनुवादक भी रखती थीं, जिसका परिचय वह अपने बॉडीगार्ड के तौर पर देती थीं. वह अपना परिचय ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक अनिवासी भारतीय के तौर पर ज़ाहिर करती थीं जो एक फ़िल्म के रिसर्च के सिलसिले में आम लोगों के जीवन को जानने की कोशिश कर रही है.
तारा कौशल ने लिखा है, "मैं 250 सवाल पूछा करती थी और सभी के लिए एक जैसी बातों पर नज़र रखती थी. लेकिन मैंने कभी उन्हें यह नहीं बताया कि मैं उन लोगों को पढ़ने की कोशिश कर रही हूं, ऐसा करने पर वे बलात्कारी के तौर पर चिन्हित होने लगते."
सहमति की समझ का अभाव
तारा इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करने लिए भी तैयार थीं. वह अपनी पॉकेट में पेपर स्प्रे (मिर्ची वाला स्प्रे) रखती हैं, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर इमर्जेंसी कॉन्टैक्ट की व्यवस्था रखती थीं. साथ ही व्हाट्सऐप पर एक सपोर्ट ग्रुप भी बनाया हुआ था जिसमें वह अपनी लाइव लोकेशन शेयर करती थीं.
हालांकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि अंतरंग सवालों के जवाब देते वक्त तीन लोग अश्लील हरकत करने लगेंगे.
उत्तर भारत के एक शख़्स ने जाड़े की धूप में छत के बरामदे पर बैठकर क्या कुछ किया था, इस बारे में तारा ने लिखा है, "छोटे क़द का वो आदमी मेरे सामने बैठा था. मैं जितने लोगों से मिली वह उनमें सबसे शातिर यौन अपराधी (ये उसने खुद स्वीकार किया) था. उसने अपने छोटे से गांव की कई महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया था."
"उसे जेल में होना चाहिए था या फिर समाज से निष्कासित होना चाहिए था लेकिन वह अपने समुदाय का प्रभावी शख़्स बना हुआ था. छत के बरामदे पर वह मेरे सवालों से ही उत्तेजित हो गया था और अश्लील हरकतें करने लगा था."
इन अनुभवों का तारा के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर देखने को मिला.
तारा ने बीबीसी को बताया, "जब मैंने इन इंटरव्यू को पूरा किया तब मुझे महसूस हुआ कि इस आघात से निपटने के लिए मुझे थेरेपी की ज़रूरत है. मैं काफी अवसाद में आ गई थी. कई रातें तो ऐसी रही है जब मैंने नींद में ही अपने पाटर्नर को काटते हुए कहा कि मुझे छेड़ना बंद करो."
हालांकि अंत में तारा को यह मालूम चला, "इन पुरुषों को सहमति की कोई समझ नहीं थी और ना ही उन्हें ये मालूम था कि बलात्कार क्या होता है?"
जब तारा ने अपनी रिसर्च शुरू की तो उन्होंने जेंडर आधारित हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर महिलाओं से बात की.
तारा ने बताया, "इन महिलाओं से बात करके मुझे दो पुरुषों के बारे में पता चल गया. लेकिन अन्य सात लोगों को तलाशना काफ़ी मुश्किल भरा रहा. मुझे स्थानीय पुलिस, स्थानीय मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और जासूसी करने वाली एजेंसियों से भी संपर्क करना पड़ा."
तारा के साथ बातचीत करने वाले लोगों में अधिकांश ने बलात्कार ही नहीं कई बलात्कारों की बात स्वीकार की. हालांकि सज़ा झेल रहे बलात्कारियों से बात नहीं करने का फ़ैसला तारा ने पहले ही कर लिया था.
तारा ने बताया, "मेरे लिए, जेल बलात्कार करने वाले पुरुषों का प्रतिनिधित्व नहीं करता. लोग प्रायद्वीप पर नहीं होते हैं, लोगों के आसपास के माहौल को समझे बिना उनके बारे जानना, आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकता."
हालांकि तारा कौशल से उलट शैफील्ड हालाम यूनिवर्सिटी में अपराध विज्ञान की लेक्चरर डॉ. मधुमिता पांडेय ने बलात्कार मामलों में सज़ा झेलने वालों को अपनी रिसर्च का विषय बनाया.
उन्होंने अपनी रिसर्च दिल्ली में दिसंबर, 2012 में हुए गैंगरेप के बाद शुरू की. उन्होंने बताया, "बलात्कारियों को शैतान क़रार दिया गया और उनके ख़िलाफ़ सामूहिक आक्रोश था. उनके अपराध से हमलोग इतने भयभीत हुए कि उन्हें अपने से अलग, अपनी संस्कृति से अलग दूसरा मानने लगे थे."
एक रिसर्चर के तौर पर डॉ. मधुमिता ने उस धारणा पर काम करने का फ़ैसला लिया जिसमें माना जाता है कि बलात्कारी पुरुषों में महिलाओं के प्रति कहीं ज़्यादा परंपरागत और दमनकारी दृष्टिकोण मौजूद होता है.
वह जानना चाहती हैं, "क्या ये पुरुष वाक़ई में महिलाओं के प्रति अपनी सोच में इतने अलग होते हैं, जितना हम मान रहे हैं?"
कोई भी बलात्कारी हो सकता है
डॉ. मधुमिता ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद 100 से ज़्यादा बलात्कारियों का साक्षात्कार किया है. इन सब लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं.
एक सामूहिक बलात्कार की सज़ा झेल रहे शख़्स ने कहा कि वह हादसे के तुरंत बाद भाग निकला था. मंदिर के एक सफ़ाई कर्मचारी ने बताया कि पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के लिए उसे उकसाया गया था. वहीं एक युवा ने दावा किया कि आपसी सहमति से उसने संबंध बनाए थे, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने जब दोनों को एक साथ देख लिया तब उस पर बलात्कार का आरोप लगाया गया.
डॉ. मधुमिता को पांच साल की बलात्कार पीड़िता के बारे में जब मालूम हुआ तो उन्होंने पीड़िता के परिवार से मिलने का फ़ैसला लिया.
डॉ. मधुमिता ने कहा, "बेटी के साथ बलात्कार की ख़बर मिलने के बाद पिता मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गए और परिवार को छोड़कर कहीं चले गए. लेकिन मां पुलिस के पास पहुंची. न्याय की बहुत उम्मीद नहीं होने के बाद भी उन्होंने सभी पेपरवर्क करके मामला दर्ज कराया."
डॉ. मधुमिता महिलाओं के प्रति इन पुरुषों की सोच को समझना चाहती थीं ताकि उन्हें यौन हिंसा की सोच का पता चल सके.
उन्होंने बताया, "अपराध की प्रकृति में अंतर के बावजूद एक बात कॉमन देखने को मिली, समाज में पुरुषों को जिस तरह का विशेषाधिकार मौजूद है उसका असर दिखा."
उन्होंने भी देखा कि बलात्कार पीड़िताओं पर दोष डाल रहे हैं और उनमें सहमति की समझ का अभाव है. अपनी रिसर्च के माध्यम से मधुमिता ने तारा की तरह ही एक प्रचलित धारणा का खंडन किया कि 'बलात्कारी आमतौर पर परछाइयों में छिपे अजनबी होते हैं.'
मधुमिता ने बताया, "लेकिन इस मामले में ज़्यादातर लोग पीड़िताओं के पहचान वाले थे. इसलिए कोई कैसे बलात्कारी हो जाता है, इसे समझना आसान होता है, ये लोग कोई असाधारण लोग नहीं होते हैं."
पुराने आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ज़्यादातर मामलों में बलात्कारी पीड़िता की पहचान वाले होते हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 95 प्रतिशत मामलों में ऐसा होता है. हालांकि इस मुद्दे पर काम कर रहे लोगों के मुताबिक इस वजह से भी सभी बलात्कार के मामले दर्ज नहीं होते.
सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली संस्था प्रोजेक्ट 39 ए के कार्यकारी निदेशक डॉ. अनूप सुरेंद्रनाथ ने बताया, "बलात्कार के सभी मामले दर्ज नहीं होते क्योंकि अधिकांश में बलात्कारी पहचान वाले होते हैं. इसके चलते पीड़िता और उनके परिवार वालों पर अपराध की शिकायत दर्ज नहीं कराने के लिए कई तरह के दबाव काम करने लगते हैं."
ज़्यादातर वही मामले दर्ज होते हैं, जिसमें अपराध जघन्य होते हैं और वे सुर्खियों में आते हैं.
मौत की सज़ा है निदान?
भारत दुनिया का कोई अकेला देश नहीं है जहां इतने बड़े स्तर पर बलात्कार की घटनाएं होती हैं लेकिन कइयों का मानना है कि पितृसत्तात्मक समाज और असमान लैंगिक अनुपात के चलते स्थिति बद से बदतर हो रही है.
बीबीसी के भारतीय संवाददाता सौतिक बिस्वास कहते हैं, "ताक़त प्रदर्शित करने के लिए बलात्कार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का चलन बढ़ा है और इसके ज़रिए समाज के दबे कुचले लोगों को भयभीत किया जाता है."
"बलात्कार के मामलों को दर्ज करने के लिहाज़ से स्थिति बेहतर हुई है. लेकिन भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था काफ़ी हद तक राजनीतिक दबाव में काम करती है इसमें कई बार अभियुक्तों को सज़ा नहीं मिलती है, यही वजह है कि बलात्कार के कम मामलों में ही सज़ा होती है."
हालांकि 2012 में दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना के बाद क़ानूनों को कहीं ज़्यादा सख़्त किया गया है. जघन्य मामलों में दोषियों को मौत की सज़ा का प्रावधान भी किया गया है. लेकिन तारा और डॉ. मधुमिता, दोनों को लगता है कि मौत की सज़ा का प्रावधान समस्या का दीर्घकालीन हल नहीं है.
डॉ. मधुमिता का कहना है, "मेरा पूरा यक़ीन सुधार और पुनर्वास में है. हमें अपना ध्यान समाज में बदलाव की ओर लाना चाहिए जिससे देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच एकसमान स्तर का ढांचा बन पाए."
तारा इससे सहमति जताते हुए कहती हैं, "हमें इस अपराध के एक्टिव एजेंट पर नए सिरे से ध्यान फोकस करना होगा, ये एक्टिव एजेंट पुरुष हैं. हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए हमें उन्हें बचपन से बेहतर शिक्षा देनी होगी."
तारा ने जिन पुरुषों का इंटरव्यू किया है उनमें समाज के सभी तबके के लोग शामिल थे लेकिन किसी को भी स्कूली स्तर पर सेक्स एजुकेशन नहीं मिली थी.
तारा बताती हैं, "शिक्षा तो नहीं मिली लेकिन उन्हें अपने दोस्तों के साथ, पॉर्न फ़िल्मों और सेक्स वर्करों से आधी अधूरी जानकारी मिली."
कइयों ने अपने बचपन में ऐसी हिंसा को देखा भी था. तारा ने लिखा है, "सभी मामलों में लोगों ने पिता को मां को पीटते हुए देखा था. उन्हें प्यार नहीं मिला था, पिता या घर के बड़े पुरुषों के हाथों से उन्हें कई बार मार पड़ी थी."
उन्होंने रिसर्च के अंत में लिखा है कि पुरुष जन्म से ही विशेषाधिकार के साथ बड़ा होता है.
पुरुष बलात्कार क्यों करते हैं?
डॉ. मधुमिता ने बताया, "इसका कोई एक जवाब नहीं है क्योंकि बलात्कार एक कॉम्प्लेक्स क्राइम है. हर मामला अपने आप में अलग होता है और यह काफ़ी सब्जेक्टिव भी है. कुछ लोग गैंग रेप में शामिल होते हैं तो कुछ पीड़िता की पहचान वाले होते हैं तो कुछ एकदम अनजान को बलात्कार का शिकार बनाते हैं. बलात्कारी भी कई तरह के होते हैं - गुस्से में आकर बलात्कार करने वाले, क्रूरता के साथ दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की नीयत से बलात्कार करने वाले और कई बलात्कार करने वाले सीरियल रेपिस्ट."
डॉ. मधुमिता के मुताबिक ये बलात्कारी कोई भी हो सकता है - पति, सहकर्मी, नज़दीकी दोस्त, डेट पर मिलने वाला दोस्त, क्लासमेट, प्रोफेसर.
डॉ. मधुमिता ने बताया, "देश के आम लोगों की तरह मैं भी सोचती थी कि जेल के अंदर मैं क्या सवाल जवाब करूंगी. यह धारणा बॉलीवुड फिल्मों के जेल देखकर बनी थी. मुझे लगता था डरावने दिखने वाले पुरुष होंगे - जिनके चेहरे पर कटे का निशान हों और धारीदार कपड़े पहने होंगे. ये लोग मेरे से दुर्व्यवहार कर सकते हैं, या अभद्रता भरे कमेंट्स पास कर सकते हैं जो मुझे बुरा लगेगा, यह सब सोच मुझे डर भी लगता था."
लेकिन जल्दी ही डॉ. मधुमिता को लगा कि ये ऐसे लोगों का समूह नहीं है. उन्होंने बताया, "जितना मैं उन लोगों से बात करने लगी, उनकी कहानियां सुनने लगीं तब वे मुझे विचित्र नहीं लगने लगे. यह हम सबको समझने की ज़रूरत है."
डॉ. मधुमिता के मुताबिक जेंडर वायलेंस के मुद्दे के निदान के लिए समाज को सामूहिक तौर पर आत्म अवलोकन करने की ज़रूरत है. वह ब्रिटिश प्रोफेसर लिज़ कैली की यौन उत्पीड़न की अवधारणा का ज़िक्र करते हुए कहती हैं जिसके मुताबिक यौन उत्पीड़न एक निरंतरता है जिसमें अलग अलग तरह की यौन हिंसाएं एक दूसरे से गुंथी होती हैं.
डॉ. मधुमिता ने बताया, "हमारे आसपास मौजूद पुरुष ख़तरनाक हो सकते हैं, यह विचार डराने वाला है लेकिन नया नहीं है. हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं. कोई आपका रेप नहीं करता है लेकिन वह अपना प्रभुत्व कई दूसरी तरह से ज़ाहिर करता है. समाज के लिए यह बिलकुल सामान्य बात है."
डॉ. मधुमिता के मुताबिक रोज़मर्रा के जीवन में महिलाओं के साथ भेदभाव पर चर्चा नहीं होती. कार्यस्थल से लेकर सड़कों पर होने वाले उत्पीड़न की ओर संकेत करते हुए डॉ. मधुमिता बताती हैं कि जब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हो जाती तब तक कोई ध्यान नहीं देता.
वह पूछती हैं, "हमें गुस्सा आता है जब पता चलता है कि बलात्कारी ने पीड़िता के कपड़ों पर टिप्पणी की है और उसे बलात्कार करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया है. लेकिन हम इससे इतने भयभीत क्यों होते हैं? हमें इस पर अचरज क्यों होता है कि हम हर दिन जिस व्यवहार को सामान्य बताते हैं वही बढ़ते बढ़ते कहीं चरम रूप में ज़ाहिर होता है."
डॉ. मधुमिता ने बताया, "जब मैं बलात्कारी से बातचीत पूरी कर लेती थी, तो उसकी सामाजिक शब्दावली पर ध्यान देती थी. अपराध करने के लिए बनाया गया उसका बहाना, उस सामाजिक कथन को बताता है जिसमें वह बड़ा हुआ होता है."
डॉ. मधुमिता अब भारत में बलात्कारियों को लेकर सोच बदलने वाली पुनर्वास कार्यक्रम से जुड़ी हैं.
उन्होंने बताया, "मैं भारत में यौन अपराधियों के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम देखना चाहती हूं जो बलात्कार से जुड़े मिथकों और महिलाओं के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण को बदलने के लिए अन्य गतिविधियों के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर सत्र आयोजित हों."
"सुबह जगने से लेकर रात सोने तक, हर वक्त मेरे दिमाग़ में यही चल रहा होता है. इससे मुझे काफ़ी उम्मीद मिलती है." (bbc.com)