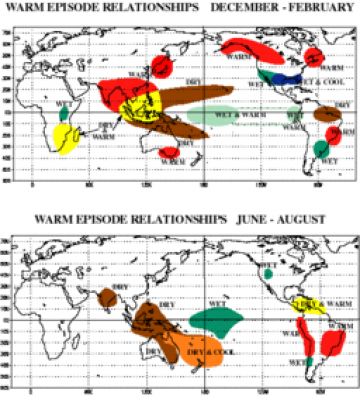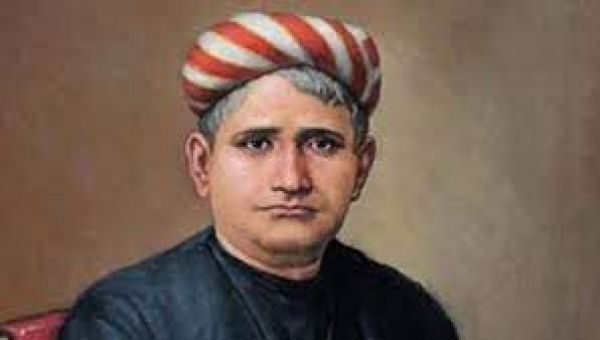सामान्य ज्ञान

भारत में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को महाभियोग के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग यानी इमपीचमेंट शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है पकड़ा जाना। इस शब्द की जड़ें भले ही लैटिन भाषा से निकलती हों, परंतु इस वैधानिक प्रक्रिया की शुरूआत ब्रिटेन से मानी जाती है। यहां 14वीं सदी के उत्तरार्ध में महाभियोग का प्रावधान किया गया था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4)127 में सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के जज को हटाए जाने का प्रावधान है। महाभियोग के जरिए हटाए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण जज इन्क्वायरी एक्ट 1968 द्वारा किया जाता है। किसी जज को हटाए जाने के लिए जरूरी महाभियोग की शुरुआत लोकसभा के 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों के सहमति वाले प्रस्ताव से की जा सकती है। ये सदस्य संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी को जज के खिलाफ महाभियोग चलाने की अपनी मांग का नोटिस दे सकते हैं।
प्रस्ताव पारित होने के बाद संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा तीन जजों की एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश और एक कानूनविद को शामिल किया जाता है। यह तीन सदस्यीय समिति संबंधित जज पर लगे आरोपों की जांच करती है। जांच पूरी करने के बाद यह समिति अपनी रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी को सौंपती है। आरोपी जज जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, को भी अपने
पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट में अगर आरोपी जज पर लगाए गए दोष सिद्ध हो रहे हैं तो पीठासीन अधिकारी मामले में बहस के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सदन में वोट कराते हैं। किसी जज को तभी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई मतों (उपस्थिति और वोटिंग) से यह प्रस्ताव पारित हो जाए। हालांकि अभी तक देश की न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा मौका नहीं आया है।
क्या है मध्यस्थता और सुलह (संशोधन विधेयक)
लोकसभा ने 17 दिसंबर 2015 को ध्वनि मत से मध्यस्थता और सुलह (संशोधन विधेयक) 2015 को पारित कर दिया। इस विधेयक में मामलों के शीघ्रता से निपटारे के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया को और अधिक सुलभ, लागत प्रभावी और उपयुक्ते बनाने के प्रावधान हैं. यह भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिसक मध्यस्थात केन्द्र बनाने की सुविधा भी प्रदान करेगा।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने पूर्व प्रचारित अधिनियम, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित और इससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2015 को इस अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दी थी और इसकी सिफारिश राष्ट्रपति के समक्ष भेज दी थी।