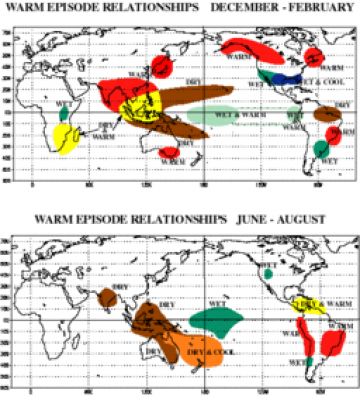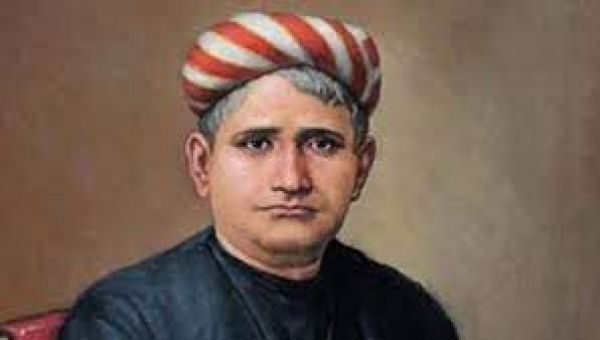सामान्य ज्ञान

तुलसी का औषधीय प्रयोग काफी होता है। तुलसी का पौधा प्राय: सभी गर्म प्रदेशों में अपने आप उत्पन्न होता है। कुछ स्थानों पर कृष्ण और श्वेत तुलसी ही श्यामा और रामा के नाम से जानी जाती है। तुलसी की अनेक किस्में हैं जिनमें से देश-भेद के हिसाब से पांच प्रमुख हैं- कृष्णा तुलसी, दद्रिह तुलसी, राम तुलसी, बाबी तुलसी और तुकाशमीय।
कृष्णा तुलसी लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती है। कंठ विकार, कफ विकार, एकांतज्वर, फुप्फुस विकार, नासिका व्रण, व्रण कृमि, कर्णशूल ,मूत्र रोग, चर्मरोग आदि अनेक रोगों में इसका उपयोग किया जाता है।
दद्रिह तुलसी अधिकांशत: बंगाल, नेपाल, चटगांव, महाराष्ट्र, आदि प्रांतों में होती है। इसके उपयोग से अपानवायु की शुद्धि होती है, कंठ शोष दूर होता है और कंठ आद्र्र बनता है। विशेषत: बलगम तरल बनता है और हाथ-पैर का शोथ और संधिवात मिटता है।
रामतुलसी चीन, ब्राजील, पूर्वी नेपाल के अलावा बंगाल, बिहार , चटगांव और दक्षिण भारत के प्रांतों में भी देखने को मिलती है। इसकी पत्तियों में अधिक सुगंध होती है। इसका उपयोग कुष्ठ आदि बीमारियों में किया जाता है। स्त्री-पुरषों के रोगों पर और शरीर के बाएं-दाएं भागों के रोगों में इसकी एक विशिष्ट किस्म की तुलसी का प्रयोग लाभदायक होता है।
बाबी तुलसी भारत वर्ष के उष्ण और साधारण उष्ण वाले क्षेत्रों में विशेषकर पंजाब से त्रावणकोर तक दिखाई देती है। बंगाल, बिहार, अवध, ईरान आदि प्रदेशों में भी यह तुलसी पैदा होती है। यह तुलसी स्वाद में कटु, उष्ण रुचिकर, अग्निप्रदीपक, हृदय के लिए लाभकारी, रुक्ष, पचने में हल्की होती है। यह कफ- वात, नेत्र रोग, रक्त विकार, दाह, कृमि, विषविकार, खुजली, वमन, कर्ण-शूल, कुष्ण और ज्वर को दूर करने वाली होती है। यह प्रसूता संबंधी रोगों को भी दूर करती है। इसके बीजों को पानी में भिगोकर या फिर रोटी के साथ मिलाकर खाया जाता है।
तुकाशमीय तुलसी भारत में पश्चिम के अंचलों में पाई जाती है। ईरान में भी तुलसी की यह किस्म देखने को मिलती है। इसका उपयोग गले से अंत:भाग, आमांश और कुष्ठ रोग में किया जाता है। इसके सेवन से शरीर की दुर्बलता दूर होती है।
राग हिंडोल
राग हिंडोल या राग हिंदोल का जन्म कल्याण थाट से माना गया है। इसमें मध्यम तीव्र तथा निषाद व गंधार कोमल लगते हैं। ऋषभ तथा पंचम वर्जित है। इसकी जाति ओड़व ओड़व है तथा वादी स्वर धैवत व संवादी स्वर गांधार है। गायन का समय प्रात:काल है। शुद्ध निषाद, रिषभ और पंचम इस स्वर इसमें वर्ज्य हैं। तीव्र मध्यम वाला यह एक ही राग है जिसको प्रात:काल गाया जाता है। अन्य सभी तीव्र मध्यम वाले रागों का गायन समय रात्रि में होता है।
राग चिकित्सा में इस राग को जोड़ों के दर्द के लिए लाभकारी माना गया है।