आजकल

दो दिन पहले एक खबर आई कि अपने पिता की बीमारी से परेशान एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। और इस खबर से कुछ घंटों के भीतर ही बीमार पिता चल बसा। एक साथ दोनों की अर्थी निकली। अभी उस खबर की स्याही सूखी भी नहीं थी कि आज पास से ही एक दूसरी खबर आई कि पिता की मौत से सदमे में आई बेटियों ने रेलवे पटरी पर जाकर जान देने की कोशिश की, एक बहन मौके पर ही खत्म हो गई, और दूसरी बुरी तरह से जख्मी हालत में अस्पताल में है। अब इन दोनों ही खबरों में खुदकुशी करने वाले लोग नौजवान हैं। जाहिर है कि इन्होंने अपने परिवार में, आसपास में कुछ तो मौतें देखी हुई होंगी। इसके बावजूद अपने पिता की बीमारी या मौत को बर्दाश्त कर पाना इनके लिए इतना भारी था।
कैसे कुछ लोग इतने कमजोर दिल के होते हैं कि पिता की बीमारी या मौत को बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाएं? अगर माता-पिता अपने किसी औलाद के लिए ऐसा महसूस करें, तो भी समझ पड़ता है कि वे जिंदा हैं, और उनकी अगली पीढ़ी इस तरह चल बसी। औलाद के चले जाने का गम मां-बाप के चले जाने के गम से अधिक शायद इसलिए भी होता होगा कि प्राकृतिक जीवनचक्र के मुताबिक तो मां-बाप ही जल्दी बूढ़े होते हैं, और जल्दी जाते हैं। इसलिए औलाद का जाना जाहिर तौर पर अधिक तकलीफ का होता है।
क्या लोगों की मौत को समझने के लिए अलग-अलग धर्मों की नसीहतें कुछ अलग-अलग हद तक लोगों को तैयार करती हैं? क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति लोगों को मजबूत बना देती है कि वे तकलीफ झेल सकें? क्या बहुत गरीब परिवारों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की मौतें वक्त के पहले होती हैं, और गरीबी भी लोगों को ऐसी तकलीफ झेलने के लिए कुछ अधिक हद तक तैयार करती है? हमारे पास इसका कोई सीधा-सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि अलग-अलग धर्मों के मानने वालों के बीच अपने धार्मिक संस्कारों और मान्यताओं की वजह से मृत्यु को लेकर स्वर्गवासी होने, या मुक्ति पा लेने, मोक्ष पा लेने जैसी अलग-अलग सोच रहती होगी। और शायद नास्तिक लोग इन तमाम मामलों में अधिक प्राकृतिक या वैज्ञानिक नजरिया रखते होंगे, और हो सकता है कि वे भी दिमागी रूप से आसपास के लोगों की मौत देखने के लिए कुछ अधिक हद तक तैयार रहते हों।
समाज में लोगों को एक-दूसरे को मजबूती देना भी आना चाहिए। यह तो अधिकतर लोगों को समझ में आ जाता है कि बीमारी बीमार को कब मौत के करीब पहुंचाती है, और वैसे में मौत के लिए तैयार रहने का हौसला परिवार के लोगों को देने वाले लोग भी रहना चाहिए। रिश्तेदार, पड़ोस के लोग, या कि दोस्त इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और जाने वाले के साथ चले जाने की निराशा से आसपास के लोगों को उबार सकते हैं। हम तो बहुत मामूली समझ के साथ इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता बेहतर तरीके से ऐसी नौबत से निपटना बता सकते हैं, दिक्कत महज यह है कि ऐसे परामर्शदाता गिनती के हैं, और ऐसी निराशा कुछ या अधिक हद तक बड़ी आम है।
बहुत से लोगों को अपने परिवार के लोगों को मृत्यु के डर से, और अकेले रह जाने की आशंका से जूझना सिखाना चाहिए। शायद किशोरावस्था के आने तक सभी लोग इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि वे जीवन और मृत्यु के इस सिलसिले को समझ सकें कि किसी भी काबू से परे यह सिलसिला हमेशा चलता है, और नई पीढ़ी के आने के बाद एक वक्त पुरानी पीढ़ी की रवानगी धीरे-धीरे शुरू हो जाती है। लोगों को अपने जाने का वक्त आने के पहले ही उसकी चर्चा शुरू करना चाहिए, अपनी वसीयत के बारे में बात करनी चाहिए, गुजरने के बाद देहदान की बात करनी चाहिए, किसी ब्रेन-डेथ की नौबत आने पर अंगदान की बात करनी चाहिए, उसके फॉर्म भरने चाहिए, जब कभी ऐसी खबरें कहीं आएं, तो परिवार के लोगों को दिखानी चाहिए कि किसी गुजरे हुए के अंगों से कितने लोगों की जिंदगी मिली है। आज का चिकित्सा विज्ञान मौत की तकलीफ को दवाओं से मरीज के लिए तो कम करता ही है, देहदान और अंगदान जैसी चीजों से वह ऐसी चर्चा का मौका भी देता है कि परिवार के लोग परिवार में मौत के लिए दिल-दिमाग से बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।
कम से कम बौद्ध धर्म का तो हमें याद पड़ता है जिसमें मृत्यु को दुख नहीं माना जाता, और इसे जीवनचक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। बौद्ध मानते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, इससे डरना नहीं चाहिए, और मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। इसलिए मृत्यु को शांति और खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। महाराष्ट्र के बौद्ध लोगों के कम से कम कुछ समुदायों में यह चलन है कि अंतिम यात्रा के दौरान बैंडबाजे के साथ लोग नाचते-गाते अर्थी ले जाते हैं। इस तरह धर्म की सोच और धार्मिक संस्कार भी लोगों को मौत का सामना करने, या कि परिजनों के गुजरने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करते हैं।
दो दिनों में ऐसी दो घटनाओं को अपने एकदम आसपास देखकर तकलीफ हो रही है। नौजवान लोग भी अगर माता-पिता के जाने के लिए तैयार न हों, तो नाबालिग छोटे बच्चों के बारे में क्या कहा जा सकता है? इस बारे में सोचते हुए एक घटना याद आती है कि किस तरह कुछ बरस पहले एक टीवी चैनल पर समाचार पढ़ रही एक एंकर को यह समाचार पढऩा पड़ा कि उसके पति की एक सडक़ हादसे में मौत हो गई है, और बुलेटिन शुरू होने के बाद मिली इस खबर को पढ़ते हुए भी उसने आपा नहीं खोया, काम छोडक़र नहीं उठी।
लोगों को खुद होकर आसपास की किसी मौत की खबर पर अपने परिवार के भीतर भी ऐसी नौबत की चर्चा करनी चाहिए। दूसरों की मिसाल देकर यह मजबूती लानी चाहिए कि किसी के चले जाने के बाद भी बाकी लोग उसे याद करते हुए भी कुछ बेहतर बनकर दिखा सकते हैं, बजाय खुदकुशी करने के, या कि निराश होने के। अंग प्रत्यारोपण की हसरत जाहिर करना भी परिवार के लोगों को अपरिहार्य मृत्यु के बारे में बेहतर तैयार कर सकता है। आपके जाने के बाद पीछे रह गए लोग आपके पास पहुंचने की हड़बड़ी में कुछ ऐसा न कर बैठें, यह भी आपकी ही जिम्मेदारी रहती है। मृत्यु की चर्चा हमेशा ही अप्रिय और विचलित करने वाली हो ऐसा जरूरी तो है नहीं, ऐसी चर्चा अपने जीते-जी अधिक तैयारी करवाने वाली भी हो सकती है।





.jpg)
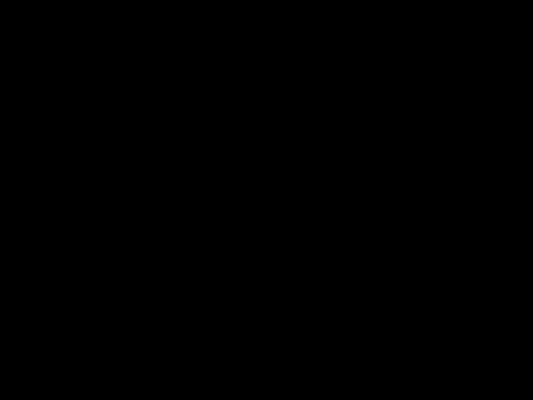



.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
