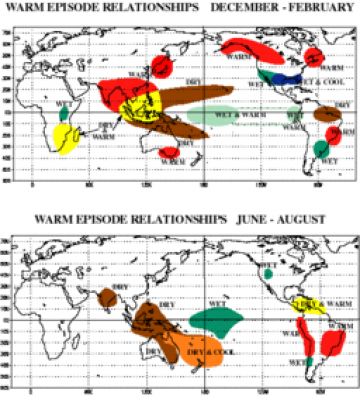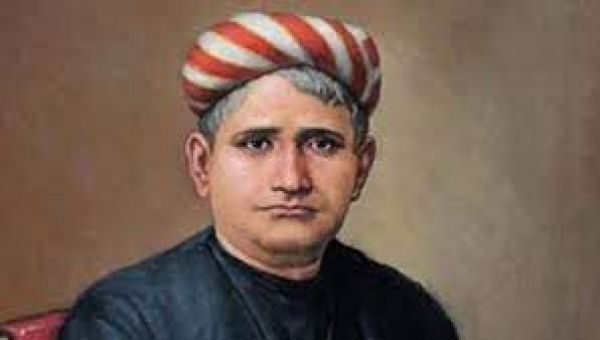सामान्य ज्ञान

हिन्दी साहित्य में कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। रसखान को रस की ख़ान कहा जाता है। इनके काव्य में भक्ति, श्रृगांर रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं।
रसखान कृष्ण भक्त हैं और प्रभु के सगुण और निर्गुण निराकार रूप के प्रति श्रृध्दालु हैं। रसखान के सगुण कृष्ण लीलाएं करते हैं। यथा- बाललीला, रासलीला, फागलीला, कुंजलीला आदि। उन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधी में इन असीमित लीलाओं का बहुत सूक्ष्म वर्णन किया है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने जिन मुस्लिम हरिभक्तों के लिये कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिन्दू वारिए उनमें रसखान का नाम सर्वोपरि है। सैय्यद इब्राहीम रसखान का जन्म उपलब्ध स्रोतों के अनुसार सन् 1533 से 1558 के बीच कभी हुआ होगा। अकबर का राज्यकाल 1556-1605 है, ये लगभग अकबर के समकालीन हैं। जन्मस्थान पिहानी कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के समीप है। कुछ और लोगों के मतानुसार यह पिहानी उत्तरप्रदेश के हरदोई जि़ले में है। मृत्यु के बारे में कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलते हैं। रसखान ने भागवत का अनुवाद फारसी में भी किया।
मथुरा (उप्र) के महावन में रसखान की समाधि बनी हुई है।
भारत में छपाई
छपाई एक कलाकृति है। यह प्रारंभिक चित्र के समान प्रकार में लगभग विविधता की अनुमति देती है। भारत में छपाई का इतिहास 1556 से शुरू होता है। इस युग में गोवा में पुर्तगालियों ने छपाई की मशीन लगाई। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखने पर यह ज्ञात होता है कि कला की यह विधा ग्यूटेर्नबर्ग कीबाइबल की एक शताब्दी बाद भारत में आई। प्रसिद्ध कालाकार थोमस डैनियल (1749-1840) तथा विलियम डैनियल (1769-1837) ने ओरियन्टल सिनरी शीर्षक से कलमकारी की 6 श्रृंखलाओंको प्रस्तुत किया। 1786 में डैनियल ने ट्वेल्व व्यूज ऑफ कलकत्ता शीर्षक वाले एक रंग की कलमकारी का एलबम प्रकाशित किया। यह पहला मौका था जब भारत में लिथोग्राफी एक ही कागज पर छपाई की संभावना की तलाश की गई। 1822 में फ्रांसीसी कलाकार डी. सैविगनैक ने एक ही कागज पर लिथोग्राफी रूप में छपाई की।
1870 के दशक में कैलेन्डर, पुस्तक तथा अन्य प्रकाशनों के लिए छपी हुई तस्वीरों की मांग बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कागज परछपाई की लोकप्रियता बढ़ी। आगे पूरे भारत में अनेक आर्ट स्टुडियो तथा छापेखाने तैयार हुए। कोलकाता के शोवा बाजार और चितपुर बट-ताला को 19वीं शताब्दी के प्रमुख छपाई केंद्र के रूप में देखा गया। मुंशी नवल किशोर ने 1858 में लखनऊ में नवल किशोर प्रेस तथा बुक डिपो की स्थापना की। इसे एशिया में सबसे पुराने छपाई और प्रकशन प्रतिष्ठान के रूप में मान्यता मिली और यहीं स्टोनब्लॉक के साथ अखबार और किताबों की छपाई होने लगी। इसके अतिरिक्त 19वीं शताब्दी के अंत में राजा रवि वर्मा ने मुंबई केघाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस स्थापित किया। रवि वर्मा के प्रेस को प्रसिद्धि मिली और उनके अनेक धार्मिक और धर्म निस्पेक्ष चित्रों की कॉपियों तैयार हुई और आम जनता के लिए तैल चित्र रूप में इनकी छपाई हुई।
20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में अबनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर तथा समरेंद्रनाथ टैगोर द्वारा छपाई को सृजनात्मक माध्यम का रूप दिया गया। इन तीनों ने सामूहिक रूप से बिचित्र क्लब की स्थापना की ताकि कटी हुई लकड़ी तथा कटे हुए पत्थरों से चित्रकारी और छपाई हो सके। इस क्लब के एक अन्य प्रमुख व्यक्ति थे मुकुलचंद्र डे,जिन्हें 1916 में रवींद्रनाथ टैगोर ने जेम्स ब्लाइंडिंग स्लोन से नक्काशी तकनीक सीखने के लिए अमेरिका भेजा। 1921 में शांति निकेतन में नंदलाल बोस ने कला भवन की स्थापना की। इसके साथ भारत में छपाई कला लोकप्रिय हुई। 1924 में चीन और जापान की यात्रा से वह चीनी घिसाई तथा जापानी रंग वाली लकड़ी से छपाई का माध्यम लेकर आए। इस कारण कला भवन के विद्यार्थियों ने सुदूर पूर्व की मौलिक छपाई के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। 1930 से 40 के बीच बिनोदबिहारी मुखर्जी तथा रामकिंकर बैज ने इस माध्यम का उपयोग किया।
के. जी. सुब्रह्मण्यम ने अपनी कला में लिथोग्राफी, कलमकारी और सेरीग्राफी को शामिल किया। 1970 से लक्ष्मा गौड़, देवराज डाकोजीतथा डीएलएन रेड्डी ने हैदराबाद, आरएम पलनियप्पन तथा आरपी भास्करण ने चेन्नई में तथा चित्त प्रसाद भट्टाचार्य अतिन बसाक में तथा अमिताभ बनर्जी ने कोलकाता में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। अहमदाबाद में रॉबर्ट राउसनबर्ग तथा नई दिल्ली के एनजीएमए की छपाई संग्रह से पूरी दुनिया में अपनाए गए विभिन्न व्यवहारों की छाप दिखाई दी। 1990 के दशक में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना के साथ आशा की नई किरण जागी। छपाई के क्षेत्र में डिजीटल टेक्नोलॉजी तथा मेकेनाईज्ड सॉफ्वेटर के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ।