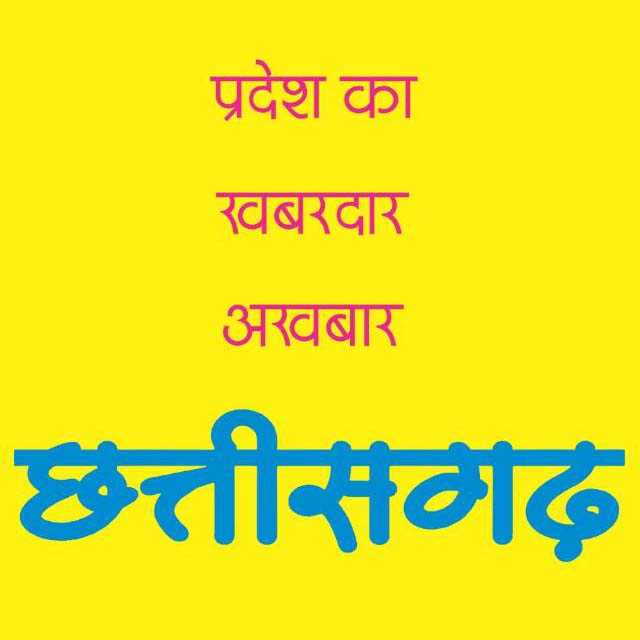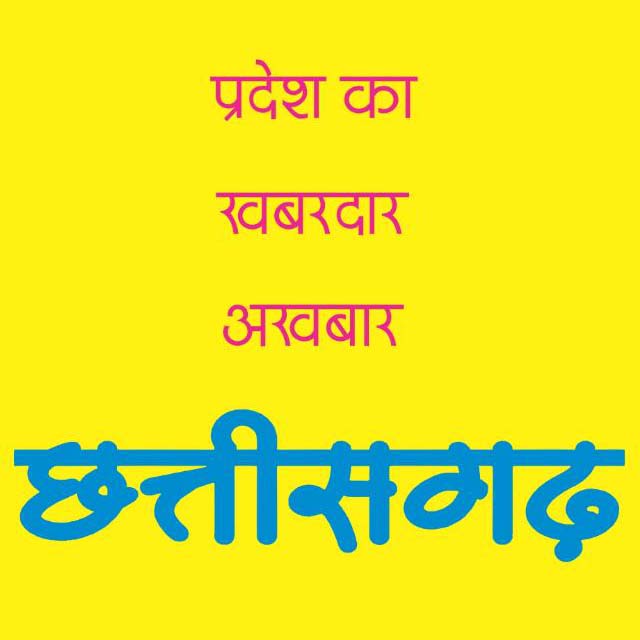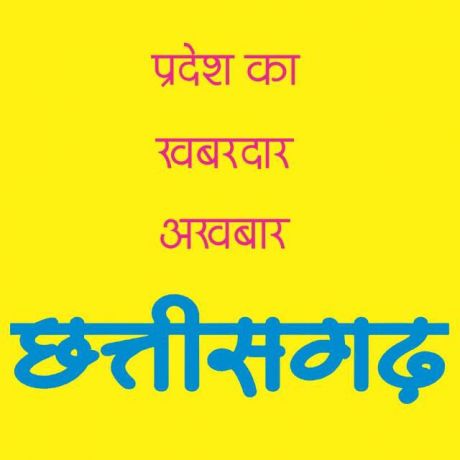अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख बातें
- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित दिया
- शरीफ़ ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ उत्पीड़न का अभियान जारी है
- पाकिस्तानी पीएम ने कहा- भारत के मुसलमान भेदभावपूर्ण क़ानून, हिजाब बैन, मस्जिदों पर हमले और लिंचिंग का शिकार बन रहे
- उन्होंने कहा पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहता है
- शहबाज़ ने अपने देश में आई भयंकर बाढ़ का ज़िक्र भी किया और राष्ट्रपति बाइडन का धन्यवाद भी कहा
- अमेरिका के न्यूयॉर्क में जारी संयुक्त राष्ट्र की 77वीं आम सभा में शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने अपने देश में आई बाढ़ से लेकर भारत, इसराइल, फ़लस्तीन, इस्लामोफ़ोबिया और कश्मीर तक पर अपनी बात रखी है.
शहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में आई भारी बाढ़ से अपनी बात की शुरुआत करते हुए उन्होंने भारत से शांति तक पर अपनी बात रखी.
भारत पर बोलते हुए शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, ''भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ उत्पीड़न का आधिकारिक रूप से प्रायोजित अभियान चल रहा है जो कि इस्लामोफ़ोबिया का सबसे ख़राब रूप है. मुसलमान भेदभावपूर्ण क़ानून और नीतियों, हिजाब बैन, मस्जिदों पर हमले और हिंदुओं की भीड़ की लिंचिंग के शिकार बन रहे हैं.''
शहबाज़ शरीफ़ ने इसके बाद भी भारत के ख़िलाफ़ बोलना जारी रखा. उन्होंने कहा कि वो ख़ासतौर पर भारत के कुछ अतिवादी समूहों को लेकर चिंतित हैं जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ 'जनसंहार' की अपील की हुई है.
उन्होंने कहा, "इस्लामोफ़ोबिया अब एक वैश्विक तथ्य है. 9/11 के बाद से मुसलमानों के ख़िलाफ़ डर, उनको लेकर शक और उनके साथ भेदभाव महामारी के अनुपात में बढ़ा है."
"पाकिस्तान सभी तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा करता है. आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है. यह रूढ़िवाद, ग़रीबी, अभाव, अन्याय और अज्ञानता और निहित स्वार्थों के ज़रिए फैलाया गया होता है."
इसके बाद शहबाज़ शरीफ़ ने एक बार फिर वही बात कही जो इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान कहते रहे हैं. शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि 'पाकिस्तान आतंकवाद से मुख्य तौर पर पीड़ित रहा है. बीते दो दशकों में हमने आतंकी हमलों की वजह से 80 हज़ार लोगों की जान और 150 अरब डॉलर का आर्थिक नुक़सान उठाया है.'
भारत पर और क्या बोले
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अपने आधे घंटे के भाषण में शांति और कश्मीर समाधान का ज़िक्र भी किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहता है, जिसमें भारत भी शामिल है. इसके बाद उन्होंने यह भी जोड़ा की दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता कश्मीर विवाद के समाधान पर निर्भर करती है.
उन्होंने कहा, ''इस लंबे समय से चले आ रहे (कश्मीर) विवाद के केंद्र में कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार न देना है. कश्मीरियों के ख़िलाफ़ भारत लगातार दमन का अभियान चला रहा है, जिसमें बराबर तेज़ी जारी है. कश्मीरियों का कई तरीक़ों से दमन हो रहा है, जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशिल किलिंग्स, क़ैद करना, हिरासत में उत्पीड़न और मौत, अंधाधुंध बल प्रयोग, पैलेट गन से कश्मीरी युवाओं को जानबूझकर निशाना बनाना और पूरे समुदाय को सामूहिक दंड देना शामिल है.''
शहबाज़ शरीफ़ ने भारत पर आरोप लगाया कि वो अवैध डेमोग्राफ़िक बदलावों के ज़रिए मुस्लिम बहुल जम्मू-कश्मीर को हिंदू बहुल क्षेत्र में तब्दील कर रहा है.
पाकिस्तानी पीएम ने कहा, "पाकिस्तान के लोग हमारे कश्मीरी भाई-बहनों के साथ हमेशा से उनके साथ एकजुटता से खड़े रहे हैं और वो तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत आत्म-निर्णय का अधिकार नहीं मिल जाता."
इसके बाद शहबाज़ शरीफ़ ने भारत को नसीहत देते हुए कहा, 'भारत को अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करना चाहिए और 15 अगस्त 2019 को लिए गए अवैध फ़ैसले को पलटते हुए शांति और बातचीत के रास्ते पर चलना चाहिए.''
हालांकि भारत कई बार यह दोहरा चुका है कि जम्मू-कश्मीर उसका अंदरूनी मामला है और वो उसका हमेशा से अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा.
भारत का कहना है कि उसके पाकिस्तान से तब तक संबंध सामान्य नहीं रह सकते हैं, जब तक कि उसका वातावरण आतंक, हिंसा और दुश्मनी से मुक्त नहीं होगा.
भारत ने दिया जवाब
शहबाज़ शरीफ़ के भाषण के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत अपना जवाब दिया है. भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन के फ़र्स्ट सेक्रेटरी मिजिटो विनिटो ने यह जवाब दिया.
उन्होंने कहा कि 'यह बहुत ही अफ़सोसजनक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के ख़िलाफ़ झूठे आरोप लगाने के लिए इस महासभा के मंच का इस्तेमाल किया है. उन्होंने अपने ही देश के कुकर्मों को दबाने और भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई को सही ठहराने के लिए ऐसा किया है. एक सरकार जो अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहती है वो कभी भी सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगी, न ही भयानक मुंबई आतंकी हमलों के योजना बनाने वालों को पनाह देगी. और वो तब उनके होने के बारे में बताते हैं जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दबाव होता है.'
"भारतीय उपमहाद्वीप में शांति, सुरक्षा और प्रगति की इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब सीमापार आतंकवाद ख़त्म हो, जब सरकारें अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अपने लोगों के साथ साफ हों, जब अल्पसंख्यकों को सताया न जाए और कम से कम हम इन असलियत को इस महासभा से पहले से जानते हैं."
शहबाज़ ने संयुक्त राष्ट्र में और क्या-क्या कहा
- मुझे लगता है कि भारत को यह संदेश समझना चाहिए कि दोनों देशों के पास बहुत सारे हथियार मौजूद हैं लेकिन युद्ध कोई विकल्प नहीं है.
- केवल शांतिपूर्ण बातचीत ही इन मुद्दों को सुलझा सकती है ताकि आने वाले समय में दुनिया और शांतिपूर्ण बन सके.
- हम अपने भारतीय समकक्षों से कहना चाहते हैं कि बैठकर बात करें ताकि भविष्य का रास्त साफ़ हो और हमारी पीढ़ियां पीड़ित न हों और हम अपने संसाधनों को दुखों को कम करने में ख़र्च करें.
- भारत को एक निर्माणकारी जुड़ाव के लिए वातावरण बनाने की ज़रूरत है. हम पड़ोसी हैं और हम हमेशा रहेंगे. यह हमारी इच्छा है कि हम शांति में रहें या एक-दूसरे से लड़ते रहें. 1947 से अब तक तीन युद्ध हो चुके हैं. नतीजा यह हुआ कि दोनों तरफ सिर्फ बदहाली, ग़रीबी और बेरोज़गारी बढ़ी है.
- भारत और पाकिस्तान को अब और हथियारों को ख़रीदने और तनाव को बढ़ाने में अपने और संसाधन नहीं ख़र्च करने चाहिए.
- पाकिस्तान की अभी प्राथमिकता तेज़ी से आर्थिक विकास सुनिश्चित करना और लाखों लोगों को ग़रीबी और भुखमरी से बाहर निकालना है.
- बीते 40 दिनों और 40 रातों से हम पर बाढ़ का क़हर जारी है जिसने शताब्दी पुराने मौसम रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है.
- 3.3 करोड़ लोग जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं वो स्वास्थ्य ख़तरों की चपेट में हैं जिनमें 6.5 लाख महिलाओं ने तंबुओं में बच्चों को जन्म दिया है.
- पाकिस्तान ने जलवायु परिवर्तन के असर का इतना कठोर और विनाशकारी उदाहरण कभी नहीं देखा. पाकिस्तान की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई है.
- मेरे लोगों को इतने बड़े स्तर के जलवायु परिवर्तन की क़ीमत क्यों अदा करनी चाहिए.
बाइडन और शहबाज़ की मुलाक़ात
वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से मुलाक़ात की है जिस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाने के लिए उनका शुक्रिया कहा है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा में आए विश्व के नेताओं के लिए राष्ट्रपति बाइडन ने एक रिसेप्शन का आयोजन किया था जिस दौरान दोनों नेताओं की मुलाक़ात हुई.
शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालाय ने बयान जारी किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाढ़ में मारे गए हज़ारों लोगों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान कहा कि वो इस कठिन मानवीय संकट से निकलने के लिए मदद जारी रखेंगे.
पाकिस्तान में भाषण की चर्चा
संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए शहबाज़ शरीफ़ के भाषण के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस भाषण को लेकर बहस तेज़ हो गई है.
शहबाज़ शरीफ़ के समर्थक जहां उनके भाषण के लिए उनकी दाद दे रहे हैं वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के समर्थक उनके भाषण की आलोचना कर रहे हैं.
इमरान ख़ान की पार्टी पीटीआई की महिला विंग की अध्यक्ष कंवल शौज़ाब ने इमरान ख़ान के पिछले भाषण के दौरान यूएन के हॉल की कुर्सियां और शहबाज़ शरीफ़ के भाषण के दौरान ख़ाली कुर्सियों की तस्वीरें ट्वीट की हैं.
कंवल ने लिखा है, "जब मुस्लिम उम्मत का सच्चा नेता बोलता है तो दुनिया के बड़े-बड़े राजा बैठकर सुनते हैं."
अनस हफ़ीज़ ने ट्वीट किया कि, "इमरान ख़ान ने जनरल असेंबली में कश्मीर का मामला कुछ इस अंदाज़ में पूरी दुनिया के सामने उठाया था."
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के भारत पर इतने आरोप लगाने के बाद अब भारत की ओर से प्रतिक्रिया भी आ गई है. वहीं शनिवार को भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण देंगे. (bbc.com/hindi)
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र आम सभा (यूएनजीए) की 77वीं बैठक चल रही है. दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेने पहुँचे हैं.
यूएनजीए में दुनिया के आठ देशों ने भारत का ज़िक्र किया.
1. तुर्की के राष्ट्रपति रैचेप तैय्यप अर्दोआन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत-पाकिस्तान संबंधों का ज़िक्र किया. अर्दोआन ने कहा कि वह कश्मीर में उचित और स्थायी शांति की उम्मीद करते हैं.
तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, ''75 साल पहले भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु देश बने लेकिन दोनों मुल्कों के बीच शांति और एकता स्थापित नहीं हो पाई है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हम उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर में उचित और स्थायी शांति की स्थापित हो.''
2 . फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को दोहराया.
उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में मुलाक़ात का ज़िक्र करते हुए कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी सही थे जब उन्होंने कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है. यह पश्चिम से बदला लेने के लिए या पूर्व के ख़िलाफ़ पश्चिम का विरोध करने के लिए नहीं है. ये वक़्त है कि सभी समान संप्रभु देश एक दूसरे का साथ दें ताकि वो सामने कड़ी चुनौतियों से निपट सकें.’’
3. गुयना के राष्ट्रपति इरफ़ान अली ने भारत से निर्यात बंद होने की वजह से खाने की चीज़ें महंगी होने का मुद्दा उठाया.
4. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और चीज़ों के निर्यात को लेकर भारत का ज़िक्र किया.
5. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस ने भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ संबंध मज़बूत करने पर ज़ोर दिया.
उन्होंने अपने भाषण में कहा- ‘‘हम भारत, इसराइल, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे लोकतांत्रिक देशों से अपने संबंध गहरे कर रहे हैं. हम इंडो-पैसिफ़िक और गल्फ़ में अपनो मित्रों से नए सुरक्षा संबंध बना रहे हैं.’’
6. जर्मनी के चांसलर ओलाफ़ शॉल्त्स ने भारत और G7 की अध्यक्षता का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हमने जी7 के रूप में अपनी चर्चाओं में अफ्रीकी संघ और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के अध्यक्षता वाले देशों के साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया है.’’
7. पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के विस्तार की भारत की मांग का समर्थन किया.
8. वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत पर कई आरोप लगाए. (bbc.com/hindi)
नयी दिल्ली, 24 सितंबर। ‘इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी’ (आईएमएसडी) नामक संस्था ने ईरान में ड्रेस-कोड का कथित तौर पर उल्लंघन करने वाली युवती की पुलिस हिरासत में मौत को लेकर वहां के “प्रगति विरोधी” और “तानाशाही” कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई है।
ईरान पुलिस ने बीते सप्ताह तेहरान में पहनावे से संबंधित कानून का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोप में 22 वर्षीय महसा अमीनी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस का कहना है कि अमीनी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई थी, लेकिन युवती के परिवार ने पुलिस के बयान पर संदेह जताया है।
आईएमएसडी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, “आईएमएसडी ईरान के प्रगति विरोधी और तानाशाही कानूनों तथा नागरिकों के अधिकारों के दमन की कड़ी निंदा करता है।”
समूह ने कहा कि 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में महज सिर न ढंकने के लिए किसी की हत्या कर देना एक बर्बर कृत्य है।
बयान में कहा गया है, “इसके साथ ही भारतीय मौलानाओं द्वारा ईरानी महिलाओं के अधिकारों का समर्थन नहीं करने पर भी सवाल खड़े होते हैं। भारत में हिजाब विवाद के परिप्रेक्ष्य में इससे नए तर्क पैदा होते हैं।”
आईएमएसडी के बयान का लगभग सौ हस्तियों ने समर्थन किया है। इनमें स्वतंत्रता सेनानी जी जी पारिख, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, जीनत शौकत अली, योगेंद्र यादव और तुषार गांधी शामिल हैं। (भाषा)
दमिश्क/बेरूत, 24 सितंबर | सीरियाई तट के पास एक नाव के डूबने से कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री हसन अल-गबाश ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि सीरिया के तटीय शहर टार्टस के अल-बासेल अस्पताल में नाव के डूबने के बाद 20 लोगों को बचा लिया गया है और इलाज के लिए भेज दिया है।
सी पोर्ट्स के सीरियाई जनरल डायरेक्टर समीर कोब्रोस्ली ने शुक्रवार को बचाए गए लोगों की गवाही का हवाला देते हुए कहा, नाव मंगलवार को लेबनान से अवैध प्रवासियों को 'अज्ञात गंतव्यों' पर ले जा रही थी।
कोब्रोस्ली ने कहा कि सीरिया के अधिकारियों द्वारा शुरू किए गए एक खोज और बचाव अभियान के दौरान शुक्रवार को 31 शव मिले।
सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख रामी अब्दुल-रहमान ने शुक्रवार को सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि नाव की मूल क्षमता केवल 30 लोगों की थी, लेकिन उसमें 100 से 150 लोग सवार थे।
लेबनान के लोक निर्माण और परिवहन मंत्री अली हमीह के अनुसार, बचाए गए 20 प्रवासियों में पांच लेबनानी, 12 सीरियाई और 3 फिलिस्तीनी हैं। (आईएएनएस)|
वाशिंगटन, 24 सितंबर | उत्तर कोरिया अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की दक्षिण कोरिया और जापान की आगामी यात्रा के दौरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। प्योंगयांग इस तरह के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। समाचार एजेंसी योनहाप ने शनिवार को बताया कि अधिकारी ने चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया को नया परीक्षण करने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
अधिकारी ने शुक्रवार को हैरिस की अगले सप्ताह की यात्रा के दौरान उत्तर कोरियाई परमाणु परीक्षण की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कहा, "यह संभव है और हमने पहले कहा था कि डीपीआरके परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है।"
डीपीआरके का मतलब डेमोकेट्रिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है।
बताया जा रहा है कि प्योंगयांग कुछ समय से परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है।
अधिकारी ने दक्षिण कोरिया को उसके आधिकारिक नाम से संदर्भित करते हुए कहा, "हमने स्पष्ट किया था कि इस तरह के परीक्षण के परिणामस्वरूप कोरिया गणराज्य और हमारे जापानी सहयोगियों की सुरक्षा के प्रति अमेरिका द्वारा अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी।"
कमला हैरिस 26 सितंबर से जापान की चार दिवसीय यात्रा पर जाने वाली हैं। अधिकारी ने एक टेलीफोनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल के साथ बैठक के लिए 29 सितंबर को दक्षिण कोरिया पहुंचेंगी।
पिछले साल की शुरुआत में पदभार ग्रहण करने के बाद कमला हैरिस की यह जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पहली यात्रा होगी।
यून के अलावा, कमला प्रधानमंत्री हान डक-सू से भी मुलाकात करेंगी। अमेरिकी प्रशासन के अधिकारी के अनुसार, कमला-हान की बैठक 26 सितंबर को टोक्यो में होगी।
उपराष्ट्रपति कमला सियोल की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान एक समूह के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। (आईएएनएस)|
(योषिता सिंह)
संयुक्त राष्ट्र, 24 सितंबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने शुक्रवार को यहां कहा कि पाकिस्तान भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ अमन चाहता है, लेकिन दक्षिण एशिया में स्थायी शांति एवं स्थिरता कश्मीर मुद्दे के उचित और स्थायी समाधान पर निर्भर करती है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए शरीफ ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बदलने के लिए पांच अगस्त, 2019 को भारत के "अवैध और एकतरफा" कदम ने शांति की संभावनाओं को और कमतर किया है और क्षेत्रीय तनाव को भड़काया है।
उन्होंने कहा, “ हम भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ अमन चाहते हैं। दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता, जम्मू- कश्मीर मुद्दे के उचित और स्थायी समाधान पर निर्भर है।”
शरीफ ने कहा, “मेरे ख्याल से यह सही वक्त है जब भारत को यह संदेश साफ तौर पर समझना चाहिए कि दोनों देश हथियारों से लैस हैं। जंग कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ शांतिपूर्ण संवाद ही इन मुद्दों को हल कर सकता है ताकि आने वाले वक्त में दुनिया और ज्यादा शांतिपूर्ण हो जाए।”
शरीफ ने कहा कि नयी दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, जिससे यह दुनिया का सबसे ज्यादा सैन्यीकृत क्षेत्र बन गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आवाम कश्मीरियों के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी।
उन्होंने कहा कि वह ‘‘अपने भारतीय समकक्षों के साथ’’ बातचीत करने के लिए आगे आने को तैयार हैं ताकि "हमारी पीढ़ियों को परेशानी न झेलनी पड़े और हम अपने संसाधनों को अपनी तकलीफों को कम करने और बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं का सामना करने के लिए संरचनाओं के निर्माण पर खर्च कर सकें।”
शरीफ ने कहा, “मैंने विश्व मंच को आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। भारत को उपयोगी वार्ता के लिए माहौल बनाने के वास्ते उचित कदम उठाने चाहिए।”
भारत पाकिस्तान से कई बार कह चुका है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग था, है और रहेगा।
शरीफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को अधिक गोला-बारूद खरीदने और तनाव को बढ़ावा देने की कोशिश में अपने संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
अफगानिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार को अलग-थलग करने से अफगान लोगों की पीड़ा बढ़ सकती है।
शरीफ ने आतंकवाद पर कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से संचालित प्रमुख आतंकवादी समूहों से उत्पन्न खतरे को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता को साझा करता है। (भाषा)
जाग्रेब, 23 सितम्बर | क्रोएशिया की जनसंख्या में पिछले एक दशक में 413,056 व्यक्तियों या 9.64 प्रतिशत की कमी आई है, देश की 2021 की जनगणना के अंतिम परिणामों से यह जानकारी दी गई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, क्रोएशियाई सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, 2021 में देश की जनसंख्या 3,871,833 थी, जिसमें 1,865,129 पुरुष और 2,006,704 महिलाएं थीं।
नतीजे बताते हैं कि देश में क्रोएट्स का हिस्सा 91.63 प्रतिशत है, जो 2011 की जनगणना से 90.42 प्रतिशत था।
इसके बाद 3.20 प्रतिशत पर सर्ब थे, जो 2011 में 4.36 प्रतिशत से नीचे थे, इसके बाद बोस्नियाई (0.62 प्रतिशत), रोमा (0.46 प्रतिशत), इटालियन (0.36 प्रतिशत) और अल्बानियाई (0.36 प्रतिशत) थे, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के अन्य सदस्यों की हिस्सेदारी व्यक्तिगत रूप से 0.30 प्रतिशत से कम है।
सभी क्रोएशियाई काउंटियों में जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जनसंख्या का सबसे बड़ा पलायन पूर्वी क्रोएशिया में, वोकोवर-श्रीजेम काउंटी (20.3 प्रतिशत) में दर्ज किया गया था। (आईएएनएस)|
(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, 22 सितंबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बृहस्पतिवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के सामने पेश हुए और एक महिला न्यायाधीश के खिलाफ की गई अपनी विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगने की इच्छा जताई, जिसके बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।
अदालत द्वारा महिला न्यायाधीश के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए 69 वर्षीय खान को अवमानना की कार्यवाही में आधिकारिक तौर पर अभ्यारोपित किए जाने की संभावना थी।
खान कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अदालत में पेश हुए।
खान की ओर से अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ज़ेबा चौधरी से माफी मांगने की इच्छा व्यक्त करने के बाद, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही स्थगित कर दी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह की अगुवाई वाली बड़ी पीठ कर रही थी जिसमें न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कियानी, न्यायमूर्ति मियां गुल हसन औरंगज़ेब, न्यायमूर्ति महमूद जहांगीर और न्यायमूर्ति बाबर सत्तार शामिल हैं।
जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष ने अपना बयान रिकॉर्ड में रखने की इजाजत मांगी और कहा कि उन्हें पिछली सुनवाई पर भी बोलने से रोक दिया गया था।
पूर्व क्रिकेटर एवं सियातसदां ने अदालत से कहा, “ मैं महिला न्यायाधीश से माफी मांगने को तैयार हूं।” उन्होंने कहा, “अदालत को लगता है कि मैंने हद पार की है। मेरा इरादा महिला न्यायाधीश को धमकाना नहीं था। अगर अदालत कहती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीश के पास जाकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं।”
उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया, "मैं भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करूंगा।" उन्होंने कहा, "अगर मैंने हद लांघी है तो मुझे खेद है।"
मुख्य न्यायाधीश मिनाल्लाह ने खान से कहा, “ व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीश से मिलना, आपका निजी फैसला होगा.. अगर आपको गलती का एहसास हो गया है और आप इसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हैं... तो यह काफी है।”
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री से कहा कि वह एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें उन बातों का विवरण हो जो उन्होंने कही हैं और मामले की सुनवाई तीन अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
राजधानी में 20 अगस्त को एक रैली के दौरान, खान ने अपने सहयोगी शाहबाज़ गिल के साथ की गई बदसुलूकी को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। गिल को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने न्यायाधीश ज़ेबा चौधरी के उस फैसले पर ऐतराज़ जताया था जिसमें उन्होंने गिल को दो दिन की हिरासत में भेजने की पुलिस की गुज़ारिश को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि उन्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
भाषण के कुछ घंटों बाद, खान पर अपनी रैली में पुलिस, न्यायपालिका और राज्य के अन्य संस्थानों को धमकाने के आरोप में आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था।
न्यायमूर्ति आमिर फारूक ने गिल की पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए खान के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया था।
उच्च न्यायालय ने अदालत को संतुष्ट करने के वास्ते लिखित जवाब देने का खान को दो बार मौका दिया था, लेकिन वह अदालत को संतुष्ट करने में नाकाम रहे। इसके बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें अभ्यारोपित करने की घोषणा की थी। (भाषा)
अमेरिकी डॉलर की तुलना में गुरुवार को भारतीय रुपये में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गयी है. बुधवार को भारतीय रुपया 79.98 के स्तर तक पहुंच गया था.
लेकिन गुरुवार को भारतीय मुद्रा में गिरावट जारी रही.
इसके साथ ही डॉलर की तुलना में रुपया 80.47 के स्तर पर पहुंच गया है.
सरल शब्दों में कहें तो फॉरेन एक्सचेंज पर एक डॉलर के बदले में 80.47 रुपये मिल सकते हैं.
रुपये में गिरावट के लिए अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की ब्याज़ दरों में बढ़त को ज़िम्मेदार माना जा रहा है. (bbc.com/hindi)
ईरान में एक महिला महसा आमिनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है. लगातार पांचवे दिन ईरान के अलग-अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है.
बीबीसी को तेहरान, तालेश, मशाद, ज़हेदान, अहवाज़, सिरजन, अमोल, केशम और नौशहर समेत तमाम अन्य शहरों से वीडियो मिले हैं.
इन विरोध प्रदर्शनों में 'तानाशाह की मौत हो' के नारे लगाए जा रहे हैं. ये नारा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के लिए लगाया जा रहा था.
पांचवे दिन हुए विरोध प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से भिड़ते हुए नज़र आए. इसके साथ ही ईरान के कई हिस्सों में सोशल मीडिया एप्स जैसे इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
महिलाओं ने लगातार पांचवे दिन भी कई जगहों पर हिजाब जलाकर विरोध करना जारी रखा है.
ईरान में ताज़ा प्रदर्शनों की शुरूआत महसा आमिनी नाम की एक लड़की की पुलिस हिरासत में मौत के बाद शुरू हुए हैं.
ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत की 22 वर्षीया महसा आमिनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी.
उन्हें पिछले हफ़्ते तेहरान में 'हिजाब से जुड़े नियमों का कथित तौर पर पालन नहीं करने के लिए' गिरफ़्तार किया गया था.
तेहरान की मोरलिटी पुलिस का कहना है कि ईरान में 'सार्वजनिक जगहों पर बाल ढँकने और ढीले कपड़े पहनने' के नियम को सख़्ती से लागू करने के सिलसिले में कुछ महिलाएँ हिरासत में ली गई थीं.महसा भी उनमें थीं.
तेहरान पुलिस के कमांडर हुसैन रहीमी ने सोमवार को कहा कि पुलिस के ख़िलाफ़ 'कायराना इल्जाम' लगाए जा रहे हैं. महसा के साथ कोई हिंसा नहीं की गई थी और पुलिस उन्हें ज़िंदा रखने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी, पुलिस ने किया. (bbc.com/hindi)
रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आंशिक लामबंदी की घोषणा के विरोध में रूस में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं. पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध के लिए लाखों रिज़र्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाया जाएगा और हथियारों में निवेश भी बढ़ाया जाएगा.
पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को लोगों को गिरफ़्तार किया है. रूसी मानवाधिकार संगठन ओवीडी-इन्फो के मुताबिक़, गिरफ़्तार होने वालों की संख्या एक हज़ार से ज़्यादा है.
मॉस्को और सेंट पीट्सबर्ग में सबसे ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. इसके साथ ही पुलिस ने साइबेरियाई शहरों इरकुत्स्क और याकातेरिबर्ग में दर्जनों लोगों को गिरफ़्तार किया है.
पुतिन के एलान के बाद रूस से बाहर जाने वाली फ़्लाइट्स की बुकिंग में भी जबरदस्त तेजी देखी गयी. कुछ समय बाद एक भी फ़्लाइट में जगह नहीं बची.
मॉस्को के प्रॉसिक्यूटर ऑफिस ने बुधवार को चेतावनी दी है कि इंटरनेट पर अनाधिकृत विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए आह्वान करने या उनमें हिस्सा लेने पर 15 सालों तक जेल में रहने की सजा दी जा सकती है.
यूक्रेन युद्ध से जुड़ा “दुष्प्रचार” फैलाने पर कड़ी सजाएं देने के प्रावधानों एवं पुतिन विरोधी सामाजिक कार्यकर्ताओं की पुलिस प्रताड़ना के बाद रूस में सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन काफ़ी दुर्लभ हो गए हैं.
पुतिन ने बीते बुधवार आंशिक सैन्य लामबंदी का एलान किया है जिसका अर्थ तीन लाख आरक्षित सैनिकों को भेजा जाना है.
पुतिन ने टीवी पर प्रसारित अपने भाषण में कहा है कि वह रूस की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए ‘सभी उपलब्ध साधनों’ का इस्तेमाल करेंगे.
पश्चिमी दुनिया में पुतिन के इस बयान का अर्थ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से लगाया जा रहा है. यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने पुतिन के इस बयान की निंदा की है. (bbc.com/hindi)
-स्टीव रोज़नबर्ग
आज से पहले तक रूस दावा करता रहा है कि यूक्रेन में उसका सैन्य अभियान योजना के अनुसार ही चल रहा है.
लेकिन अब ऐसा नहीं है.
व्लादिमीर पुतिन रूसी सेना के रिज़र्व सैनिकों को वापस बुलाने का एलान करके ये मान चुके हैं कि युद्ध के मैदान पर उन्हें अतिरिक्त सैनिकों की ज़रूरत है.
रूसी राष्ट्रपति को सुनने से ऐसा नहीं लगता कि उन्हें सात महीने पहले यूक्रेन पर हमला करने का ज़रा भी खेद है.
पुतिन ने बताया है कि रूस की दिक्कतों के लिए पश्चिमी देश ज़िम्मेदार हैं. ये कहते हुए उन्होंने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि वे रूस को तोड़ना चाहते हैं.
उन्होंने कहा है, “अगर रूस की क्षेत्रीय अखंडता को ख़तरा पैदा होता है तो हम उपलब्ध सभी साधनों का इस्तेमाल करेंगे."
रूस ने यूक्रेन के जिन इलाक़ों पर हाल में कब्ज़ा किया है वहाँ आने वाले दिनों में जनमत संग्रह करवाया जा रहा है.
ये यूक्रेन और पश्चिमी देशों को सीधा संदेश है – हमने जिस ज़मीन पर कब्जा किया है और जिस पर हम दावा करेंगे, उसे वापस लेने की कोशिश न की जाए.
ये स्पष्ट करने के लिए उन्होंने धमकी दे डाली है.
उन्होंने कहा है, “जो हमें परमाणु हथियारों से धमकाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हवाएं उनकी तरफ़ भी बह सकती हैं.” (bbc.com/hindi)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को यूक्रेन में युद्ध के लिए आंशिक लामबंदी का एलान किया है. इसका अर्थ है कि यूक्रेन युद्ध में रूस और अधिक संसधान और सैन्य टुकड़ियों को शामिल करेगा.
पुतिन ने टीवी पर प्रसारित हुए देश के नाम संबोधित अपने भाषण में कहा है कि ‘यह रूस की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखने के लिए ये एक ज़रूरी कदम था.’
उन्होंने कहा कि ‘पश्चिमी दुनिया रूस का ख़ात्मा चाहती थी जैसे उसने सोवियत संघ का ख़ात्मा ककर दिया.’
भाषण में क्या कहा –
- पुतिन ने यूक्रेन में जारी सैन्य संघर्ष में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां भेजने का एलान किया है. इसका अर्थ ये है कि रूसी सेना में सेवाएं दे चुके लोगों को वापस बुलाया जाएगा.
- इन सैन्य टुकड़ियों की रवानगी आज से शुरू होगी.
- पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस को परमाणु हमले के नाम पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है.
- पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों की धमकियों का जवाब देने के लिए उनके पास काफ़ी हथियार हैं.
- उन्होंने कहा है कि डोनबास में ‘अपनों’ की सुरक्षा के लिए हर संभव साधन जुटाए जाएंगे.
- उन्होंने रूस में हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फंडिंग का आदेश दिया है.
- रूसी संसद दूमा के सदस्य येवगेनी पोपोव ने बीबीसी को बताया है कि ‘जैसा मैं समझता हूं, कुछ अनुभवी सैनिकों को तैनात किया जाएगा और जो लोग अभी-अभी सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें बुलाया जा सकता है. ये आम लोगों को युद्ध के मैदान में भेजने की बात नहीं है.’ (bbc.com/hindi)
-सोफिया बेट्टिज़ा
इज़ियम शहर पर यूक्रेन के दोबारा क़ब्ज़े के बाद रूसी सेना के अत्याचारों के आरोप सामने आ रहे हैं. इस शहर में रह रहे श्रीलंकाई लोगों के एक समूह ने रूसी सेना पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं.
रूसी सैनिकों के ज़ुल्म की दास्तां बयान करने वाले इन श्रीलंकाई नागरिकों को यहां कई महीनों से क़ैद रखा गया था.
इन कैदियों में से एक दिलुजान पतथिनाजकन ने कहा, '' ऐसा लग रहा था कि हम यहां से ज़िंदा नहीं निकल पाएंगे. ''
दिलुजान उन सात श्रीलंकाई लोगों में से एक हैं जिन्हें रूसी सैनिकों ने मई में पकड़ लिया था. रूसी हमले में अपनी जान को ख़तरे में देखते हुए यह समूह कुपियांस्क में अपने घर से ज़्यादा सुरक्षित खारकीएव की ओर से निकला था. कुपियांस्क से खारकीएव 120 किलोमीटर दूर है.
लेकिन पहली ही चेक पोस्ट पर श्रीलंकाई लोगों का ग्रुप रूसी सैनिकों के हाथ पड़ गया. इन सैनिकों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी. उनके हाथ पीछे की ओर बांध दिए गए और उन्हें रूसी सीमा के पास वोवचांस्क में एक मशीन टूल फैक्टरी में ले जाया गया.
ये चार महीने के उनके दु:स्वप्न की शुरुआत थी. उन्हें यहीं बंद रखा गया. उनसे ज़बर्दस्ती काम लिया जाता था और प्रताड़ना भी दी जाती थी.
श्रीलंकाई लोगों का यह दल यूक्रेन में रोज़गार या पढ़ाई के लिए आया था. लेकिन अब वे क़ैदी थे जो रूसियों के क़ब्जे़ में नाम मात्र के भोजन पर ज़िंदा थे. इन कै़दियों को दिन में एक बार सिर्फ़ दो मिनट के लिए टॉयलेट जाने की इजाज़त थी.
उम्र के तीसरे दशक में चल रहे पुरुषों को एक कमरे में बंद रखा गया था. जबकि 50 साल की महिला मेरी एडिट उथाजकुमार को उनसे अलग रखा गया था.
वह बताती हैं,'' उन्होंने हमें एक कमरे में बंद रखा था. हम जब नहाने निकलते थे तो रूसी सैनिक हमारी पिटाई करते थे. उन्होंने मुझे दूसरे बंधकों से मिलने भी नहीं दिया. हम तीन महीने तक अंदर फंसे रहे. ''
मेरी का चेहरा पहले ही श्रीलंका में हुए एक विस्फोट में झुलस चुका है. उन्हें दिल की बीमारी है. लेकिन यहां उन्हें इसकी कोई दवा नहीं दी गई.
लेकिन अकेले कमरे में बंद रखे जाने का उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा असर हुआ है.
वह कहती हैं, ''अकेले बंद रखे जाने की वजह से मैं काफी तनाव में आ जाती थी. रूसी सैनिकों ने कहा कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है. मुझे दवा दी जाती थी, लेकिन मैंने नहीं ली. ''
पैर के अंगूठे के नाखून उखाड़े
दूसरे लोगों पर भी ज़ुल्म ढाए गए. कै़द किए गए एक शख्स ने जूते उतारकर अपना अंगूठा दिखाया. उनके अंगूठे के नाखून प्लायर से निकाल लिए गए थे. एक और शख्स को प्रताड़ित किया गया था.
बंधक बनाए लोगों का कहना है कि उन्हें बिना वजह के पीटा जाता था. रूसी सैनिक शराब पीकर उन पर टूट पड़ते थे..
35 साल के थिनेश गगनथिन बताते हैं, '' एक सैनिक ने मेरे पेट में घूंसे मारे. इससे मैं दो दिनों तक दर्द से तड़पता रहा. इसके बाद उसने मुझसे पैसे मांगे''.
25 साल के दिलुकशान रॉबर्टक्लाइव ने बताया, ''हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था. हम बेहद दुखी थी और हर दिन रोते थे. हमें सिर्फ एक ही चीज ने जिंदा रखा था, वह थी हमारी प्रार्थना. दूसरी चीज थी हमारे परिवार की यादें ''
रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान नागरिकों को निशाना बनाए जाने या युद्ध अपराधों को अंजाम देने से इनकार किया है. लेकिन श्रीलंकाई नागरिकों पर जुल्म की यह ख़बर ऐसे वक्त में आई है जब रूसी सैनिकों पर ऐसे आरोप लगातार लग रहे हैं.
'शवों पर यातना के निशान'
यूक्रेन इज़ियम की क्रबगाहों से शवों के अवशेष निकाल रहा है. कुछ शवों के शरीर पर यातना के निशान हैं.
यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदोमीर जे़लेंस्की ने कहा ,''खारकीएव में आजाद कराए जा रहे इलाकों और कई शहरों में दस से अधिक टॉर्चर चैंबर मिले हैं. ''
रूसी सैनिकों की कैद से इन श्रीलंकाई लोगों को तब छुड़ाया गया है, जब यूक्रेनी सैनिकों ने इस महीने वोवचांस्क समेत कई इलाकों पर दोबारा कब्जा करना शुरू किया.
रूसी सैनिकों के कब्जे से रिहा श्रीलंकाई लोगों का यह दल एक बार फिर खारकीएव की ओर चल पड़ा था. लेकिन उनके पास फोन नहीं थे. अपने परिवार के लोगों से संपर्क करने का उनके पास कोई जरिया नहीं था.
कैसे मिली मुक्ति?
लेकिन आखिरकार उनकी किस्मत ने पलटी खाई. कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में पहचान लिया और पुलिस को फोन कर दिया. एक पुलिस अफसर ने उन्हें अपना फोन दिया. 40 साल के एंकरनाथन गणेशमूर्ति ने फोन स्क्रीन पर अपनी पत्नी और बेटी को देखा तो फफक पड़े. फोन आते रहे और आंसू बहते रहे. पुलिस अफसर को इन लोगों ने गले से लगा लिया.
इस दल को खारकीएव ले जाया गया. वहां उनका इलाज किया गया और नए कपड़े दिए गए. उन्हें एक पुनर्वास केंद्र में रखा गया है जहां स्विमिंग पूल और जिम है. चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए दिलुकशान कहते हैं. अब मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूं. '' (bbc.com/hindi)
सैन फ्रांसिस्को, 21 सितंबर | अमेरिकन एयरलाइंस ने डेटा ब्रीच की पुष्टि की है। इसके तहत कुछ ग्राहकों के नाम, जन्मदिन, मेलिंग और ईमेल पते, फोन, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट नंबर और 'कुछ चिकित्सा जानकारी' प्रभावित हुई है। हालांकि, एयरलाइन ने कहा कि उसके पास यह बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि 'आपकी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया गया है।'
जुलाई में हुए डेटा उल्लंघन का खुलासा करते हुए, एक बयान में कहा गया, "फिर भी, सावधानी से, हम आपको घटना और सुरक्षात्मक उपायों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहते थे।"
अमेरिकल एयरलाइंस ने कहा, "जुलाई 2022 में हमने पाया कि एक अनधिकृत हैकर ने सीमित संख्या में अमेरिकन एयरलाइंस टीम के सदस्यों के ईमेल खातों से छेड़छाड़ की। घटना का पता चलने पर, हमने लागू ईमेल खातों को सुरक्षित कर लिया और एक फोरेंसिक जांच करने के लिए एक थर्ड पार्टी की साइबर सुरक्षा फोरेंसिक फर्म को नियुक्त किया।"
जांच ने निर्धारित किया कि कुछ व्यक्तिगत जानकारी ईमेल खातों में थी।
एयरलाइन ने सूचित किया, "इस घटना में शामिल व्यक्तिगत जानकारी में आपका नाम, जन्म तिथि, डाक पता, फोन नंबर, ईमेल पता, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर और/या आपके द्वारा प्रदान की गई कुछ चिकित्सा जानकारी शामिल हो सकती है।"
एयरलाइन ने कहा कि वह प्रभावित ग्राहकों की पहचान की चोरी का पता लगाने और समाधान में मदद करने के लिए एक्सपीरियन के आइडेंटिटीवर्क्स की दो साल की मुफ्त सदस्यता प्रदान करेगी।
यह प्रोडक्ट "आपको बेहतर पहचान का पता लगाने और पहचान की चोरी का समाधान प्रदान करता है।"
अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा, "हालांकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया गया है, हम अनुशंसा करते हैं कि आप एक्सपीरियन की क्रेडिट निगरानी में नामांकन करें।"
इससे पहले अमेरिकन एयरलाइंस मार्च 2021 में डेटा ब्रीच की चपेट में आ गई थी। (आईएएनएस)|
तोक्यो, 21 सितंबर। जापान की राजधानी तोक्यो में बुधवार तड़के एक बुजुर्ग ने कथित तौर पर अगले हफ्ते शिंजो आबे की राजकीय अंत्येष्टि के विरोध में प्रधानमंत्री कार्यालय के पास खुद को आग लगा ली। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
समाचार एजेंसी ‘क्योदो न्यूज’ में प्रकाशित खबर के मुताबिक, बुजुर्ग के पास से उसके द्वारा कथित तौर पर लिखा गया एक नोट बरामद हुआ है, जिसमें कहा गया है, “व्यक्तिगत तौर पर मैं शिंजो आबे (जापान के पूर्व प्रधानमंत्री) का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए जाने के सख्त खिलाफ हूं।”
खबर के अनुसार, आत्मदाह करने वाले बुजुर्ग की उम्र 70 साल से अधिक है और उसके शरीर का बड़ा हिस्सा झुलस गया है। हालांकि, वह होश में था।
वहीं, पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग ने खुद पर तेल छिड़कने के बाद आग लगा ली। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तोक्यो दमकल विभाग के एक अधिकारी ने राजधानी के कासुमिगासेकी जिले में एक बुजुर्ग द्वारा आत्मदाह किए जाने की पुष्ट की। हालांकि, उन्होंने मामले को संवेदनशील करार देते हुए संबंधित व्यक्ति की पहचान और आत्मदाह के पीछे की वजहों व परिस्थितियों के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।
तोक्यो पुलिस ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। उसने आग में एक पुलिसकर्मी के घायल होने से संबंधित मीडिया रिपोर्ट पर भी कोई टिप्पणी नहीं की।
गौरतलब है कि यूनिफिकेशन चर्च से सत्तारूढ़ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) और आबे के संबंधों को लेकर अधिक जानकारी सामने आने के साथ ही जापान में पूर्व प्रधानमंत्री की राजकीय अंत्येष्टि को लेकर विरोध बढ़ने लगा है।
आबे की हत्या के आरोपी को भी कथित तौर पर लगता था कि उसकी मां द्वारा यूनिफिकेशन चर्च को दिए गए दान से उसका परिवार बर्बाद हो गया। एलडीपी ने कहा है कि उसके लगभग आधे सांसद यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े हैं।
जापान में किसी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना एक दुर्लभ घटना है, लेकिन प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने कहा है कि आबे इसके हकदार हैं, क्योंकि वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले ऐसे नेता थे, जिनके शासन में जापान ने उल्लेखनीय राजनयिक व आर्थिक उपलब्धियां हासिल कीं।(एपी)
संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में आज संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमारी दुनिया संकट में है और दुनिया की व्यवस्था लाचार हो गई है.
सहयोग और संवाद ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है. कोई भी शक्ति या समूह अकेले किसी बड़ी वैश्विक चुनौती का हल नहीं खोज सकती. हमें दुनिया की एकजुटता की ज़रूरत है.
गुटेरेस ने महासभा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे युग की नाटकीय चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार या इच्छुक नहीं है.
''यूएन चार्टर और इसके द्वारा प्रस्तुत आदर्श खतरे में हैं.कार्रवाई करना हमारा कर्तव्य है. हमें अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के संरक्षण के संबंध में हर जगह ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है.
गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर नफ़रत और नकारत्मकता फैलाने का भी आरोप लगाया.
दुनियाभर के 193 देशों के नेता न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं.
भारत के विदेश मंत्री एस.जयशंकर भी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं लेकिन चीन और रूस के राष्ट्रपति इस बार बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं.
महासभा के एजेंडे में इस बार जलवायु संकट से लेकर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं. (bbc.com/hindi)
ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया समुद्र तट पर एक साथ चौदह स्पर्म व्हेल्स मरी मिली हैं.
स्थानीय लोगों ने सबसे पहले तट पर इन मरी हुई व्हेल को देखा और अधिकारियों को इसकी सूचना दी.
व्हेल यहां कैसे फंस गईं, इसके कारणों का अभी पता नहीं चला है. वन्यजीव जीवविज्ञानी और एक पशु चिकित्सक को जांच के लिए वहाँ भेजा गया है.
हालांकि तस्मानिया में व्हेल का तटों पर फंसना कोई नई बात नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि ये द्वीप इस तरह की घटनाओं का ''हॉटस्पॉट'' है.
सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि हवाई सर्वेक्षण से पता चलेगा कि इलाके में कहीं और जीव तो नहीं फंसे हैं.
पूरी दुनिया में स्पर्म व्हेल की प्रजाति पर ख़तरा मंडरा रहा है. ये 18 मीटर तक लंबी और 45 टन तक भारी हो सकती हैं.
सितंबर साल 2020, में ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में वेस्ट कोस्ट पर फंसने से 380 पायलट व्हेल की मौत हो गई थी. (bbc.com/hindi)
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हॉन्ग कॉन्ग के एक 43 वर्षीय शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. ये शख्स महारानी को श्रद्धांजलि देने सोमवार रात ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास पहुंचा था.
पुलिस ने बीबीसी की चीनी सेवा को बताया कि इस व्यक्ति को औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून के तहत हिरासत में लिया गया था.
स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि ये ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास के बाहर अपने हारमोनिका पर कई गाने बजा रहा था. इनमें 2019 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े गानों के साथ ब्रिटिश राष्ट्रगान भी शामिल था.
सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए फुटेज में वाणिज्य दूतावास के बाहर खड़े इस शख्स को हारमोनिका पर "ग्लोरी टू हॉन्ग कॉन्ग" बजाते हुए दिखाया गया है. ये हॉन्ग कॉन्ग में 2019 के लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों का अनौपचारिक गाना था.
पुलिस ने बीबीसी को बताया कि शख्स को "देशद्रोह के इरादे से काम" करने के संदेह में हिरासत में लिया गया था.
हॉन्ग कॉन्ग ब्रितानी शासन के अधीन था, लेकिन साल 1997 में इसे 'एक देश दो विधान' सिद्धांत के तहत चीन को सौंप दिया गया था.
चीन एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत के तहत हॉन्ग कॉन्ग पर शासन करने के लिए सहमत हुआ, जहां अगले 50 साल तक उसे विदेश और रक्षा मामलों को छोड़कर राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी हासिल होती.
इस समझौते के बाद हॉन्ग कॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बन गया लेकिन यहां के लोगों का मानना है कि विरोधियों पर कार्रवाई, चीन द्वारा अपने राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लागू करना और केवल राष्ट्रवादियों को ही शासन करने की अनुमति देने जैसे कानून साल 1997 के हैंडओवर सिद्धांतों का उल्लंघन है. (bbc.com/hindi)
तालिबान के एक सहयोगी हाजी बशीर नूरज़ई अमेरिका में कई दशकों की क़ैद के बाद आख़िरकार रिहा हो गए और सोमवार को अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल पहुँचे.
अफ़ग़ानिस्तान की सरकारी मीडिया के मुताबिक़, नूरज़ई उन आख़िरी क़ैदियों में शामिल थे जिन्हें दुनिया की सबसे बदनाम जेल में रखा गया था.
ग्वांतानामो बे 'चरमपंथ के ख़िलाफ़ जंग' की शुरुआत के बाद साल 2002 में शुरू की गई थी और यहाँ उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अमेरिकी सरकार 'चरमपंथी' घोषित करती थी.
ग्वांतानामो बे में पहली बार 11 जनवरी 2002 को 20 क़ैदी लाए गए थे और इसके बाद से यहाँ सैकड़ों लोगों को रखा जा चुका है. इनमें से अधिकतर पर ना ही कोई आरोप तय किए गए और न ही मुक़दमा चलाया गया.
नूरज़ई की रिहाई तालिबान शासकों और अमेरिका के बीच लंबी बातचीत के बाद तय हुई अदला-बदली का नतीजा है. साल 2020 में बंधक बनाए गए एक अमेरिकी इंजीनियर मार्क फ़्रेरिच की रिहाई के बदले तालिबान के नूरज़ई को छोड़ा गया है. नूरज़ई साल 2005 से अमेरिका की जेल में बंद थे.
अमेरिका ने हालाँकि तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन सोमवार को दोनों देशों में अधिकारियों ने कहा कि लंबे दौर की बातचीत के बाद क़ैदियों की अदला-बदली पर सहमति बनी है. साथ ही ये भी कहा था कि तालिबान और बाइडन प्रशासन के बीच बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, "मार्क फ्रेरिच की रिहाई के लिए बातचीत आसान नहीं थी. ये अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि ऐसे फ़ैसलों को स्वीकार किया जाए."
तालिबान ने कहा है कि फ्रेरिच को सोमवार को काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले किया गया. बदले में अमेरिकी अधिकारियों ने ड्रग तस्करी के आरोप में जेल में बंद नूरज़ई को तालिबान के हवाले किया.
60 साल के फ्रेरिच का तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने से एक साल पहले अपहरण कर लिया था. फ्रेरिच काबुल में 10 साल से बतौर सिविल इंजीनियर काम कर रहे थे.
फ्रेरिच की बहन शार्लीन ककोरा ने कहा कि उन्हें भाई के रिहा होने की पूरी उम्मीद थी. एक बयान में ककोरा ने कहा, "मैं यह सुनकर बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई सही सलामत है और घर लौट रहा है. पिछले 31 महीने से मेरा परिवार हर दिन उनके लिए प्रार्थना कर रहा था."
कौन हैं नूरज़ई?
नूरज़ई तालिबान के लिए कितने अहम हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगस्त 2021 में अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता छीनने से कई महीने पहले उन्होंने अमेरिका से फ्रेरिच की रिहाई के बदले नूरज़ई को छोड़ने की मांग की थी.
हालाँकि तब अमेरिका की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले थे कि वह तालिबान के इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर है.
नूरज़ई के अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल लौटने पर उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया. सोशल मीडिया पर जारी कुछ वीडियो में दिख रहा है कि बड़ी संख्या में तालिबान फूल मालाओं से नूरज़ई का स्वागत कर रहे हैं.
बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में नूरज़ई ने कहा, "अमेरिका की इच्छा से मेरी रिहाई दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करेगी."
नूरज़ई तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के क़रीबी थे और 1990 के दशक में बनी तालिबान सरकार को उन्होंने आर्थिक मदद की थी.
अफ़ग़ानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को समाचार एजेंसी एएफ़पी को बताया- नूरज़ई के पास तालिबान का कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन उन्होंने हथियार और दूसरे तरीक़ों से हमारी मदद ज़रूर की थी.
नूरज़ई को हेरोइन तस्करी के मामले में अमेरिकी अदालत ने दोषी ठहराया था. उन्होंने 17 साल जेल में गुज़ारे. आरोप था कि नूरज़ई कंधार प्रांत में बड़े पैमाने पर अफ़ीम का कारोबार करता है. उस वक़्त कंधार तालिबान का मज़बूत ठिकाना था.
2005 में जब नूरज़ई को गिरफ़्तार किया गया था तो उनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़ी ड्रग तस्करों में होती थी. अफ़ग़ानिस्तान के क़बायली नेता नूरज़ई को न्यूयॉर्क की अदालत ने 5 करोड़ डॉलर की ड्रग तस्करी के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी.
अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि नूरज़ई ने बड़े पैमाने पर अफ़ीम की खेती तो करवाई ही थी, साथ ही अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान में ऐसी लैब भी बनाई थी जिनमें अफ़ीम को प्रोसेस कर हेरोइन बनाया जाता था.
हालाँकि तब नूरज़ई के वकील ने कहा था कि नूरज़ई को इंसाफ़ नहीं मिला है. उन्होंने ये भी दावा किया था कि नूरज़ई पर लगे आरोप ग़लत हैं और अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिया था कि नूरज़ई को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा. (bbc.com/hindi)
सिडनी, 20 सितम्बर | ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटेट ने मंगलवार को घोषणा की कि, राज्य में अपराधी जो शव के स्थान के बारे में जानकारी देने से मना करते हैं, वे नए कानूनों के तहत पैरोल के लिए पात्र नहीं होंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पेरोटेट ने कहा कि सरकार के प्रस्तावित विधेयक का मतलब होगा कि अपराधियों को जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करना चाहिए और पैरोल पर रिहा होने के किसी भी मौके के लिए अवशेषों के स्थान का खुलासा करना चाहिए। किसी प्रियजन के शव का पता लगाने में असमर्थ होना पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के लिए बेहद दुखद और दर्दनाक है।
उन्होंने कहा, ये कानून हत्या या हत्या के अपराध के दोषी, कैदियों को पैरोल मिलने से रोकने के लिए हैं, जब तक कि वे पीड़ित परिवार के दर्द को खत्म करने के लिए पुलिस की मदद नहीं करते हैं और उनके प्रियजनों का शव उन्हें वापस नहीं करते है। कानून, जो अभी भी प्रस्ताव के अधीन है, उसका अर्थ ये होगा कि राज्य पैरोल प्राधिकरण पैरोल से इनकार करने के लिए बाध्य है, जब तक कि उसे एनएसडब्ल्यू पुलिस बल के आयुक्त से लिखित सलाह के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक जानकारी प्राप्त न हो, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अपराधी ने पीड़ित की पहचान और पता बताने में संतोषजनक रूप से सहयोग किया है।
कानून में बदलाव पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि यह क्रिस डॉसन के हाई-प्रोफाइल मामले का अनुसरण करता है, जिसे पिछले महीने 40 साल पहले अपनी पत्नी लिनेट की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसका शव कभी नहीं मिला। सुधार मंत्री जेफ्री ली ने कहा कि, सुधार अन्य न्यायालयों में कानूनों पर आधारित हैं और एनएसडब्ल्यू में सभी मौजूदा और भविष्य के कैदियों पर लागू होंगे, जिन्हें दोषी अपराधियों को पकड़ने के लिए अभी तक पैरोल के लिए विचार नहीं किया गया है।
ली ने कहा, पेरोल के लिए आने वाले जेल में किसी भी अपराधी को पुलिस के साथ सहयोग करने से इनकार करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, अगर वह पैरोल पाने की अपनी संभावनाओं को बरकरार रखना चाहते हैं। (आईएएनएस)|
वेलिंगटन, 20 सितंबर | न्यूजीलैंड के ताओपो ज्वालामुखी में मंगलवार को अलर्ट का स्तर पहली बार बढ़ा दिया गया। यह पहली बार है जब ज्वालामुखी चेतावनी को स्तर 1 तक बढ़ा दिया गया है, हालांकि यह ताओपो में पहली ज्वालामुखी उपद्रव नहीं है, जियोनेट ने कहा, जो न्यूजीलैंड के लिए भूवैज्ञानिक खतरे की जानकारी प्रदान करता है।
जियोनेट के एक बयान में कहा गया है, "पिछले 150 वर्षों में अनरेस्ट के 17 एपिसोड हुए हैं। इनमें से कई अधिक गंभीर थे।"
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जीएनएस विज्ञान ज्वालामुखी टीम के निको फोरनियर ने कहा कि इनमें से कोई विस्फोट में नहीं बदला।
फोरनियर ने कहा, ताओपो ज्वालामुखी में अंतिम विस्फोट 232 ईस्वी के आसपास हुआ था।
"ताओपो में विस्फोट की संभावना बहुत कम रहती है," उन्होंने कहा। मामूली ज्वालामुखी अशांति से जमीन की विकृति हो रही है।
जीएनएस साइंस, जियोनेट कार्यक्रम के माध्यम से, गतिविधि के संकेतों के लिए ताओपो ज्वालामुखी और अन्य सक्रिय ज्वालामुखियों की लगातार निगरानी करता है।
फोरनियर ने कहा, "जबकि कुछ भूकंप ताओपो झील के आसपास के क्षेत्रों में महसूस किए जा सकते हैं, विरूपण वर्तमान में केवल हमारे संवेदनशील निगरानी उपकरणों द्वारा ही पता लगाया जा सकता है।"
ताओपो झील के मध्य भाग के नीचे भूकंप का क्रम जारी है, उन्होंने कहा, लगभग 700 छोटे भूकंप, मुख्य रूप से झील के नीचे 4 से 13 किमी की गहराई पर स्थित हैं।
फोरनियर ने कहा, "हम ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा और हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों की गति के कारण होने वाली भूकंप गतिविधि की व्याख्या करते हैं। हमने रसायन विज्ञान में परिवर्तन के लिए झील के चारों ओर स्प्रिंग्स और गैस वेंट का भी नमूना लिया है जो भूकंप और जमीन के उत्थान से संबंधित हो सकते हैं।"
उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी चेतावनी स्तर 1 ज्यादातर पर्यावरणीय खतरों से जुड़ा है, लेकिन विस्फोट के खतरों की संभावना भी मौजूद है। (आईएएनएस)|
ब्यूनस आयर्स, 20 सितंबर | अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के तकनीकी कर्मचारियों ने अर्जेटीना के साथ संगठन के ऋण राहत समझौते की दूसरी समीक्षा को मंजूरी दे दी है, जिससे आने वाले हफ्तों में दक्षिण अमेरिकी देश के लिए 3.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आईएमएफ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "अर्जेटीना की 30-महीने की ईएफएफ (विस्तारित फंड सुविधा) व्यवस्था के तहत दूसरी समीक्षा पर आईएमएफ कर्मचारी और अर्जेटीना के अधिकारी स्टाफ-स्तरीय समझौते पर पहुंच गए हैं।"
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह मंजूरी दूसरी तिमाही में सरकार द्वारा मात्रात्मक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के अनुरूप है।
समझौता आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के अनुमोदन के अधीन है, जिसकी आने वाले हफ्तों में बैठक होने की उम्मीद है।
आईएमएफ ने कहा, "एक बार समीक्षा पूरी हो जाने के बाद अर्जेटीना की पहुंच करीब 3.9 अरब डॉलर हो जाएगी।"
इसमें कहा गया है, "पहले की असफलताओं को ठीक करने के उद्देश्य से हाल की निर्णायक नीतिगत कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय भंडार के पुनर्निर्माण सहित आत्मविश्वास को बहाल करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने में मदद कर रही हैं।"
आईएमएफ स्टाफ और अर्जेटीना के अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की कि व्यवस्था के अनुमोदन पर स्थापित प्रमुख उद्देश्य, जिनमें प्राथमिक वित्तीय घाटे और शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय भंडार से संबंधित हैं, 2023 तक अपरिवर्तित रहेंगे।
आईएमएफ ने कहा, "आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने और अर्जेटीना की गहरी चुनौतियों, विशेष रूप से उच्च और लगातार मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए दृढ़ नीति कार्यान्वयन आवश्यक है।"
अर्जेटीना और आईएमएफ ने मार्च में एक ऋण राहत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे देश को 44.5 अरब डॉलर के कर्ज पर अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी। (आईएएनएस)|
रामल्लाह, 20 सितंबर | पूर्वी यरुशलम में करीब 150 फिलिस्तीनी स्कूल इजरायली पाठ्यक्रम को लागू करने के इजरायल सरकार के प्रयासों के विरोध में बंद हो गए हैं। आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी डब्लूयएएफए ने बताया, सोमवार को लगभग 100,000 छात्र हड़ताल के चलते स्कूलों में नहीं गए। इजरायल सरकार स्कूलों को फिलीस्तीनी पाठ्यक्रम छोड़ कर इजरायली पाठ्यक्रम अपनाने के लिए मजबूर कर रही है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने ड्ब्लूएफए का हवाला देते हुए कहा कि, पूर्वी यरुशलम में माता-पिता के संघ के प्रमुख जि़याद अल-शामाली ने कहा कि, अगर इजराइल के प्रयास सफल होते हैं, तो यह यरूशलेम में हमारे 90 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा पर नियंत्रण हो जाएगा।
अल-शामाली के अनुसार, किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 12 तक के करीब 115,000 बच्चे यरुशलम में 280 से अधिक फिलीस्तीनी स्कूलों में पढ़ते हैं।
रविवार की रात, वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए, जिसमें पूर्वी यरुशलम के निवासियों ने सामान्य हड़ताल की और फिलिस्तीनी पाठ्यक्रम के लिए 'हां' और इजरायली पाठ्यक्रम के लिए 'ना' लिखे पोस्टर लगाए।
जुलाई के अंत में, इजराइल ने पूर्वी यरुशलम में छह फिलिस्तीनी स्कूलों के स्थायी लाइसेंस को रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि, उनकी पाठ्यपुस्तकों में इजराइल और उसकी सेना के खिलाफ उकसाने वाली सामग्री है।
दशकों से, पूर्वी यरुशलम में फिलिस्तीनी स्कूलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों पर विवाद दोनों पक्षों के बीच रहा है।
फिलिस्तीनियों ने पाठ्यपुस्तकों के चुनाव में हस्तक्षेप करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पश्चिमी देशों से शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने से रोकने के लिए इजराइल की आलोचना की।
1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम पर कब्जा कर लिया था, दोनों पर फिलिस्तीनियों का दावा है और तब से इजरायल इस क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा है। (आईएएनएस)|
अदीस अबाबा, 20 सितंबर| इथियोपिया के ओरोमिया क्षेत्रीय राज्य में एक यातायात दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई है। राज्य से संबद्ध फाना ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेट (एफबीसी) ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया, यातायात दुर्घटना ओरोमिया क्षेत्र के पश्चिम अर्सी क्षेत्र में स्थित अदाबा जिले में सोमवार को हुई, जब सड़क पर यात्रा कर रही एक मिनीबस खाई में गिर गई, जिससे छह लोगों की मौत हो गई।
पुलिस ने आगे कहा कि, दुर्घटना से कुछ 15 अन्य लोगों को गंभीर और हल्की शारीरिक चोटें आई हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, घायलों का नजदीकी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज चल रहा है।
पुलिस ने घटना का मुख्य कारण ओवरलोड को बताया, जिसमें 28 लोगों को ले जाने की क्षमता वाली बस दुर्घटना के समय 40 लोगों को ले जा रही थी।
इथियोपिया में दुनिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति कार स्वामित्व दर है, घातक यातायात दुर्घटनाएं काफी आम हैं।
दोष अक्सर खराब सड़कों, लापरवाह ड्राइविंग, एक दोषपूर्ण ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रणाली और सुरक्षा नियमों के ढीले प्रवर्तन पर लगाया जाता है। (आईएएनएस)|
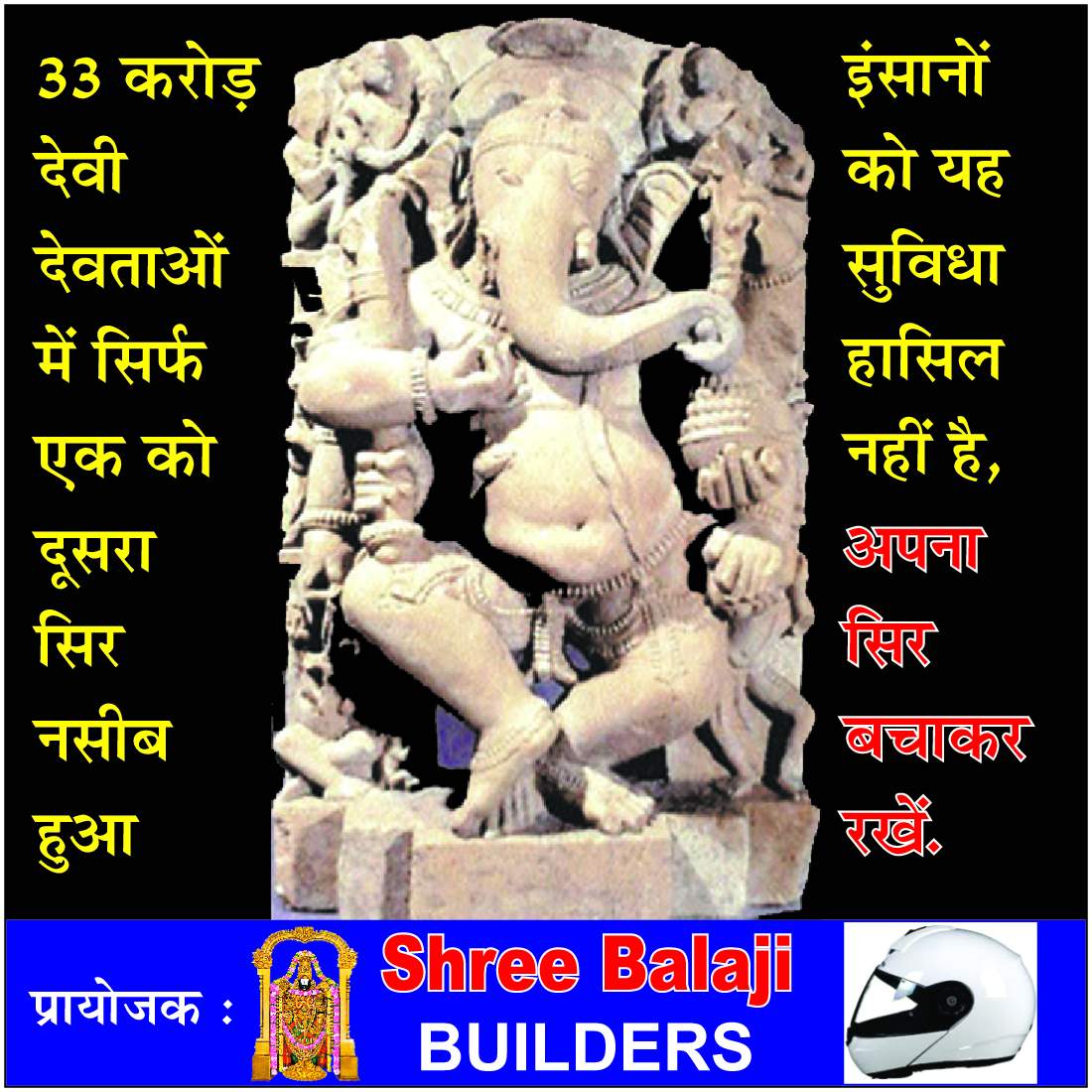


.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)





.jpg)

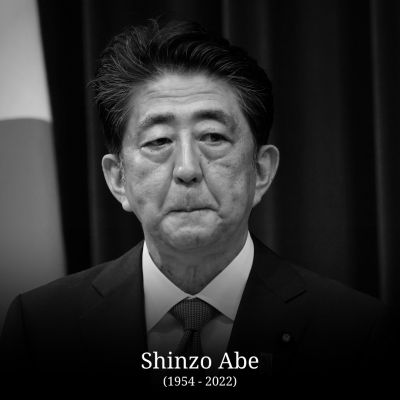
.jpg)

.jpg)
.jpg)