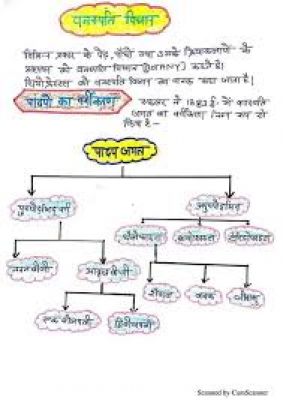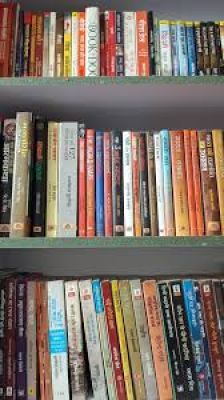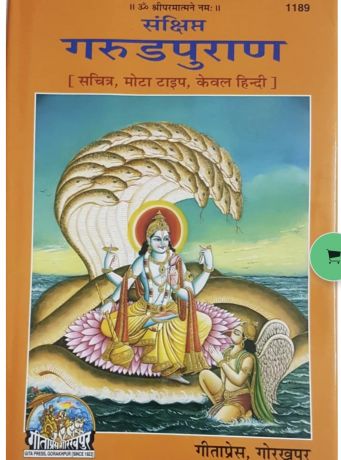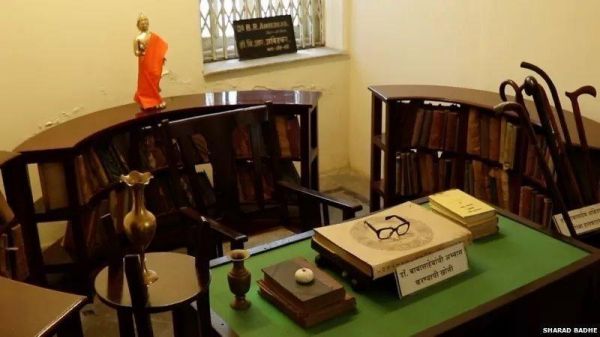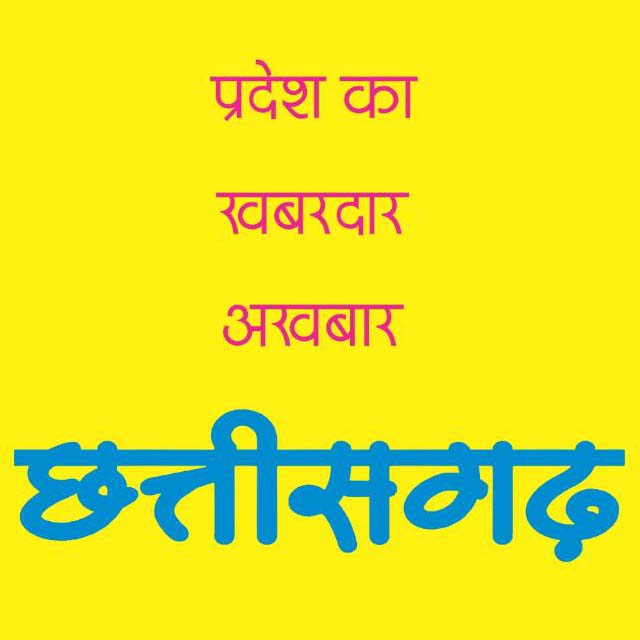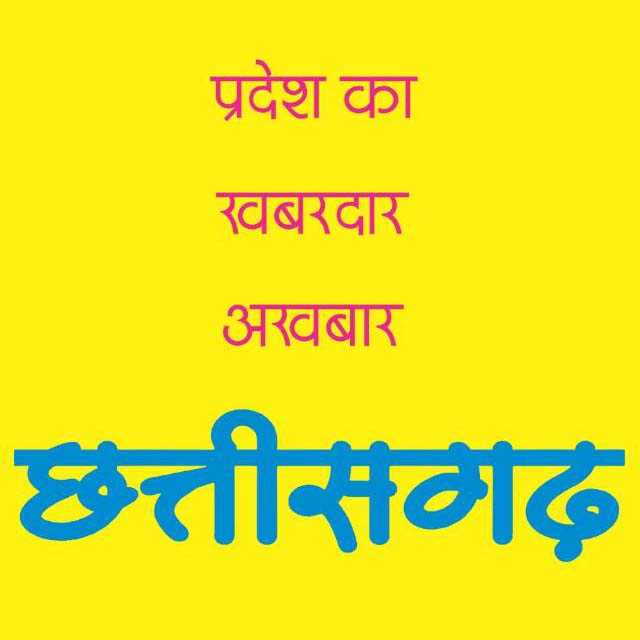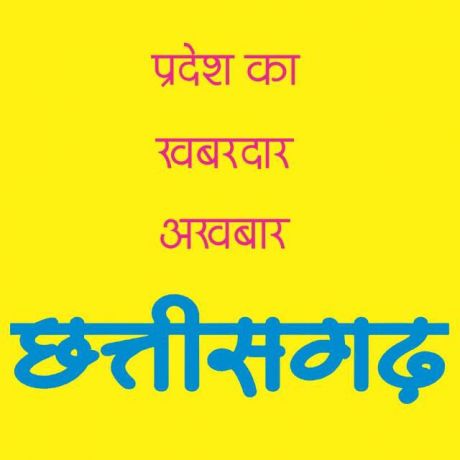विचार/लेख
भूख कई वजह से मर जाती है। पेट भरा हो या हमारा जी मिचलाए या उल्टी का जी हो तो खाने की इच्छा मर जाती है। क्या हर मामले में क्रियाविधि एक ही होती है या हर बार तंत्रिका तंत्र में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही होती है? सेल रिपोर्ट्स में प्रकाशित ताज़ा शोध में शोधकर्ताओं ने इसी सवाल का जवाब खोजा है। इसके लिए उन्होंने मॉडल के तौर पर चूहों को लिया और उनके मस्तिष्क में झांक कर देखा कि हर स्थिति में खाने के प्रति यह अनिच्छा ठीक कहां जागती है।
दरअसल पूर्व में हुए अध्ययन में बताया गया था कि पेट भर जाने और मितली होने, दोनों मामलों में खाने के प्रति अनिच्छा मस्तिष्क में एक ही जगह से नियंत्रित होती है - सेंट्रल एमिगडेला (CeA) के एक ही न्यूरॉन्स समूह (Pkco) से।
लेकिन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस के वेन्यू डिंग को इस बात पर संदेह था। इस संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने ऑप्टोजेनेटिक्स नामक प्रकाशीय तकनीक से लंबे समय से भूखे कुछ चूहों में इन न्यूरॉन्स को सक्रिय किया; ऐसा करने पर चूहों ने कुछ नहीं खाया जबकि वे एकदम भूखे थे। जब इन न्यूरॉन्स को ‘शांत’ कर दिया गया तो चूहे खाने लगे। और तो और, भोजन के दौरान ही इन न्यूरॉन्स को सक्रिय करने पर चूहों ने फिर खाना छोड़ दिया।
इससे शोधकर्ताओं को लगा कि यही न्यूरॉन्स मितली या जी मिचलाने जैसी अनुभूतियों में शामिल होंगे। इसलिए उन्होंने चूहों को मितली पैदा करने वाले रसायनों का इंजेक्शन लगाया और फिर उनके मस्तिष्क का स्कैन किया। पाया गया कि जब चूहों को मितली महसूस होती है तो CeA के मध्य भाग (CeM) के DLKv न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं। लेकिन ये न्यूरॉन्स तब सक्रिय नहीं हुए थे जब चूहों का पेट सामान्य रूप से भर गया था या उन्हें सामान्य रूप से तृप्ति का एहसास हुआ था। अर्थात मस्तिष्क में तृप्ति और मितली के कारण खाने की अनिच्छा दो अलग जगह से नियंत्रित होती है। फिर शोधकर्ताओं ने मितली से परेशान और भूखे चूहों में इन न्यूरॉन्स की गतिविधि को अवरुद्ध करके देखा। पाया कि मितली की समस्या होने के बावजूद चूहों ने खाना खा लिया।
मस्तिष्क में मितली या तृप्ति को नियंत्रित करने वाले स्थान के बारे में समझना अनियमित खानपान, जैसा मोटापे या क्षुधानाश (एनोरेक्सिया) में होता है, जैसी समस्या को समझने में महत्वपूर्ण हो सकता है।
यह इन समस्याओं को थामने के लिए ऐसे उपचार तैयार करने में मददगार हो सकता है जो भूख को दबाकर तृप्ति का एहसास दें लेकिन मितली का अहसास न जगाएं। दूसरी ओर, मितली के अहसास को दबाकर खाने की इच्छा जगाई जा सकती है। मितली कई तरह के कैंसर उपचारों का एक आम साइड-इफेक्ट है जिसके कारण खाने के प्रति अरुचि पीडि़त को पर्याप्त पोषण नहीं लेने देती, जिसके चलते शरीर और कमज़ोर होता जाता है।(स्रोतफीचर्स)
इलेक्ट्रॉनिंग वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफियेबिल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी याचिकाओं को ख़ारिज किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100 फीसदी मिलान करने की याचिका को खारिज किया है।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ‘हमने दो निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश ये कि सिंबल के लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस यूनिट को सील किया जाए। सिंबल स्टोर यूनिट को कम से कम 45 दिन के लिए रखा जाए।’
वीवीपीएटी स्लिप पर पार्टी का चुनाव चिह्न और उम्मीदवार का नाम छापने के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट का इस्तेमाल होता है।
बीते साल चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नई सुविधा का एलान किया था। इसके जरिए पेपर ट्रेल मशीनों पर सिंबल लोड करने की प्रक्रिया में एक विज़ुअल डिस्प्ले जोड़ा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- लोकतंत्र सामंजस्य बनाए रखने के लिए होता है और आंख मूंदकर चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा ना करने से बिना कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है तो चुनाव आयोग उम्मीदवारों को उनकी फीस लौटाएगा।
चुनाव के नतीजे घोषित होने के 7 दिन के भीतर ईवीएम के माइक्रोकंट्रोल के वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवार चुनाव आयोग से गुज़ारिश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक तय फ़ीस देनी होती है।
चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों की शिकायत पर चुनाव आयोग ईवीएम निर्माता को ईवीएम के माइक्रोचिप के वेरिफिकेशन के लिए कह सकता है।
कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, ‘हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो है, इनमें एक ऐसी मेमरी होती है, जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि वीवीपैट की जांच करनी चाहिए। जो पर्ची निकलती है, उसे बैलेट बॉक्स में डालकर मिलान करना चाहिए।’
भूषण ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिकाओं को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ये जांच करे, सारे बैलेट पेपर पर हम बार कोड डाल दें तो उसकी मशीन के जरिए गिनती हो सकती है या नहीं।’
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के ज़रिए डाले गए सभी वोटों का वीवीपैट के साथ मिलान के लिए आग्रह करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था।।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कोर्ट ने चुनाव आयोग के सामने उठाए गए सभी सवालों के जवाब का संज्ञान लेने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रखा था।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है क्योंकि ईवीएम के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के जो जवाब आयोग की तरफ से दिए गए हैं, उसमें बहुत कुछ साफ नहीं है।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पीठ ने चुनाव आयोग के अधिकारी से ईवीएम के काम से जड़े पांच सवाल पूछे थे।
ईवीए पर उठते रहे हैं सवाल
ईवीएम, भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है।
भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में इसकी अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि करीब दो दशक से हर संसदीय और विधानसभा चुनाव में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है।
अपने 45 साल के इतिहास में ईवीएम को शंकाओं, आलोचनाओं और आरोपों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में ईवीएम बहुत अहम भूमिका निभाती है।
ईवीएम में गड़बड़ी या इसके ज़रिये धांधली से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने समय-समय पर कई कोशिशें भी की हैं।
इस लेख में हम जानेंगे कि ईवीएम क्या है, यह कैसे काम करती है, इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ, इन्हें बनाने में कितना खर्च होता है और इनके आने के बाद चुनाव प्रक्रिया कैसे बदली।
क्या होती है ईवीएम, मतपत्र से कैसे अलग है?
ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। साधारण बैटरी पर चलने वाली एक ऐसी मशीन, जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है।
ये मशीन तीन हिस्सों से बनी होती है। एक होती है कंट्रोल यूनिट (सीयू), दूसरी बैलेटिंग यूनिट (बीयू)। ये दोनों मशीनें पांच मीटर लंबी एक तार से जुड़ी होती हैं। तीसरा हिस्सा होता है- वीवीपैट।
बैलेटिंग यूनिट वह हिस्सा होता है, जिसे वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है और बैलेटिंग यूनिट को पोलिंग ऑफिसर के पास रखा जाता है।
ईवीएम से पहले जब बैलट पेपर यानी मतपत्र के जरिये वोटिंग होती थी, तब मतदान अधिकारी मतदाता को कागज का मतपत्र दिया करते थे। फिर मतदाता मतदान कंपार्टमेंट जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे मुहर लगा देते थे। फिर इस मतपत्र को मतपेटी में डाल दिया जाता था।
लेकिन ईवीएम की व्यवस्था में कागज और मुहर का इस्तेमाल नहीं होता।
अब मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर ‘बैलट’ बटन दबाते हैं, उसके बाद मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे लगा नीला बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करते हैं।
यह वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो जाता है। यह यूनिट 2000 वोट दर्ज कर सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना इसी यूनिट के माध्यम से की जाती है।
एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं।
अगर उम्मीदवार अधिक हों तो अतिरिक्त बैलेटिंग यूनिट्स को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है।
चुनाव आयोग के अनुसार, ऐसी 24 बैलेटिंग यूनिट एकसाथ जोड़ी जा सकती हैं, जिससे नोटा समेत अधिकतम 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान करवाया जा सकता है।
भारत के चुनाव आयोग के मुताबिक़, ईवीएम बहुत ही उपयोगी है और यह पेपर बैलट यानी मतपत्रों की तुलना में सटीक भी होती है, क्योंकि इसमें ग़लत या अस्पष्ट वोट डालने की संभावना खत्म हो जाती है।
इससे मतदाताओं को वोट देने में भी आसानी होती है और चुनाव आयोग को गिनने में भी। पहले सही जगह मुहर ना लगने के कारण मत खारिज हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता।
चुनाव आयोग कहता है कि इसके इस्तेमाल के लिए मतदाताओं को तकनीक का ज्ञान होना भी ज़रूरी नहीं है। निरक्षर मतदाताओं के लिए तो इसे और भी ज़्यादा सुविधाजनक बताया जाता है।
वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल
(वीवीपैट) क्या है?
ईवीएम को लेकर कई राजनीतिक दल आपत्ति जताते रहे हैं।
इन शंकाओं को दूर करने के इरादे से चुनाव आयोग एक नई व्यवस्था लेकर आया, जिसे वोटर वेरिफ़ायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएट) कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे वीवीपैट भी कहा जाता है।
यह ईवीएम से जोड़ा गया एक ऐसा सिस्टम है, जिससे वोटर यह देख सकते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं।
ईवीएम की बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबते ही बग़ल में रखी वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम, क्रम और चुनाव चिह्न वाली एक पर्ची छपती है, सात सेकंड के लिए वह वीवीपैट मशीन में एक छोटे से पारदर्शी हिस्से में नजऱ आती है और फिर सीलबंद बक्से में गिर जाती है।
वीवीपैट वाली ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार साल 2013 में नगालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान किया गया था। अब हर चुनाव में वीवीपैट को इस्तेमाल किया जाता है और यह ईवीएम का अभिन्न अंग है।
शंकाओं का निदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई है कि हर चुनावक्षेत्र की किसी एक मशीन का रैंडम तरीके से चयन किया जाता है और फिर ईवीएम मशीन के वोटों का मिलान, वीवीपैट पर्चियों के वोटों से किया जाता है।
चुनाव आयोग के अनुसार, अगर कहीं पर मशीन में आ रहे वोटों के आंकड़े वीवीपैट की पर्चियों के आंकड़ों से अलग आते हैं तो वीपीपैट के आंकड़ों को तरजीह दी जाएगी।
भारत में कौन सी कंपनियां बनाती हैं ईवीएम
ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को आयात नहीं किया जाता। इन्हें भारत में ही डिज़ाइन किया गया है और यहीं इनका निर्माण होता है।
चुनाव आयोग के अनुसार, इसके लिए दो सरकारी कंपनियां अधिकृत हैं। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) करती है, जो रक्षा मंत्रालय के तहत आती है और दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) जो डिपार्टमेंट ऑफ़ एटॉमिक एनर्जी के तहत आती है।
ये दोनों कंपनियां चुनाव आयोग की ओर से बनाई टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी (टीईसी) के मार्गदर्शन में काम करती है।
ईवीएम का अविष्कार और इस्तेमाल
दुनिया के अलग-अलग देशों में कई तरह की वोटिंग मशीनें प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही हैं। हालांकि, उनका स्वरूप भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम से अलग रहा है।
भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीन को डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ईवीएम (डीआरई) कहा जाता है।
चुनाव आयोग के अनुसार, भारत में वोटिंग के लिए मशीन इस्तेमाल करने का विचार सबसे पहले साल 1977 में सामने आया था।
तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एस।एल। शकधर ने इन्हें इस्तेमाल करने की बात की थी।
उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को ईवीएम डिजाइन और विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
1979 में ईवीएम का एक शुरुआती मॉडल विकसित किया गया, जिसे 6 अगस्त 1980 में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित किया।
बाद में बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को भी ईवीएम विकसित करने के लिए चुना गया।
पहली बार चुनावों में इस्तेमाल
भारत में चुनावों में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल साल 1982 में हुआ था। केरल विधानसभा की पारूर सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान बैलटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाली ईवीएम इस्तेमाल की गई।
लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज कर दिया था।
इसके बाद, साल 1989 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया और चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान किया।
इसके बाद भी इसके इस्तेमाल को लेकर आम सहमति साल 1998 में बनी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों में हुए चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ।
बाद में साल 1999 में 45 सीटों पर हुए चुनाव में भी ईवीएम इस्तेमाल की गई।
फऱवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम इस्तेमाल की गई।
मई 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुद्दुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों में सभी सीटों में मतदान दर्ज करने के लिए ईवीएम इस्तेमाल हुईं।
उसके बाद से हुए हर विधानसभा चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल होती आ रही हैं। 2004 के आम चुनावों में सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में मतदान के लिए 10 लाख से ज़्यादा ईवीएम इस्तेमाल की गई थीं।
अदालतों में याचिकाएं
ईवीएम के जरिये मतदान में धांधली के आरोप शुरू से ही लगते रहे हैं। इस तरह के मामले अदातों में भी पहुंचे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि विभिन्न हाई कोर्ट ने ईवीएम को भरोसेमंद माना है।
साथ ही, ईवीएम के पक्ष में हाई कोर्टों द्वारा दिए गए कुछ फैसलों को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों को खारिज कर दिया।
क्या है ईवीएम की लागत और क्या इनका इस्तेमाल महंगा है
जैसा कि अब तक हम जान गए हैं, वोटिंग मशीन के तीन मुख्य हिस्से होते हैं- कंट्रोल यूनिट (सीयू), बैलेटिंग यूनिट (बीयू) और वीवीपैट। भारत सरकार की प्राइस नैगोसिएशन कमेटी ने इन हिस्सों के दाम तय करती है।
चुनाव आयोग के मुताबिक, बीयू की कीमत है 7991 रुपये, सीयू की 9812 रुपये और सबसे महंगा हिस्सा है- वीवीपैट, जिसका दाम है 16,132 रुपये।
एक ईवीएम कम से कम 15 साल तक चलती है। इससे चुनाव प्रक्रिया सस्ती होने का भी दावा किया जाता है।
हालांकि, आलोचकों का कहना है कि चुनावों के बाद ईवीएम को स्टोर करके इनकी लगातार हाईटेक निगरानी करने में भारी भरकम खर्च आता है।
मगर चुनाव आयोग का कहना है कि भले ही शुरुआती निवेश कुछ ज़्यादा लगता है, लेकिन हर चुनाव के लिए लाखों की संख्या में मतपत्र छापने, उन्हें ढोने, स्टोर करने में होने वाले खर्च से बचत होती है।
इसके अलावा चुनाव आयोग के मुताबिक, मतगणना के लिए ज़्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक में कमी आने से निवेश की तुलना में कहीं ज़्यादा भरपाई हो जाती है। (bbc.com/hindi)
सलमान रावी
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाक़े कांकेर में 26 अप्रैल को मतदान होना है।
पड़ोस के जिले बस्तर में बीते 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। इस मतदान से पहले 16 अप्रैल को कांकेर जि़ला मुख्यालय से करीब 160 किलोमीटर दूर आपाटोला-कलपर जंगल के क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए थे।
पुलिस प्रशासन इस मुठभेड़ को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है।
इस घटना के 48 घंटों के अंदर माओवादियों ने प्रेस रिलीज़ जारी करके कहा कि ‘हमारे साथियों ने जंगल क्षेत्र में पनाह ली थी और उनको घेर कर मारा गया है।’
कांकेर के पुलिस अधीक्षक कल्याण एलेसेला ने बीबीसी हिंदी को बताया, ‘19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होना था। उससे ठीक पहले 15 अप्रैल को हमें बड़े नक्सली दस्ते के जमा होने की पुख्ता जानकारी मिली। यह इलाक़ा बस्तर और कांकेर, दोनों से नजदीक है। वहां पर बहुत बड़े कैडर और कमांडर थे, 60 से 70 की संख्या में माओवादी थे। हमने इलाके को घेरा और मुठभेड़ हुई।’
चुनाव से पहले पसरा सन्नाटा
माओवादियों ने जो बयान जारी किया है, उसमें सुरक्षाबलों पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है, ‘पुलिस के हमले में 12 साथियों की गोली लगने से मौत हुई थी। बाकी 17 साथियों को पुलिस ने घायल अवस्था में या जिंदा पकडक़र निर्मम हत्या की है।’
हालांकि बस्तर संभाग के आईजी पुलिस सुंदरराज पी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा, ‘सहानुभूति हासिल करने के लिए माओवादी इस तरह की दावे करते रहे हैं। ये उनके प्रोपेगैंडा का तरीका है।’ इस कथित मुठभेड़ में मारे जाने वालों में शंकर राव और उनकी पत्नी रीता डिविजनल कमेटी रैंक के माओवादी थे।
शंकर पर 25 लाख रुपये का इनाम घोषित था, जबकि रीता पर दस लाख रुपये का इनाम था।
कांकेर में 26 अप्रैल को मतदान होना है। माओवादियों ने पहले से चुनाव बहिष्कार करने की अपील की हुई है। लेकिन अब चुनाव से ठीक एक दिन पहले बंद का ऐलान किया गया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने इसे ‘क़त्ल कांड’ बताते हुए 25 अप्रैल को नारायणपुर, कांकेर, मोहला-मानपुर बंद को सफल बनाने की अपील की है।
ऐेसे माहौल में सुरक्षा बल के जवानों की मुस्तैद नजऱें और सडक़ों पर पसरा सन्नाटा, कई मायनों में डराने वाला लगता है।
माओवादियों के जिस तरह के बड़े लीडर इस घटना में मारे गए हैं, उसे देखते हुए पुलिस प्रशासन को आशंका है कि इसका बदला लेने के लिए माओवादी हमला कर सकते हैं।
नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव नक्सलबाड़ी से हुई है जहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 मे सत्ता और सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र आन्दोलन शुरू किया था।
साल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माओवादी हिंसा को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था, इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरुआत हुई।
साल 2009 में गृह मंत्री पी. चिदबंरम ने संसद में बताया था कि देश में माओवाद प्रभावित जि़लों की संख्या 223 थी। हालांकि मुख्य रूप से इनका असर देश के दस राज्यों के करीब 75 जि़लों में माना गया है।
किस बात की है आशंका
यूपीए सरकार के दौर में माओवादियों के खिलाफ सशस्त्र अभियान शुरू हुआ, वह बीते दस सालों से एनडीए सरकार के दौरान भी जारी रहा है।
बस्तर संभाग के आईजी पी सुंदरराज कहते हैं, ‘बस्तर संभाग में बीते तीन साढे तीन महीने में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 79 माओवादी मारे गए हैं। काफी हथियार भी बरामद हुए हैं। माओवादी अरेस्ट भी हो रहे हैं। उनके इकोसिस्टम पर असर पड़ा है।’
माओवादी हमले के पूर्ववर्ती मामलों को देखते हुए ये आशंका भी जताई जा रही है कि माओवादी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए भी कोई हमला कर सकते हैं।
हालांकि दूसरी ओर इस बात की आशंका भी है कि सुरक्षा बल के जवान माओवादियों के किसी दूसरे समूह को अपना निशाना बना लें।
यही वजह कि सडक़ों पर फैले सन्नाटे में भी खौफ़ पसरा हुआ है। 16 अप्रैल को हुए मुठभेड़ की जगह से सबसे नज़दीक गांव है छोटे बेठिया। उस गांव का कोई व्यक्ति किसी अनहोनी की आशंका में कैमरे पर कुछ नहीं बोलना चाहता।
एक तो दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालने की चिंता और ऊपर से दशकों से माओवादियों और सुरक्षाबल के बीच पिस रहे इन लोगों की जिंदगी में तकलीफ और अनिष्ट की आशंका ही स्थायी साथी बन गए हैं।
छोटे बेठिया गांव के लोगों में इस बात की राहत तो है कि इस मुठभेड़ में कोई गांव वाला नहीं मरा है, लेकिन यह राहत कब तक रहेगी, इसका कोई भरोसा उन्हें नहीं है। ना तो केंद्रीय सुरक्षा बल और ना ही राज्य सरकार, उन्हें अमन और चैन का भरोसा दिला पाई हैं।
इस इलाक़े में आम आदिवासियों की जिंदगी में कोई भी दिन ऐसा हो सकता है, जहां से परिवार तबाह हो सकते हैं। ये तबाही किन रूपों में आ सकती है- आप घर से बाहर निकले और क्रॉस फ़ायरिंग की चपेट में आ जाएं, सुरक्षा बल या माओवादी, किसी की भी गोली लग सकती है या फिर मुखबरी करने के आरोप में माओवादी आपको निशाना बना लें। या फिर माओवादी होने के शक में पुलिस मार दे।
बेगुनाह परिवारों का दर्द
यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि माओवाद पर अंकुश लगाने की इस लड़ाई में आम आदिवासियों की जि़ंदगी दांव पर लगी हुई है।
जब दांव पर जि़ंदगी लगी हो तो लोकतंत्र के महापर्व को लेकर भी बहुत उत्साह नहीं दिखता। लेकिन अच्छी बात यह है कि आम आदिवासी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना जान चुके हैं।
19 अप्रैल को बस्तर में करीब 68 प्रतिशत लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था। उम्मीद की जा रही है कि कांकेर में भी अच्छा मतदान होगा।
लेकिन इस लड़ाई का असर आम आदिवासियों पर कितना पड़ रहा है?
छत्तीसगढ़ के सबसे माओवाद प्रभावित इलाके अबूझमाड़ के इलाके की सरहद से लगा हुआ है पेवारी गाँव। कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग सौ किलोमीटर दूर सुदूर जंगल के बीच बसे इस गाँव में सूरजवती हिडको का भी घर है।
बीबीसी हिंदी की टीम जब इस घर तक पहुंची तो ख़ामोशी और उदास चेहरे ही दिखे। सूरजवती अनिल हिडको की वयोवृद्ध माँ है।
आँगन के एक कोने में बैठी हुई सूरजवती हिडको अपने आंसू पोछ रही हैं। दो महीने पहले परिवार में कमाने वाला बेटा था, बहू थी और पोता और पोती। लेकिन 24 फरवरी, 2024 को इन सबकी दुनिया उजड़ गई।
मां बताती हैं कि 28 साल का बेटा अनिल हमेशा की तरह 15 किलोमीटर दूर जंगल में तेंदू पट्टों को बाँधने के लिए रस्सी का इंतज़ाम करने गया हुआ था।
सूरजवती कहती हैं, ‘इसके अगले दिन यानी 25 फरवरी को शाम के समय उनके गाँव के लोगों ने ख़बर दी कि उनके बेटे की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। ये मुठभेड़ मरदा गाँव के पास की पहाड़ी पर हुई थी। कोई नहीं बता रहा है कि क्या हुआ, मेरे बेटे को रात 11 बजे दफऩाया गया। लाश देर से मिली हमें और बदबू की वजह से हम उसको घर में रख नहीं पाए साहब, परिवार वाले भी उसका चेहरा नहीं देख पाए।’
वहीं पास ही में गोद में बच्चे को लिए अनिल की पत्नी सूरजा हिडको का भी रो-रो कर बुरा हाल था। काफ़ी देर के बाद उन्होंने बात करनी शुरू की। उनकी चिंता थी कि वयोवृद्ध सास और ससुर के साथ साथ दो छोटे बच्चों को लेकर वो बाक़ी की जि़न्दगी कैसे गुजारेंगी।
वो कहती हैं, ‘मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। सास-ससुर के काम करने की उम्र नहीं है। घर में केवल मेरा पति कमाने वाला था। अब बताइए क्या करूं मैं। वो जंगल से रस्सी का सामान लाने गए थे। उनको मार दिया।’
फज़ऱ्ी मुठभेड़ का आरोप
25 फऱवरी को हुई जिस मुठभेड़ में अनिल के मारे जाने की बात कही जा रही है उसके बारे में सुरक्षा बलों का दावा है कि पेवारी गाँव से 25 किलोमीटर दूर मरदा गाँव के पास के पहाड़ में मुठभेड़ हुई थी जिस दौरान तीन माओवादी छापामारों को सुरक्षा बलों ने मारा था।
मगर पेवारी गाँव के मुखिया मंगलू राम का दावा है कि अनिल उनके यहां ट्रैक्टर चलाने की नौकरी करते थे।
घटना के बाद गाँव के सभी लोगों ने कांकेर जि़ले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है कि अनिल न तो माओवादी थे, ना ही उनका संगठन से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क रहा है।
मंगलू राम का कहना था, ‘वो हमारे घर का आदमी था। गाँव का लडक़ा है जो मेहनत मजदूरी करने वाला था। रोजगार गारंटी के तहत भी मजदूरी करता था। उसका कार्ड भी है। उसके अलावा उसका आधार कार्ड और पैन के साथ-साथ आयुष्मान कार्ड भी है। राशन लेने भी वो ही जाता था।’
‘हर महीने राशन लेने के बाद उसी के हस्ताक्षर हैं रजिस्टर पर और राशन कार्ड पर। वो तो जंगल गया था तेंदू पट्टे के लिए रस्सी बनाने का सामान इकठ्ठा करने। हमेशा जंगल जाता था। मुठभेड़ हुई बताया गया, गोली मार दी उसको। वो जंगल वाला आदमी (माओवादी) नहीं था। आम आदमी था। मेरा ट्रैक्टर भी चलाता था अनिल।’
बस्तर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज स्वीकार करते हैं कि छापामार युद्ध में इस बात की बहुत संभावना रहती है कि संघर्ष के दौरान आम आदमी भी पिस जाए।
वो ये भी दावा करते हैं कि ऐसी स्थिति में स्वतंत्र जांच करवाई जाती है और पीडि़तों के परिवारों को ‘मुआवजा भी दिया’ जाता है।
25 फरवरी को इन दोनों मौतों के बारे में उन्होंने कहा, ‘इन परिवारों की तरफ से शिकायतें मिली हैं, इसकी जांच कराई जा रही है।’
पी. सुंदरराज ने ऐसे मामलो के सामने आने पर कहा, ‘अगर माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ होती है और अगर उसमे कोई निर्दोष ग्रामीण को नुकसान होता है तो हम उस हकीकत को स्वीकार करते हैं। उसका जो मुआवजा बनता है वो उसके आश्रितों को देते हैं।’
निर्दोष ग्रामीण की मौत पर आश्रित परिवार को पांच लाख रुपये और घायल होने की सूरत में एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है।
लेकिन अहम सवाल यही है कि क्या कोई मुआवज़ा सूरजवती या फिर सूरज की उजड़ी दुनिया में रौनक वापस ला सकता है। या फिर मरदा गाँव के ख़ासपाड़ा में सोमारी बाई नेगी के परिवार की खुशियां वापस लौटा सकता है।
यह पूरा परिवार शोक में डूबा है, उनके पुत्र रामेश्वर नेगी भी 25 फरवरी को हुई मुठभेड़ में मारे गए। उनके परिवार ने भी सरकार को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि ये फर्जी मुठभेड़ थी।
क्यों है डर का माहौल
कांकेर में हुई मुठभेड़ 25 किलोमीटर दूर रहने वाले ग्रामीण कैलाश कुमार और पास के घरों में रहने वाले सवाल उठाते हैं कि अगर 25 फरवरी को मुठभेड़ हुई थी तो किसी सुरक्षा बल के जवान को कैसे कोई खरोंच भी नहीं आई?
गाँव वाले कहते हैं कि पुलिस दावा कर रही है कि एक देसी बंदूक भी बरामद की है मगर पूरे गाँव में किसी के पास कोई हथियार नहीं है।
कैलाश फऱवरी महीने में हुई मुठभेड़ के बारे में कहते हैं, ‘अगर दोनों तरफ़ से फायरिंग हुई होती तो जिन्हें पुलिस नक्सली कह रही है वो भी पुलिस पर हमला करते। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो हमारे आदमी को नक्सली कहकर मार दिए हैं।’
दंतेवाड़ा में रहने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता और पेशे से वकील बेला भाटिया ने बीबीसी हिंदी को बताया, ‘कई ऐसे मामले आए हैं जहां मुठभेड़ हुई और कई लोग मारे गए। कुछ मामलों में दो या तीन माओवादियों की शिनाख्त हुई और कई ऐसे भी रहे हैं जिनका माओवाद से कुछ लेना-देना नहीं था। बेगुनाह लोग जो क्रॉस फायरिंग में मारे जाते हैं उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। न माओवादी न कोई और संस्था, इसलिए डर का माहौल है।’
25 फरवरी को हुई मुठभेड़ को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाए थे।
इस महीने की बड़ी घटना के बाद फिर सवाल उठने लगे हैं कि अगर माओवादी कमज़ोर पड़ गए हैं और पीछे हट गए हैं तो फिर इतनी बड़ी तादाद में वो किस तरह हमला करने वाले थे।
इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने मीडिया को जो जानकारी दी, उसके मुताबिक घटना स्थल से 'एलएमजी, एनसास, कार्बाइन और एके-47' जैसे हथियार भी बरामद किए गए थे।
सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मारे गए माओवादियों के पास से इतने अत्याधुनिक हथियार कैसे बरामद हुए हैं?
इन सवालों पर पी सुंदरराज दावा करते हैं, ‘माओवादियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर भी हमले किए हैं और पिछले सालों में शस्त्रागार भी लूटे हैं। इनमे से बहुत सारे हथियार वैसे भी हैं। इसके अलावा वो देसी तरीक़े से भी हथियार बनाते हैं। वे विस्फ़ोटक भी बनाते हैं। इन विस्फोटकों से सुरक्षा बलों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है।’
बंदूक़ से नहीं निकलेगा रास्ता
सुरक्षा बलों और माओवादियों के इस संघर्ष के बीच पिसने वाले स्थानीय ग्रामीण आदिवासियों को अपने भविष्य को लेकर किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं दिखती।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सरकार में आने के बाद माओवादियों के ख़िलाफ़ अभियान में तेजी दिखी है लेकिन 16 अप्रैल की मुठभेड़ के बाद राज्य सरकार ने अब माओवादियों के साथ बातचीत की पेशकश भी की है।
राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं हो सकता इसलिए सरकार माओवादियों से बातचीत के लिए तैयार है।’
विजय शर्मा कहते हैं, ‘विकास भी बंदूक़ की नोक पर नहीं हो सकता इसलिए बातचीत का रास्ता अपनाना ही बेहतर होगा।’
लेकिन बीते तीन दशकों से बस्तर के इलाक़े में माओवादी और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव ही हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है। (bbc.com/hindi)
इकबाल अहमद
हाल ही में अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कांग्रेस से निकाले जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि फि़लहाल कांग्रेस में सत्ता के पांच केंद्र हैं।
संजय निरुपम के मुताबिक़- पार्टी के पांच केंद्र सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खडग़े और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं।
निरुपम मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी कर रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने बग़ावती सुर अपना लिए थे जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में संजय निरुपम शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल हो गए।
संजय निरुपम ने पार्टी आलाकमान और पार्टी अध्यक्ष की क़तार में केसी वेणुगोपाल की गिनती कर पार्टी के क़द्दावर महासचिव के सियासी क़द को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है या फिर केसी वेणुगोपाल वाक़ई कांग्रेस में सत्ता के पांचवें केंद्र बन गए हैं?
केसी वेणुगोपल पिछले सात सालों से कांग्रेस महासचिव हैं, लेकिन ऐसे महासचिव हैं जिनके बारे में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नपे-तुले शब्दों में कहा 'पार्टी के तमाम फ़ैसलों में उनकी अहम भूमिका है।'
पार्टी के तमाम बड़े फ़ैसलों और दूसरी पार्टी के साथ साझेदारी की बातों में अंतिम फ़ैसला वेणुगोपाल के ज़रिए ही सार्वजनिक होता है।
2023 में बने इंडिया गठबंधन के संयोजन समिति के वे प्रभावी सदस्य हैं, हालांकि ये बात और है कि केसी वेणुगोपाल ख़ुद को बेहद लो प्रोफ़ाइल रखते आए हैं।
दक्षिण भारत से छपने वाले सबसे बड़े अंग्रेज़ी अख़बार में काम करने वाली एक वरिष्ठ महिला पत्रकार ने अपना नाम ज़ाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, राहुल गांधी उन पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और पिछले पांच-छह सालों में निश्चित रूप से केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही ताक़तवर नेता बनकर उभरे हैं।
कांग्रेस पार्टी को दशकों से कवर कर रहे रशीद कि़दवई कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के संविधान में ही ऐसा कुछ है कि महासचिव (संगठन) गांधी परिवार और अगर अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का है तो उसके बाद सबसे शक्तिशाली पोस्ट है।
लेकिन क्या बात सिफऱ् यही है कि उस पद के कारण ही वेणुगोपाल इतने ताक़तवर बन गए हैं?
‘तीन मियां और एक मीरा’
इसका जवाब देते हुए रशीद कि़दवई कहते हैं, कांग्रेस में नेहरू (भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू) के बाद इंदिरा गांधी के ज़माने से ही कुछ लोग सर्वोच्च नेता के बहुत कऱीबी बनते रहे हैं जो कि पार्टी और (कांग्रेस या कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए) सरकार दोनों में दख़ल रखते थे।
रशीद कि़दवई आगे कहते हैं, इंदिरा गांधी के समय आरके धवन, एमएल फ़ोतेदार, यशपाल कपूर थे। राजीव गांधी के समय अरुण नेहरू, अरुण सिंह, नरसिम्हा राव के समय जितेंद्र प्रसाद, सीताराम केसरी के समय तारिक़ अनवर, सोनिया गांधी के समय अहमद पटेल और मौजूदा दौर में केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के उतने ही कऱीब और उतने ही शक्तिशाली बन गए हैं।
राजीव गांधी ने 1985 में अरुण सिंह, ऑस्कर फर्ऩांडीस और अहमद पटेल को अपना संसदीय सचिव बनाया था। यह एक शक्तिशाली गुट था और अनौपचारिक बातचीत में इन्हें ‘अमर-अकबर-एंथनी’ कहा जाता था।
जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे तो उनके कऱीबियों के लिए उस समय कांग्रेस के क़द्दावर नेता शरद पवार कहा करते थे, तीन मियां, एक मीरा (अहमद पटेल, ग़ुलाम नबी आज़ाद, तारिक़ अनवर और मीरा कुमार)।
यह अलग बात है कि कुछ ही दिनों बाद जब शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल को मुद्दा बनाकर कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया और अपनी नई पार्टी एनसीपी बनाई तो तारिक़ अनवर उसके एक संस्थापक सदस्य बने और अहमद पटेल, केसरी के बाद अध्यक्ष बनीं सोनिया गांधी के सबसे कऱीबी और गांधी परिवार के बाद पार्टी के सबसे ताक़तवर नेता बने।
अगर केसी वेणुगोपाल पर वापस लौटें तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि दक्षिण के एक छोटे से राज्य केरल से दिल्ली पहुंच कर उन्होंने कैसे यहां गांधी परिवार और ख़ासकर राहुल गांधी के कऱीबी लोगों में अपनी जगह बना ली।
लेकिन उससे भी पहले यह जानते हैं कि केसी वेणुगोपाल के राजनीतिक सफऱ की शुरुआत कैसे हुई।
वेणुगोपाल का सफऱ
दक्षिण भारत के वरिष्ठ पत्रकार केए शाजी कहते हैं कि सीपीएम के गढ़ माने जाने वाले उत्तरी केरल के कन्नूर से किसी कांग्रेसी नेता के लिए उभरकर आना बड़ी बात है।
सीपीआई (बाद में सीपीएम) के क़द्दावर नेता एके गोपालन कन्नूर जि़ला के ही थे। 1963 में कन्नूर जि़ले के पय्यानूर में जन्मे केसी वेणुगोपाल ने छात्र आंदोलन के रास्ते अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की।
केसी का परिवार पुराना कांग्रेसी और गांधीवादी था। उन्होंने अपनी जि़ंदगी का पहला चुनाव उस वक़्त लड़ा जब वो केवल 13 साल के थे और हाईस्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के इस चुनाव में उनको चुनौती दी थी सीपीएम के छात्र संगठन एसएफ़आई के उम्मीदवार ने।
केसी केरल स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने और फिर बाद में वो केरल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। 1987 में सीपीएम की सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने 10 लाख नौकरी देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया।
केरल की राजनीति में के करुणाकरण और एके एंटनी कांग्रेस के दो बड़े गुट रहे हैं। केसी वेणुगोपाल करुणाकरण गुट के वफ़ादार रहे। करुणाकरण ने 1991 में उन्हें कासरगोड से लोकसभा का टिकट दिलवाया था। उस वक्त उनकी उम्र महज़ 28 साल थी। उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा लेकिन मामूली अंतर से चुनाव हार गए।
1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव ने जब अर्जुन सिंह को पार्टी से निकाला तो करुणाकरण राव के साथ थे। इस समय केसी ने पहली बार करुणाकरण का सार्वजनिक रूप से विरोध किया था।
1995 के मार्च में एके एंटनी मुख्यमंत्री बने। एंटनी के सीएम बनने के बाद रमेश चेन्नीथला, जी कार्थीकेयन और एमआई शनावास जैसे नेताओं ने केरल कांग्रेस में एक तीसरा गुट बनाने की कोशिश की।
केसी इस तीसरे गुट में शामिल हो गए। यह लोग ख़ुद को सुधारवादी गुट कहते थे और उनके अनुसार वे लोग केरल कांग्रेस को करुणाकरण और एंटनी दोनों के प्रभावों से मुक्त कराना चाहते थे।
रशीद कि़दवई के मुताबिक़, एक राज्य ईकाई में भी तीसरे पायदान के नेता के लिए राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आना और एक शक्तिशाली महासचिव के अलावा पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का आंख और कान बन जाना केसी की बहुत बड़ी कामयाबी है।
1996 में वो पहली बार एमएलए बने। 2001 और 2006 में भी विधानसभा का चुनाव जीता। 2004 में ओमन चांडी की सरकार में पहली बार मंत्री बने। फिर 2009 में अलाप्पुझा से सांसद बने। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यमंत्री बनाए गए।
राजनीतिक शिखर की ओर
2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर के सामने कांग्रेस महज़ 50 सीटों के आस-पास सिमट गई तो वो केरल के अलाप्पुझा से दोबारा जीतकर लोकसभा पहुंचे और उन्हें पार्टी का व्हिप बनाया गया।
लेकिन उनके राजनीतिक करियर में अब तक का सबसे अहम मोड़ तब आया जब 2017 में अशोक गहलोत को राजस्थान वापस भेजा गया और राहुल गांधी ने उनकी जगह केसी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बनाया।
2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लडऩे का फ़ैसला किया। साल 2020 में वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए। लेकिन 2024 में वे एक बार फिर अलाप्पुझा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं।
2019 में कांग्रेस के गठबंधन वाली यूडीएफ़ ने केरल की 20 में से 19 सीटें जीती थीं। अलाप्पुझा अकेली ऐसी सीट थी जिसे सीपीएम ने जीती थी। इस सीट को दोबारा जीतने के लिए केरल कांग्रेस के सभी नेताओं ने केसी वेणुगोपाल से अपील की थी कि वो यहां से चुनाव लड़ें।
केसी को टिकट देने के लिए पार्टी को आखिऱी समय में केरल की लिस्ट में कुछ बदलाव भी करने पड़े ताकि सभी जाति और धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके।
इन सबके बावजूद उनके इस फ़ैसले की कुछ हलक़ों में आलोचना भी हो रही है। अगर वो लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं और अपनी राज्यसभा सीट छोडऩे का फ़ैसला करते हैं तो उनकी राज्यसभा की सीट बीजेपी के पास चली जाएगी क्योंकि राजस्थान में इस वक़्त बीजेपी की सरकार है और आंकड़े उनके पक्ष में हैं।
केसी ने मीडिया में इसका जवाब देते हुए कहा है, पार्टी की प्राथमिकता ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना है।
राहुल से निकटता
वरिष्ठ पत्रकार केए शाजी के अनुसार केरल में केसी की छवि साफ़ सुथरी रही है और जब ओमन चांडी सरकार में पर्यटन मंत्री थे तब उन्होंने कई अच्छे काम किए थे। एक सांसद के रूप में भी सदन में उनका रोल बहुत अच्छा रहा है। लेकिन केरल से दिल्ली पहुंचकर गांधी परिवार और ख़ासकर राहुल गांधी के कऱीब जगह बनाने में वो कैसे कामयाब हुए, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है।
लंबे समय से कांग्रेस को कवर करने वाले और केरल के रहने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपना नाम ज़ाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, यह एक रहस्य ही है कि दोनों कैसे कऱीब आए और इसका सही-सही जवाब शायद सिफऱ् दो ही लोगों के पास है राहुल गांधी और ख़ुद केसी वेणुगोपाल। और जब तक वो दोनों या उनमें से कोई एक ख़ुद नहीं बताता उस वक्त तक सिफऱ् अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार रशीद कि़दवई का आकलन है कि 2009 में लोकसभा पहुंचने के बाद केसी को जो घर मिला वो राहुल गांधी के घर के पास था। वो दोनों पड़ोसी बन गए। दोनों नेता फि़टनेस को लेकर काफ़ी अलर्ट रहते हैं।
2004 में सांसद बनने के बाद राहुल गांधी ने सदन में पीछे बैठने का फ़ैसला किया। केसी भी जब 2009 में चुनाव जीतकर आए तो उन्होंने भी सदन में पीछे बैठना शुरू कर दिया। इस वजह से दोनों में ज़्यादा मुलाक़ात होने लगी।
कि़दवई के अनुसार राहुल और केसी के कऱीब आने में इन सब ने भी अहम भूमिका निभाई है। दक्षिण भारत से छपने वाले सबसे बड़े अंग्रेज़ी अख़बार में काम करने वाली एक वरिष्ठ महिला पत्रकार ने भी माना कि दिल्ली में राहुल गांधी और केसी के घर आस-पास होने की वजह से भी उन्हें एक दूसरे के कऱीब आने का मौक़ा मिला।
केसी का एक्स फ़ैक्टर
राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल चाहे जिन कारणों से भी कऱीब आए हों लेकिन फिर भी यह सवाल तो उठता ही है कि केसी में ऐसा क्या है कि राहुल गांधी उन्हें इतना पसंद करते हैं और उन पर इतना भरोसा करते हैं।
केए शाजी कहते हैं, गांधी परिवार से उनकी वफ़ादारी उनकी सबसे बड़ी ताक़त है। गांधी परिवार को उनकी वफ़ादारी पर पूरा भरोसा है। उनके अनुसार केसी अपने नेता राहुल गांधी को पूरी तरह फ़ॉलो करते हैं, उसमें किसी तरह के शक-शुब्हे की कोई गुंजाइश नहीं है।
केसी को यह बात पता है कि एक परिवार के दबदबे वाली कांग्रेस पार्टी में वफ़ादारी की क्या अहमियत है। इस वफ़ादारी के कारण कई बार आपको अपने सर्वोच्च नेता के लिए कवच का काम करना होता है और अपने नेता को निशाना बनाते हुए चलाए गए विरोधियों के तीर ख़ुद अपने शरीर पर लेने होते हैं। कांग्रेस पार्टी को कवर करने वालों के अनुसार केसी ने कई बार ऐसा किया है।
दक्षिण भारत की वरिष्ठ महिला पत्रकार कहती हैं, राहुल गांधी को लगता है कि अगर केसी नहीं होते तो वो संसद में नहीं पहुंच पाते। ज़्यादातर पत्रकारों की तरह उनका भी मानना है कि केसी ने ही राहुल गांधी को 2019 में केरल के वायनाड से चुनाव लडऩे के लिए तैयार करवाया क्योंकि उन्हें अंदाज़ा लग गया था कि यूपी में अमेठी से वो चुनाव हार सकते हैं।
नतीजे आने के बाद हुआ भी वही, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंचे।
उनके अनुसार राहुल को लगा कि केसी नए आइडियाज़ वाले व्यक्ति हैं और वो अकबर रोड (कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय) की कोटरी(बेहद कऱीब लोगों) में शामिल नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केसी की नियुक्ति के ज़रिए राहुल गांधी अहमद पटेल को भी एक संदेश देना चाहते थे।
क्या ये राहुल के अहमद पटेल हैं?
केसी की एक और ख़ूबी का जि़क्र करते हुए वो कहती हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में आधिकारिक ख़बरें आने से पहले ही सबको पता चल जाती हैं लेकिन जबसे केसी संगठन महासचिव बने हैं पत्रकारों को तो दूर ख़ुद पार्टी के एमपी और एमएलए को भी कोई ख़बर नहीं मिल पाती है जब तक कि उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है।
राहुल से उनकी निकटता की एक मिसाल देते हुए वो कहती हैं कि लोकसभा का सत्र चल रहा था और राहुल गांधी केरल में एक आयुर्वेदिक सेंटर में किसी उपचार के लिए गए थे तो वहां भी केसी उनके साथ थे।
केरल के रहने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक़, आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के भविष्य और वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर राहुल गांधी की जो सोच है, केसी उससे पूरी तरह सहमत दिखते हैं। केसी एक पक्के कांग्रेसी और गांधीवादी हैं। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी के कऱीबी लोगों ने जिस तरह से पार्टी छोडक़र बीजेपी का दामन थामा है उस हालत में केसी की कट्टर कांग्रेसी विचारधारा उन्हें राहुल के और कऱीब लाती है।
कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के लिए वही हैसियत रखते हैं जो कभी अहमद पटेल सोनिया गांधी के लिए रखते थे। पीवी नरसिम्हा जब प्रधानमंत्री थे तब 10 जनपथ (सोनिया गांधी का निवास) से किसी भी तरह की बातचीत के लिए अहमद पटेल का सहारा लेते थे।
यह भी माना जाता है कि केसी के संबंध मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े से बहुत अच्छे हैं और इस कारण वो राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं।
कांग्रेस कवर करने वाले केरल के वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार अहमद पटेल और केसी के काम करने के तौर-तरीक़े में भी फक़ऱ् है। उनके अनुसार अहमद पटेल को जब कोई काम करवाना होता था तो वो कई बार सोनिया गांधी का नाम लेते थे, लेकिन केसी को किसी से भी कोई काम करवाना होता है तो वो कभी भी राहुल गांधी का नाम नहीं लेते हैं कि राहुल ऐसा चाहते हैं।
रशीद कि़दवई के अनुसार दोनों की तुलना सही नहीं है। सबसे बड़ा फक़ऱ् तो यह है कि अहमद पटेल के बारे में जितनी भी बातें होती हैं वो उस दौरान की हैं जब केंद्र (2004-2014) में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि केसी राहुल गांधी के साथ उस समय से हैं जब कांग्रेस ना केवल विपक्ष में है बल्कि पार्टी पिछले दो चुनावों (2014, 2019) में पचास सीटों तक सिमट कर रह गई है।
केसी और विवाद
रशीद कि़दवई के अनुसार राजनीतिक सूझ-बूझ, फ़ंड जमा करने और दूसरी पार्टियों से तालमेल के मामले में अहमद पटेल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है।
रशीद कि़दवई कहते हैं, अहमद पटेल सबकी बात सुनते थे और अपनी तरफ़ से उसमें कुछ भी जोड़े बग़ैर सोनिया गांधी तक वो बात पहुंचा देते थे जबकि केसी पर यह आरोप लगते हैं कि वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का सही फ़ीडबैक राहुल गांधी तक नहीं पहुंचाते हैं।
अहमद पटेल कांग्रेस के जि़ला कार्यकर्ता को भी उनके पहले नाम से जानते थे, जबकि केसी को हिंदी हार्टलैंड की राजनीति की जानकारी थोड़ी कम है।
रशीद कि़दवई कहते हैं कि केसी का क़द इतना बड़ा नहीं है कि वो दिल्ली के गलियारों में ख़ुद कोई फ़ैसला कर सकें इसीलिए वो रणदीप सुरजेवाला की गुना-भाग करने वाली क्षमता और जयराम रमेश की बौद्धिक क्षमता पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं।
ऐसा नहीं है कि केसी का नाम कभी विवादों में नहीं रहा। केरल सोलर स्कैम में भी उनका नाम आया और 2018 में यौन उत्पीडऩ के एक मामले में क्राइम ब्रांच ने उन पर केस भी दर्ज किया। लेकिन इन आरोपों के बावजूद केसी की पार्टी के अंदर बढ़ते क़द में कोई रुकावट नहीं आई।
बाद में सीबीआई ने उनको क्लिन चिट दे दी और अदालत ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी थी।
कुछ महीने पहले मीडिया में इस तरह की ख़बरें भी आईं थीं कि कांग्रेस का एक गुट केसी को उनके पद से हटाने की कोशिश कर रहा है।
दक्षिण भारत से प्रकाशित होने वाले अख़बार के वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सांसद ने उनसे कहा था कि हमलोग कऱीब 20 साल तक अहमद पटेल की शिकायत करते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सोनिया गांधी का पूर्ण समर्थन हासिल था, केसी के मामले में भी यही है उन्हें राहुल गांधी का पूर्ण समर्थन हासिल है। (bbc.com/hindi)
हाथ हिलाकर विदा कहना, झुककर अभिवादन करना, ठेंगा दिखाना, ऐसे कई इशारे या भंगिमाएं हम अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आपस में इसी तरह मेलजोल करते एक ‘शिष्ट’ पक्षी जोड़े को देखा है।
जापान के नागानो में लिए गए वीडियो में दो जापानी टिट पक्षी (Parus mino) कैद हुए हैं। वीडियो में दिखता है कि जब पक्षियों का ये जोड़ा अपने चूज़ों के लिए भोजन लेकर घोंसले को लौटता है तो मादा घोंसले के पास वाली डाल पर जाकर बैठ जाती है और पंख फडफ़ड़ा कर अपने साथी को पहले घोंसले में जाने का इशारा करती है। जब साथी घोंसले के अंदर चला जाता है तो उसके पीछे-पीछे वह भी घोंसले मे चली जाती है।
करीब 8 पैरस माइनर जोड़ों के 300 से अधिक बार घोंसले में लौटने के अवलोकनों से पता चला कि मादाओं का फडफ़ड़ाना अधिक था; वे फडफ़ड़ा कर ज़ाहिर करती हैं कि उनके साथी पहले घोंसले में जाएं और वे उनके अंदर जाने तक रुकी रहती हैं। लेकिन जब मादा पंख नहीं फडफ़ड़ाती तो इसका मतलब होता है वह पहले घोंसले में जाना चाहती है। पक्षियों में ‘पहले आप’ की शिष्टता उजागर करते ये नतीजे करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं।
मादा पंख फडफ़ड़ाते हुए अपने साथी की ओर मुखातिब थी, न कि घोंसले की ओर। इससे पता चलता है वह केवल घोंसले का पता नहीं बता रही थी बल्कि कोई संदेश भी दे रही थी। रुचि की किसी चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित करने का व्यवहार कौवों सहित अन्य पक्षियों में देखा गया है, लेकिन सांकेतिक इशारों को अधिक जटिल माना जाता है। इस तरह से संदेश देने के व्यवहार इसके पहले प्रायमेट्स के अलावा अन्य किसी प्राणि में नहीं देखे गए हैं।
इसका वीडियो यहां देख सकते हैं: https://www.science.org/content/article/after-you-female-bird-s-flutter-conveys-polite-message-her-mate (स्रोतफीचर्स)
सलमान रावी
वह 2009 का लोकसभा चुनाव था। उसमें आखिरी बार कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में कांग्रेस ने 440 उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से 209 सीटों पर उसे जीत मिली थी।
उसका यह प्रदर्शन लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से कम था। इसलिए संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन (यूपीए) की सरकार दोबारा बनी।
इससे पहले 2004 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को सिफऱ् 145 सीटें ही मिलीं थीं, जबकि उसने 417 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 529 सीटों पर चुनाव 1996 में लड़ा था।
18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान शक्रवार को हो चुका है। इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है।
कांग्रेस अब तक 301 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और उसके 300 से 320 सीटों पर ही चुनाव लडऩे की संभावना है। यह 1951 से लेकर अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में 464 उम्मीदवार उतारे थे, वहीं 2019 के चुनाव में उसने 421 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। साल 2019 में उसे 421 सीटों में से केवल 52 पर ही जीत मिली थी।
इस समय कैसी है कांग्रेस की हालत
ऐसे में कांग्रेस की इस स्थिति पर कई सवाल उठने लाज़मी हैं। राजनीतिक गलियारों में इस पर ख़ूब चर्चा भी हो रही है कि सबसे पुराने राष्टीय दल कांग्रेस को ऐसा क्यों करना पड़ा।
जानकार बताते हैं कि पिछले 10 साल में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से चरमरा गया है। यह स्थिति उसी तरफ़ इशारा करती है।
लंबे समय से कांग्रेस पर नजर रखने वाले लेखक और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने बीबीसी से कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
उन्होंने कहा, ‘इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समझ में आने लगा था कि वो सिफऱ् अपने बूते भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उसने क्षेत्रीय दलों पर ज़्यादा भरोसा किया। इसे एक तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है कि उसने त्याग की भावना से ऐसा किया है।’
किदवई कहते हैं कि बीजेपी और एनडीए को सीमित करने के लिए क्षेत्रीय दलों का सहारा लेने के सिवा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था।
वो मानते हैं कि ‘इस बार कांग्रेस ने अपनी जीत का लक्ष्य भी कम ही रखा हुआ है। वो आधे की भी आधी सीटें जीत पाए तो वो संगठन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।’
लेकिन कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कितना मजबूत होगा, यह तो समय ही तय करेगा।
रशीद किदवई कहते हैं, ‘कांग्रेस ने गठबंधन तो कर लिया है मगर उसके साथ आने वाले दल अपने अलग-अलग घोषणापत्र लेकर आए हैं। उन दलों ने कांग्रेस के घोषणापत्र को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है। इसलिए कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को कितना चुनावी लाभ मिल पाएगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। कांग्रेस के घोषणापत्र को इण्डिया गठबंधन का साझा घोषणापत्र होना चाहिए था। यहां भी कांग्रेस चूक गई।’
कितनी सीटों पर लड़ाई में हैं क्षेत्रीय दल
जानकार कहते हैं कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से लगभग 200 ऐसी सीटें हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय दलों से सीधा चुनावी संघर्ष है। इस मायने में भी कांग्रेस के पास इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं था।
वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह कहते हैं कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस का जो हाल हो चुका है, यानी जिस तरह पिछले पांच साल में संगठन के बड़े और छोटे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन एक-एक कर थामा है, वैसी परिस्थिति में कांग्रेस के सामने सिर्फ यही एक विकल्प बचा हुआ था।
एनके सिंह अभी विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बागडोगरा एयरपोर्ट से फोन पर कहा कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है, जहां उसे योग्य उम्मीदवारों का भी अभाव होने लगा है।
उनका कहना था, ‘कांग्रेस के पास तो मौजूदा हालात में सभी सीटों पर लड़ाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में यही एक विकल्प उसके सामने था कि वो क्षेत्रीय दलों का ही समर्थन करे और उनसे समर्थन ले।’
इस क्रम में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों को दे दीं। इसमें अकेले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में कुल 201 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 20 या उससे कम सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी।
उसी तरह वो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 17 पर ही चुनाव लड़ेगी जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 पर और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस 10 पर लड़ रही है।
क्या भाजपा ने पकड़ी है कांग्रेस की राह
राजनीतिक टिप्पणीकार विद्याभूषण रावत कहते हैं कि जो कांग्रेस कर रही है वो राजनीति में कुछ नया नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कर चुकी है। वो कहते हैं कि विभिन्न दलों के बीच गठबंधन ही भविष्य की राजनीति का स्वरूप होने वाला है।
उनका कहना था, ‘काफी कुछ बदला है राजनीति में भी। अब क्षेत्रीयता भी बढ़ रही है और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भी। जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है, उसमें काफी कुछ बदलने वाला है। आने वाले सालों में राष्ट्रीय दलों का मत प्रतिशत भी कम होता चला जाएगा। कांग्रेस के लिए यही बेहतर विकल्प था कि वो ख़ुद हाथ-पांव मारने की बजाय और मतों का विभाजन करवाने की बजाय क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूत गठबंधन करे। उसने ऐसा ही किया है। इसके लिए कांग्रेस ने 200 से ज़्यादा सीटों की कुर्बानी भी दी है।’
जानकार यह भी कहते हैं कि जिस दौर से कांग्रेस अभी गुजर रही है, ऐसे में उसके राजनीतिक भविष्य के लिए यही बेहतर रहेगा कि वो कम से कम सीटों पर लड़े और बीजेपी के उम्मीदवार को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करे।
रावत कहते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में राजनीति कर रही है, इससे पहले कांग्रेस यही किया करती थी। चाहे वो फिल्मी सितारों को मैदान में उतारने की बात हो या दूसरे राजनीतिक दलों से अपने संगठन में नेताओं को शामिल करने की बात हो।
उन्होंने अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त और राजेश खन्ना का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने भी उस समय के दिग्गज विपक्षी नेताओं के खिलाफ सिनेमा के इन बड़े सितारों को उतारा था।
वो कहते हैं, ‘पहले समाज और नौकरशाही का ‘एलीट’ तबक़ा कांग्रेस के साथ हुआ करता था। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाती है, यह देखने वाली बात होगी। इसी पर कांग्रेस का भविष्य भी निर्भर करेगा।’ (bbc.com/hindi)
-राजीव
हाल ही में देश के सबसे बड़े एवं प्रतिष्ठित परीक्षा बोर्ड सीबीएसई ,नई दिल्ली ने देश के बीस स्कूलों को फर्जी उपस्थिथि मामले में कार्रवाई की और उनकी मान्यता रद्द कर दी . इस तरह की संभवत यह स्कूली शिक्षा के इतिहास में पहली और सबसे बड़ी कार्रवाई है . यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि कक्षा ग्यारवीं और बारवीं में अध्यनरत व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे नीट ( मेडिकल प्रवेश) एवं जी.ई.ई. (इंजीनियरिंग/आई.आई.टी.) पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने स्कूल में उपस्थिथि न देकर उसी समय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग ले रहे थे और स्कूल उनकी गैरमौजूदगी में भी उपस्थिथि दर्शा रहे थे .
देश के तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में नियमित विद्यार्थियों के लिए एक तय प्रतिशत हाजिरी जरूरी है. सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में यह पचहतर प्रतिशत है. स्कूल में ना जाकर कोचिंग में पढ़ना यह समस्या पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गई है. यह इतनी बढ़ गई है कि पूरे देश खासकर महानगरों के अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले स्कूलों में ग्यारवीं और बारवीं के विद्यार्थियों की संख्या लगभग नगण्य हो गई हैं. अच्छे अकादमी रिकॉर्ड वाले स्कूल ऐसी फर्जी हाजरी के चलन से अपने आप को बाहर रखे हुए हैं क्योंकि यह नैतिक रूप से गलत है .देश में बहुत से स्कूल अपनी हायर सेकण्ड्री कक्षाएं ( ग्यारवीं और बारहवीं ) बंद करने की भी सोच रहे हैं. उनका मानना है कि अभी सिर्फआर्ट्स एवं कॉमर्स के विद्यार्थी ही हायर सेकण्ड्री कक्षाएं में अपनी हाजिरी दे रहे हैं . साइंस विषय के लगभग सारे विद्यार्थी ऐसे डमी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं जिनका कोचिंग संस्थानों से साठ-गांठ है.
आर्ट एवं कॉमर्स के बच्चों की भी आगे उपस्थिथि को लेकर अनिश्चय की स्थिति है. पूरे देश में विश्विद्यालयों में प्रवेश के लिए एक परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है और बहुत से विश्विद्यालय अब इसी प्रवेश परीक्षा के मेरिट से प्रवेश ले रहें है. यह विद्यार्थी भी एंट्रेंस के लिए कोई ना कोई जुगाड़ बैठाएंगे , कोचिंगों में जाएंगे और इनकी भी हाजिरी लगातार कम होने की संभावना है . फर्जी उपस्थिथि वाले पूरे मामले में एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि पैसे वाले पैसों से अपने बच्चों के लिए उपस्थित खरीद रहे हैं .
ऐसा भी नहीं है सीबीएसई बोर्ड की हालिया कार्यवाही से विद्यार्थी स्कूलों जाने लग जाएंगे. यह कोचिंग और फर्जी उपस्थिथि का सिलसिला नहीं रुकेगा . देश या किसी भी प्रदेश में इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के विषय में कोई सोच भी नहीं रहा जबकि स्कूली शिक्षा को बचाने और बच्चों को मानसिक दबाव से मुक्त करने के लिए इसका उपाय खोजना बहुत जरूरी हो गया है.
जो बड़ा नुकसान सामने से नहीं दिखता वह इन कोचिंग में जाने के बाद इन बच्चों का बौद्धिक, शारीरिक विकास का रुक जाना है. समझ लीजिए हम खुले बगीचे से बच्चों को गैस के ऊपर रखे प्रेशर कुकर के समान बैठा देते हैं. यह अत्यंत ही चिंतनीय है. लेकिन अगर कोई समस्या सामने आन खड़ी है तो उसका इलाज भी ढूंढना होगा. आखिर इस समस्या से कैसे निपटा जाए ?
आज जो स्थिति है उसमें तीन पक्ष है. पहले विद्यार्थी खुद ,दूसरे उसके पालक, तीसरा पक्ष कोचिंग और स्कूल है जो लगभग एक दूसरे के आमने-सामने है. आज के समय में कोई भी पालक अपने बच्चों को दौड़ में पीछे नहीं रखना चाहता , कोई मां-बाप अपने बच्चों को यह नहीं कहता की परीक्षा में दूसरा या तीसरा आना . हर मां-बाप अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देखना चाहते हैं.
मौजूदा परिस्थिथि का एक बड़ा कारण भारत में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का सिंगल विंडो सिस्टम है इस एंट्रेंस एग्जाम के पाए हुए नंबर से तय हो रही मेरिट से महाविद्यालयों में प्रवेश मिल रहा है . यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि पूरे देश में अलग-अलग सिलेबस और परीक्षा बोर्ड है. बोर्ड / सिलेबस अलग-अलग होने से आंकलन का पैमाना तय नहीं किया जा सकता. अब समय आ गया है की कम से कम सिलेबस में एकरूपता लाई जाए एकरूपता लाने से कई फायदे होंगे .पहला और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बारहवीं के प्राप्तांक को प्रवेश परीक्षा के अंकों के साथ जोड़कर महाविद्यालय प्रवेश की मेरिट तय की जा सकती है . इसका एक अन्य रूप जी.ई.ई. में है जिसमें के आई आई टी के प्रवेश में बारहवीं में पचहतर प्रतिशत अंक लाने जरूरी है .इससे न केवल बारवीं कक्षा की परीक्षा को महत्व मिलेगा बल्कि स्कूलों में आमद बढ़ेगी.
एक बहुत जरूरी सुधार जो सभी परीक्षा बोर्ड को करना चाहिए वह यह की व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा खासकर नीट एवं जी.ई.ई. दे रहे विद्यार्थियों में भाषा के पाठ्यक्रम को हायरसेकण्ड्री के सिलेबस में काम कर दे या हटा दे . इससे ग्यारवीं और बारवीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर समग्र रूप से पढाई का बोझ कम होगा तथा स्कूल में उपस्थिथि का समय कम हो जायेगा .स्कूल में उपस्थित का समय अन्य कक्षाओं की अपेक्षा इन दोनों कक्षाओं में कम किया जाना भी एक कारगर उपायों में से हो सकता है . दिन का बचा हुआ समय विद्यार्थी अपनी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में लगा सकता है. विद्यार्थियों को स्वयं से पढाई या किसी विशेषज्ञ टीचर से पढ़ने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा.
इस वर्ष नीट (मेडिकल प्रवेश) में पच्चीस लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा आवेदन फॉर्म भरा है और उपलब्ध सीट संख्या एक लाख के आसपास हैं उसमे से भी आधी ही शासकीय मेडिकल कॉलेज की है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट या आईआईटी की परीक्षा में दबाव है. हर श्रेणी के विद्यार्थी पर बहुत अच्छा करने का दबाव है .
परीक्षा के इस दबाव को कम करने के लिए शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं और इन विद्यार्थियों का भला चाहने वाले लोगों को मिल बैठकर काम करना होगा .
 डॉयचे वैले पर जिया उर रहमान की रिपोर्ट-
डॉयचे वैले पर जिया उर रहमान की रिपोर्ट-
कई जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के रिश्तों में मौजूदा तनाव की वजह पाकिस्तान में सीमापार से बढ़ता आतंकवाद है। लेकिन पाकिस्तान ने भी हाल के समय में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे अफगानिस्तान की तालिबान सत्ता नाराज है। पिछले साल, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार पर कई तरह की पाबंदियां लगा दीं। इसके अलावा पाकिस्तान में बिना दस्तावेज रह रहे करीब पांच लाख अफगानों को देश से बाहर निकाला और सख्त वीजा नीतियां लागू कीं।
पिछले महीने, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, जिसमें आठ लोग मारे गए। इसके बाद अफगान बलों ने भी सीमा पर जवाबी कार्रवाई की।
आशा से तनाव तक
वॉशिंगटन डीसी में एक थिंकटैंक पोलिटैक्ट में दक्षिण एशिया फेलो नाद-ए-अली सुलेहरिया ने डीडब्ल्यू को बताया कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जिस तरह उसने हमेशा तालिबान का साथ दिया है, जब वे सत्ता में आएंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा।
सुलेहरिया के अनुसार, खासकर पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और अन्य पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के खिलाफ कदम उठाएगी, और ‘अफगानिस्तान में उनके अड्डों को खत्म किया जाएगा।’ लेकिन काबुल में तालिबान शासन के पहले साल के भीतर ही पाकिस्तान की यह उम्मीद टूट गई। इसके बजाय, पाकिस्तान में आतंकवाद और बढ़ गया क्योंकि तालिबान के सत्ता में लौटने से टीटीपी का हौसला और ताकत, दोनों बढ़ीं।
इस्लामाबाद के सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में आतंकवादी हमलों से होने वाली मौतों में 56 फीसदी का इजाफा हुआ है, जिसमें 500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों के साथ-साथ 1,500 से अधिक लोग मारे गए।
इसी हफ्ते, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दो जिलों में दो अलग-अलग हमलों में दो पुलिस अधिकारी मारे गए और छह लोग घायल हो गए।
तालिबान का समर्थन क्यों किया है?
तालिबान के साथ पाकिस्तान का रिश्ता बड़ा ही पेचीदा और अक्सर विरोधाभासी रहा है, जो लगातार ऐतिहासिक घटनाओं और रणनीतिक समीकरणों के कारण बदलता रहता है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, लेकिन 1893 में अंग्रेजों द्वारा खींची गई 2,640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा डूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है।
इस रेखा ने पश्तून कबायली भूमि को विभाजित कर दिया। इससे पश्तूनों के लिए अलग देश ‘पश्तूनिस्तान’ की भावना ने जन्म लिया जिसमें सीमा के दोनों ओर के पश्तून क्षेत्र शामिल हों। हालांकि यह देश कभी नहीं बन सका, लेकिन इस पर विवाद आज भी जारी है।
दूसरी ओर, 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के बाद पाकिस्तान ने सीमापार मुस्लिम चरमपंथियों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली।
इस्लामाबाद में स्थित अफगान इतिहास शोधकर्ता उबैदुल्ला खिलजी कहते हैं, ‘सोवियत प्रभाव से निपटने के लिए पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और उसके जरिए उन अफगान मुजाहिद्दीन को हर तरह की मदद पहुंचाई, जो सोवियत हमले का मुकाबला कर रहे थे।’
सोवियत वापसी के बाद, अफगानिस्तान गृहयुद्ध में उलझ गया, जिससे एक नए इस्लामी कट्टरपंथी गुट तालिबान का जन्म हुआ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने 1996 में अफगानिस्तान के तालिबान शासन को मान्यता दी, और उन्हें महत्वपूर्ण सैन्य सहायता और संसाधन दिए।
11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अफगानिस्तान पर हमला किया और इसके बाद 2001 के अंत में अफगानिस्तान में तालिबान शासन का खात्मा हो गया।
हालांकि, तालिबान के कुछ सदस्यों को पाकिस्तान के अंदर, खासकर सरहदी इलाके में शरण मिल गई। पाकिस्तान ने 9/11 के बाद अमेरिका का साथ दिया। यह जगजाहिर है कि पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ लोगों ने तालिबान को गुप्त समर्थन भी दिया। और इस समर्थन ने अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता वापसी में अहम भूमिका निभाई।
तालिबान सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर कहा, ‘तालिबान ने पाकिस्तान का इस्तेमाल अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए एक ठिकाने के तौर पर किया, जबकि पाकिस्तान ने हमें अफगानिस्तान में बढ़ते भारतीय प्रभाव से निपटने के हथियार के तौर पर देखा था।’
तालिबान की सत्ता में वापसी ने नाटकीय रूप से चीजों को बदल दिया है। क्विंसी इंस्टीट्यूट के मध्य पूर्व विभाग के उप निदेशक एडम वाइनस्टीन के अनुसार, तालिबान अब पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है, तालिबान अब ‘खुद को पाकिस्तान के अधीन देखने या उसकी मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं मान रहा है।’
तालिबान नेता पाकिस्तान की पिछली मदद को स्वीकार करते हैं लेकिन वे यह भी बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने तालिबान नेताओं का उत्पीडऩ किया, उनकी गिरफ्तारियां कीं और उन्हें अमेरिका को सौंपा। तालिबान और टीटीपी के बीच की वैचारिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समानताएं भी तालिबान प्रशासन को एक जटिल समस्या में डाल देते हैं।
तालिबान अधिकारी ने कहा, ‘पाकिस्तान की मांग के अनुसार, टीटीपी पर कार्रवाई करने से खुद तालिबान के भीतर ही समस्या खड़ी हो सकती है। इस वजह से लोग, पहले से ही तालिबान से लड़ रहे चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट में जा सकते हैं।’
तालिबान नए सहयोगी चाहता है
जहां पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठंडे पड़ रहे हैं, वहीं तालिबान प्रशासन नई साझेदारियां बना रहा है। पश्चिमी देश झिझक रहे हैं, लेकिन चीन, रूस, ईरान, भारत और कुछ मध्य एशियाई देश बेहद सावधानी के साथ तालिबान से संबंध बढ़ा रहे हैं। पोलिटैक्ट फेलो सुलेहरिया बताते हैं कि तालिबान प्रशासन अपने प्रचुर खनिज संसाधनों को इस्तेमाल कर चीन के विदेशी निवेश के जरिए अच्छा-खासा पैसा कमा रहा है।
सुलेहरिया ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कदम रखने के लिए ईरान का रुख कर रहे हैं, जो साझेदारी में नएपन का संकेत है।’ हालांकि अफगान तालिबान के लिए कोई भी नई साझेदारी इतनी मजबूत नहीं है जो पाकिस्तान की जगह ले सके। फिर भी, तालिबान आत्मनिर्भरता के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता का लाभ भी उठा सकता है। और चूंकि सभी देश स्थिरता चाहते हैं, तो तालिबान को इसका भी फायदा मिल सकता है।
क्विंसी इंस्टीट्यूट के एडम वाइनस्टीन ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘अफगानिस्तान के पड़ोसी देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय व्यापार, वित्तीय मदद और राजनयिक संपर्कों से तालिबान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हैं। यह सब इसलिए ताकि तालिबान ही सत्ता पर नियंत्रण रख सके क्योंकि दुनिया बाकी संभावित विकल्पों से डरती है: जैसे गृह युद्ध, या एक मजबूत आईएसकेपी, या फिर वैश्विक अस्थिरता।’
(dw.com)
अदिति नारायणी पासवान
अप्रैल को ‘दलित इतिहास माह’ के तौर पर मनाया जाता है। ये महीना हर साल हम दलितों को ये याद दिलाता है कि हम अपने होने का जश्न मनाएं। ये जश्न संघर्षों और यादों का प्रतीक है।
ये महीना पूरे साल दुनियाभर में रहने वाले दलितों को एकजुटता की एक जि़ंदा मिसाल बनकर प्रेरणा देता है, चाहे वो कनाडा में रहते हों, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में।
ऐसा नहीं है कि अप्रैल महीने में सिफऱ् बाबा साहेब का ही जन्म हुआ था। इसी महीने में जाति व्यवस्था के ख़िलाफ़ संघर्ष करने वाले कई और नायकों ने भी जन्म लिया था। इनमें बाबू जगजीवन राम और महात्मा ज्योतिबा फुले भी शामिल हैं। 4 अप्रैल को हिंदुस्तान की आज़ादी की एक बहादुर योद्धा झलकारी बाई का बलिदान दिवस भी होता है।
दलित समुदाय के लोग अक्सर जाति व्यवस्था की गहरी दरारों में गिरकर गुम हो जाते हैं। उन्हें मुख्यधारा की शब्दावलियों और जश्नों में सदा के लिए भुला दिया जाता है, और आखऱिकार उन्हें आने वाली पीढिय़ों की यादों से भी हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है।
अप्रैल का महीना हमें एक ऐसा झरोखा मुहैया कराता है कि हम अपने उन पुरखों की समृद्ध विरासत को याद कर सकें। हमारे इन पूर्वजों ने दलित समुदाय को हमेशा दबाकर और हाशिए पर धकेले रखने वाली जाति व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाइयां लड़ीं और जो कुर्बानियां दीं। हम इस महीने में उनके योगदान का मान-सम्मान करते हैं।
दलितों के संघर्ष का लंबा इतिहास
1757 में हुआ प्लासी का युद्ध हो, जिसमें दुसाधों ने मुगल सम्राट के खिलाफ जंग लड़ी और उसे शिकस्त दी। या फिर, 1857 की बगावत। झलकारी बाई से लेकर मंगू राम और ऊदा देवी तक, इनमें से कितने लोगों के बारे में आप कितना जानते हैं?
इतिहास के पन्ने ऐसी तमाम दास्तानों से भरे पड़े हैं, जहाँ आजादी की लड़ाई लडऩे से लेकर, राष्ट्र निर्माण तक में हमारी भूमिकाओं की या तो अनदेखी की गई या फिर उसे मिटा दिया गया।
लेकिन दलितों का सबसे बड़ा संघर्ष तो उनका रोजमर्रा का संघर्ष ही है। दलितों ने ये लड़ाई पानी के लिए, छुआछूत से निजात पाने के लिए, मेहनत का मान सम्मान पाने के लिए, मंदिरों में प्रवेश करने तक के लिए लड़ी हैं। मैं ये दावा तो नहीं करूंगी कि सदियों से हमारे हालात में कोई बदलाव नहीं आया है।
सामाजिक सुधारों को लेकर हमारी संस्कृति में जो मूल्य रचे बसे हैं। हमारे धर्म का जो बदलाव के मुताबिक़ ढलने का मिज़ाज है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की जो बुनियाद पड़ी है, उन सबने मिलकर ये सुनिश्चित किया है कि हमें भागीदारी मिल सके।
बदलावों के बीच जातिवाद पर चर्चा
आज जाति हमारी रोज़मर्रा की बातचीत का हिस्सा बनती जा रही है। हमारे इर्द-गिर्द जाति को लेकर हो रही चर्चाओं की वजह से आज जाति पर आधारित चेतना और उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है।
यहाँ तक कि बॉलीवुड किरदारों में भी बदलाव आते देख रहे हैं। लगान में जहाँ ‘कचरा’ का किरदार दिखाया गया था लेकिन आज बॉलीवुड फिल्मों में दलित किरदारों को अधिक जुझारू, अक्लमंद और सक्षम इंसान के तौर पर पेश किया जा रहा है। ‘चक्रव्यूह’, ‘मांझी दि माउंटेन मैन’, ‘सैराट’, ‘दहाड़’, ‘जय भीम’, ‘कांतारा’ और ‘कटहल’ जैसी फिल्में इस बदलाव की मिसाल हैं।
इसके बावजूद हर दिन मैं सवर्ण-समृद्ध तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोगों का सामना करती हूँ, जो इस बात पर जोर देते हैं कि जातिवाद कोई बड़ी सामाजिक समस्या नहीं है क्योंकि उनकी नजर में जाति आधारित भेदभाव समाप्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही शादी का मौका आता है वे सजातीय जीवनसाथी की तलाश शुरू कर देते हैं, अँग्रेज़ी के अखबारों में वैवाहिक विज्ञापनों के कॉलम जाति के आधार पर ही बँटे होते हैं और लोग केवल अपनी जाति के वर या वधू ढूँढते हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते।
ऐसे बुनियादी विरोधाभास मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि लोग कैसे बेफिक्री से ये दावा कर लेते हैं किसी को उसकी जाति की वजह से कोई भेदभाव नहीं झेलना पड़ता, वे कहते हैं कि उन्होंने अपने ख़ानदान में कभी किसी को जातिवादी व्यवहार करते नहीं देखा।
जातिवाद को लेकर मिथ गढऩे की कोशिशें
इसके अलावा जाति और उसकी ऐतिहासिक बुनियाद को लेकर भी नई कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। जाति को परिभाषित करने के लिए धार्मिक शास्त्रों से लेकर, जाति शब्द की उत्पत्ति का इतिहास खंगाला जा रहा है। वर्ण और जाति का अंतर बताने के लिए ढेरों किताबें लिखी जा चुकी हैं। व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी की दुनिया में ‘जाति’ शब्द की विचित्र समझ से जुड़ी जानकारियां भरी पड़ी हैं।
जाहिर है, अंग्रेजी का कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के ‘कैस्टस’ से बना है। इसी बात का चतुराई से इस्तेमाल करके कहा जाता है कि जाति एक पश्चिमी परिकल्पना है, जिसे अंग्रेजों ने हमें साम्राज्यवाद के पंजों में जकडऩे के लिए इस्तेमाल किया था।
वैसे मैं न तो इस शब्द की उत्पत्ति को लेकर कोई सवाल खड़ा करती हूँ और न ही इस बात से इनकार करती हूँ कि विदेशियों ने इसका दुरुपयोग किया। मुझे जो बात सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, वो दलितों की मौजूदा हालात। आज अपनी ताकत दिखाने के लिए आखऱि कौन दलितों का बलात्कार कर रहा है? आज के समाज में हम कहां खड़े हैं?
हम अपनी ऐतिहासिक भूमिका को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में हम इज्जत की जिंदगी जी सकें।
ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पूरा यकीन है कि देश में कोई जातिवादी भेदभाव नहीं है। वो ये भी बताना नहीं भूलते कि उन्होंने अपने बुजुर्गों को दलितों के साथ अच्छा व्यवहार करते देखा है। मुझे तो पानी जैसी बुनियादी जरूरत की चीज के लिए अपने समुदाय का सदियों का संघर्ष अच्छी तरह याद है।
मगर कई बार उनके ऐसे दावे सुन-सुनकर दिल-दिमाग थक जाता है कि देश में अब जातिवादी व्यवहार नहीं होता, जब भी कोई ये कहता है कि उसने तो जातिवाद नहीं देखा, तो इस बात की पक्की संभावना होती है कि वो किसी सवर्ण-समृद्ध परिवार में पैदा हुए होंगे।
वो क्या जाने पीर पराई
ऐसे में सवाल ये है कि जिस शख़्स ने कभी जाति के नाम पर होने वाले ज़ुल्म झेले ही नहीं, वो भला हमारी कई पीढिय़ों के दर्द को कैसे समझ सकेगा? आप दलितों को कहने दें कि उन्होंने जातिवाद का दर्द नहीं झेला। जो पीडि़त और शोषित रहे हैं, जरा वो भी तो अपनी जुबान से एलान करें कि उनकी तकलीफों का अंत हो गया है।
अगर किसी ने जातिवाद को नहीं झेला, तो ये उसका सौभाग्य है लेकिन ये हकीकत नहीं है कि जातिवाद नहीं है। सामाजिक सच्चाइयों के प्रति ऐसी बेखबरी तकलीफ पहुँचाती है। जातिवाद की बातें सुनकर और खासतौर से तब, जब मैं एक दलित महिला के तौर पर अपने तजुर्बे साझा करती हूँ तो लोगों के चेहरों पर जो हैरानी का भाव उभरता है वो उनकी जहालत की गवाही दे रहा होता है।
उनकी नादानी हमारे संघर्ष को हाशिए पर धकेल देती है। और जब हम अपने तजुर्बे बयान करते हैं तो हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि हम ये सारी बातें आरक्षण पाने के लिए कह रहे हैं। आरक्षण न तो कोई खैरात है, और न ही ये पुरानी करतूतों का प्रायश्चित है। ये उस समानता और बराबरी की तरफ बढऩे के लिए हमारा अधिकार है, जिसके लिए बाबासाहेब ने संघर्ष किया था, और जिसके लिए हम अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं।
आज विदेशी ताकतें हमारा देश छोडक़र जा चुकी हैं और हमारे देश में कोई ये नहीं कहता कि वो जाति व्यवस्था में यक़ीन करता है, या फिर जातिवादी बर्ताव करता है।
तो फिर ये सब कौन कर रहा है?
ऐसे में मेरे ज़हन में सवाल उठते हैं कि फिर आखिर दलित लड़कियों से बलात्कार करके उन्हें कौन जिंदा जला रहा है? सीवर साफ करते हुए दलित क्यों मर रहे हैं? आज भी घोड़े पर चढऩे के लिए क्यों गोली मारी जा रही है? आज भी मूंछें रखने पर दलितों का क़त्ल क्यों हो रहा है? आज भी क्यों ताकत दिखाने का सार्वजनिक मंच किसी दलित के शरीर को समझा जाता है? ये जुल्म कौन ढा रहा है?
मैं मिसालों के जरिए ख़ुद को पीडि़त के तौर पर पेश करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ लेकिन, सवाल ये है कि ऐसा कौन कर रहा है? अक्सर सुना जाता है कि फलाँ दलित नेता सत्ता का भूखा है। निश्चित रूप से हम सत्ता के केंद्र में रहना चाहते हैं। सदियों से हम हुकूमतों के हाशिए पर धकेले जाते रहे हैं। अब हम सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं।
हम एक ऐसा नेटवर्क, ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, जहां अमेजन में काम करने वाले, सिएटल में रहने वाले लोग हमें भी जानते हों ताकि वो हमारा बायोडेटा आगे बढ़ा सकें। हम भी कैम्ब्रिज में रहने वालों से अपना परिचय बढ़ाना चाहते हैं, जिससे वो हमें हमारे करियर में आगे बढऩे में मदद कर सकें।
हमें इन सबसे वंचित रखा जाता रहा है। अब हम ये सब चाहते हैं और हम अपना ये अधिकार मज़बूती से जताने का इरादा भी रखते हैं।
दलित इतिहास माह में आइए स्वीकार करें कि हम सब जातिवादी हैं। हम सभी किसी न किसी रूप में जातिवादी बर्ताव करते हैं। जाति हमारी चेतना की गहराइयों में रची बसी है। एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में जाति के गहरी जड़ें जमाए होने की इस सच्चाई को अगर हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो फिर बाबासाहेब के नाम पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना बेमानी है।
सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि जाति का अस्तित्व है। इसको स्वीकार करना होगा, इसके प्रति संवेदनशील होना होगा। उसके बाद ही हम खुद को जाति की बंदिशों से आज़ाद करने की चर्चा शुरू कर सकते हैं। (bbc.com/hindi)
(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)
एक रिपोर्ट में गुवाहाटी को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है. तेज शहरीकरण, गाड़ियों की बढ़ती संख्या जैसे कई कारण इसके जिम्मेदार हैं. हालांकि कई लोग नहीं मानते कि गुवाहाटी की हवा इतनी खराब है.
 डॉयचे वैले पर साहिबा खान की रिपोर्ट-
डॉयचे वैले पर साहिबा खान की रिपोर्ट-
असम के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अरूप कुमार मिश्रा का कहना है,"हम सस्ते और निचले दर्जे के सेंसर इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो हमें गलत जानकारी दें.” मिश्रा ने स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ग्रुप की हालिया रिपोर्ट को गलत बताते हुए यह बात कही. इस रिपोर्ट में गुवाहाटी को सबसे प्रदूषित हवा वाले शहरों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर रखा गया है.
2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी नाम की इस रिपोर्ट में बिहार का बेगूसराय सबसे ऊपर है, वहीं दिल्ली तीसरे स्थान पर है. देशों की सूची में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत तीसरे स्थान पर है.
रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी की हवा में पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 प्रदूषक का घनत्व 105.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है. रिपोर्ट के मुताबिक निर्धारित सीमा से यह 20 गुना ज्यादा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है.
भारत का अपना मानक 40 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर है. पीएम 2.5 ऐसा प्रदूषक है जो इंसान के बाल से 30 गुना ज्यादा बारीक होता है. अगर यह खून में प्रवेश करता है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
रिपोर्ट पर विवाद
अरूप कुमार मिश्रा ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद ठहराया है. डीडब्ल्यू से बातचीत में कुमार ने कहा कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है. मिश्रा का कहना है,"हमारी सभी गाइडलाइन अमेरिका की एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से मेल खाती हैं, और हम उन सभी का पालन करते हैं.”
हालांकि नई दिल्ली की सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक, अनुमिता रॉयचौधुरी कहती हैं कि बात केवल यह नहीं है कि गुवाहाटी सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर है. उनका कहना है, "मसला यह है कि गुवाहाटी में कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ा है जिसके जिम्मेदार तीव्र शहरीकरण और गाड़ियों का बढ़ना है.”
हालांकि रिपोर्ट के गुणा भाग पर उनके भी सवाल है. उनका कहना है,"गुवाहाटी से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर बर्नीहाट शहर है जो मेघालय और असम की सीमा पर पड़ता है. अगर गुवाहाटी का प्रदूषण नापते हुए बर्नीहाट का प्रदूषण भी उसमें आंका गया है, तब नंबर के हिसाब से गुवाहाटी का औसतन प्रदूषण बढ़ा हुआ दिखाई देने की ज्यादा संभावना है. यह भी पक्का नहीं है कि क्या उन्होंने सरकारी आंकड़ों को देख कर यह रिपोर्ट तैयार की है.”
गुवाहाटी उत्तर-पूर्व का सबसे बड़ा व्यापार अड्डा
अरूप मिश्रा ने बताया कि यह बात सच है कि 2022 के दिसंबर महीने में गुवाहाटी में भयंकर प्रदूषण था. वे कहते हैं, "2022 में गुवाहाटी में निर्माण कार्य चरम पर था, कई हाईवे बन रहे थे और ब्रह्मपुत्र नदी से भी काफी धूल शहर में आ रही थी. हालांकि 2023 तक बड़े निर्माण कार्य खत्म हो चुके थे. इसलिए गुवाहाटी 2023 में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर नहीं आ सकता है.”
मिश्रा का कहना है कि गुवाहाटी उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है और हाल के दिनों में यहां बड़े निर्माण कार्यों ने जोर पकड़ लिया है. रिपोर्ट में किस तरह से गणना हुई है यह अभी सामने नहीं आ पाया है. मिश्रा ने कहा, "ना ही असम सरकार को इस रिपोर्ट से जुड़े किसी व्यक्ति ने संपर्क किया, ना ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को. ना ही हमें ये पता है कि क्या उन्होंने अच्छे सेंसर इस्तेमाल किए हैं.”
मिश्रा कहते हैं, "आस-पास के राज्य अपना कचरा जलाते हैं और उस धुएं का खामियाजा गुवाहाटी को भुगतना पड़ता है.” ऐसे ही कई दावे सर्दियों की वायु प्रदूषण में दिल्ली सरकार भी करती है. हालांकि रॉयचौधुरी का इस पर कहना है, "यह सच है कि एक जगह का प्रदूषण दूसरी जगह पर असर डालता है, लेकिन दूसरे शहर की वजह से हमारे शहर में प्रदूषण होता है, यह कहना गलत होगा. अगर उनका हमारे वायु प्रदूषण में योगदान है तो हमारा भी उनकी प्रदूषण में योगदान होगा.”
रॉयचौधुरी ने बताया कि नोएडा में भी 40 फीसदी वायु प्रदूषण का जिम्मेदार दिल्ली है. उनका कहना है, "चूंकि गुवाहाटी एकदम से शहरीकरण की ओर बढ़ा है, वहां बहुत तेजी से निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसने यहां की वायु गुणवत्ता पर काफी बुरा असर डाला.”
गाड़ियों की संख्या भी बड़ी वजह
1971 की जनगणना के अनुसार, गुवाहाटी की जनसंख्या 300,000 से कम थी. 2011 में, जब भारत ने अपनी आखिरी जनगणना की, तो यह संख्या करीब 10 लाख हो गई. रॉयचौधुरी कहती हैं, "जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे-वैसे शहर में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई और शहर इतनी तेजी से गाड़ियों की बढ़ती संख्या के लिए तैयार नहीं था.” एक तो गाड़ियों की बढ़ती संख्या, उस पर से पुरानी गाड़ियों का अभी तक सड़कों पर होना इस वायु प्रदूषण में आग में घी का काम करता है.
गाड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ शहर में जंगलों की कटाई भी हो रही है. 2023 में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने असम में गुवाहाटी और ग्वालपाड़ा के बीच एक हाईवे परियोजना के लिए लगभग 2,000 पेड़ों को काटने के आरोपों पर स्वत: संज्ञान लिया था.
कचरा-प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी
आबादी के साथ जो एक चीज बेतहाशा बढ़ती है वो है कचरा. रॉयचौधुरी मानती हैं कि गुवाहाटी में सही ढंग से कचरा इकट्ठा ना करने से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है. "शहर के पास ही लैंडफिल है जहां कचरा जमा होता है. जब वहां सही ढंग से कचरा नहीं डाला जाता, तब वो सड़ता रहता है. इस सड़ते हुए कचरे में जब तब आग लग जाती है और उस से वायु प्रदूषण होता है.”
एक रिपोर्ट के अनुसार पास के गांव बेलोरतोल में ही गुवाहाटी का सारा कचरा फेंका जाता है. कचरे में कुछ समय पहले आग लग गई थी जो कई हफ्तों तक जलती रही. प्लास्टिक और बाकी कचरे के जलने से निकलने वाली खतरनाक गैसों ने भी गुवाहाटी की हवा खराब की.
रॉयचौधुरी ने गुवाहाटी की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जिक्र किया. उन्होंने बताया, "चूंकि गुवाहाटी पर घाटी का प्रभाव पड़ता है, वहां वायु प्रदूषण की सघनता और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि भारी हवा के बाहर निकलने के रास्ते कम हो जाते हैं.”
रिपोर्ट का असर
अरूप मिश्रा ने बताया कि किस तरह से ऐसी रिपोर्टों का राज्य के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर असर पड़ता है. उन्होंने कहा, "बड़ी कंपनियां तो आ जाती हैं क्योंकि उन्हें यहां काम करना है, लेकिन जो सैलानी केवल कुछ दिनों के लिए गुवाहाटी आते हैं, वो ऐसी रिपोर्ट देख कर निराश हो जाते हैं और फिर नहीं आते. इससे काजीरंगा नेशनल पार्क के पर्यटन पर खासा असर पड़ता है.”
अरूप का अंदाजा है कि विदेशी कंपनियां अपने फायदे के लिए भी ऐसी रिपोर्टें ला सकती हैं. "कई कंपनियां एयर प्यूरीफायर जैसे उपकरण बनाती हैं. ऐसा भी हो सकता है कि इन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद कई लोग इनके बनाये हुए प्यूरीफायर खरीदें.”
सुधार मुश्किल लेकिन जरूरी है
रॉयचौधुरी को लगता है कि इस बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए नीतियों में सुधार लाना होगा. उनका कहना है, "प्रदूषण राज्य सीमाओं को नहीं समझती. अगर एक जगह प्रदूषण हो रहा है तो बगल वाले शहर तक तो वो पहुंचेगा ही. इसलिए हमें जरूरत है एक रीजनल पॉलिसी एक्शन प्रोग्राम की, जो केवल एक या दो शहरों में नहीं बल्कि उस पूरे इलाके को देखे.”
रॉयचौधुरी यह भी कहती हैं कि वाहन प्रदूषण रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर देना होगा. कचरे को भी ठीक ढंग से फेंकना और इकट्ठा करना होगा. जो गीला कचरा है वो कंपोस्ट हो, जो सूखा कचरा है वो रिसायकिल हो. जनता के बीच इस जागरूकता को फैलाना होगा.
मिश्रा ने भी बताया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत सिटी एक्शन प्लान जारी है इसके तहत उन सभी स्रोतों को पहचाना जाएगा जो प्रदूषण में अहम भूमिका निभा रहे हैं और फिर उन्हें कम करने की नीति बनाई जाएगी. फिलहाल, असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह अध्ययन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ कर रहा है. (dw.com)
-श्रीकांत बंगाले
‘जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे तो उन्होंने 16-17 वादे किए थे। उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। क्या यही मोदी की गारंटी है?’
यह कहते हुए दिगंबर गुल्हाने दोनों हाथ अपने सिर की ओर ले जाते हैं। दिगंबर गुल्हाने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दाभडी गांव में रहते हैं।
इसी गांव में 20 मार्च, 2014 को उस समय एनडीए के प्रधानमंत्री पद के दावेदार और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ ‘चाय पर चर्चा’ की थी।
साल 2014 के चुनाव से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के 1,500 से अधिक स्थानों के किसानों ने ऑनलाइन भाग लिया, जबकि दाभडी में किसानों ने व्यक्तिगत रूप से मोदी से बातचीत की थी।
इस चर्चा के दौरान मोदी ने किसानों की समस्याएं जानीं और बताया कि उनके लिए क्या समाधान हो सकता है।
उस समय पीएम मोदी ने कहा था, ‘मैं देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि हम देश के कृषि क्षेत्र को बदल सकते हैं। देश का जीवन स्तर बदल सकता है। देश के गांवों को बदल सकते हैं। मुझे बस आपका समर्थन चाहिए। हम देश के किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे।’
साल 2014 में एनडीए सरकार बनी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। अब इस बात को 10 साल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार आम लोगों से सरकार बनाने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं।
लेकिन उन्होंने दस साल पहले जो वादे किए थे, उनकी क्या स्थिति है? क्या उनकी सरकार के दौरान किसानों के जीवन में कुछ बदलाव आया है?
‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम में मोदी ने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों से बातचीत की थी। पिछले 10 सालों में उनके जीवन में क्या बदलाव आया है? ये जानने के लिए बीबीसी मराठी की टीम दाभडी पहुंची।
हम लोग सुबह करीब 9 बजे दाभडी पहुंचे। दाभडी गांव यवतमाल जि़ले के अरनी तालुका में आता है। गांव के मुख्य चौराहे के पास एक खेत है। इसी फार्म में पीएम मोदी का ‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम हुआ था।
थोड़ा आगे बढऩे पर रास्ते में हमारी मुलाकात भास्कर राऊत से हुई। वे एक गाड़ी पर कपास की फसल लाद रहे थे। उन्होंने बताया कि अरनी तालुका में जहां दाभडी गांव स्थित है, वहां कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की ओर से होने वाली खरीद बंद होने के कारण वे निजी व्यापारियों को कपास बेच रहे हैं। भास्कर के पास चार एकड़ खेत है। इसमें वे कपास का उत्पादन करते हैं।
‘बाघ और सांप से ख़तरा’
जब उनसे कपास की क़ीमत के बारे में पूछा तो, उन्होंने कहा, ‘कपास की दरें उलट गई हैं। 15 दिन पहले तक रेट 7700 तक चला गया था। आज यह 7,200 या 7,300 तक है। लेकिन हम लोगों को 9-10 हज़ार का रेट मिलने की उम्मीद थी।’
भास्कर 2014 में अपने गांव में हुए नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
पिछले 10 सालों में किसानों के जीवन में क्या बदलाव आया है? इस सवाल पर उन्होंने कहा, ‘2014 के बाद यह संतोषजनक नहीं है, लेकिन बदलाव ज़रूर आया है। जहां तक कृषि उपज की क़ीमत की बात है तो यह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के हिसाब से तय होती है। 2014 से पहले भी कपास की क़ीमतें कम थीं। यह 10 वर्षों में बढ़ी हैं।’
भास्कर ने बताया कि उन्हें पीएम किसान योजना के तहत हर साल छह हजार रुपये मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना छह हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 2019 में शुरू हुई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को यवतमाल में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने पीएम किसान के लाभार्थियों की जानकारी देते हुए कहा था, ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक देशभर के 11 करोड़ किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा हो चुकी है। इसमें महाराष्ट्र के किसानों को 30 हज़ार करोड़ रुपये और यवतमाल के किसानों को 900 करोड़ रुपये मिले हैं।’
लेकिन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर भास्कर का अनुभव अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को अपर्याप्त वर्षा, ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान, सूखा या फसल में कीट लग जाने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुई क्षति पर ही बीमा का लाभ मिलता है।
भास्कर ने कहा, ‘फसल बीमा योजना में फजऱ्ीवाड़ा हो रहा है। गांव के दो-तीन किसानों को ही फ़ायदा होता है। मैंने बीमा के लिए आवेदन किया था। कपास को नुकसान हुआ। लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला।’
हमने दाभडी में पीएम किसान योजना और फसल बीमा योजना के लाभार्थियों के बारे में जानने के लिए कृषि अधिकारियों से संपर्क किया।
अरनी तालुका के कृषि अधिकारी आनंद बडख़ल ने बीबीसी मराठी को बताया, ‘दाभडी गांव के 383 किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है। 2023-24 में 550 किसानों को स्थानीय आपदा क्षतिपूर्ति हेतु 32 लाख 17 हजार का बीमा प्राप्त हुआ है। इस साल फसल कटाई के बाद के बीमा मामले अभी तक तय नहीं हुए हैं।’
पीएम मोदी ने ‘चाय पर चर्चा’ में कहा था, ‘यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों के उत्पादन की न्यूनतम लागत वहन करे। खेती में उपयोग होने वाली चीजें कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए और किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इससे युवा कृषि क्षेत्र में आएंगे और यह किया जा सकता है।’
आज 10 साल बाद भी दाभडी के किसान अपनी कृषि उपज की सही कीमत का इंतज़ार कर रहे हैं। भास्कर बताते हैं, ‘किसानों को सरकार से केवल एक ही उम्मीद है, वह है हमें हमारी उपज का सही मूल्य मिलना। हमें कुछ भी मुफ्त नहीं चाहिए। कीमत उत्पादन की लागत के मुताबिक होनी चाहिए।’
भास्कर के मुताबिक किसानों की हालत आर्थिक रूप से खस्ताहाल होती जा रही है क्योंकि लागत अधिक है और मूल्य कम मिलता है।
भास्कर ये भी बताते हैं कि हमें खेती के लिए दिन में बिजली मिलनी चाहिए। रात की बजली हम किसानों के लिए बाघ और सांप के ख़तरे साथ लेकर आता है। बाघ हमारे सिर को दबोचता है जबकि सांप पैर में काट सकता है।’
‘आजकल बिना मुंह भरे कुछ नहीं होता’
भास्कर से बातचीत के बाद जब हम आगे बढ़े तो एक घर के सामने गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ दिखा। ये डिके परिवार का घर है। दरअसल पीएम मोदी ने ‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम में इस परिवार से बातचीत की थी।
जब मैं घर के पास गया तो मैंने देखा कि दीवारें मिट्टी से सनी हुई हैं। अनिकेत हॉल में बैठे थे। ‘चाय पर चर्चा’ के वक्त वह 14 साल के थे।
उन्होंने इस कार्यक्रम में मोदी को बताया था कि उनके पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। 51 वर्षीय मीरा दिलीपराव डिके अनिकेत की मां हैं। अनिकेत ने उन्हें बुलाया तो वे हॉल में आकर बातें करने लगीं।
उन्होंने बताया, ‘मेरे पति ने 2005 में आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि खेती से आमदनी नहीं हो रही थी। बैंक का कर्ज था। उस दिन मैं मज़दूरों के साथ खेत पर गई थी। उन्होंने घर में ही फांसी लगा ली। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आऊंगा। उस समय अनिकेत दूसरी कक्षा में और स्नेहा छठी कक्षा में थी।’
महाराष्ट्र में अगर किसी किसान की आत्महत्या सरकारी मानदंडों के अनुसार ‘आत्महत्या’ की श्रेणी में आती है, तो परिवार को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। मीरा को वह मदद मिल गई थी, लेकिन इस रकम के सहारे जीवन भर गुज़ारा नहीं चल सकता। 2006 से मीरा आंगनवाड़ी में सहायिका के तौर पर काम करने लगीं।
मीरा अनिकेत की ओर देखते हुए कहती हैं, ‘मैंने अपने बच्चों का पालन-पोषण कितनी मुश्किलों से किया है। इतनी शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। आजकल बिना रिश्वत दिए कुछ नहीं होता।’
अनिकेत ने अमरावती से बीसीए की पढ़ाई पूरी की है। वह फिलहाल नौकरी की तलाश में हैं।
पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद किसानों के जीवन में क्या बदलाव आया है, इस सवाल पर मीरा ने कहा, ‘मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों के लिए ये सब करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया गया। किसानों को सोयाबीन और कपास का दाम नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर, मजदूरी दरों में वृद्धि हुई है।’
अनिकेत ने कहा, ‘आज तक कुछ भी नहीं बदला है।’
अनिकेत की मां ये भी बताती हैं कि उन्हें किसी तरह की योजना का लाभ नहीं मिलता है। इतना ही नहीं अनिकेत के मुताबिक पिता की आत्महत्या के बाद उनके नाम की जमीन उनके चाचा के नाम कर दी गई और इसके चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उनके चाचा को मिलता है।
क्या 2024 में आपकी आय दोगुनी हो गई? ऐसा सवाल पूछे जाने पर अनिकेत का जवाब था, ‘नहीं।’
हालांकि अनिकेत ने यह भी कहा, ‘किसानों के लिए योजनाएं हैं। किसानों को उनका लाभ मिल रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे यहां भी राज्य सरकार अपने स्तर पर कुछ नहीं कर रही है। तीन पार्टियों की सरकार है, आप कह सकते हैं कि एक थाली में तीन लोग खाना खाने बैठे हैं और कोई भूखा नहीं है।’
‘मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते’
हमारी बातचीत चल ही रही थी कि अनिकेत के चाचा विनोद डिके घर में आ गए। उनके हाथों से लग रहा था कि वे खेतों की तरफ से आ रहे हैं।
क्या चल रहा है काम, मैं बात करने लगा। उन्होंने कहा, ‘15 दिन से खेत में लाइट नहीं है। खराबी का पता चला और लाइट चालू कर दी गई। अगर आज रोशनी नहीं आती तो पूरी फसल खराब हो जाती।’
यह कहते हुए उन्होंने अपने हाथों पर लगे काले धब्बे दिखाए। दस साल में आपकी जि़ंदगी में क्या बदलाव आया है, इस सवाल पर उन्होंने कहा, ‘कुछ नहीं बदला, आप स्थिति देखिए। मोदी सर ने कहा था कि हम आत्महत्या करने वाले पीडि़तों के बेटों को सेवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। लेकिन मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते।’
दोपहर में गांव में घूमने के दौरान कुछ लोग पूछने लगते हैं कि ये क्या सर्वे हो रहा है। जब मैं गांव की नेम प्लेट की फोटो लेने लगा तो मोटरसाइकिल पर दो युवक आए और पूछा कि क्या काम है।
ग्रामीणों ने इसलिए लगाया बैनर
दाभडी की आबादी करीब तीन हज़ार है। गांव के लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कुछ लोग तालुका स्थानों में काम करने के लिए अरनी जाते हैं। वहां दुकानों में मजदूर का काम करते हैं।
दाभडी में खरीफ सीजन के दौरान कपास और सोयाबीन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। रबी सीजन में गेहूं, चना की फसल पैदा होती है। गांव से सटी नहर और कुएं का पानी खेती के लिए पानी का मुख्य स्रोत है।
कुछ समय बाद हमारी मुलाकात विजय वानखड़े से हुई। वह दाभडी की सरपंच सरिता वानखड़े के पति हैं। विजय के पास 10 एकड़ खेत है।
बीबीसी मराठी से विजय ने कहा, ‘मैं मोदी के कार्यक्रम में था। घटना के बाद कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ वैसा का वैसा है। कुछ नहीं बदला है। 2014 के बाद भी गांव में एक-दो किसानों ने आत्महत्या की है।’
‘मोदी ने कपड़ा मिलों, सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग का वादा किया था। तो लोगों को लगा कि वो सच में ऐसा करने जा रहे हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़ा उत्साह था, लोगों को लगा था कि वादे पूरे होंगे।’
विजय ने बताया, ‘मोदी को उनके वादे याद दिलाने के लिए गांव में बैनर लगाया गया कि आपने वादे किए थे, पूरे नहीं किए, यहां ध्यान दीजिए। लेकिन, उस दिन चैनल पर बोलने वालों को ही एक दिन के लिए थाने में नजऱबंद रखा गया। उन्हें लगा कि ये लोग मोदी के कार्यक्रम में बाधा डालेंगे।’
चैनल पर बोलने के बाद नोटिस मिला
नरेंद्र मोदी 28 फरवरी, 2024 को यवतमाल में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले थे। यहां उनकी बैठक निर्धारित थी।
इस बैठक से पहले दाभडी के ग्रामीणों ने मोदी को उनके वादों की याद दिलाते हुए गांव में एक बैनर लगाया था।
इस बैनर के सामने कुछ लोगों ने मीडिया से बातचीत की। इसमें दिगंबर गुल्हाने और गणेश राठौड़ शामिल थे। मोदी की सभा से पहले अरनी पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया था।
बीबीसी मराठी से दिगंबर ने कहा, ‘हमने 25 फरवरी को चैनल पर बात की थी। इसके बाद हमें नोटिस भेजा गया। मोदी की सभा से पहले हम कोई हंगामा ना करें, इसके लिए गणेश राठौड़ और मुझे पूरे दिन अरनी थाने में नजऱबंद रखा गया। वहीं बिठाया गया। मोदी की सभा तक हम नहीं निकल सके। लेकिन मैंने सच बोला।’
‘नहीं बोलोगे तो बाबा साहेब को क्या जवाब दोगे?’
दिगंबर के पास तीन एकड़ खेत है। वे इसमें कपास का उत्पादन करते हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘आपका कपास जिला है, मोदी ने कई घोषणाएं की थीं जैसे हम यहां कपड़ा उद्योग लगा देंगे, हम किसान के बेटों के लिए दुकानें खोल देंगे। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया।’
2014 में दाभडी में एक कार्यक्रम में दाभडी के तत्कालीन सरपंच ने पीएम मोदी से सवाल पूछा था कि विदर्भ और यवतमाल के किसानों को कपास-सोयाबीन की अच्छी कीमत दिलाने के लिए आप क्या करेंगे?
उस पर प्रतिक्रिया देते हुए, मोदी ने कहा था, ‘जो लोग यहां कपास उगाते हैं, हमें मूल्य वृद्धि के लिए जाना होगा। आज क्या हो रहा है यहाँ कपास का निर्माण होता है, सूत बनाने के लिए कोल्हापुर जाना पड़ता है। यदि कपास यहां है तो धागा यहां क्यों नहीं बनता? जब धागा यहीं बनता है तो कपड़ा यहां क्यों नहीं बनता? अगर यहां कपड़े बनते हैं तो रेडीमेड कपड़े क्यों नहीं बनते? इससे कपास का मूल्यवर्धन होगा। इससे कपास किसानों को फायदा होगा।’
दिगंबर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं।
लेकिन उन्होंने आगे कहा, ‘मोदी पीएम किसान योजना में दो हज़ार देते हैं। हम डीएपी खाद लेते हैं। कांग्रेस काल में इसकी क़ीमत 500 रुपये थी। अब इसके लिए 1700 रुपये चुकाने होंगे। एक लाख की खाद पर 18 हज़ार जीएसटी देना होगा। एक बच्चे की पेंसिल पर 25 फीसदी जीएसटी लगता है और चावल मुफ्त में मिलता है।’
जब उनसे पूछा गया कि पुलिस नोटिस के बारे में वह क्या सोचते हैं तो उन्होंने कहा, ‘ऐसा करना ठीक नहीं है। क्योंकि हम बाबा साहेब द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करते रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा तो बाबा साहेब को क्या जवाब देंगे? मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा।’
भास्कर राऊत की तरह दिगंबर गुल्हाने ने भी फसल बीमा योजना को लेकर अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, ‘पीक बीमा का निरीक्षण करते हैं। उसके लिए आने वाले लडक़े 500 रुपये लेते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह सरकार भ्रष्ट नहीं है?’
इस बीच, अरनी तालुका के कृषि अधिकारी आनंद बडख़ल ने बीबीसी मराठी को बताया कि अगर कोई फसल बीमा निरीक्षण के लिए 500 रुपये लेता है, तो किसानों को इसे लिखित रूप में देना चाहिए और संबंधित के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराना चाहिए।
किसान मौखिक रूप से शिकायत करते हैं कि उन्हें फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है। बडख़ल ने बताया, ‘हमने अपील की थी कि किसी को भी फसल बीमा निरीक्षण के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए।’
दिगंबर कहते हैं, ‘हमें पीएम किसान सम्मान राशि नहीं चाहिए, हमें कजऱ् माफ़ी नहीं चाहिए। किसान की उपज का उचित मूल्य ही मिलना चाहिए। किसान दुनिया की रोटी और मक्खन मुहैया कराते हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए।’
क्या कहते हैं क्षेत्र के विधायक?
भाजपा के संदीप धुर्वे अरनी-केलापुर निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं।
दाभडी गांव के विकास कार्यों के सवाल पर बीबीसी मराठी से उन्होंने कहा, ‘दाभडी गांव के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा पुल था। यह गांव और मंदिर को जोडऩे वाला एक पुल था। उनके लिए ढाई करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसका भूमिपूजन भी संपन्न हो गया। इसके अलावा आरओ वॉटर प्लांट ने भी काम किया है।’
नरेंद्र मोदी ने 2014 में किए वादे पूरे नहीं किए हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में नाराजग़ी है। इस बारे में पूछे जाने पर संदीव धुर्वे ने कहा, ‘नरेंद्र मोदी ने उस वक्त प्रोसेस इंडस्ट्री की बात की थी। लेकिन, उद्यमियों के बीच से भी किसी को आगे आना चाहिए। उद्यमियों में से कोई भी कपास और सोयाबीन को संसाधित करने के लिए सामने नहीं आया है।’
उन्होंने कहा, ‘मेरा निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे वर्तमान उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार ने कपास आधारित प्रसंस्करण उद्योग लाने का वादा किया है।’
‘मोदी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है’
2014 में ‘चाय पर चर्चा' कार्यक्रम से पहले नरेंद्र मोदी ने कैलास अरंकार के खेत में जाकर नुकसान का जायज़ा लिया था। जैसे ही हम गांव के मुख्य चौराहे पर वापस आए, खेत फिर से दिखाई देने लगा।
फार्म मालिक कैलास अरंकर ने बीबीसी मराठी को बताया, ‘चाय पर चर्चा के उसी दिन, मोदी ने दोपहर तीन बजे हमारे खेतों में नुकसान का निरीक्षण किया था। क्योंकि उस समय ओलावृष्टि हुई थी और चने और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था। उस साल गांव में लगभग 17 आत्महत्याएं हुई थीं।’
मोदी के 10 साल के कार्यकाल के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘जब मोदी गांव आए तो उन्होंने कहा, ‘हमें बताएं कि आपकी समस्याएं क्या हैं?' मोदी ने कोई आश्वासन नहीं दिया थे। लेकिन मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। लोग यह नहीं समझते। गांव में पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है, सडक़ों का निर्माण कराया गया है, मंदिर के लिए बैठक कक्ष की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है।’
‘चैनलों ने हमारे गांव को नुकसान पहुंचाया है, आप जाइए’
दोपहर करीब एक बजे जब हम लोग गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे तो वहां कुछ लोग बातें कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव का माहौल क्या है तो एक शख्स ने कहा, ‘हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं।’
दूसरे ने कहा, ‘क्या पूछ रहे हो? फिर मेरे साथ वाले आदमी ने उनसे स्थानीय बोली में बात की तो हमारी बातचीत होने लगी।’
पीएम मोदी के आने और जाने के बाद क्या बदला, इस सवाल पर एक शख्स ने कहा, ‘गांव में कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमने यहां ‘चाय पर चर्चा’ का बैनर लगा दिया।’
उन्हें रोकते हुए अनिल राठौड़ ने गांव में बनी पानी की टंकी की ओर इशारा किया और कहने लगे, ‘2014 के बाद गांव में पानी सप्लाई के लिए एक करोड़ रुपये की टंकी बनी थी। हंसराज अहीर के गृह मंत्री रहते हुए गांव में 50 लाख की सीमेंट-कंक्रीट सडक़ें बनाई गईं। मोदी के गांव आने के बाद विकास तो हुआ, लेकिन उतना नहीं, जितना चाहिए था।’
हंसराज अहीर विदर्भ से बीजेपी नेता हैं। वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं।
यह पूछे जाने पर कि और क्या किया जाना चाहिए, अनिल ने कहा, ‘हमें गांव में एक बैंक की जरूरत है। हमारे बच्चों के खेलने के लिए एक स्टेडियम की ज़रूरत है। साथ ही एक गोदाम की भी जरूरत है ताकि किसान वहां 1000-2000 बोरियां रख सकें।’
‘हमारा देश बड़ा है, सरकार को हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सब कुछ एक बार नहीं होगा। हमारे विधायक पांच साल में एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए।’
किशन चव्हाण दाभडी गांव की विवादों को निपटाने वाली तंटामुक्त समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं।
उन्होंने कहा, ‘मोदी जब भी यवतमाल आते थे, तो हमारे गांव का नाम लेते ही थे। इस साल वह यवतमाल आए थे। लेकिन उन्होंने हमारे गांव का नाम नहीं लिया।’
इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए अनिल राठौड़ ने कहा, ‘समाचार चैनलों की वजह से हमारे गांव को नुकसान हुआ है। जब चैनल आया तो गांव के लोगों ने कहा, ‘गांव में कोई काम नहीं हुआ है।’ तब नेताओं को लगता है कि गांव के लोगों ने काम करने के बावजूद कुछ नहीं कहा। वही रिपोर्ट ऊपर जाती है। फिर नेता गांव के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए अब तुम जाओ।’
2014 के बाद भी आत्महत्या का सिलसिला जारी है
पीएम मोदी ने इस गांव में 2014 में कहा था कि आत्महत्या कृषि की समस्याओं का समाधान नहीं है।
उन्होंने कहा था, ‘हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बने जो किसानों के प्रति इतनी संवेदनशील होगी, नीतियां प्रगतिशील होंगी और किसानों की रक्षा होगी, किसान प्रगति करेंगे।’
लेकिन, 2014 के बाद भी दाभडी गांव में किसानों की आत्महत्या जारी है। गणेश राठौड़ के चाचा वि_ल राठौड़ ने 2015 में आत्महत्या कर ली थी।
बीबीसी मराठी से गणेश ने बताया, ‘मेरे चाचा वि_ल राठौड़ ने मोदी जी के आने के बाद 2015 में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के बाद हमें सरकार से आर्थिक सहायता मिली।’
ज्ञानेश्वर मानकर के किसान भाई ने 2017 में आत्महत्या कर ली थी। उनका नाम कैलास मानकर था। ज्ञानेश्वर ने कहा कि कैलास ने कर्ज के कारण आत्महत्या की थी।
राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 के पहले दो महीनों में महाराष्ट्र में 427 किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें से सबसे ज़्यादा 48 आत्महत्याएं यवतमाल में हुई हैं।
28 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी यवतमाल के दौरे पर थे। इस अवसर पर उनके द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मोदी ने यवतमाल के लोगों की तारीफ़ की।
उन्होंने कहा, ‘जब मैं 10 साल पहले ‘चाय पर चर्चा’ करने यवतमाल आया था तो आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। फिर मैं फरवरी 2019 में यवतमाल आया। फिर भी आपने हम पर प्यार बरसाया। अब, 2024 के चुनाव से पहले, जब मैं विकास के उत्सव में भाग लेने आया हूं, तो पूरे देश में एक ही नारा सुनाई दे रहा है ‘अब की बार, चार सौ पार।’
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ‘यवतमाल में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया गया है। आज किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं। गांव की महिलाओं को आर्थिक मदद मिल रही है। युवाओं को उनका भविष्य बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है।’
मोदी ने यह भी कहा, ‘पिछले 10 साल से हम गांव में रहने वाले हर परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित तौर पर कोशिश कर रहे हैं।’
मोदी से बातचीत करने वाले विशेषज्ञ अब क्या सोचते हैं?
‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ के तौर पर किशोर तिवारी से बातचीत की। वे कई सालों से विदर्भ में कृषि मुद्दों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा था कि यूपीए-1 और यूपीए-2 सरकार के दौरान विदर्भ में करीब 11 हज़ार किसानों ने आत्महत्या की थी। किसानों की आत्महत्या के लिए सरकारी नीतियां जि़म्मेदार लगती हैं तो क्या आप यूपीए सरकार की इन किसान विरोधी नीतियों को जारी रखेंगे या हम एनडीए से उम्मीद कर सकते हैं?
इसके जवाब में पीएम मोदी ने नदी जोड़ो परियोजना और सिंचाई के महत्व पर प्रकाश डाला था। पीएम मोदी ने तब कहा था, ‘अगर हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो हमें कृषि-समर्थक नीतियों को मजबूत करना होगा। बीजेपी और एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई सभी पहलों को मजबूत करना चाहते हैं।’
लेकिन क्या मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों के लिए नीतियां मजबूत की हैं, तो किशोर तिवारी कहते हैं, ‘मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार किसानों के मुद्दों पर काम करेगी। उन्होंने 2019 तक उस दिशा में प्रयास किया। लेकिन, 2019 के बाद छोड़ दिया। 2019 से 2024 तक सरकार की योजना के तहत किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं हुआ है। सरकार सिफऱ् दावे करती रही है। मोदी के कार्यकाल में भी कई किसानों ने आत्महत्या की है।’
आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार के अनिकेत और मीरा को अब भी सरकार से उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि केंद्र में कोई भी सरकार आए, उसे मुख्य रूप से दो काम करने चाहिए।
अनिकेत कहते हैं, ‘सरकार को यथासंभव अधिक से अधिक रिक्तियों पर भर्ती करनी चाहिए। बच्चों को रोजग़ार देना चाहिए, ताकि वे अवसाद का शिकार न बनें। और सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ योजनाएं सरकार की ओर से आती हैं। लेकिन, किसान को इसकी जानकारी नहीं है। योजनाओं के बारे में किसानों को बताना चाहिए।’ उनकी मां मीरा ने कहा, ‘हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार को किसान की उपज का दाम देना चाहिए।’ जब हम अनिकेत के घर से निकले तो वह और उनकी माँ हमें छोडऩे घर के बाहर आए। जब हम उन्हें अलविदा कह रहे थे तो अनिकेत ने कहा, ‘सर, नौकरी के बारे में कुछ हो, तो बताना।’ (bbc.com/hindi)
डॉ. भोलेश्वर दुबे
पिछले कुछ दिनों से प्रकृति वैज्ञानिकों, खासतौर पर वनस्पति शास्त्रियों को एक खबर ने विचलित कर रखा है। हुआ यूं कि अमेरिका की एक पुरानी और ख्याति प्राप्त संस्था ड्यूक विश्वविद्यालय ने अपने सौ साल पुराने प्रतिष्ठित हर्बेरियम को बंद करने की घोषणा कर डाली। घोषित कार्ययोजना के अनुसार अगले 2-3 वर्षों में विश्वविद्यालय के छात्रों, प्राध्यापकों और शोधार्थियों से यह सुविधा छिन जाएगी। हालांकि इस निर्णय के खिलाफ वैज्ञानिक समुदाय पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहा है किन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन हर्बेरियम के रख-रखाव पर होने वाले भारी भरकम खर्च के बहाने इसे बंद या अन्यत्र स्थानांतरित करने पर अड़ा हुआ है।
ड्यूक विश्वविद्यालय प्रकृति विज्ञान संकाय की अध्यक्ष सुसान अल्बर्ट्स का कहना है कि 8,25,000 संरक्षित नमूनों को फिलहाल गई-गुजऱी हालत में रखा हुआ है जिसकी व्यवस्थित साज-संभाल के लिए भरपूर धन की आवश्यकता होगी। यद्यपि वे इस प्रतिष्ठित संग्रह और जीव विज्ञान के क्षेत्र में इसकी महत्ता की भी भरपूर तारीफ करती हैं।
येल विश्वविद्यालय के वैकासिक जीव वैज्ञानिक माइकल डॉनोग्हू का तो कहना है कि अपने विश्व स्तरीय हर्बेरियम से मुक्त होने का ड्यूक विश्वविद्यालय का निर्णय एक त्रासद भूल है, यह ड्यूक विश्वविद्यालय में पर्यावरण और मानविकी की चुनौतियों का अध्ययन करने वाले छात्रों और शिक्षकों को मिलने वाली अकादमिक सुविधा को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वे पूछते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंद होने की कतार में क्या अगला नंबर ग्रंथालयों का होगा?
आइए पहले यह जानने की कोशिश करें कि आखिर ड्यूक विश्वविद्यालय के हर्बेरियम की ऐसी क्या खासियत है।
ड्यूक हर्बेरियम, जिसे संक्षेप में ष्ठ्यश्व कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े हर्बेरियमों में से एक है। देश में यह 12वें क्रम पर आता है और प्रायवेट विश्वविद्यालयों में हारवर्ड के बाद दूसरे क्रम पर। यह हर्बेरियम स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक विशिष्ट और मूल्यवान संसाधन साबित हुआ है।
हर्बेरियम में लाखों संवहनी पौधों (1ड्डह्यष्ह्वद्यड्डह्म् श्चद्यड्डठ्ठह्लह्य) के अलावा ब्रायोफाइट्स, शैवाल (एल्गी), लाइकेन और फफूंदों (कवकों) के नमूने संरक्षित हैं। यह एक विशेष बात है क्योंकि संवहनी पौधों के संग्रह तो कई जगह मिल जाते हैं किन्तु इतनी बड़ी संख्या में मॉसेस, शैवाल और कवकों का दुर्लभ संयोग ड्यूक को वैश्विक सम्मान का हकदार बनाता है।
इनमें 2000 वे नमूने भी शामिल हैं जिनके आधार पर पौधों का प्रारंभिक नामकरण किया गया है। इसी के साथ इस हर्बेरियम में विशेषज्ञों द्वारा पहचान किए गए कई महत्वपूर्ण पौधों के प्रतिनिधि नमूने भी संरक्षित हैं, जिन्हें ‘वाउचर स्पेसिमेन’ कहते हैं। आणविक जीवविज्ञान, जैव रसायन और आनुवंशिकी शोध में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पादप संग्रहालय में लगभग चार लाख संवहनी पौधों का संग्रह है। यह संस्था कैरोलिनास और पूरी दुनिया के इलाकों (खासतौर से मीसोअमेरिकन क्षेत्र) में इन पौधों की पारिस्थितिकी, विविधता और वितरण की सूचनाएं भी देती है। ड्यूक हर्बेरियम के 60 प्रतिशत नमूने दक्षिण-पूर्व यूएस से हैं जो कि अमेरिका का जैव-विविधता का हॉट-स्पॉट है। यही कारण है कि जैव-विविधता, पारिस्थितिक विज्ञानियों और संरक्षण जीव वैज्ञानिकों के लिये यह स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं है। यह हर्बेरियम संग्रहित पौधों के नमूनों के चित्र और उनसे सम्बंधित जानकारियों को ऑनलाइन डैटाबेस के रूप में शोधार्थियों को उपलब्ध करवाने में भी अग्रणी है।
क्या होता है हर्बेरियम
असल में हर्बेरियम पौधों के नमूनों का संग्रह है जिन्हें लंबे समय तक संरक्षित रखने की व्यवस्था की जाती है। प्रकृति विज्ञान, विशेष रूप से वनस्पति शास्त्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पौधों की जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। पुरानी वनस्पतिशास्त्र की पुस्तकों में प्राय: ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं कि कुछ व्यक्ति हाफ पैंट और घुटनों तक के बूट पहने, सिर पर हैट लगाए, कंधे पर पेटी नुमा चीज़ लिए कुछ वनस्पतियां इक_ी कर रहे हैं। असल में आज भी यही कुछ किया जाता है किंतु तरीका बदल गया है। हर्बेरियम बनाने के लिए छोटे-छोटे पूरे पौधे, बड़ी झाडिय़ों या वृक्षों की पत्तियों, फूलों सहित टहनियां, और संभव हो तो फल और बीज इक_े कर लिए जाते हैं। पौधों की इस सामग्री को पहले टिन की पेटी (जिसे वेस्कुलम कहते हैं) में रखकर लाया जाता था जिसमें गत्ते या अखबार का अस्तर बिछा होता था ताकि यह सामग्री सूखे नहीं। अब यह काम पॉलीथीन की थैलियों में किया जाता है। इस सामग्री को प्लांट प्रेस में दबाया जाता है। हम जैसे महाविद्यालयीन छात्र इन्हें पत्रिकाओं के बीच व्यवस्थित रख कर किताबों के वजन से दबा दिया करते थे और 1-2 दिन में उलटते-पलटते रहते थे। दबाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पौधे का हर भाग और उसकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें। प्लांट प्रेस से या अन्य विधि से दबाए गए नमूनों को या तो धूप में या फिर गर्म हवा वाली ड्राइंग प्रेस या बिजली के बल्ब वाले ओवन में सुखाया जाता है। शैवाल, कवक, जलीय पौधों और मांसल पौधों को संरक्षित करने के लिए अलग विधि अपनाई जाती है। जलीय पौधों को प्रेसिंग पेपर के छोटे टुकड़े पर धीरे से फैला कर उठा लिया जाता है और इसे सीधे प्रेसिंग शीट पर रख देने से वे चिपक जाते हैं। सामान्य पौधों के नमूने सूख जाने पर इन्हें 29ङ्ग41 सेंटीमीटर की मोटी शीट पर सरेस, गोंद या पारदर्शी गोंद युक्त कपड़े की पट्टियों या सैलोटेप से चिपका दिया जाता है। कहीं-कहीं नमूनों को शीट पर इथाइल सेल्यूलोज़ और रेजिन के मिश्रण से भी चिपकाते हैं। इस प्रकार एकत्रित किए गए नमूने की एक शीट तैयार होती है, जिस पर उस पौधे से सम्बंधित जानकारियां (जैसे संग्रह का स्थान, कुल का नाम, संग्रह करने की तारीख, प्राकृतवास, संग्राहक का नाम, पहचान हो गई हो तो पौधे के वंश और प्रजाति का नाम) अंकित की जाती हैं।
हर्बेरियम शीट्स को हर्बेरियम केबिनेट में मानक वर्गीकरण के आधार पर नियत खण्ड (पिजन होल) में रखा जाता है। कवक और कीटों से सुरक्षा के लिए उन्हें समय-समय पर उल्टा-पल्टा जाता है तथा कीटनाशक रसायनों का फ्यूमिगेशन किया जाता है और केबिनेट में नेफ्थालिन की गोलियां भी रखी जाती हैं। इस तरह से सुखाकर शीट पर चिपकाए गए पौधों के भाग हर्बेरियम नमूने कहलाते हैं।
इसके अलावा हर्बेरियम में बीज, सूखे फल, शैवाल, कवक, काष्ठ की काट, पराग कण, सूक्ष्मदर्शी स्लाइड द्रव में संरक्षित फल और फूल, सिलिका में दबाकर संग्रहित चीज़ें, यहां तक कि डीएनए निष्कर्षण भी उपलब्ध होते हैं। आधुनिक विकसित हर्बेरियम में डैटा संग्रह, वानस्पतिक चित्र, नक्शे और उस क्षेत्र से संबंधित पौधों के बारे में साहित्य भी उपलब्ध होता है।
हर्बेरियम बनाने की शुरुआत सोलहवीं शताब्दी में पिसा विश्वविद्यालय में औषधि और वनस्पतिशास्त्र के प्राध्यापक ल्यूका घिनि ने की थी। उन्होंने एक ही शीट पर कई पौधों को सुन्दर तरीके से चिपकाया और ऐसी कई शीट की जिल्दबंद किताबें बना दी थीं, जिनका उपयोग ग्रंथालय में संदर्भ के लिए किया जाने लगा। इस विधि में नमूनों को एक बार जिस क्रम में चिपका दिया उसे बदलने की कोई संभावना नहीं थी। अत: वर्गीकरण के मान से सुधार की गुंजाइश खतम हो गई। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध प्रकृतिविद, वनस्पतिशास्त्र के विद्वान केरोलस लीनियस ने 1751 में अपनी कृति फिलॉसॉफिया बॉटेनिका में सुझाव दिया था कि एक शीट पर एक ही नमूना चिपकाया जाए और इसकी जिल्द न बनाई जाए। लीनियस ने इन शीट को रखने के लिये विशेष प्रकार की केबिनेट भी बनाई थी। ऐसा करने से शीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने व वर्गीकरण के मान से होने वाले नवाचार के अनुसार उनका स्थान बदलने की गुंजाइश हमेशा बनी रही। तब से लेकर आज तक विश्व के सभी प्रमुख हर्बेरियम में यही विधि अपनाई जा रही है।
वनस्पतिशास्त्र, मुख्यत: वर्गीकरण विज्ञान तथा जैव विविधता, के अध्ययन में हर्बेरियम का बहुत महत्व है। हर्बेरियम में संरक्षित मूल नमूनों (जिन्हें टाइप स्पेसिमेन कहा जाता है) से मिलान करके किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की पहचान सुनिश्चित की जाती है। प्रामाणिक हर्बेरियम में उपलब्ध पौधे से यदि पौधा मेल नहीं खाता तो उसे नई प्रजाति माना जाता है। पौधों की नई प्रजातियों की जानकारी को वनस्पतिशास्त्र में शामिल करने का काम यहीं से शुरू होता है।
ज़ाहिर है, सभी प्राचीन विश्वविद्यालयों, वानस्पतिक शोध संस्थानों और बड़े महाविद्यालयों के अपने व्यवस्थित हर्बेरियम होते हैं जो उस क्षेत्र की वनस्पतियों के नमूनों का संग्रह वनस्पतिशास्त्र के विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाते हैं। आज भी दुनिया भर में कई हर्बेरियम को उनके वर्षों पुराने पौधों के संग्रह और दी जाने वाली सेवाओं के लिये विशेष सम्मान दिया जाता है। इनमें लंदन स्थित रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, फ्रांस में पेरिस का नेचुरल हिस्ट्री नेशनल म्यूजिय़म, न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क बॉटेनिकल गार्डन का हर्बेरियम प्रमुख हैं।
आज दुनिया भर के 183 देशों के करीब 3500 हर्बेरियम पंजीकृत हैं जिनमें कुल मिलाकर 40 करोड़ नमूने संग्रहित हैं। भारत में भी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में 30 लाख नमूने संरक्षित हैं। इसी के साथ 1795 में हावड़ा में स्थापित सेन्ट्रल नेशनल हर्बेरियम में बीस लाख, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (देहरादून) में साढ़े तीन लाख और नेशनल बॉटेनिकल गार्डन (लखनऊ) में ढाई लाख से ज़्यादा नमूने संरक्षित हैं।
हर्बेरियम नमूनों की मदद से पौधों की पहचान करने में मदद मिलती है। इनके माध्यम से पौधों के आवास की भौगोलिक सीमा, फूलने-फलने के समय की जानकारी भी मिलती है। पौधों के वर्गीकरण और नामकरण में तो हर्बेरियम की प्रमुख भूमिका है ही। इसके साथ पौधों के उद्विकास (जाति वृत्त), आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी, वानिकी, औषधि विज्ञान, प्रदूषण, चिकित्सा विज्ञान तथा विज्ञान की अन्य कई शाखाओं में भी इनका अच्छा खासा योगदान है।
विज्ञान जगत का दुर्भाग्य ही है कि पिछले 30 वर्षों में कई छोटे-बड़े हर्बेरियम बंद हो गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सदमा पहुंचाने वाली घटना 2015 में मिसौरी विश्वविद्यालय द्वारा 119 वर्ष पुराने डन पामर हर्बेरियम को बंद करने का निर्णय था जहां एक लाख सत्तर हज़ार से अधिक पौधों के नमूने संरक्षित थे। इन नमूनों को 200 कि.मी. दूर स्थानांतरित कर दिया गया था जिससे विश्वविद्यालय के छात्र और प्राध्यापक उस का लाभ लेने से वंचित हो गए। यही कहानी आज ड्यूक विश्वविद्यालय में भी दोहराई जा रही है।
1921 में ट्रिनिटी कॉलेज से शुरू हुए ड्यूक विश्वविद्यालय के हर्बेरियम को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने के लिए ह्यूगो एल. ब्लोमक्विस्ट ने नॉर्थ केरोलिना के पी.ओ. शैलर्ट का 16,000 नमूनों का संग्रह खरीदा था। इसके बाद ख्याति प्राप्त पारिस्थितिक वैज्ञानिक हेनरी ऊस्टिंग और अन्य वैज्ञानिकों के प्रयासों से 1963 में यह संस्था उष्णकटिबंधीय अध्ययन संगठन (ह्रञ्जस्) का हिस्सा बनी और नवउष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के अध्ययन का प्रमुख केन्द्र बन गई।
एक शताब्दी से अधिक समय से किए गए अथक परिश्रम से इस हर्बेरियम ने जो ऊंचाइयां हासिल की उसे आर्थिक संकट के चलते बंद या स्थानांतरित करने का निर्णय गंभीर वनस्पतिशास्त्रियों को झकझोर देने वाला समाचार है। हर्बेरियम के शुभचिंतकों ने न केवल विरोध के स्वर मुखर किए हैं बल्कि उन्होंने इसे बचाने के लिए वित्तीय मदद हेतु दानदाताओं से अपील भी की है। एक दानी ने दस लाख डॉलर देने की पेशकश भी की है। मगर विश्वविद्यालय प्रशासन ढाई करोड़ डॉलर की आवश्यकता बता रहा है।
कुल मिलाकर विज्ञान विषयों की आधारभूत सुविधाओं जैसे प्रयोगशालाओं, ग्रंथालयों, वानस्पतिक उद्यानों, परिभ्रमणों, हर्बेरियम, म्यूजिय़म आदि को समाप्त कर कहीं हम प्रयोग और प्रयोगशाला विहीन विज्ञान को बढ़ावा देने की ओर कदम तो नहीं बढ़ा रहे हैं। एक कहावत है-‘‘बुढिय़ा मर गई इसका अफसोस नहीं है मगर मौत ने घर देख लिया यह चिंता की बात है।’’ स्थिति यही है आज ड्यूक विश्वविद्यालय के हर्बेरियम का अस्तित्व मिट रहा है; ऐसा न हो, सभी विश्वविद्यालय उसी राह पर चल पड़ें। अत: वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को गंभीरता पूर्वक विचार कर इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। (स्रोतफीचर्स)
सारिका सिंह
बहुजन समाज पार्टी के नए चेहरे और उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए आकाश आनंद आजकल राजनीतिक रैलियों के अलावा मीडिया साक्षात्कारों के जरिए भी चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर भी वो पार्टी को नया कलेवर देने की कोशिशें कर रहे हैं।
आकाश आनंद राजनीतिक रैलियों में बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के युवा दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद की आलोचना करते हैं। लेकिन उनसे जुड़े सवाल पर उन्हें ‘छुटभैया’ कहकर खारिज कर देते हैं।
कभी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक हैसियत पिछले चुनावों में काफी घटी है।
पार्टी ने पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा और दस सीटें जीतीं, लेकिन इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है।
आकाश आनंद मानते हैं कि ये पार्टी की सोची-समझी रणनीति है।
क्या बीएसपी बीजेपी की बी टीम है?
बीबीसी से खास बातचीत में आकाश आनंद ने बीएसपी को बीजेपी की बी-टीम बताए जाने के आरोपों को ख़ारिज किया, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी का मक़सद राजनीतिक सत्ता में आना है। इसके लिए पार्टी जो सही होगा करेगी।
उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया।
चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर आनंद ने कहा, ‘हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि हम राजनीतिक सत्ता में आ जाएं, ताकि हम अपने समाज के लिए काम कर सकें।’
जब उनसे पूछा कि क्या आप इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि अगर आपको साथ जाना पड़े तो जाएंगे तो उन्होंने कहा, ‘हम जाएंगे नहीं लेकिन हमें किसी का इस्तेमाल करना पड़े तो करेंगे, किसी का भी इस्तेमाल करेंगे।’
‘इस्तेमाल करने’ को परिभाषित करते हुए वो कहते हैं, ‘इस्तेमाल करने की परिभाषा ये होती है कि हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, हम उनका इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने लोगों की सेवा कर सकें।’
परिवारवाद के आरोपों का किया बचाव
बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने दिल्ली में बीएसपी के दफ्तर में आकाश आनंद से साक्षात्कार किया।
बहुजन समाज पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत आकाश आनंद की रैलियों से हुई। क्या वो मायावती की जगह बीएसपी का चेहरा बन रहे हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा, ‘ऐसा नहीं है, मायावती की कम से कम 45 रैलियों की योजना है, वो हर क्षेत्र में ख़ुद जाकर कमान संभाल रही हैं। हम तो उनके लिए वार्मअप कर रहे थे, माहौल तैयार कर रहे थे, अब वो मैदान में जाएंगी तो ख़ुद अपना मैसेज डिलिवर करेंगी।’
बहुजन समाज पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है। कांशीराम के बाद पार्टी की कमान मायावती के हाथ में आई। मायवती अभी भी पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं। हालांकि, आकाश आनंद को उनके उत्तराधिकारी की तरह पेश किया गया है। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं।
आकाश आनंद को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने के बाद वंशवाद के आरोप भी लगे हैं।
हालांकि आनंद इन आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहते हैं, ‘हमसे पहले, और परिवार को आगे रखने से पहले बहनजी ने कम कम से चार लोगों को मौका दिया जो परिवार से नहीं थे, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, कुछ वक़्त बाद पार्टी के सीनियर लीडर्स ने सलाह दी कि परिवार से ही किसी को आगे बढ़ाया जाए, कस्टोडियन के रूप में, उसके बाद मुझे जि़म्मेदारी मिली, हम कस्टोडियन की तरह हैं ना कि उत्तराधिकारी, ये विरासत नहीं है बल्कि जि़म्मेदारी है, हम इसे ऐसे ही निभाएंगे।’
आकाश आनंद में ‘एंग्री यंग मैन’ की छवि?
आकाश आनंद ने कई भावुक भाषण दिए हैं। इस दौरान वो एक ‘एंग्री यंग मैन’ की भूमिका में भी नजर आए हैं।
आकाश आनंद कहते हैं, ‘रैलियों में हम जो मुद्दे उठाते हैं वो अलग है, महत्वपूर्ण हैं इसलिए इमोशनल हो जाना नैचुरल है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसके पेपर लीक हो जाएं तो वो जो गुस्सा है वो मेरा अकेले का गुस्सा नहीं, हम इसके ज़रिए विपक्ष और सरकार में बैठे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं।’
आकाश आनंद सिफऱ् मौजूदा सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं पर भी निशाना साध रहे हैं।
आनंद कहते हैं, ‘हमारी लड़ाई संविधान को बचाने और लोगों के हक़ के लिए है, हम किसी विपक्ष से नहीं लड़ रहे, हम अपने वोटर्स के लिए लड़ रहे हैं, हम उन्हें समझाने के लिए लड़ रहे हैं।’
राहुल गांधी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेताओं से तुलना से जुड़े सवाल पर आकाश कहते हैं, ‘जहां तक सीनियर लीडर्स की बात है, उनका एक राजनीतिक नजरिया है, वो उसके साथ हैं, अखिलेश यादव की पार्टी जो मुद्दे लेकर आई है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन देने की बात है, वो हर समाज के अल्पसंख्यकों के मुद्दे को सही तरीके से सामने नहीं ला पा रहे, जहां तक राहुल गांधी की बात है, कांग्रेस पार्टी की 60 -70 साल से ज़्यादा वक़्त सरकार कई राज़्यों में रही है, वो सबसे लंबे वक़्त तक सेंटर मे भी रहे हैं, आज भी उन्हें इतना वक्त लेने के बाद वो वक्त मांग रहे हैं, अगर उन्हें बताना पड़ रहा है कि वो रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, पिछड़े समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए बहुत देर हो चुकी है।’
भीम आर्मी के चंद्रशेखर का नाम क्यों नहीं लेते हैं आकाश
आकाश आनंद भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर से जुड़े सवालों पर बात करने से बचते हैं।
चंद्रशेखर को एक राजनीतिक खतरे के रूप में खारिज करते हुए आकाश कहते हैं, ‘जो एक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते आप नेशनल पार्टी से उसकी तुलना कहां कर रही हैं, कहां से आप ख़तरा मान रही हैं, ये तो विपक्षी पार्टियां समय-समय पर छोटे-छोटे दल खड़े कर देती हैं, उनको फंड कर देती हैं, ये वो हैं।’
आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद को कई पार्टियों की बी-टीम बताते हुए कहते हैं, ‘वो किसी एक की नहीं सबकी बी टीम है, पता नहीं कहां-कहां जाता है, आप उनकी बात छोडि़ए।’
हालांकि, आकाश आनंद ने चंद्रशेखर का नाम अपनी रैलियों में नहीं लिया है। इस सवाल पर वो कहते हैं, ‘उन्हें महत्व देकर क्या मिलेगा, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों की बात कर रहे हैं, ऐसे में उनकी बात करना सही नहीं है, मुझे लगता है जब आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं तो उनके मुद्दों की बात की जाए, ना कि छुटभैया लोगों या चीज़ों की, उसके जैसे हज़ारों मिल जाएंगे आजकल समाज में या सडक़ों पर घूमते हुए, जो ‘जय भीम’ कह कर लोगों को भटकाते हैं, उनका मकसद है बीएसपी से लोगों को किसी तरह दूर करने का।’
इंडिया गठबंधन से क्यों बनाई दूरी
बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह बताते हुए आनंद कहते हैं बीएसपी ने इस बार अलग संदेश देने की कोशिश की है। आनंद कहते हैं कि पार्टी के पास उसके अपने मतदाता हैं। यही पार्टी को अकेले लडऩे का आत्मविश्वास देता है।
आनंद कहते हैं, ‘अगर विपक्ष को साथ लेकर आएं तो सीटें निकल आती हैं और वो अगर हमसे दूर रहें तो हमारा वोट काटते हैं, हमारी सीटें हाथ से निकल जाती हैं, तो इसलिए इस बार हम अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, इंडी अलायंस कह रहा है कि हम वोट काटते हैं, हम किसी पार्टी की बी-टीम हैं, वो सही नहीं है।’
बहुजन समाज पार्टी ने इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी मुसलमान आबादी वाली सीटों पर पांच मुसलमान उम्मीदवार दिए हैं।
बीएसपी पर वोट काटने और बीजेपी की बी-टीम की तरह काम करने के आरोपों को ख़ारिज करते हुए आनंद कहते हैं, ‘हमने इसलिए मज़बूत मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं क्योंकि वहां पर उस इलाक़े में मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद बड़ी है, और हम ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं जो जीत सकता है, टक्कर दे सकता है, अगर मुसलमान और दलित समुदाय के कैंडिडेट को देखें तो वो जीतने वाले उम्मीदवार होते हैं।’
क्या मुसलमान बीएसपी को वोट करेंगे?
आनंद ये मानते हैं कि भले ही अभी मुसलमान वोटर बीएसपी के साथ मज़बूती से ना हो लेकिन पार्टी मुसलमानों को साथ लाने का प्रयास कर रही है।
आनंद कहते हैं, ‘हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं, मुसलमान शायद हमारे साथ खड़ा हो सकता है, अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा हो सकता है, ये तो मुसलमान लोगों को सम्मान देने जैसा है कि हम उन्हें विकल्प दें।’
हाल के कई चुनावों में बीएसपी राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या दलित वोट बैंक अब बीएसपी से खिसक रहा है।
आनंद कहते हैं, ‘अगर आप ग्राउंड पर रिपोर्ट लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यकों में किसी को नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी उनके लिए नहीं लड़ रही।’
आनंद मानते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके समर्थन में तर्क देते हुए वो कहते हैं, ‘कास्ट सेंसस जरूरी है। किस समुदाय की क्या ज़रूरत है किस पर कितना ध्यान देने की जरूरत है ये भी वहीं से निकल कर आएगा, तो ये जरूरी है।’
केंद्रीय जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल के विपक्ष के आरोपों पर आनंद कहते हैं कि पहले भी उनका इस्तेमाल होता रहा है। (bbc.com/hindi)
मानव आबादी का अस्तिस्व बनाए रखने के लिए जरूरी है कि प्रति प्रजननक्षम व्यक्ति के 2.1 बच्चे पैदा हों। इसे प्रतिस्थापन दर कहते हैं। काफी समय से जननांकिकीविदों का अनुमान था कि कुछ सालों के बाद प्रजनन दर इस जादुई संख्या (2.1) से कम रह जाएगी।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग (UNPD) की 2022 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि यह पड़ाव वर्ष 2056 में आएगा। 2021 में विट्गेन्स्टाइन सेंटर फॉर डेमोग्राफी एंड ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल ने इस पड़ाव के 2040 में आने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन दी लैंसेट में प्रकाशित हालिया अध्ययन थोड़ा चौंकाता है और बताता है कि यह मुकाम ज़्यादा दूर नहीं, बल्कि वर्ष 2030 में ही आने वाला है।
देखा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता लाने के प्रयास, लोगों के शिक्षित होने, बढ़ती आय, गर्भ निरोधकों तक बढ़ती पहुंच जैसे कई सारे कारकों की वजह से कई देशों में प्रजनन दर में काफी गिरावट आई है, और यह प्रतिस्थापन दर से भी नीचे पहुंच गई है। मसलन, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रजनन दर 1.6 है, चीन की दर 1.2 है और ताइवान की 1.0 है। लेकिन कई देशों, खासकर उप-सहारा अफ्रीका के गरीब देशों, में यह दर अभी भी काफी अधिक है- नाइजर की 6.7, सोमालिया की 6.1 और नाइजीरिया की 5.1।
चूंकि हर देश की प्रजनन दर बहुत अलग-अलग हो सकती है, ये रुझान विश्व को दो हिस्सों में बांट सकते हैं- कम प्रजनन वाले देश, जहां युवाओं की घटती संख्या के मुकाबले वरिष्ठ नागरिकों की आबादी अधिक होगी; और उच्च-प्रजनन वाले देश, जहां निरंतर बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा पहुंचा सकती है।
यहां यह स्पष्ट करते चलें कि प्रजनन दर का प्रतिस्थापन दर से नीचे पहुंच जाने का यह कतई मतलब नहीं है कि वैश्विक जनसंख्या तुरंत कम हो जाएगी। ऐसा होने में लगभग 30 और साल लगेंगे।
इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME) के शोधकर्ताओं ने अपने मॉडल में प्रजनन दर कब प्रतिस्थापन दर से नीचे जाएगी, इस समय का अनुमान इस आधार पर लगाया है कि प्रत्येक जनसंख्या ‘समूह’ (यानी एक विशिष्ट वर्ष में पैदा हुए लोग) अपने जीवनकाल में कितने बच्चों को जन्म देंगे। इस तरीके से अनुमान लगाने में लोगों के अपने जीवनकाल में देरी से बच्चे जनने के निर्णय लेने जैसे परिवर्तन पता चलते हैं। इसके अलावा IHME के इस मॉडल ने अनुमान लगाने में लोगों की गर्भ निरोधकों और शिक्षा तक पहुंच जैसे चार कारकों को भी ध्यान में रखा है जो प्रजनन दर को प्रभावित कर सकते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है यह पड़ाव चाहे कभी भी आए, देशों की प्रजनन दर में बढ़ती असमानता (अन्य) असमानताओं को बढ़ाने में योगदान दे सकती है। मध्यम व उच्च आय के साथ निम्न प्रजनन दर वाले देशों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से कम होने से वहां काम करने वाले लोगों की कमी पड़ सकती है और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों, राष्ट्रीयकृत स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर दबाव पड़ सकता है। वहीं, निम्न आय के साथ उच्च प्रजनन दर वाले देशों के आर्थिक रूप से और अधिक पिछडऩे की संभावना बनती है। साथ ही, बहुत कम संसाधनों के साथ ये देश बढ़ती आबादी को बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और शिक्षा मुहैया नहीं करा पाएंगे। बहरहाल, इस तरह की समस्याओं को संभालने के लिए हमें समाधान खोजने की जरूरत है। (स्रोतफीचर्स)
प्रिय दर्शन
1. जिसे गंभीर साहित्य कहते हैं, वह आठवीं से मैंने पढऩा शुरू किया। मां, पापा, मामा- सबने हिंदी में एमए किया था। घर में प्रेमचंद के ‘गोदान’, प्रसाद की ‘कामायनी’ के अलावा ‘चंद्रगुप्त’ और ‘ध्रुवस्वामिनी’, मोहन राकेश का ‘आषाढ़ का एक दिन’ और दिनकर का ‘चक्रवाल’ जैसा विराट संग्रह और ‘रश्मिरथी’ थे। इसके अलावा निराला, महादेवी और पंत के कविता संग्रह थे। अज्ञेय के भी कविता संग्रह थे। आलोचना की कई किताबें थीं जिनमें मेरी दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा धर्मयुग और सारिका जैसी पत्रिकाएं आती थीं। दिनकर मेरे प्रिय कवि हो चुके थे।
2. लेकिन जिसे धुआंधार पढ़ाई कहते हैं, वह इंटरमीडिएट के बाद शुरू हुई। रांची के दो पुस्तकालयों- रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी और फादर कामिल बुल्के शोध संस्थान को अगले तीन साल में मैंने छान मारा। इसके अलावा कुछ किताबें स्टेट लाइब्रेरी और संतुलाल पुस्तकालय से भी पढ़ीं। इस दौरान दोस्तों से किताबों का लेन-देन भी चला।
3 लेकिन मैंने उन दिनों कुल कितनी किताबें पढ़ी होंगी? कुछ महीने जब रोज़ एक किताब पढऩे की नासमझ धुन थी और जिसके तहत शरतचंद्र के सारे उपन्यास निबटाए गए थे- शायद सप्ताह में एक किताब का औसत पड़ा होगा। यानी साल में 52 किताबें। विश्वविद्यालय के समय के चार साल में यही औसत जोड़ ले और महीनों की रोजमर्रा पढ़ाई भी शामिल कर लें तो अधिकतम 250 किताबें।
4 बाद के वर्षों में पढऩा कम हो गया। बहुत उदार हो कर जोड़ूं तो शायद पंद्रह दिन में एक किताब का औसत। यानी पच्चीस किताबें हर साल। इस ढंग से बीते तीस साल में 750 किताबें। हालांकि यह गिनती बहुत बढ़ा-चढ़ाकर की गई है। कहने का मतलब यह कि अभी तक कुल मिलाकर हजार किताबें भी शायद मुश्किल से पढ़ी हों। यह भी संभव है कि असली संख्या इसकी आधी या उससे भी कम हो।
5. दरअसल आज का आदमी अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से पांच सौ-हज़ार किताबें पढ़ सकता है- भले ही उसके निजी पुस्तकालय में कई हजार किताबें हों। तो कभी किसी ऐसे विद्वान के आतंक में न आएं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसने हजारों किताबें पढ़ रखी हैं।
6. एक किताब का हवाला मैं अक्सर दिया करता हूं- This Is Not the End of the Book. यह उंबेर्तो इको और जां क्लाद केरियर के बीच की बातचीत पर आधारित है। दोनों बताते हैं कि उनकी लाइब्रेरी में बीस हजार से ज़्यादा किताबें हैं। शायद एक के पास पचास हजार भी। लेकिन दोनों मानते हैं कि उन्होंने इनमें बहुत कम किताबें पढ़ी हैं।
7. दोनों बताते हैं - और यह हम अपने अनुभव से भी जानते हैं- कि कुछ किताबों के बारे में हम दूसरों से इतना सुन चुके होते हैं कि लगता है कि हमने तो इन्हें पढ़ रखा है। कुछ किताबें हम अधूरी पढ़ कर छोड़ देते हैं। कुछ किताबें संदर्भ के लिए बीच-बीच में पलटते हैं। और कुछ किताबें हमेशा अछूती रह जाती हैं।
8. निष्कर्ष क्या है? आप दुनिया की सारी अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकते। जो क्लासिकल साहित्य है, उसी का खजाना इतना बड़ा है कि आप उसका एक अंश भी नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे अनमोल और अंतर्दृष्टिपूर्ण लेखन से वंचित रह जाना हम सबकी नियति है। समकालीन संदर्भों में भी जो लिखा जा रहा है, उसे भी पूरा पढऩा असंभव है।
9. फिर क्या करें? बस गिनी-चुनी किताबें पढ़ें। लेकिन इनका चुनाव कैसे करें? क्या इसमें अपनों की, अपने आसपास के लोगों की किताबें शामिल हो पाएंगी? क्या हम? तथाकथित महान किताबों के चक्कर में अपने लेखकों को पढऩा छोड़ दें? लेकिन फिर उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? और हमें ही कौन पढ़ेगा।
10. दुनिया में बड़े और भव्य स्थापत्यों की कमी नहीं, वहां हम घूमने भले चले जाएं, लेकिन आवाजाही अंतत: अपनों के घरों में ही होती है- भले ही वे मामूली और कम कलात्मक या कम भव्य हों। शायद किताबें चुनते हुए भी हमारा पैमाना यही होता है। दुनिया की महान किताबें पढ़ें, लेकिन अपनों की किताबों के लिए भी समय निकालें। अपने समय और समाज की धूल-मिट्टी आखिर इनमें ही मिलती है। बस अपने लोग यह कृपा करें कि एक सुधी पाठक के पढऩे की सीमा समझें और जबरन अपनी किताब उस पर न ठेलें।
यह कैसे तय होता है कि हम अपनी सुबह की चाय या कॉफी का कप किस हाथ से उठाएंगे या मंजन किस हाथ से करेंगे? हाल ही में शोधकर्ताओं ने नेचर कम्युनिकेशंस में 3,50,000 से अधिक व्यक्तियों के जेनेटिक डैटा की पड़ताल के नतीजे प्रकाशित किए हैं, जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि वह क्या है जो यह तय करता है कि हम दाएं हाथ से काम करने में सहज होंगे या बाएं हाथ से। इस पड़ताल में उन्हें ट्यूबुलिन प्रोटीन की भूमिका का पता चला है जो कोशिकाओं के आंतरिक कंकाल की रचना करता है।
दरअसल मानव विकास में भ्रूणावस्था के दौरान मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से की वायरिंग अलग-अलग तरह से होती है, जो आंशिक रूप से जन्मजात व्यवहारों को निर्धारित करती है। जैसे कि हम मुंह में किस ओर रखकर खाना चबाएंगे, आलिंगन किस ओर से करेंगे, और हमारा कौन-सा हाथ लगभग सभी कामों को करेगा या प्रमुख होगा। अधितकर लोगों का दायां हाथ प्रमुख हाथ होता है। लेकिन लगभग 10 प्रतिशत मनुष्यों का बायां हाथ प्रमुख होता है।
चूंकि अधिकांश लोगों में एक हाथ की तुलना में दूसरे हाथ के लिए स्पष्ट रूप से प्राथमिकता होती है, प्रमुख हाथ से सम्बंधित जीन का पता लगने से मस्तिष्क में दाएं-बाएं विषमता का जेनेटिक सुराग मिल सकता है।
पूर्व में हुए अध्ययनों में यूके बायोबैंक में सहेजे गए जीनोम डैटा की पड़ताल कर 48 ऐसे जेनेटिक रूपांतर खोजे गए थे जो बाएं हाथ के प्रधान होने से सम्बंधित थे। ये ज़्यादातर डीएनए के गैर-कोडिंग हिस्सों, यानी उन हिस्सों में पाए गए थे जो किसी प्रोटीन के निर्माण का कोड नहीं हैं। इनमें वे हिस्से भी थे जो ट्यूबुलिन से सम्बंधित जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकते थे। ट्यूबलिन प्रोटीन लंबे, ट्यूब जैसे तंतुओं में संगठित होते हैं जिन्हें सूक्ष्मनलिकाएं कहा जाता है, जो कोशिकाओं के आकार और आंतरिक गतियों को नियंत्रित करती हैं।
लेकिन अब नेदरलैंड के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलिंग्विस्टिक्स के आनुवंशिकीविद और तंत्रिका वैज्ञानिक क्लाइड फ्रैंक्स और उनकी टीम ने यूके बायोबैंक में संग्रहित जीनोम डैटा में प्रोटीन-कोडिंग हिस्से में जेनेटिक रूपांतर खोजे हैं। इसमें 3,13,271 दाएं हाथ प्रधान और 38,043 बाएं हाथ प्रधान लोगों का डैटा था। विश्लेषण में उन्हें ञ्जक्चक्च4क्च ट्यूबुलिन जीन में एक रूपांतर मिला, जो दाएं हाथ प्रधान लोगों की अपेक्षा बाएं हाथ प्रधान लोगों में 2.7 गुना अधिक था।
माइक्रोट्यूब्यूल्स हाथ की वरीयता को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि वे सिलिया- कोशिका झिल्ली में रोमिल संरचना-बनाते हैं जो विकास के दौरान एक असममित तरीके से द्रव प्रवाह को दिशा दे सकती है। ये निष्कर्ष यह पता करने में मदद कर सकते हैं कि कैसे सूक्ष्मनलिकाएं प्रारंभिक मस्तिष्क विकास को ‘असममित मोड़’ दे सकती हैं।(स्रोतफीचर्स)
कनुप्रिया
शाकाहार और माँसाहार की सतत चलती बहसों के बीच मुझे यही कहना है कि मैं माँसाहार नहीं करती, राजस्थान से हूँ जो कि देश का सबसे अधिक शाकाहारी प्रदेश माना जाता है तो इसका भी असर हो सकता है। अंडा खाती हूँ कभी कभी, मगर जानवरों के प्रति कभी क्रूरता न की हो इसके दोष से पूर्णतया बरी हूँ कह नहीं सकती।
रेशम पहनती हूँ कभी कभी, चमड़े के बैग इस्तेमाल किये हैं, ऊन भी इस्तेमाल की है, गाय का दूध भी पिया है, इन सबमे कहीं न कहीं क्रूरता होती है। इसके अलावा लकड़ी का फर्ऩीचर है घर मे, जो जंगलों को काटकर बनता है, जिन जगहों पर रही हूँ जिन कॉलोनियों में वो कभी जंगल रहे होंगे, हज़ारों जानवरो का घर उजड़ा होगा, बच्चे मरे होंगे तो मेरा फ्लैट बना होगा, जिन खेतों से खाना आता है उनकी जमीन भी जंगलों को साफ़ करके बनाई गई होगी, जंगलों की ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है। फिर जिन इंडस्ट्रीज़ का माल काम मे लेती हूँ वो भी जंगलों को उजाड़ कर बनाई गई होंगी। जिन मंदिरों में घण्टा बजाकर पूजा की है वहाँ भी कोई जंगल रहा होगा। तो मैं नहीं जानती अप्रत्यक्ष तौर पर कितने जानवरों के बसेरे उजाडऩे में मेरा हाथ रहा है, दुनिया की कितनी जीव प्रजातियाँ नष्ट हुई होंगी तो मेरे जीवन का कारोबार चल रहा है।
मैं ये भी नहीं जानती कि पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाए तो उसके लिये खेत लगेंगे और उन खेतों के लिये कितने जंगल उजड़ेंगे।
शाकाहार मांसाहार स्वाद की चॉइस तो हो सकती है मगर जो शाकाहार के लिये श्रेष्ठता भाव से ग्रस्त हैं उनसे मुझे पूछना है कि जितनी शिद्दत से वो शाकाहार पर बोलते हैं उतनी ही शिद्दत से जब जंगल काटे जाते हैं तब क्यों नहीं बोलते, तब क्या उन्हें जानवरो के प्रति क्रूरता नजऱ नहीं आती? जो आदिवासी जंगल बचाते हैं उनके पक्ष में खड़े क्यों नहीं होते? जो लोग प्रकृति और और उसके संसाधन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष पर आपका जानवर प्रेम कहाँ चला जाता है।
जो इन सब मामलों में चुप रहकर महज शाकाहार पर बोलते हैं, जंगल उजाड़ कर जीव की बात करने वाले, महज पाखंडी हैं इसके सिवा कुछ नहीं। उनका और मेरा शाकाहार महज दूसरों को नीचा दिखाने वाला श्रेष्ठता बोध है, यह श्रेष्ठता बोध मेरे धर्म से आता है या जाति से , पता नहीं।
मुझे तो बस ये जानना है कि अगर ऐसे लोग सचमुच ही बहुत बड़े जीव प्रेमी हैं तो उनकी दीवारें धनिकों के लालच के लिये जंगलों की कटाई पर हमेशा ही ख़ामोश क्यों रहती हैं?
जगदीश्वर चतुर्वेदी
बलराज साहनी उन चंद अभिनेताओं में हैं जो खुलकर कहते हैं कि मैं ईश्वर की सत्ता नहीं मानता,आजकल हालात यह हैं कि फिल्म रिलीज के दिन या पहले अभिनेता-अभिनेत्रियां मंदिरों और दरगाहों पर मत्था टेकते रहते हैं, हिंदी फिल्मों के अभिनेता-अभिनेत्रियां सार्वजनिक मसलों पर बोलने से डरते हैं। कलाकार की इस समाज-विमुखता को किसी भी तर्क से स्वीकृति नहीं दी जा सकती। हमारे यहां हालात इतने खराब हैं कि अभिनेता-अभिनेत्री हमेशा पापुलिज्म के दबाव में रहते हैं। ऐसा करके वे कला की कितनी सेवा करते हैं यह हम नहीं जानते लेकिन उनका सामाजिक-राजनीतिक सवालों से किनाराकशी करना अपने-आपमें नागरिक की भूमिका से पलायन है।
बलराज साहनी का एक निबंध है ंमेरा दृष्टिकोणं,इसमें उन्होंने साफ लिखा हैं, मैं ईश्वर को बिलकुल नहीं मानता, जो लोग आए दिन धर्म और ईश्वर के नाम पर समझौते करते रहते हैं और धर्म की भूमिका की अनदेखी करते हैं, उनके लिए यह निबंध जरूर पढऩा चाहिए। साहनी ने लिखा ंएक नास्तिक के लिए आस्तिकता के साथ जरा-सा भी समझौता करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में धर्म एक ऐसी व्यापारिक संस्था बन गया है कि उसके ंसेल्समैनं हर तरफ भागे-दौड़े फिर रहे हैं, जिनसे अपने-आपको बचाये रखने के लिए हर समय चौकन्ना रहने की जरूरत है।
बलराज साहनी घोषित माक्र्सवादी थे और माक्र्सवाद के प्रति अपनी आस्थाओं को उन्होंने कभी नहीं छिपाया। उन्होंने लिखा ं मैं माक्र्सवाद को दर्शनशास्त्र की सर्वोच्च उपलब्धि मानता हूँ। माक्र्सवाद के अनुसार सृष्टि ही वास्तविक सत्य है, और उसे अपने विकास के लिए किसी बाह्य आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। और सृष्टि को समझने-बूझने के लिए विज्ञान ही सबसे अधिक सार्थक साधन है, धर्म या अध्यात्म नहीं।ं
आजकल जो लोग प्राचीनकाल में इंटरनेट और विज्ञान आदि की नई-नई खोजें पेश कर रहे हैं, उस तरह के विचारकों को केन्द्र रखकर लिखा, ंअध्यात्मवादियों, योगियों, ज्योतिषियों और दर्शनशास्त्रियों ने सृष्टि को लेकर पूर्ण रूप से समझने के जो दावे किए हैं,वे मुझे हास्यजनक प्रतीत होते हैं।
इन दिनों भारत के मध्यवर्ग से लेकर साधारण जनता तक में संतों- महंतों के पीछे भागने की प्रवृत्ति नजर आ रही है। इन संस्थाओं के बारे में साहनी ने लिखा ंमैं संस्थापित धर्मों और मत-मतान्तरों का विरोधी हूँ, और मेरा ख्याल है कि इन धर्मों के जन्मदाता भी संस्थापित धर्मों के उतने ही विरोधी थे। महापुरुषों के विशाल चिन्तन को किसी सीमित घेरे में बांधकर लोगों को पथभ्रष्ट करना प्राचीन काल से शासकवर्ग की साजिश चली आ रही है।
संस्थापित धर्मों से स्वतंत्र रहने वाले मनुष्य के विचारों में स्वतंत्रता आ जाती है।, और वह बुद्ध, ईसा, मुहम्मद और नानक जैसे धार्मिक महापुरुषों को भी प्लेटो, सुकरात, अरस्तू, शंकर, नागार्जुन, महावीर, कांट, शोपनहॉवर हीगेल आदि की तरह उच्चकोटि के चिन्तक और दार्शनिक मानने लगता है,जिन्होंने कि मानव विकास के विभिन्न पड़ावों पर मनुष्य के चिन्तन को आगे बढाया है। इसी प्रकार, वह उनके अमूल्य विचारों का पूरा लाभ उठा सकता है, जो कि मानव सभ्यता का बहुत बड़ा विरसा है।
तुरहब असगर
‘हमें थाने में नंगा कर हमारे साथ मारपीट की गई। हमें जलील किया गया। इसके जवाब में आईजी साहब ने अपने वीडियो संदेश में पुलिस पर किए गए अहसानों को गिनवाया। कितना अच्छा होता कि वह इस घटना के बाद अपनी पुलिस फ़ोर्स के साथ खड़े होते।’
‘मेरे साथ ही कोई भी यहां ड्यूटी नहीं करना चाहता। इतनी मार खाते देखकर और जिल्लत के बाद तो जनता में भी पुलिस का डर बाक़ी नहीं रहा होगा। हमारे नेतृत्व ने हमें बहुत निराश किया है।’
ये बातें उन पुलिस अधिकारियों में से एक ने कही हैं, जिन्हें जिला बहावलनगर के ‘थाना डिवीजऩ ए’ में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर हिंसा का निशाना बनाया गया।
पंजाब के शहर बहावलनगर में एक थाने पर फौजियों के धावा बोलने और वहां पुलिस अधिकारियों से मारपीट की घटना हुए एक हफ्ता होने को है। मगर इसकी गूंज अभी तक पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर सुनाई दे रही है।
नाम उजागर ना करने की शर्त पर बीबीसी से पंजाब पुलिस के कई जवानों और अधिकारियों ने बात की है।
इन अधिकारियों के अनुसार बहावलनगर घटना ने पुलिस फोर्स के मनोबल को काफी प्रभावित किया है।
ईद के दिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज़ शेयर किए गए, जिनमें वर्दी पहने सेना के अधिकारियों को थाने में पुलिस अधिकारियों को पीटते हुए देखा गया था।
इस घटना के दो दिन बाद पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ‘आईएसपीआर’, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की ओर से इस घटना की ‘पारदर्शी और संयुक्त जांच’ की बात कही गई।
कहा गया कि जांच के जरिए सच्चाई सामने लाने की कोशिश होगी ताकि कानून का उल्लंघन और अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने वालों की पहचान की जा सके। इस काम के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई।
इस मामले पर गृह मंत्री मोहसिन नक़वी ने सोमवार को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्ऱेंस के दौरान एक बार फिर कहा, ‘यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुछ लोग इस मामले को उछाल रहे हैं।’
पुलिस के मनोबल के बारे में उन्होंने कहा कि एक घटना से ‘मोराल डाउन’ नहीं होता और पुलिस के हौसले बुलंद हैं।
उन्होंने दावा किया कि भारत में बिल्कुल इसी तरह की घटना हुई थी मगर वहां प्रतिक्रिया ऐसी नहीं थी जैसी यहां देखी गई।
पुलिस का मनोबल गिरने और पुलिस अधिकारियों की दूसरी आशंकाओं के बारे में जब बीबीसी ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, ‘जेआईटी बना दी गई है लेकिन मैं दूसरे सवालों और बातों पर कोई राय नहीं देना चाहता हूं।’
‘किसकी हिम्मत है कि फ़ौज को कसूरवार कहे’
सुलह, स्पष्टीकरण और जेआईटी के गठन के बावजूद अभी तक इस मामले पर बहुत से लोग आशंका जता रहे हैं। इनमें आम लोगों के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों और जवानों की बड़ी संख्या शामिल है। कई पुलिस अधिकारियों ने यह दावा भी किया कि बहावलनगर पुलिस उस घटना के विरोध में ड्यूटी करने को तैयार नहीं थी।
नाम छिपाने की शर्त पर बीबीसी से एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘बहावलनगर घटना ने पुलिस को कमजोर किया है। इससे भी अधिक नुकसान पुलिस को आईजी साहब के वीडियो मैसेज से हुआ है। हम जानते हैं कि फौज को अपनी ताकत दिखाना अच्छा लगता है लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वह देश की दूसरी संस्थाओं का सम्मान ना करे। कानून तो सबके लिए बराबर है।’
उन्होंने कहा, ‘मैं जिस पद पर हूं, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं कैसे अपने जूनियर को उत्साह से काम करने के लिए कहूं। इसमें कोई शक नहीं कि इस घटना के बाद पुलिस में बेचैनी, ग़ुस्सा और अविश्वास की स्थिति है। इन हालात को उच्च स्तर पर नजऱअंदाज़ करने की कोशिश की जा रही है।’
एक और अधिकारी ने पुलिस के मनोबल के बारे में कहा कि ‘सब अच्छा है, हम भाई-भाई हैं’ का राग सुनाने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। ‘नारे तो लगवा दिए थे लेकिन आईजी साहब को चाहिए था कि अपनी फोर्स के लिए डटकर खड़े होते। अगर वह ऐसा करते तो सारी पुलिस फ़ोर्स उनके पीछे खड़ी होती।’
इस बारे में एक एसएचओ का कहना था, ‘हमें यह बताया गया है कि हमारी क्या हैसियत है। पिछले एक साल से यही फौज और पुलिस मिलकर काम कर रहे थे। जब पुलिस की जरूरत कम हो गई तो फौज ने कहा कि हमें याद करवा दें कि इस देश में वो जो चाहें...कर सकते हैं।’
उन्होंने यह दावा भी किया कि जो जेआईटी बनाई गई है उसकी जांच में दोषी पुलिस ही निकलेगी। ‘किसकी हिम्मत है कि कोई फौज को कसूरवार कहे, चाहे वह हमारे आईजी ही क्यों न हों।’
बीबीसी से एक बड़े अधिकारी का कहना था कि डॉक्टर उस्मान (आईजी) ने पुलिस फ़ोर्स के लिए बहुत काम किए हैं, इसलिए उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे मामले पर झुक जाएंगे।
उन्होंने कहा, ‘हमने पिछले दो वर्षों में देखा है कि पुलिस फोर्स के मनोबल में इजाफा हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पुलिस की लीडरशिप फोर्स के साथ खड़ी थी। फोर्स को जो कमांड दी गई उन्होंने वह पूरा करके दिखाया। इसके बाद भी आईजी का अपनी फोर्स के साथ खड़ा होने की बजाय उन्हें कसूरवार कहना सबके लिए निराशाजनक है।’
‘ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनमें कुछ ही सामने आती हैं’
बहावलनगर इस तरह की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इससे मिलती-जुलती घटनाएं हो चुकी हैं।
साल 2020 में रेंजर्स पर आईजी सिंध को कथित तौर पर अगवा करने का इल्जाम लगा था। उसी साल पुलिस पर मुस्लिम लीग (नवाज) की नेता मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का दबाव डालने का आरोप सामने आया था।
इस घटना के बाद आईजी समेत पुलिस के दूसरे अधिकारियों ने दस दिन छुट्टी पर जाने का आवेदन दे दिया था।
पुलिस की प्रतिक्रिया, राजनीतिक और जनता के दबाव के बाद उस समय के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने इस मामले में शामिल रेंजर्स के अधिकारियों की जांच का आदेश दिया था। उन्होंने उन अधिकारियों को जांच पूरी होने तक उनके पद से हटाने का आदेश दिया था।
इस बारे में पूर्व आईजी एहसान गऩी का कहना था कि ऐसी घटनाएं होती रहती है।
वो बोले, ‘इनमें से कुछ सामने आ जाती हैं। जब मैं आईजी था तो मुझे याद है कि इस तरह की एक घटना हमारे एएसआई और सेना के बीच हुई थी। मैं एएसआई के लिए खड़ा हो गया था। मुझ पर प्रेशर आया था लेकिन मैंने फिर भी फौज की बात न मानते हुए कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज की थी।’
क्या ऐसी घटनाओं का पुलिस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है?
पूर्व आईजी एहसान गनी ने इस मामले पर बीबीसी से कहा, ‘यह सच है कि पुलिस फोर्स का मनोबल ऐसी घटनाओं से गिरता है। मैं अलग-अलग रैंक के पुलिस अधिकारियों को एकेडमी में लेक्चर देता हूं। इस घटना के बाद उनकी ओर से भी ऐसे सवाल किए जा रहे हैं और आशंकाएं जताई जा रही हैं। इससे पता चलता है कि पुलिस पर कितना असर पड़ा है।’
उन्होंने कहा, ‘जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इससे फोर्स के आत्मविश्वास पर गलत असर पड़ता है। यही नहीं बल्कि जनता भी पुलिस को गंभीरता से नहीं लेती। इससे कानून लागू करवाने में समस्याएं आती हैं।’
‘परेशानी उस समय होती है जब कोई भी संस्था या फोर्स अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कोई काम करती है। जैसा कि बहावलनगर की घटना में हुआ। देखा जाए तो इस घटना में अगर पुलिस की गलती निकाली जा रही है तो इसी तरह जो फौज ने किया वह भी कानूनी तौर पर गलत था।’
उन्होंने कहा कि कहने को तो इस मामले पर जेआईटी बना दी गई है लेकिन सब जानते हैं कि इस देश में जेआईटी उस वक्त बनाई जाती है जब किसी मामले को दबाना हो।(bbc.com/hindi)
अणु शक्ति सिंह
गीता प्रेस इसलिए भी निन्दित है कि उसने ईश्वर को मनुष्यों का आराध्य या मित्र भर नहीं रहने दिया, उसे सबसे बड़ा डर बना दिया।
हालाँकि यह डर कुछ हद तक सभ्यता को नियंत्रित रखने में सहायक था। एक तरह से हिन्दू धर्म के लिए अनाधिकारिक रूल बुक की तरह भी काम कर रहा था, हम बड़े स्तर पर देखें तो गीता प्रेस के गुटकों और चालीसाओं में एक खास तरह का डर वर्णित किया जाता है।
आपने इस कथा का पाठ नहीं किया तो ईश्वर का दंड मिलेगा। इस भगवान की अवहेलना की तो ऐसे पाप के भागी होंगे। गरुड़ पुराण के वर्तमान रूप में औरतों और दलितों के लिए ऐसे दंड वर्णित हैं कि रूह काँप जाए।
बानगी देखिए, पति की बात नहीं सुनने वाली स्त्रियों की तुलना जोंक से की गई है। वैसे ही व्यवहार की बात भी की गई है।
इनके एक प्रमुख लेखक स्वामी रामसुख दास गृहस्थ जीवन पर अपनी निर्देशिका में लिखते हैं, ‘पति से मार खाने वाली औरतों को यह मानना चाहिए कि उनके पूर्व जन्म का पाप कट रहा है।’
आश्चर्य यह है कि गीता प्रेस पिछले कई दशकों से धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में वही लिजलिजी किताबें छाप रहा है। कल्याण पत्रिका की बात तो छोड़ ही दी जाए। विधवा विवाह से लेकर सती प्रथा उन्मूलन तक का विरोध इसने किया है। कई पीढिय़ों से बहुसंख्यक समाज में लडक़े और लड़कियाँ इसे पढक़र ही अमूमन अपना मानस तैयार कर रहे हैं।
ऐसा नहीं होता तो भक्तों का यह रेला देखने को नहीं मिलता। मैं यह मानती हूँ कि नौ साल से जो हो रहा है, गीता प्रेस ने उसकी पीठिका सौ साल पहले से तैयार कर दी थी।
हाँ, एक करोड़ लौटाने के बारे में, 2017 से 2022 के दरमियान इस प्रेस के कुल व्यापार में बाईस करोड़ का उछाल आया है। यह डॉक्यूमेंटेड यानी वाइट मनी का आंकड़ा है। हमारे देश में काले धन की लीला तो लोग जानते ही हैं।
जब इतने पैसे यूँ ही बरस रहे हों तो कोई नाखून काटकर शहीद क्यों न बने? अर्थात् थोड़े पैसे छोडक़र वाहवाही क्यों न हासिल करे?
अपूर्व गर्ग
शिवसेना का टूटना, एनसीपी का दो फाड़ होना ये बातें मुझे कोई बड़ी खबर नहीं लगतीं।
कांग्रेस के लोगों के बीजेपी में जाने को मैं ‘कांग्रेस को लगा झटका’ नहीं मानता।
आप, तृणमूल कभी भी अपना स्टैंड बदलें तो मुझे हैरत नहीं होगी।
सपा, आरजेडी में भी कभी ख़ुशी कभी गम, कभी प्यार कभी नाराजगी होती रहेगी।
इन सबके लिए रिवर्स गियर है।
इससे हमारा कोई विश्वास न टूटता है न कोई फर्क पड़ता है।
पर एक दिन एक किसान नेता जब सर्कुलर निकालते हैं कि किसान चुनाव प्रचार से दूर रहें ये बात चुभती है।
जिन लेखकों की पुस्तकें आप खरीदते हैं प्रगतिशील विचारों के चलते उनके यू-ट्यूब पर अपना पैसा फूँकते हैं जब वो घुमा फिराकर फूहड़ गायक और सांसद प्रत्याशी के पक्ष में ट्वीट करता है ‘..ने वहाँ काफी काम भी किया है’।
तो समझ आता है अंदरूनी संक्रमण कितना फैला हुआ है!!
रोज सुबह उठकर जांच लेना चाहिए जिन पौधों को पानी दे रहे वो अमरबेल तो नहीं।
अमरबेल तो अमर हो जाएगी पर समर में आप पिछड़ जायेंगे।
ये दुनिया आज विज्ञान पर कम गणित के आंकड़ों पर ज़्यादा चल रही है।
अंदरखाने बहुत से आंकड़े बनते-बिगड़ते रहते हैं और एक दिन हमें झटका लगता है कि जिन पर हमारी सारी उम्मीद रहती है वो किसी और के लिए गाने लगते हैं।
इस पार्टी के प्रवक्ता उस पार्टी के प्रवक्ता बन कर दांत निपोरते हैं तो तकलीफ नहीं होती पर संगठनों-जनसंगठनों के के नेताओं के बेईमानी दांत जब निकल आते हैं तो खुद की अक्ल दाढ़ तुड़वाने की इच्छा होती है।
बेईमानी के सफेद झक्क उजले कुर्ते पहने लोगों से नहीं कमीज के भीतर बेईमानी की बनियान पहने लोगों से डर लगता है अब...।
अशोक पांडे
एक बार एक गुरुजी थे। जाहिर है उनके बहुत सारे चेले थे। उनका एक प्रिय चेला भी था जिसे भोर से आधी रात तक गुरुजी की सेवा का जिम्मा मिला हुआ था। कभी-कभार उससे गलती हो जाती। गुरुजी क्रोधी स्वभाव के थे सो गलती होने पर कभी लात-घूंसा करते कभी चेले का दो-दो दिन तक खाना बंद। चेला अभी लडक़ा ही था सो भले दिनों की आस में बगैर शिकायत किए खटता रहता।
लोग बताते थे गुरुजी किसी जमाने में चीन गए थे। वहां रहने वाले उनके एक भक्त ने उन्हें चीनी मिट्टी से बना एक बहुत महंगा कप तोहफे में दिया था। गुरुजी सुबह-शाम की चाय उसी कप में पीते। चाय पीते हुए वे अपने चीनी भक्त की अमीरी और कप की अद्वितीयता के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहते। यह सब अनगिनत बार सुन चुकने के बाद चेले के भीतर समूची चीनी प्रजाति के प्रति ऐसी नफरत जमा हो गई कि वह सपने में कई बार उस चीनी भक्त की ठुकाई कर चुका था जिसे उसने कभी देखा तक न था।
‘हे ईश्वर! हे ईश्वर!’ उस दिन बर्तन धोते हुए चेले की तंद्रा टूटी तो उसके मुंह से बस यही निकल रहा था। उसके हाथ से फिसल कर चीनी कप चकनाचूर हो चुका था। अब गुरुजी उसकी खाल उधेड़ देंगे। उसने बगीचे की तरफ निगाह की जहाँ गुरुजी भक्तों को दोपहर का प्रवचन दे रहे थे।
बहुत देर विचार करने के बाद चेला गुरुजी के सामने जाकर खड़ा हो गया।
‘क्या बात है बेटे?’ आसपास लोग थे सो गुरुजी ने नकली लाड़ जताते हुए पूछा।
‘गुरुजी, मृत्यु क्यों आती है?’
ऐसे विषयों पर अनर्गल बोलते जाने की गुरुजी की पचास साल की प्रैक्टिस थी। आँखें बंद कीं और बोलने लगे,‘मृत्यु तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसने हर किसी के पास पहुंचना है। हर प्राणी और हर वस्तु की मृत्यु अवश्यंभावी है। हमने मृत्यु के सामना न तो भय से करना चाहिए न क्रोध से। लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो?’
‘गुरुजी ऐसा है कि मैं लम्बे समय से आपकी गद्दी के नीचे से थोड़े-थोड़े पैसे चुरा रहा था। मेरी जरूरत भर के पैसे इक_े हो गए हैं। बहुत सुन ली आपकी बकबक। जा रहा हूँ मोमो-चाऊमीन का ठेला लगाने और’ टूटे हुए कप के टुकड़े जेब से निकाल कर सामने फेंककर भागता हुआ चेला पलट कर चिल्लाया, ‘तुम्हारे इस सडिय़ल कप की भी ना वो हो गई जो सबकी होती है! क्या कहते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया!’
एलन येंटोब-नूर नानजी
बुकर पुरस्कार विजेता लेखक सलमान रुश्दी ने बीबीसी से बातचीत की है।
इस दौरान उन्होंने दो साल पहले हुए उस हमले को याद किया, जिसके बाद उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। यह हमला अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम के मंच पर चाकू से किया गया था।
हमले को याद कर रुश्दी ने कहा कि उनकी आंख ‘उबले अंडे की तरह’ उनके चेहरे पर लटक गई थी। उन्होंने कहा कि आंख का खोना उन्हें रोज परेशान करता है।
उन्होंने कहा, ‘मुझे याद है कि मैं सोच रहा था कि मैं मर रहा हूं। लेकिन संयोग से, मैं गलत था।’
रुश्दी ने कहा कि जो कुछ हुआ उसके खिलाफ लडऩे के एक तरीके के रूप में वो अपनी नई किताब, ‘नाइफ’ का उपयोग कर रहे हैं।
रुश्दी पर यह हमला अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क के एक शिक्षण संस्थान में हुआ था। वहां वे व्याख्यान देने वाले थे।
हमले और हमलावर की याद
हमले को याद करते हुए रुश्दी ने बताया कि कैसे हमलावर तेज़ी से सीढिय़ां चढ़ते हुए ऊपर आया। उन्होंने बताया कि हमले में उनकी गर्दन और पेट समेत शरीर पर चाकू से 12 जगह मारा गया। हमला 27 सेकंड तक चला।
उन्होंने कहा, ‘मैं उससे (हमलावर) लड़ नहीं सकता था। मैं उससे दूर नहीं भाग सकता था।’
उन्होंने कहा कि वे फर्श पर गिर गए, जहां उनके चारों ओर खून पसरा हुआ था।
उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें ठीक होने में छह हफ्ते लगे।
पहले ही देख लिया था हमले का सपना
76 साल के रुश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश-अमेरिकी लेखक हैं। वो आज के समय के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक हैं। उन पर हुआ यह हमला दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां बना था।
उनकी किताब ‘द सैटेनिक वर्सेज’ का प्रकाशन 1988 में हुआ था। इसके बाद उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था। उन्हें कई साल तक छिपकर रहना पड़ा था।
बीबीसी से बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने सोचा था कि एक दिन कोई दर्शकों के बीच से कूदकर बाहर आ सकता है। अगर यह बात मेरे दिमाग में नहीं आती तो यह बेतुकी होती।
उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कार्यक्रम से दो दिन पहले हमले के बारे में एक बुरा सपना आया था। इसके बाद वो उस कार्यक्रम में जाना नहीं चाहते थे।
उन्होंने कहा, ‘और फिर मैंने सोचा, यह तो एक सपना है। मुझे लगा कि वो अच्छा पैसा दे रहे हैं। सभी लोगों ने टिकट खरीद लिए हैं। मुझे वहां जाना चाहिए।’
‘रोज परेशान करता है आंख का खोना’
हमले में रुश्दी के लीवर और हाथ में चोट आई। उनके दाहिनी आंख की नसें कट गईं।
उन्होंने कहा, ‘उनकी आंख बहुत सूजी हुई लग रही थी। यह मेरे चेहरे से लटकी हुई थी, मेरे गाल पर बैठा था, मैंने उसे नरम उबले अंडे की तरह और फिर खुद को अंधा पाया।’
रुश्दी ने कहा कि ‘एक आंख खोना मुझे हर दिन परेशान करता है।’ उन्होंने कहा कि सीढिय़ों से नीचे उतरते समय या सडक़ पार करते समय, या यहां तक कि गिलास में पानी डालते समय भी उन्हें अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है।
लेकिन वह खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनके मस्तिष्क को नुकसान नहीं पहुंचा। वो कहते हैं, ‘इसका मतलब यह है कि मैं अभी भी अपने जैसा बनने में सक्षम हूं।’
जिस कार्यक्रम में रुश्दी पर चाकू से हमला हुआ था, उसके संचालक हेनरी रीज ने बीबीसी से कहा कि काश वो हमले को रोकने के लिए कुछ और कर पाते।
रीज ने कहा, ‘आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने जल्दी कार्रवाई की होती तो बहुत कुछ रोका जा सकता था।’
लेकिन रुश्दी का उन लोगों के प्रति आभार, जिन्होंने उस दिन उनकी मदद की। इसमें रीज और उनकी देखभाल करने वाले डॉक्टर भी शामिल थे। ‘नाइफ’ के शुरुआती पन्ने से ही यह बात साफ हो जाती है।
वो कहते हैं कि यह किताब सीधे तौर पर उन महिला-पुरुषों को समर्पित है, जिन्होंने मेरी जान बचाई।
क्या यह हत्या का कारण बन सकता है?
रुश्दी ने पहली बार यह बताया कि वह अपने कथित हमलावर से क्या कहना चाहेंगे।
न्यू जर्सी निवासी 26 साल के हादी मतर पर चाकू मारने का आरोप है। मतर ने खुद को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि उन्हें बिना जमानत के हिरासत में रखा जा रहा है।
जेल से ही ‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ को दिए एक इंटरव्यू में मतर ने कहा कि उन्होंने यूट्यूब पर रुश्दी के वीडियो देखे हैं। मतर ने कहा, ‘मुझे ऐसे कपटी लोग पसंद नहीं हैं।’
सलमान रुश्दी की नई किताब
रुश्दी ने अपनी नई किताब ‘नाइफ’ के प्रकाशन से पहले एलन येंटोब को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने उस चाकू हमले पर विस्तार से बात की, जिसने 2022 में उनके जीवन को करीब खत्म ही कर दिया था।
‘नाइफ’ में रुश्दी अपने हमलावर के साथ एक काल्पनिक बातचीत करते हैं। इसमें वो उनके सवालों का जवाब देते हैं।
वो पूछते हैं, ‘अमेरिका में, बहुत से लोग ईमानदार होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे मुखौटा पहनते हैं और झूठ बोलते हैं। और क्या यह उन सभी को मारने का कारण होगा?’
रुश्दी कभी मतर से नहीं मिले, लेकिन जब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी तो अदालत में उनका आमना-सामना होने की उम्मीद है।
इस मुकदमे में देरी इसलिए हुई क्योंकि प्रतिवादी के वकीलों का कहना है कि वे रुश्दी की किताब की समीक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि यह सबूत हो सकता है। अब सुनवाई शरद ऋतु में शुरू होने की उम्मीद है।
द सैटेनिक वर्सेज़ इतनी विवादास्पद किताब क्यों थी?
सलमान रुश्दी को 1981 में आई किताब ‘मिडनाइट्स चिल्ड्रन’ से प्रसिद्धि मिली। उस किताब की अकेले यूके में दस लाख से अधिक प्रतियां बिकी थीं।
उनकी चौथी किताब ‘द सैटेनिक वर्सेज’ में इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद का चित्रण और धर्म के संदर्भ में इसका चित्रण किया गया था। इसे ईशनिंदा माना गया। कई मुस्लिम-बहुल देशों में यह किताब प्रतिबंधित कर दी गई थी।
ईरान के तत्कालीन नेता अयातुल्लाह खोमैनी ने 1989 में एक फतवा जारी किया। इसमें रुश्दी की हत्या करने पर 30 लाख डॉलर का इनाम रखा गया था। उस फतवे को कभी भी रद्द नहीं किया गया।
इसके बाद रुश्दी को करीब एक दशक तक छिपकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।
रुश्दी इस्लाम को न मानने वाले मुसलमान के घर पैदा हुए थे। वे नास्तिक हैं। वे काफी लंबे समय से बोलने की आज़ादी के मुखर समर्थक रहे हैं।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह बहुत अधिक कठिन हो गया है। उन्होंने कहा, ‘यह कहते हुए मुझे खेद है कि युवाओं समेत बहुत से लोगों ने यह राय बना ली है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी अक्सर एक अच्छा विचार है।’
वो कहते हैं, ‘बेशक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा मुद्दा यह है कि आपको उस बात को बोलने की इजाजत देनी होगी, जिससे आप सहमत नहीं हैं।’
रुश्दी याद करते हुए यह बताया कि कैसे जब वो खून से लथपथ थे, तो वे कैसे अपने निजी सामान के बारे में मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता हो रही थी कि उनका राल्फ लॉरेन का सूट बर्बाद हो रहा है, उनके घर की चाबियां और क्रेडिट कार्ड उनकी जेब से गिर सकते हैं।
रुश्दी पर हमले पर उनकी पत्नी ने क्या कहा
हमले से एक साल पहले, रुश्दी ने अमेरिकी कवि और उपन्यासकार राचेल एलिजा ग्रिफिथ्स से शादी की थी। यह उनकी पांचवीं शादी है।
एलिजा ग्रिफिथ्स ने बीबीसी को बताया कि जब उन्होंने हमले के बारे में सुना तो वह चीखने लगीं। ‘यह मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था।’
उन्होंने उस वक्त रुश्दी के साथ होने का वर्णन किया, जब डॉक्टरों ने उनकी पलकें सिल दी थीं।
उन्होंने कहा, ‘मुझे उनकी आंखें बहुत पसंद हैं। उन्होंने दोनों आंखों के साथ घर छोड़ा था। और फिर हमारी दुनिया बदल गई। और अब मैं उनकी एक आंख से और भी अधिक प्यार करती हूं क्योंकि वह दुनिया को कैसे देखते हैं।’
डरावनी प्रेम कहानी
रुश्दी ने ‘नाइफ’ को एक प्रेम कहानी के रूप में डरावनी कहानी बताया।
उन्होंने कहा, ‘यहां दो ताकतें टकरा रही थीं। एक थी हिंसा, कट्टरता, कट्टरता की ताकत और दूसरी थी प्रेम की ताकत।’
उन्होंने कहा, ‘और अंत में, जैसा कि मैं समझता हूं, जो हुआ वह यह है कि प्यार की ताकत, अपमान की ताकतों से अधिक मज़बूत साबित हुई।’
रुश्दी ने कहा कि वह फिर से सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन भविष्य में वह अधिक सावधान रहेंगे। सुरक्षा का सवाल पहला सवाल होगा। जब तक मैं इसको लेकर संतुष्ट नहीं हो जाता है, मैं किसी कार्यक्रम में शामिल होने नहीं जाउंगा।
उन्होंने कहा कि वह काफी जिद्दी व्यक्ति हैं।
उन्होंने कहा, ‘मैं प्रतिबंधित या सीमित जीवन नहीं चाहता। मैं अपने तरह से जिऊंगा।’ (bbc.com/hindi)
-जेरेमी बोवेन
मैं 1991 में पहली बार इरेज चेकपॉइंट से होकर गाजा में दाखिल हुआ था। उस समय वहां एक शेड में कुछ ऊबे हुए इसराइली सैनिक थे। वे पहचान पत्रों की जांच कर रहे थे।
इसके बाद वे आने वाले लोगों की गाडिय़ों को कांटेदार तारों के बीच से बनाए गए रास्ते से होकर गाजा ले जाने देते थे।
बाद के सालों में यह एक चमचमाते टर्मिनल के तौर पर विकसित हुआ। इसमें कांक्रीट की दीवारें, सुरक्षा और लोहे के गेट लगे हुए थे। इनके अलावा दर्जनों सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे।
केवल बहुत भरोसेमंद और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को ही इरेज से होकर गाड़ी चलाने की इजाजत थी। पत्रकारों को अपना बैग साथ लेकर चलना पड़ता था।
बीते साल 7 अक्टूबर तक, जब हमास के लड़ाकों ने इरेज पर हमला किया। उन्होंने पास के सैन्य अड्डे पर हमला किया, इसराइली सैनिकों की हत्या कर दी और अन्य लोगों को बंधक बना लिया। उसके बाद से ही यह रास्ता इसराइल रक्षा बल (आईडीएफ) को छोडक़र अन्य लोगों के लिए बंद कर दिया गया है।
क्या कर रहे हैं बिन्यामिन नेतन्याहू
बीते दिनों आईडीएफ के हमले में वल्र्ड सेंट्रल किचन चैरिटी के सात कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। इसके बाद इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को शांत करने के लिए इरेज को मानवीय मदद लेकर आने वाले काफिलों के लिए फिर से खोलने का वादा किया।
यह इसलिए मायने रखता है, क्योंकि यह उत्तरी गज़़ा में रह रहे तीन लाख फिलस्तीनियों के लिए मदद हासिल करने का यह सबसे आसान रास्ता है।
खाद्य पदार्थों की कमी जैसी आपातस्थिति से निपटने वाली संस्था का नाम आईपीसी है। आईपीसी ने चेतावनी दी है कि इस इलाके में अगले चार हफ्ते या उसके बाद अकाल पड़ सकता है।
गज़़ा में जो बाइडन के मानवतावादी दूत डेविड सैटरफील्ड ने बुधवार को कहा, ‘गाजा की 22 लाख की आबादी में यदि पूरी के लिए नहीं तो बहुसंख्यक आबादी के लिए अकाल का खतरा हो सकता है।’
यह अकाल सात अक्टूबर के हमलों के ठीक बाद इसराइल की ओर से की गई घेराबंदी के कारण हुआ है। उस समय इसराइली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था, ‘मैंने गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है, वहां न बिजली होगी, न भोजन, न ईंधन, सब कुछ बंद है।’
उन्होंने कहा था, ‘हम इंसानी जानवरों से लड़ रहे हैं, और हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं।’
गाजा में भुखमरी के हालात
अंतरराष्ट्रीय दबाव में इसराइल को मानवीय मदद की सीमित सप्लाई की इजाजत देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन छह महीनों में यह पर्याप्त नहीं रहा।
इसराइल ने गलत तरीके से यह तर्क दिया कि गज़़ा में भुखमरी का संकट हमास की चोरी, सहायता सामग्री की जमाखोरी और जो कुछ वहां बचा था उसे बांटने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता की वजह से आया।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू के करीबी समर्थक लगातार अकाल से इनकार कर रहे हैं। नेतन्याहू के समर्थकों में से एक सांसद बोअज बिस्मथ ने मुझे इसराइल की संसद में बताया कि गज़़ा में कोई अकाल नहीं था।
उन्होंने इसराइल पर नागरिकों को भूख से मारने के आरोपों को यहूदी विरोधी भावना पर आधारित बताया। हालांकि अकाल के प्रमाण बहुत हैं।
जो बाइडन से किए प्रधानमंत्री के वादे के बाद इरेज क्रॉसिंग अभी भी बंद है। मैं इरेज टर्मिनल को देखने के लिए उसके काफी करीब पहुंचने में कामयाब रहा। वहां कुछ भी हिल-डुल नहीं रहा था।
ट्रकों की तो बात ही छोडि़ए, मुझे वहां लोग भी नजर नहीं आए। इसराइल से आने वाली खबरों में कहा गया है कि सरकार एक और क्रॉसिंग खोलने की बात कर रही है। इस क्रॉसिंग तक वे इसराइली प्रदर्शनकारी आसानी से पहुंच सकते हैं, जो गज़़ा में किसी तरह का भोजन या चिकित्सा सहायता नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। वे कुछ काफिलों को रोक रहे हैं, जबकि इसराइली बंधक अभी भी वहां हैं।
संयुक्त राष्ट्र और सहायता उपलब्ध कराने वाली अन्य संस्थाओं का कहना है कि गाजा में मानवीय आपदा में फंसे लोगों की मदद के लिए हर दिन महत्वपूर्ण है। तथ्य यह है कि इरेज़ एक रणनीति के तहत बंद है। यहूदी अतिराष्ट्रवादी नेतन्याहू को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं, वो गाजा में मदद पहुंचाने के पक्ष में नहीं हैं।
यह संघर्ष गाजा, पूर्वी यरूशलम और वेस्ट बैंक में जमीन पर इसराइल के कब्जे के कारण सालों से जारी है, इसे फलस्तीनी एक देश के रूप में चाहते हैं।
मैंने पिछले छह महीनों में कई फलस्तीनी और इसराइली नागरिकों से युद्ध के बारे में उनके विचारों पर चर्चा की है। इसराइली सैनिकों से बात करना कठिन है, कम से कम जब वे वर्दी में हों।
आईडीएफ के प्रवक्ता पत्रकारों तक पहुंचने वाले मैसेजों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसराइल की सेना का अधिकांश हिस्सा रिजर्व सैनिकों का है, इसलिए जब वे नागरिक जीवन में वापस लौटते हैं तो उनसे बात करना बहुत आसान होता है।
छह महीने के युद्ध के बाद इसराइली सैनिकों की मान्यताओं और धारणाओं को समझने के लिए मैं दक्षिणी इसराइल के बेर्शेबा शहर में स्थित नेगेव के बेन गुरियन विश्वविद्यालय गया। यह गज़़ा से केवल 25 मील की दूरी पर स्थित है।
इसराइल-गाजा युद्ध पर क्या सोचते हैं युवा
चेम हेम्स इस विश्वविद्यालय के रेक्टर (प्रमुख) हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके समुदाय के 100 से अधिक सदस्य- छात्र, कर्मचारी, शिक्षक और उनके परिवार 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए या बंधक बना लिए गए।
वो कहते हैं, ‘अस्पताल सडक़ के उस पार है, हेलीकॉप्टर लगातार गाजा से घायलों को ला रहे हैं। छात्र कक्षाओं में बैठे हैं। वे हेलीकॉप्टरों के अंदर और बाहर आने की आवाज सुनते हैं। उनमें से कई के दोस्त हैं जो अभी भी ड्यूटी पर हैं। इसका असर हर चीज पर पड़ता है।’
मैंने तीन युवाओं से बात की जिन्होंने गाजा में युद्ध के दौरान कई महीने बिताए थे। वे अपना पूरा नाम नहीं बताना चाहते थे। उनमें से एक, 28 साल के बेन सुरंगों को उड़ाने वाली एक इंजीनियरिंग इकाई में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वे वहां थे, यह उन्हें व्यक्तिगत लगा।
वो कहते हैं, ‘मुझे 7 अक्टूबर याद है। मुझे गज़़ा पट्टी के मेरे सभी दोस्त और किबुत्जिम याद हैं। संगीत समारोह के मेरे सभी दोस्त। उनसे कुछ अभी भी बंधक हैं। पूरा मुद्दा यह सुनिश्चित करना था कि यह फिर दोबारा न होने देना और हमास को वहां सरकार चलाने से हटाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे लोग फिर से सुरक्षित हैं।’
‘यह बहुत व्यक्तिगत है। पहले दिन से ही। एक शनिवार की सुबह मैं नहीं उठा और न्यूज से इस बारे में सुना। मैं उठा और ग्रुप चैट से इस बारे में जानकारी ली। अपने फोन से और मदद की भीख मांग रहे लोगों से।’
क्यों जरूरी थी लड़ाई
28 साल के ओडेड, एक लड़ाकू यूनिट में कार्यरत हैं, वो बात करने के लिए सहमत हुए।
वो कहते हैं, ‘मुझे लगता है कि यहां हर कोई किसी न किसी तरह से उस घटना से संबंधित है। हर कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसका अपहरण कर लिया गया था।’
पैराट्रूप ब्रिगेड की टोही इकाई में काम करने वाले 25 साल के इलान ने उन लोगों में हमास के प्रति सहानुभूति और समर्थन पाया, जिनके साथ वो संपर्क में आए थे।
वो कहते हैं, ‘निश्चित तौर, वहां ऐसे नागरिक भी हैं जिनका इससे कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन उनमें से कई इतने मासूम नहीं हैं। कई लोगों के पास एके 47 पकड़े हुए उनकी तस्वीरें थीं, उनके बच्चों की हथियार पकड़े हुए तस्वीरें थीं। इसराइल की सभी किताबें और तस्वीरें आग में थीं।’
वो कहते हैं, ‘मुझे लगता है कि उनमें से कई मासूम नहीं हैं। उन्हें लगता है कि जो निर्दोष हैं, उन्हें ढूंढना वाकई मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए।’
फिलीस्तीन की मांग को नकारते लोग
तीनों सैनिक छात्र इस, बात पर सहमत थे कि युद्ध जरूरी था। ओडेड ने कहा, ‘हम सभी शांति की कामना करते हैं।’
वो कहते हैं, ‘शांति के लिए, निश्चित तौर पर मैं युद्ध में लड़ाई लडऩे की बजाय यहां अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने और अपनी कॉफी पीने के लिए रहना पसंद करुंगा। लड़ाई लडऩे में मजा नहीं है, लेकिन कभी-कभी यह जरूरी है। और इस स्थिति में यह जरूरी है।’
सात अक्टूबर के हमलों के तीन हफ्ते बाद तेल अवीव विश्वविद्यालय के पीस इंडेक्स ने एक सर्वेक्षण कराया था। इसके मुताबिक अधिकांश इसराइलियों ने कहा कि वे अब उस विचार के खिलाफ हैं, जिसे जो बाइडन और पश्चिमी देशों के अन्य नेताओं द्वारा पुनर्जीवित किया है।
वह यह कि इस लंबे विवाद को खत्म करने का एकमात्र तरीका इसराइल के साथ एक फलस्तीन देश की स्थापना है। बेन ने कहा कि युद्ध की वजह से उनकी धारणा बदल गई है।
वो कहते हैं, ‘मुझे लगता है कि अगर आपने 6 अक्टूबर को मुझसे यह सवाल पूछा होता, तो मैं निश्चित तौर पर हां कहता, मैं एक फिलीस्तीनी देश का समर्थन करता। उन्हें वहां रहने दें और हम यहां रहेंगे। हम सब मिल-जुलकर रहेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद, मुझे यह साफ-साफ लगता है कि वे ऐसा उतना नहीं चाहते है, जितना मैं चाहता था।’
इलान भी बेन से सहमति जताते हैं।
युद्ध को लेकर फलस्तीन का नजरिया बिल्कुल अलग है। फिलीस्तीनी मानते हैं कि इसराइल गज़़ा में अन्य युद्ध अपराधों के साथ जनसंहार कर रहा है। जहां तक ??शिक्षा की बात है, इसराइल ने गाजा में स्कूलों और विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया है। इससे भारी नुकसान हुआ है।
उत्तरी अमेरिका के विश्वविद्यालयों से संबद्ध 2,000 से अधिक शिक्षाविदों ने एक ओपन लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने गाजा में जो हो रहा है, उसे ‘शैक्षिक हत्या’ बताया है। इन शिक्षाविदों ने इसकी निंदा की है। गाजा के सभी 12 विश्वविद्यालय तबाह और क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
इस पत्र में अन्य कार्रवाइयों के अलावा, 11 अक्टूबर को हवाई हमला कर इस्लामिक विश्वविद्यालय को नष्ट करने और 17 जनवरी को अल इसराइल विश्वविद्यालय को बैरक और लोगों को हिरासत में रखने का केंद्र के रूप में उपयोग कर उड़ा देने की निंदा की गई है। उच्च शिक्षा के नष्ट होने के साथ-साथ कोई भी बच्चा प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूलों में नहीं जा रहा है।
काहिरा में अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में युद्धविराम वार्ता चल रही है। इसके सफलता की संभावना कम हैं। इसराइल और हमास दोनों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।
दोनों पीछे नहीं हटना चाहते हैं। यह सभी के लिए बुरी खबर है, खासकर गाजा में फिलीस्तीनी नागरिकों और जीवित बचे इसराइली बंधकों के लिए। (bbc.com/hindi)
(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूजरूम की ओर से प्रकाशित)
-तुषार कुलकर्णी
किसी का पक्ष लेना और उसे ठीक से प्रस्तुत करना आम बोलचाल की भाषा में 'किसी की वकालत करना' कहलाता है. भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर एक जाने माने वकील भी थे. उन्होंने न केवल अपने मुवक्किलों के लिए वकालत की बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों की भी वकालत की. इसलिए, उनकी गिनती आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में होती है.
डॉ. आंबेडकर ने एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर क़ानून की पढ़ाई की. उन्होंने जीवनभर उसी लक्ष्य के साथ काम किया.
उन्होंने वकालत का पेशा पेशेवर उत्कृष्टता या उन्नति के लिए नहीं बल्कि उस दौर में भारत के लगभग छह करोड़ अछूतों और दबे-कुचले दलितों को न्याय दिलाने के लिए चुना था.
14 अप्रैल की उनकी जन्मतिथि के मौके पर हम आपको बताते हैं कि वे वकील कैसे बने और उन्होंने अपने मुवक्किलों के लिए कौन से प्रमुख मामले में पैरवी की और उन मामलों का नतीजा क्या रहा.
बाबा साहेब की शिक्षा
1913 में बाबा साहेब बॉम्बे के एलफिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए थे. इसके लिए उन्हें बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने आर्थिक मदद मिली थी.
यह आर्थिक मदद के बदले में उन्हें बड़ौदा के राजपरिवार के साथ एक अनुबंध करना पड़ा था कि अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बड़ौदा सरकार के अधीन नौकरी करनी थी.
साल 1913 में वे अमेरिका पहुंचे. अमेरिका में उनका परिचय दुनिया भर के विभिन्न विचारकों और उनकी विचारधाराओं से हुआ. उससे उनके सामने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया था. अमेरिका में पढ़ाई के दौरान कई जगहों पर इस बात का ज़िक्र मिलता है कि वे 18-18 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे.
इस अवधि के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, एथिक्स और मानवविज्ञान का अध्ययन किया. 1915 में 'भारत का प्राचीन व्यापार' विषय पर थीसिस प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की. 1916 में उन्होंने 'भारत का राष्ट्रीय लाभांश' थीसिस प्रस्तुत की.
डॉ. आंबेडकर जितना पढ़ रहे थे, उतना ही उनके पढ़ने और जानने की भूख बढ़ रही थी. उन्होंने बड़ौदा के महाराज सायाजीराव गायकवाड़ से आगे की पढ़ाई करने की अनुमति मांगी. उन्हें वह अनुमति मिल भी गई.
इसके बाद वो अर्थशास्त्र और क़ानून की उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लंदन पहुंचे. उन्होंने अर्थशास्त्र में शिक्षा के लिए लंदन स्कूल ऑफ़ इकॉनामिक्स में दाख़िला लिया, जबकि क़ानून की पढ़ाई के लिए ग्रेज़ इन में नामांकन लिया.
1917 में, बड़ौदा सरकार की छात्रवृत्ति समाप्त हो गई और अफ़सोस के साथ उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी. इस बीच उनके परिवार को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. इस स्थिति को देखते हुए ही आंबेडकर ने भारत लौटने का फ़ैसला लिया था.
अनुबंध के मुताबिक उन्होंने बड़ौदा सरकार के लिए काम करना शुरू कर दिया. वहां उन्हें अन्य कर्मचारियों से अत्यधिक जातिगत भेदभाव सहना पड़ता था. यहां तक कि बड़ौदा में रहने के लिए जगह ढूंढने में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. फिर उन्होंने बंबई वापस लौटने का फ़ैसला किया.
बड़ौदा सरकार के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में आंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ''मेरे पिता ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस जगह काम मत करना. शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि वहां मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा.''
दलितों के उत्थान के लिए काम
वर्ष 1917 के अंत में आंबेडकर बंबई पहुंचे. वहां उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज में प्रोफ़ेसर पद के लिए आवेदन किया. कहने की ज़रूरत नहीं है कि वे वहां जल्दी ही लोकप्रिय प्रोफ़ेसर हो गए. वे हमेशा बड़ी तैयारी के साथ पढ़ाने के लिए जाते थे. उनकी तैयारी ऐसी होती थी कक्षा से बाहर के छात्र भी उनके लेक्चर सुनने के लिए आते थे.
1919 में उन्होंने अछूत समाज की मुश्किलों को साउथबरो कमीशन के सामने प्रस्तुत किया. इस मौके पर उनकी प्रतिभा की झलक सबको दिखी थी. 1920 में उन्होंने अछूतों की दुर्दशा को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से 'मूकनायक' समाचार पत्र की शुरुआत की और आधिकारिक तौर पर एक तरह से अछूतों की वकालत शुरू की.
लेकिन चूंकि सिडेनहैम कॉलेज की नौकरी सरकारी थी, इसलिए उन पर कई तरह की पाबंदियां भी थीं. इसके चलते ही उन्होंने 1920 में प्रोफ़ेसर पद से त्यागपत्र दे दिया और सीधे दलित मुक्ति के संघर्ष में कूद पड़े.
इसी साल यानी 1920 में मानगांव में जाति बहिष्कृत वर्गों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था. इसमें हिंसा भड़क गई थी. छत्रपति शाहूजी महाराज ने कहा था कि बाबा साहेब शोषितों और वंचितों के नेता होंगे और यह बाद में सच साबित हुआ.
क़ानून की पढ़ाई के लिए जब दोबारा लंदन पहुंचे
लंदन में आंबेडकर हाउस का बाहरी नज़ारा
डॉ. आंबेडकर को अब तक यह एहसास हो गया था कि दलितों से जुड़े मुद्दे बेहद जटिल हैं, इसलिए उस पर काम करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वकालत करनी होगी और विधायिका में भी उन मुद्दों को ठीक से उठाना होगा. यही सोच कर वे क़ानून की डिग्री हासिल करने दोबारा लंदन पहुंचे.
सितंबर, 1920 में लंदन पहुंचने से पहले ही वे भारत में दलित नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे. यानी उन्हें अपनी चुनौती और भूमिका दोनों का एहसास था. इसलिए लंदन में रहने के दौरान उनका झुकाव कभी ड्रामा, ओपेरा, थिएटर जैसी चीज़ों के प्रति नहीं हुआ. वे अपना अधिकतम समय पुस्तकालय में बिताते थे.
क़िफायत से रहने के लिए लंदन में वे हमेशा पैदल चलते थे. खाने पर पैसे ख़र्च ना हों, ये सोच कर वे कई बार भूखे रह जाते थे. लेकिन पढ़ाई पर उनका पूरा ध्यान लगा रहता.
लंदन में बाबा साहेब आंबेडकर के रूममेट होते थे असनाडेकर. वे आंबेडकर से कहते, ''अरे आंबेडकर, रात बहुत हो गई है. कितनी देर तक पढ़ते रहोगे, कब तक जगे रहोगे? अब आराम करो. सो जाओ."
लेफ्टिनेंट धनंजय कीर की लिखी डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर की जीवनी में इसका ज़िक्र मिलता है. आंबडेकर अपने रूममेट को जवाब देते, ''अरे, मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए समय नहीं है. मुझे अपना कोर्स जल्द से जल्द पूरा करना है. कोई दूसरा रास्ता नहीं है.''
इससे यह पता चलता है कि डॉ. आंबेडकर अपने लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे.
1922 में क़ानून के सभी पाठ्यक्रम पूरे करने के बाद, उन्हें ग्रेज़ इन में ही बार का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया और आंबेडकर बैरिस्टर बन गये. यहां यह बताना आवश्यक है कि बाबा साहेब ने एक ही समय में दो पाठ्यक्रम पूरे किए थे.
ग्रेज़ इन में कानून की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) में उच्च अर्थशास्त्र की डिग्री भी हासिल की. 1923 में लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स ने उनकी थीसिस को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टर ऑफ़ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया. एक ही वर्ष में वे डॉक्टर और बैरिस्टर बन गए थे.
भारत में वकालत की शुरुआत

दिल्ली में बाबा साहेब के आवास 26, अलीपुर रोड पर अब एक स्मारक बनाया गया है. इमेज स्रोत, NAMDEV KATKAR
हमारे देश में ऐसे कितने वकील हैं जिनके वकील बनने की सालगिरह मनाई जाती है.
आपको यह जानकर अचरज हो सकता है कि बीते साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. आंबेडकर के वकील बनने की सौवीं वर्षगांठ मनाई थी.
यह डॉ. आंबेडकर के काम के प्रति श्रद्धांजलि थी हालांकि सौ साल पहले इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें खासा संघर्ष करना पड़ा था.
मुंबई के बार काउंसिल की सदस्यता लेने के लिए आवेदन करने तक के पैसे उनके पास नहीं थे. ऐसे में उनके मित्र नवल भथेना ने उन्हें 500 रुपये दिए थे, तब उन्होंने बार काउंसिल की सदस्यता के लिए आवेदन किया था. चार जुलाई, 1923 को उन्हें सदस्यता मिली और पांच जुलाई से उन्होंने वकालत शुरू कर दी.
वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने डॉ. आंबेडकर को ढाई हज़ार रुपये महीने की पगार पर ज़िला न्यायाधीश की नौकरी का प्रस्ताव दिया था. जो बेहद आकर्षक था लेकिन उन्होंने वकालत का पेशा ही चुना.
इसके बारे में उन्होंने बहिष्कृत भारत के अपने लेख और अपने भाषणों में इसका ज़िक्र किया है. उनके मुताबिक वे दलितों के हितों के लिए काम करना चाहते थे. उन्होंने इस बारे में स्पष्टता से लिखा है, "मैंने ज़िला न्यायाधीश सहित कोई सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की, क्योंकि स्वतंत्र रूप से वकालत करने में आज़ादी हासिल थी."
यहां ये भी देखना होगा कि हैदराबाद के निज़ाम ने उन्हें राज्य के मुख्य न्यायाधीश के पद की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया.
उस दौर में वकालत का पेशा मुख्य तौर पर ऊंची और वर्चस्व रखने वाले जातियों पर आधारित है, क्योंकि उनके मामले मुख्य तौर पर उन्हीं से आते हैं. उन्हें इस बात का अंदाज़ा था लेकिन फिर भी उन्होंने वकालत करने का जोख़िम उठाया.
डॉ. आंबेडकर के वकालत के शुरुआती दिनों के बारे में धनंजय कीर लिखते हैं, "उस दौर में आपकी त्वचा का रंग, आपकी बुद्धि से ज़्यादा चमकता था. छुआछूत का कलंक, समाज में दबी कुचली स्थिति, पेशे का नया होना और आसपास के असहयोगी माहौल ने उनकी वकालत को मुश्किल चुनौती में डाल दिया था. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. इस मुश्किल परिस्थितियों में वे भी निचली और ज़िला अदालतों में काम करते रहे."
डॉ. आंबेडकर के मुवक्किलों की स्थिति बेहद खस्ताहाल हुआ करती थे. वे ग़रीब, खेतिहर या दिहाड़ी मज़दूर हुआ करते थे. आंबेडकर इन लोगों के मामले को गंभीरता से सुनते और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करते थे.
वे इन लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक या फिर धार्मिकता के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे. उन्होंने सेक्स वर्करों को भी क़ानूनी सहायता दिलाने के लिए अपने दरवाज़े खोल रखे थे. वे किसी के साथ किसी भी तरह का पूर्वाग्रह का भाव नहीं रखते थे.
अगर आप किसी वकील के बारे में सोचते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति की छवि घूम जाती है. लेकिन बाबा साहेब एक अनुशासित और प्रखर विद्वान होते हुए भी अपने मुवक्किलों के साथ बहुत सहजता से व्यवहार करते थे. वे कई बार अपने मुवक्किलों के साथ अपना खाना तक साझा करते थे.
धनंजय कीर ने डॉ. आंबेडकर की जीवनी में लिखा है, "जैसे ही डॉ. आंबेडकर एक वकील के रूप में प्रसिद्ध हो गए, ग़रीब लोग क़ानूनी मदद की आस में उनके पास आने लगे. दलितों की पीड़ा और दुख देखकर उनका दिल व्यथित होता था. वे ग़रीबों का केस मुफ़्त में लड़ते थे."
"उस समय डॉ. आंबेडकर का घर गरीबों के लिए आशा का केंद्र बन गया था. एक दिन उनकी पत्नी रमाबाई जब घर में नहीं थीं तो दो मुवक्किल आए. आंबेडकर ने ना केवल उन्हें दिन का खाना खिलाया बल्कि रात में खुद अपने हाथों से बनाकर उन्हें खाना परोसा. वे खाना पकाने की कला में भी पारंगत थे."
वकील के रूप में कितने प्रभावी थे आंबेडकर

डॉक्टर बीआर आंबेडकर. इमेज स्रोत, NAVAYANA PUBLISHING HOUSE
समाज में दलित समुदाय की स्थिति कैसी है, इस बारे में ब्रिटिश सरकार के सामने पक्ष रखने के लिए 1928 में साइमन कमीशन के सामने गवाही देने के लिए डॉ. आंबेडकर को चुना गया था.
जिस दिन उन्हें ये गवाही देनी थी, ठीक उसी दिन उन्हें एक महत्वपूर्ण मामले में ठाणे के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपने मुवक्किल का पक्ष रखना था. अगर डॉ. आंबेडकर उस मुक़दमे में उपस्थित नहीं होते तो शायद उनके कुछ मुवक्किलों को फांसी की सज़ा मिलती. इससे ग़रीब और उपेक्षितों के बीच ये संदेश जाता कि आंबेडकर वक्त पर काम नहीं आए और इसका मलाल उन्हें जीवन भर रहता.
दूसरी ओर डॉ. आंबेडकर इस दुविधा में थे कि अगर साइमन आयोग के सामने गवाही देने के लिए नहीं गए तो देश के करोड़ों लोगों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखने का मौका हाथ से निकल जाएगा.
ऐसे में उन्होंने न्यायाधीश से अनुरोध किया कि अभियुक्तों के बचाव को अभियोजन पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए.
अमूमन होता यह है कि अभियोजन पक्ष का भाषण पहले होता है, लेकिन डॉ. आंबेडकर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना पक्ष पहले रखने की अनुमति दी गई.
डॉ. आंबेडकर की जीवनी में धनंजय कीर ने लिखा है, "बचाव के लिए दिए गए तर्कों की सटीकता और उनका आत्मविश्वास इतना मज़बूत था कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन मामलों में अधिकांश अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था."
हालांकि जब न्यायाधीश ये फ़ैसला सुना रहे थे तब डॉ. आंबेडकर साइमन कमीशन के सामने देश के दलितों की स्थिति पर अपना पक्ष रख रहे थे.
डॉ. आंबेडकर के प्रमुख मुक़दमे
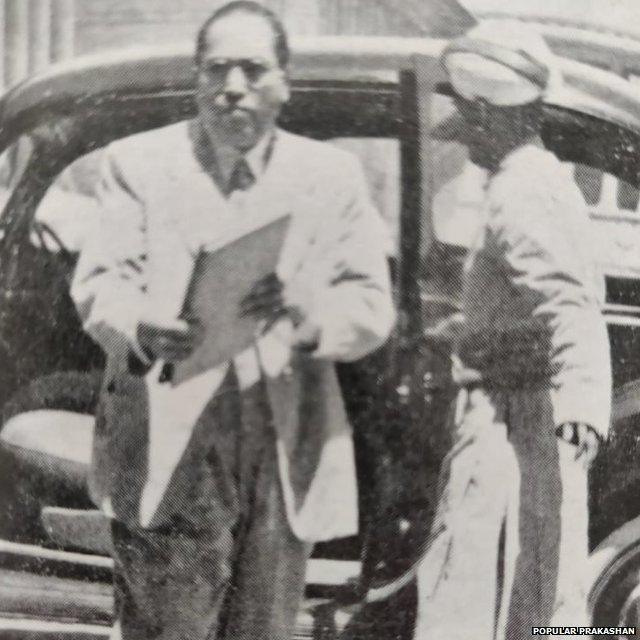
इमेज स्रोत, POPULAR PRAKASHAN
अब एक नज़र डॉ. आंबेडकर के चर्चित मुक़दमों पर...
आरडी कर्वे और समाज स्वास्थ्य पत्रिका का मुक़दमा
डॉ. आरडी कर्वे उस समय के नामचीन समाज सुधारक थे. वह महिलाओं के स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे.
आज़ादी से पहले भारत में यौन शिक्षा के बारे में बात करना लगभग असंभव था. कई जगहों पर उनकी सार्वजनिक तौर पर आलोचना होती थी.
डॉ. कर्वे को रूढ़िवादी समाज के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था. उन पर एक मुक़दमा दर्ज हुआ कि अपनी मासिक पत्रिका 'समाज स्वास्थ्य' के ज़रिए वे समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं.
डॉ. आंबेडकर ने उनकी तरफ़ से मामला लड़ना स्वीकार किया. ये 1934 की बात है. आंबेडकर ने इसके ज़रिए यह संदेश दिया कि कोई समाज सुधारक अपने काम के कारण अकेला है, तो वे उसके साथ हैं.
समाज स्वास्थ्य पत्रिका में यौन शिक्षा पर लेख प्रकाशित हुआ करते थे.
अदालत ने उनसे पूछा कि पत्रिका में दी गई जानकारी अश्लील और तोड़ मरोड़कर पेश की गई थी, इस पर उनकी क्या राय है?
तब डॉ. आंबेडकर ने कहा था, ''अगर कोई यौन समस्याओं के बारे में लिखता है तो उसे अश्लील नहीं माना जाना चाहिए.''
उन्होंने अपनी दलील देते हुए यह भी कहा था, ''अगर लोग अपने मन के सवाल पूछते हैं और इसे विकृति मानते हैं तो केवल ज्ञान ही विकृति को दूर कर सकता है. यदि नहीं तो यह कैसे दूर होगा? इसलिए उन सवालों के जवाब डॉ. कर्वे को देना चाहिए.''
हालांकि डॉ. आंबेडकर यह मामला हार गए थे. लेकिन कहा जाता है कि उनकी प्रगतिशील सोच और मदद के चलते कर्वे आख़िर में ये मामला जीतने में कामयाब हुए थे.
'देश के दुश्मन' का चर्चित मामला

इमेज स्रोत, DHANANJAY KEER
'देश के दुश्मन' केस में बाबा साहेब की भूमिका को समझने से पहले 1926 में सामने आए इस मामले को समझते हैं. दिनकर राव जावलकर और केशव राव जेधे गैर-ब्राह्मण आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे. उस समय ब्राह्मण समुदाय के लोग सामाजिक सुधारों का विरोध कर रहे थे. इस प्रबल विरोध के कारण रुढ़िवादियों ने महात्मा फुले की आलोचना भी की थी.
महात्मा फुले को क्राइस्टसेवक भी कहा जाता था. इन बातों के विरोध में दिनकर राव जावलकर ने 'देश के दुश्मन' नामक पुस्तक लिखी और केशवराव जेधे ने इसका प्रकाशन किया.
इस पुस्तक में लोकमान्य तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर को देश का दुश्मन बताया गया. उन्हें और भी कई विशेषण दिए गए. जिससे तिलक के समर्थक नाराज़ हो गए और उन लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया. मुकदमा पुणे में चला और निचली अदालत ने जेधे-जावलकर को सज़ा सुनाई.
जावलकर को एक साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि जेधे को छह महीने जेल की सज़ा सुनाई गई. इस सज़ा को चुनौती दी गई और आंबेडकर इस मामले में वकील बने. जब डॉ. आंबेडकर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वे 'देश के दुश्मन' पुस्तक पढ़ चुके हैं.
इस मामले को पुणे सेशन कोर्ट में जज लॉरेंस की अदालत में सुना गया. आंबेडकर ने एक पुराने मानहानि केस का हवाला देकर यह केस लड़ा.
उन्होंने जज फ्लेमिंग के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी मामला समान था, क्योंकि शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति, मानहानि का दावा करने वाले शख़्स का दूर का रिश्तेदार है, इसलिए इस मामले में भी सज़ा नहीं हो सकती है. क्योंकि ये शिकायत ही दर्ज नहीं हो सकती थी.
पहले के मामले का गहन अध्ययन करने के बाद डॉ. आंबेडकर ने अदालत के सामने अचूक दलीलें पेश की और दोनों की सज़ा माफ़ी हो गई.
महाड़ सत्याग्रह का मामला
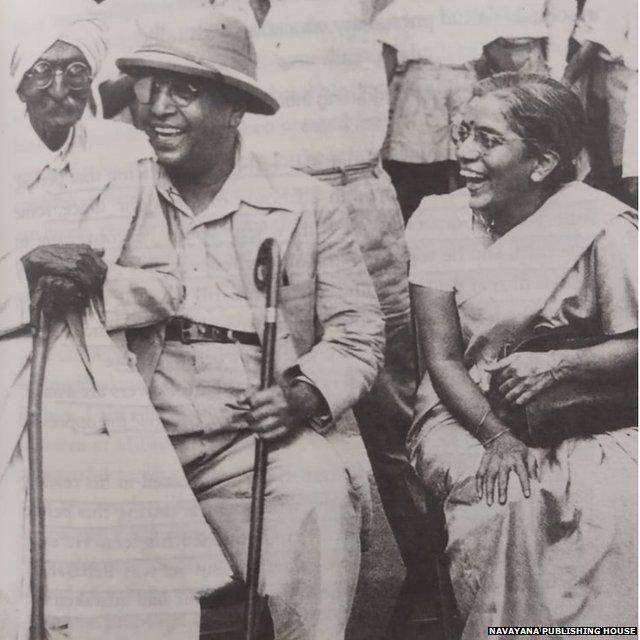
इमेज स्रोत, NAVAYANA PUBLISHING HOUSE
सदियों तक अछूतों को सार्वजनिक जलस्रोतों से पानी पीने का अधिकार नहीं था. वहां मवेशी पानी पी सकते थे लेकिन अछूतों को पानी लेने की मनाही थी.
इस अन्याय के विरुद्ध डॉ. आंबेडकर ने एकअभियान चलाया और इसके कारण ही महाड़ सत्याग्रह हुआ. यह महाड़ झील के पानी पर नियंत्रण की संदेशात्मक लड़ाई थी.
महाड़ सत्याग्रह में एक तरह से हिंदुओं और अछूतों के बीच सीधा संघर्ष था. हिंदुओं की ओर से कुछ असामाजिक तत्वों ने अछूत समुदाय के लोगों पर भी हमला किया ताकि वे लोग महाड़ झील पर न आएं और पानी को न छूएं. हिंदुओं की तरफ़ से डॉ. आंबेडकर और उनके साथियों पर कई मुक़दमे दर्ज किए गए.
इस मामले में आंबेडकर को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा. पहले कहा कि यह झील पूरी तरह से हिंदुओं की है. यह कोई सार्वजनिक ज़मीन पर नहीं बना है. यह भी कहा गया कि इससे दूसरे समुदाय के लोग भी पानी लेते हैं, किसी को रोका नहीं गया है.
तब डॉ. आंबेडकर ने अदालत को बताया कि यह झील महाड़ नगर निगम की ज़मीन पर बनी हुई है. यहां से केवल सवर्ण हिंदुओं को पानी लेने की अनुमति है. जानवरों को काटने वाले खटीक मुस्लिमों को भी यहां से पानी नहीं लेने दिया जाता है.
वकील के तौर पर आंबेडकर ने जानबूझ कर खटीक मुस्लिमों का ज़िक्र किया था, क्योंकि हिंदू यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि खटीक को यहां से पानी मिलता है, नहीं तो सवर्णों के बीच झील की शुद्धता का मुद्दा उठता.
तब इसकी सत्यता का पता चला कि यह झील 250 सालों से है और यहां से केवल सवर्ण हिंदुओं को ही पानी मिलता है. आंबेडकर ने अदालत में यह भी साबित किया कि झील नगर निगम की ज़मीन पर है, इसलिए इसे सभी के लिए खोला जाए.
हाईकोर्ट ने आंबेडकर की दलील को स्वीकार करते हुए इसे सभी के लिए खोलने का निर्देश दिया.
अदालत ने माना कि यह आंदोलन किसी एक झील या जल निकाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी सार्वजनिक जल निकायों पर भी लागू होगा और किसी की जाति और सामाजिक स्थिति को देखकर उसे पानी लेने से मना नहीं किया जा सकता. इससे ज़ाहिर तौर पर इस मामले के सामाजिक और क़ानूनी व्यापकता का पता चलता है.
डॉ. आंबेडकर के अनुसार एक अच्छे वकील में क्या गुण होने चाहिए?
डॉ. आंबेडकर ने 1923 से 1952 तक अपने लंबे करियर के दौरान कई मुक़दमे लड़े लेकिन अब बहुत कम मुक़दमों के दस्तावेज़ उपलब्ध हैं.
विजय गायकवाड़ ने उनके क़ानूनी मामलों और उसमें हुए निर्णयों को लेकर 'केसेज़ आर्ग्यूड बाय डॉ. आंबेडकर' नामक पुस्तक संपादित की है.
डॉ. आंबेडकर की वकालत को समझने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ माना जा सकता है.
डॉ. आंबेडकर एक अच्छे वकील से क्या अपेक्षा रखते थे, इसका विवरण गायकवाड़ ने अपनी पुस्तक में दिया है. 1936 में आंबेडकर के लिखे गए एक लेख के मुताबिक उनके हिसाब से अच्छा वकील वह होता है, जिसे
क़ानून के मौलिक सिद्धांतों की समझ हो
सामान्य ज्ञान की आधारभूत जानकारी हो
किसी विषय को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की कला आती हो
संवाद और तर्कों में सत्यता हो
स्पष्ट भाषा में अभिव्यक्त करने की क्षमता हो
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में हाज़िरजवाबी हो
डॉ. आंबेडकर के मुताबिक एक अच्छे वकील में सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए.
वकालत के चलते ही डॉ. आंबेडकर को पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने का मौका मिला था. उन्होंने लोगों के दुख को करीब से देखा था, इसलिए जब वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के प्रमुख बने तो उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिला.
1936 में डॉ. आंबेडकर ने तत्कालीन बंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में व्याख्यान दिया था. आज भी ये व्याख्यान हमारे देश के क़ानून को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.
1936 में बाबा साहेब ने ब्रिटिश संविधान पर ये व्याख्यान दिया और कुछ साल बाद उन्होंने इस देश का संविधान लिखा. ये महज़ एक संयोग नहीं है बल्कि यह दलितों के अलावा संपूर्ण समाज के उद्धार के लिए डॉ. आंबेडकर की तपस्या का फल है.
इसीलिए उनकी वकालत न केवल अदालतों में बल्कि देश के कोने-कोने और दुनिया भर में बेजुबानों की आवाज़ बन गई है.
जब भी मानवता, समानता, भाईचारा और लोकतंत्र के मूल्यों की बात आती है तो डॉ. आंबेडकर का योगदान याद आता है. (bbc.com/hindi)
(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित)
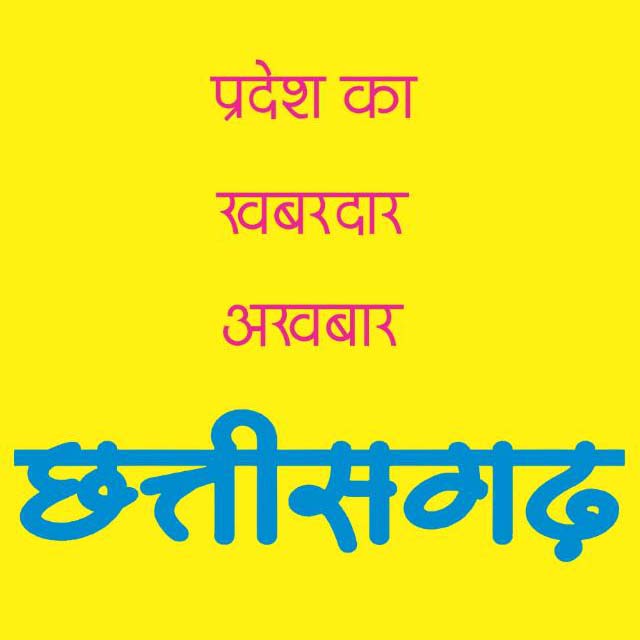

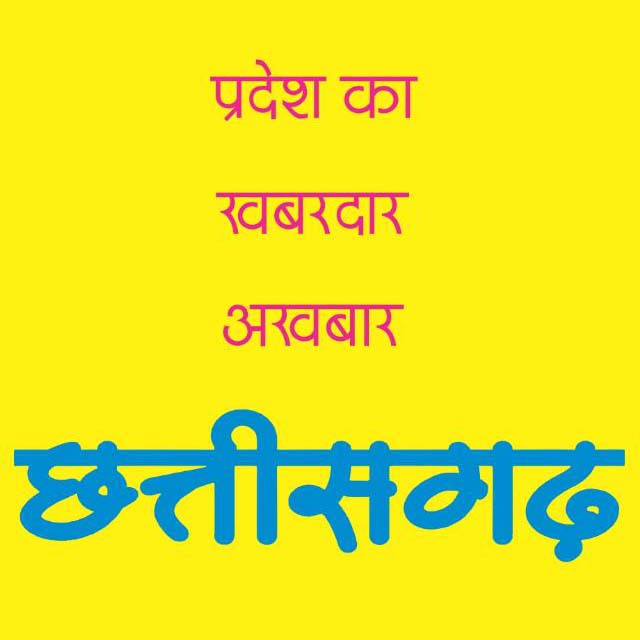





.jpg)