विचार / लेख

डॉ. गोल्डी एम.जार्ज
विश्व मूल निवासी दिवस पर विशेष
केंद्र सरकार ने चार राज्यों में स्थित 41 कोयला ब्लाकों की नीलामी करने की घोषणा की है। इनमें से दस ब्लॉक मध्यप्रदेश में हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखण्ड में नौ-नौ ब्लॉक हैं तथा तीन ब्लॉक महाराष्ट्र में हैं। इनमें से कई ब्लॉक ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां आदिवासी व अन्य मूल निवासी समुदाय निवासरत हैं और वहां के वनों पर निर्भर हैं। उनका पुनर्वास या तो संभव ही नहीं है या उसके लिए कोई योजना नहीं है। जाहिर है, यह निर्णय उनके जीवन के लिए खतरनाक है।
9 अगस्त दुनियाभर के आदिवासियों के लिए गर्व का उत्सव है, जिसे विश्व के सभी मूल निवासी अपने अन्तरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व के 195 देशों में से 90 देशों में 5000 आदिवासी समुदाय हैं, जिनकी आबादी लगभग 37 करोड है तथा उनकी अपनी 7000 भाषाएं हैं। लेकिन इनके अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन भी होता रहा है। आदिवासियों के अधिकारों का मसला और आदिवासी दिवस मनाने के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। आदिवासियों के साथ हो रहे प्रताडऩा एवं भेदभाव के मुद्दे को अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने, जो लीग ऑफ नेशन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग बना, 1920 मे उठाना शुरू किया। इस संगठन ने 1957 मे ‘इंडिजिनस एंड ट्राईबल पापुलेशन कन्वेंशन’ क्र. 107 नामक दस्तावेज को अंगीकृत किया। यह आदिवासी मसले का पहला अन्तरराष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे दुनियाभर के आदिवासियों के उपर किये जाने वाले प्रताडऩा एवं भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्रारा पारित आदिवासी अधिकारों के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भारत सरकार ने आज तक आदिवासी अधिकारों के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया है। यहां तक कि संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची जो आदिवासी स्वशासन से संबंधित है, उसे भी वास्तविक अर्थ में लागू नहीं किया। देश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रहनेवाले आदिवासियों की संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना आम राजनीतिक घटना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बुनियादी नागरिक अधिकारों से आदिवासी वंचित तो है ही, साथ ही विकास की परियोजनाओं से लगातार बेदखली, पलायन, मानव तस्करी का शिकार बने हुए हैं। वे अपनी भाषा और संस्कृति से हर रोज विस्थापित हो रहे हैं।
आदिवासी संदर्भ में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो नीतियां बनी थीं, उसी तर्ज पर स्वाधीन भारत में भी नीति और कानून बनते गए। 1952 में स्वतंत्र भारत ने अपनी वन नीति बनाई जिसके अंतर्गत वनों को राष्ट्रीय संपदा माना गया और ‘राष्ट्रहित’ को सामुदायिक हितों पर प्राथमिकता दी गई। यह साफ कर दिया गया कि स्थानीय प्राथमिकताएं व हित और स्थानीय समुदायों के दावे, व्यापक राष्ट्रीय हितों के अधीन होंगे। 1952 में ही वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत चिन्हित वन क्षेत्रों को केवल वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित कर दिया गया और उनमें मनुष्यों के रहवास और प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। सभी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभ्यारण्य इसी अधिनियम के प्रावधानों से शासित होते हैं।
1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यह अनुशंसा की कि ‘औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए लकड़ी का उत्पादन वनों का मूल प्रयोजन होना चाहिए’ और व्यक्तियों व समुदायों की आवश्यकताएं, औद्योगिक आवश्यकताओं के अधीन होनी चाहिए। उसी वर्ष, संविधान के 42वां संशोधन के जरिए वन को राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया और इस प्रकार, वनों का प्रबंधन केंद्र सरकार के हाथों चला गया।
1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत, निम्न उपाय किए गए (अ) वनों के गैर-वानिकी उपयोग पर प्रतिबंध, (ब) भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत जिन वनों को आरक्षित घोषित किया गया है उन्हें अनारक्षित करने पर रोक, (स) वन भूमि को व्यक्तियों या गैर-सरकारी संस्थाओं, निगमों आदि को लीज पर दिए जाने पर रोक और (ड) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध। मूलत: यह अधिनियम वन भूमि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार को राज्य सरकारों से वापस लेकर, केंद्र के हाथों में सौंपता है।
1947 से लेकर 1986 तक, केंद्र सरकार के पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश में औद्योगिक विकास बढ़ा, विशेषकर उत्खनन के क्षेत्र में। औद्योगिक और उत्खनन परियोजनों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर वन क्षेत्रों को साफ किया गया। इसके चार चरण थे- सिलेक्टिव फेलिंग (1947-60), क्लियर फेलिंग एंड मोनोकल्चर प्लांटेशन्स (1960-75), फॉर्म फॉरेस्ट्री (1975-85) और इम्पोर्ट एंड कैप्टिव प्लांटेशन (1985 से अब तक)। इस तरह वनों को राज्य की संपत्ति मानने की नीति जारी रही और आदिवासियों को वन और वन भूमि पर अधिकार वापस नहीं मिला। इस कारण, आदिवासी इलाकों में जमीन, जंगल, जल, से जुड़े मसलों पर कई आंदोलन और संघर्ष हुए।
इन संघर्षों के चलते, 1988 में जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, वह 1952 में बनाई गई नीति से कई मामलों में बहुत भिन्न थी। विशेषकर वन प्रबंधन के संदर्भ में। एक नीति के रूप में उसकी यह सीमा थी कि इसे कानून की तरह लागू करना संभव नहीं था। इसके बाद पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 ने विशाल उद्योगों के विरुद्ध चल रहे जन आंदोलनों में आशा की एक किरण जगाई, परन्तु यह आशा जल्दी ही समाप्त हो गई। यह अधिनियम पर्यावरण की रक्षा के लिए कानूनी ढ़ांचे की मांग और उसके लिए चल रहे संघर्षों के मद्देनजर बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत किसी भी औद्योगिक परियोजना को लागू करने से पहले उसके पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक-आर्थिक लाभ-हानि का आंकलन करना और जन सुनवाई आयोजित करना आवश्यक बना दिया गया।
पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 के अंतर्गत, औद्योगिक परियोजनाओं के प्रमोटरों के लिए ग्राम सभा से चर्चा करना और उसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक बना दिया गया है। परन्तु इन सभी प्रावधानों का कुछ ही समय तक ठीक से पालन हुआ। पिछले एक दशक के दौरान, जन सुनवाईंयां महज औपचारिकता भर रह गईं हैं जिनकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार रहती है। जिन मामलों में स्थानीय रहवासी इस आशय के पर्याप्त प्रमाण जुटा भी लेते हैं कि वे वनों पर निर्भर हैं और वनों को काटने से क्षेत्र के पर्यावरण को हानि होगी, तब भी उनकी आपत्तियों और दावों को दरकिनार कर दिया जाता है। उनकी जमीनें उनसे छीन ली जातीं हैं और उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है। पेसा और वन अधिकार अधिनियम के बावजूद पर्यावरण संबंधी कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं।
आदिवासी आज भी अपने उन नैसर्गिक अधिकारों को पाने के लिए संघर्षरत हैं, जो उनसे छीन लिए गए हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के पारित होने के बाद ऐसी आशा जगी थी कि सदियों से आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय पर कुछ लगाम लगेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिकार देने में कई विभागों और मंत्रालयों और अनेक कानूनों की भूमिका रहती है। इस अधिनियम में वन अधिकारों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है- 1) व्यक्तिगत भू अधिकार व 2) सामुदायिक भू अधिकार-अ) आदिवासियों के लिए व ब) अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए। परन्तु ये अधिकार पाने की राह में कई विभाग और कानून रोड़ा बनते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत, किसी भी विकास परियोजना या औद्योगिक गतिविधि या किसी भी बाह्य एजेंसी के लिए ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति लेना ज़रूरी है।
विकास, औद्योगिकारण और खनन परियोजनाएं, पारंपरिक रूप से वनों पर निर्भर समुदायों के जीवन और जीवनयापन से संबंधित कई चुनौतियां देती हैं। हाल में केंद्र सरकार ने चार राज्यों में स्थित 41 कोयला ब्लाकों की नीलामी करने की घोषणा की है। इनमें से दस ब्लॉक मध्यप्रदेश में हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखण्ड में नौ-नौ ब्लॉक हैं तथा तीन ब्लॉक महाराष्ट्र में हैं। इनमें से कई ब्लॉक ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां आदिवासी व अन्य मूल निवासी समुदाय निवासरत हैं और वहां के वनों पर निर्भर हैं। उनका पुनर्वास या तो संभव ही नहीं है या उसके लिए कोई योजना नहीं है। जाहिर है, यह निर्णय उनके जीवन के लिए खतरनाक है।
कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि वन अधिकारों के खतरे में पडऩे का मूल कारण यह है कि न तो औपनिवेशिक काल में और ना ही स्वाधीन भारत में, लोगों के पारंपरिक वासस्थलों और वनों पर उनकी निर्भरता को मान्यता दी गई। इसके कारण, आदिवासियों और अन्य पारंपरिक समुदायों के साथ सदियों से अन्याय होता चला आ रहा है। और यह तब जब कि वे वनों के पारिस्थितिकी तंत्र का अविभाज्य हिस्सा हैं और वनों के बचे रहने में उनकी अनिवार्य भूमिका है। हूल से लेकर उलगुलान तक और आज भी यह संघर्ष जारी है। विश्व मूल निवासी दिवस पर इन सवालों का जवाब सरकार और समाज को देना अनिवार्य होगा।
(लेखक एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तथा वर्तमान में फॉरवर्ड प्रेस नई दिल्ली में सलाहकार संपादक है।)



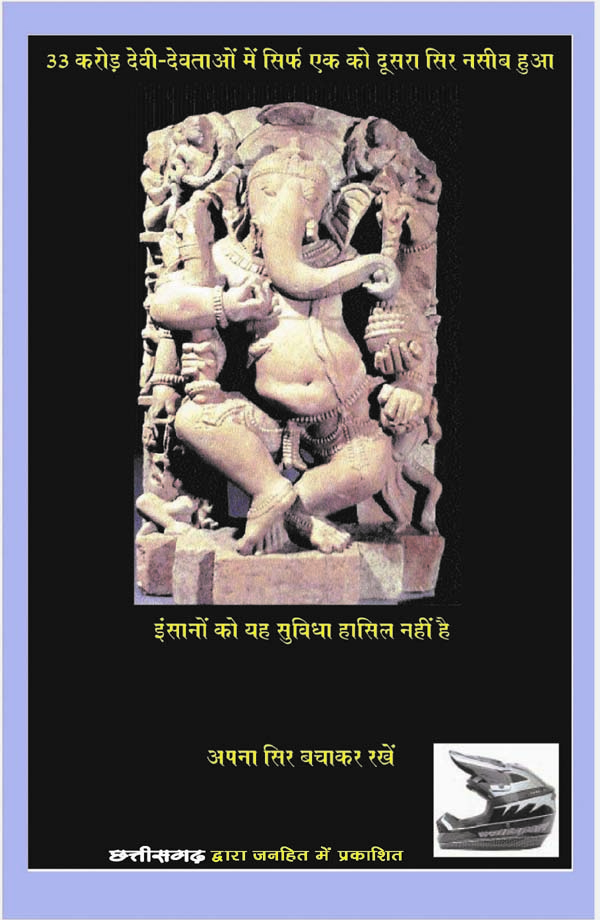

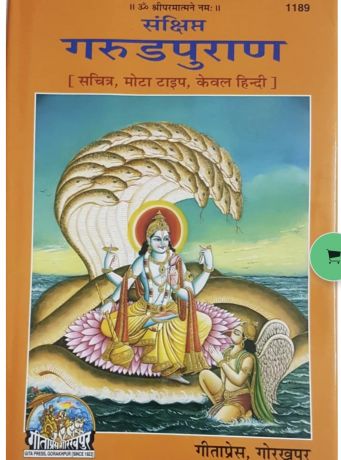










.jpg)

.jpg)













.jpg)











