विचार / लेख

डॉ. गोल्डी एम. जार्ज
अठारवीं सदी में अंग्रेजों ने जब से वन क्षेत्र में घुसपैठ करनी शुरू कर दी जो आदिवासियों के वास स्थल थे और इस कारण उनके बीच सीधा टकराव शुरू हुआ। भारत में आदिवासी विद्रोहों के पहले 100 सालों (1760 के दशक से लेकर 1860 के दशक तक) में वन कानून नहीं थे और इस दौरान जंगलों से इमारती लकड़ी और अन्य संसाधनों का अनियंत्रित दोहन हुआ। इस सौ साल के दरमियान सैकड़ों आदिवासी विद्रोह हुए। इसमें से तिलका मांझी (1770-85) के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसके बाद अंग्रेजों के सामने वन क्षेत्र के रहने वाले आदिवासियों के संदर्भ में गंभीर सवाल खड़ा हुआ।
अंग्रेजों द्वारा उन्नीसवीं सदी में वन विभाग की स्थापना करने और वनों से संबंधित कानून बनाने के समय से ही दो महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। पहला, आदिवासियों और अन्य मूलनिवासी समुदायों द्वारा वनों के संरक्षण और उनके धारणीय उपयोग के लिए सदियों पुरानी सुस्थापित पारंपरिक प्रणालियां और वनों की पर्यावर्णीय, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका। इसमें 1855 में सिदो-कान्हु के नेतृत्व में हुए हूल विद्रोह सबसे निर्णायक था जिसके बाद अंग्रेजों ने एक सख्त वन कानून की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया।
सन् 1855 के संथाल विद्रोह के मद्देनजर, 1856 में गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने एक स्थाई वन नीति बनाने पर जोर दिया। 1864 में अंग्रेजों ने इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की। सन् 1865 में भारत के पहले वन कानून आया, जिसका संशोधन 1876 में किया गया और नये संशोधनों के साथ फॉरेस्ट एक्ट, 1878 लागू किया गया। इसके बाद सन् 1894 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी वन नीति बनायी। अंत में सन् 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बनाया जो सन 1878 में वनों के दोहन के लिए बनाई गई नीति के अनुरूप था। कुल मिलाकर आदिवासी अपने ही वन क्षेत्र में ही बाहरी व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गए।
वन विभाग की स्थापना से पहले, अर्थात 1864 से पूर्व, जो प्रमुख विद्रोह हुए उन्हें केवल किसानों का अंग्रेजों या ज़मींदारों या साहूकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर विद्रोह नहीं कहा जा सकता। उन्हें हमें बाहरी शक्तियों द्वारा आदिवासियों के वासस्थलों, जो मुख्यत: जंगल और पहाड़ थे, में जबरदस्ती घुसने के प्रयासों के संदर्भ में समझना होगा। इन विद्रोहों और आंदोलनों के पृष्ठभूमि और इतिहास के गहराई से अध्ययन से हमें यह पता लगेगा कि सिर्फ जमीन और जंगलों के आर्थिक और परंपरागत महत्व को नजरअंदाज करना या लोगों से इन संसाधनों को छीनन ही इन विद्रोहों के पीछे का कारण नहीं था। इनके पीछे था वह अघोषित सांस्कृतिक युद्ध जिसमें एक ओर थे आदिवासी तो दूसरी ओर गैर-आदिवासी निहित स्वार्थी तत्त्व, जिन्हें सरकार का समर्थन और सहयोग हासिल था।
वनभूमि से संबंधित कानून के आने से पहले के दौर में हुए आदिवासी विद्रोहों में प्रमुख थे, तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह (1770-85), हल्बा डोंगर (हल्बा), बस्तर (1774-79), महादेव कोली, महाराष्ट्र (1784-85), तमर, छोटानागपुर (1781; 1894-95), पंचेट एस्टेट सेल (1798), कुरुचि, वायनाड (1812), सिंघ्पो, आसाम (1825; 28; 43; 47), कोल विद्रोह (हो और मुंडा सहित) (1832), खोंड, ओडिशा (1850), संथाल, छोटानागपुर (1855), सोनाखान, छत्तीसगढ़ (1856-57), भील, गुजरात (1857-58), अंडमानीज़, अंडमान (1859), लुशाई, त्रिपुरा (1860), सिंतेंग, जैंतिया हिल्स (1860-62), जुआंग, ओडिशा (1861) और कोय, आंध्रप्रदेश (1862)।
सन् 1855 में संथाल परगना के भगनाडीह गांव के चार मुर्मू भाईयों, सिदो, कान्हु, चंद और भैरव के नेतृत्व में हूल विद्रोह पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हुआ था। यद्यपि ऐसे कहा जाता है कि इस विद्रोह का कारण महाजनों और ज़मींदारों की ज्यादतियां थीं, परन्तु शायद आदिवासियों को यह भी महसूस हो रहा था कि उनकी ज़मीनों और जंगलों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। 1857 का सोनाखान विद्रोह, इसी वर्ष कुछ समय बाद हुए एक और बहुचर्चित विद्रोह से पहले हुआ था। इसका नेतृत्व आदिवासी राजा नारायण सिंह ने किया था और इस विद्रोह के मुद्दे भी 1855 के संथाल विद्रोह से मिलते-जुलते थे। सोनाखान एक वनक्षेत्र है और इसके पास बार नवापारा के घने जंगल भी हैं। 1852 में बम्बई और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले कोल और अन्य वन-आधारित समुदायों में बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने को लेकर भारी गुस्सा था, परन्तु वह विद्रोह में परिवर्तित नहीं हुआ।
सन् 1864 के बाद से, ब्रिटिश ने भारत में केन्द्रीयकृत राजनैतिक-प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी और इसके साथ ही वनों और वनवासियों के बीच विभाजक की रेखा खींच दी गई। औपनिवेशिक सरकार ने वनों पर अपने स्वामित्व को क़ानूनी जामा पहना दिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि वनों में रहने वाले समुदाय गैरकानूनी कब्जाधारी हैं और उन्होंने सरकार की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इसका एक दूसरा परिणाम यह था कि वनक्षेत्र में रहनेवाले आदिवासी और मूलनिवासियों पर शिकार करने का प्रतिबन्ध लगा गया, लेकिन अंग्रेज़ अधिकारियों. ज़मींदारों, जागीरदारों को शिकार की खुली छूट थी।
इस दौर में अनेक आदिवासी विद्रोह हुए। जब भी आदिवासियों के जीवन में बेजा हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई, जब भी उन्हें उनकी भूमि या जंगलों से बेदखल करने के प्रयास हुए, जब भी उनकी पारंपरिक संस्कृति, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, नागरिक अधिकारों या न्याय व्यवस्था का उल्लंघन या तिरस्कार किया गया, उन्होंने इसका तीव्र, त्वरित और आक्रामक प्रतिरोध किया। इस दौर में हुए महत्वपूर्ण विद्रोहों धनबाद में संथालों (1869-70), उत्तरपूर्व में नागाओं (1879), तम्मनडोरा के नेतृत्व में ओडिशा के मलकानगिरी में कोयायों (1880), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेंटिनेलियों (1883), छोटानागपुर में मुंडाओं (1889), लुशाईयों (1892), बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं का उलगुलान (1895), बस्तर के आदिवासियों का भूमकाल और गुंडा धुर के नेतृत्व (1910-11), गोविन्द गुरू के नेतृत्व में संप सभा और गुजरात व राजस्थान के मानगढ़ पहाडिय़ों में भीलों (1913-16), मणिपुर में कुकियों (1917-19), रम्पा में कोयायों (1922), उत्तरपूर्व में नागाओं (1932), तेलंगाना के आदिलाबाद में गोंड और कोलम जनजातियों (1941) और लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में कोरापुट, ओडिशा में आदिवासियों (1942) का विद्रोह शामिल थे।
हूल विद्रोह के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलनों में से एक है उलगुलान (महान हलचल)। उलगुलान बिरसा मुंडा के नेतृत्वि में उन्नीसवीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह है, जो झारखंड का सबसे बड़ा आदिवासी विप्लव था, जिसमे हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए।
धरती आबा के नाम से जाने जाने वाले बिरसा मुंडा, 1 अक्टूबर 1894 को सभी मुंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजो से लगान (कर) माफी के लिये आन्दोलन किया। यह अंग्रेजों का आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप के खिलाफ सशस्त्र संग्राम था। बिरसा मुंडाओं के बीच अंग्रेजी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना शुरू कर चुके थे। जब सरकार द्वारा उन्हें् रोका गया और गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने मुंडा समुदाय में धर्म व समाज सुधार के कार्यक्रम शुरू किए और तमाम कुरीतियों से मुक्ति का प्रण लिया।
1895 में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में दो साल के कारावास की सजा दी गयी। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीडि़त जनता की सहायता करने की ठान रखी थी। 1897 से 1900 के बीच अंग्रेज के हर हस्तक्षेप के खिलाफ मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा और उसके साथियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके चार सौ सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गयी लेकिन इसके बाद उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ़्तारी हुई।
1898 में डोम्ब री पहाडिय़ों पर मुंडाओं की विशाल सभा हुई, जिसमें आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। आदिवासियों के बीच राजनीतिक चेतना फैलाने का काम चलता रहा। अंत में 24 दिसम्बर 1899 को बिरसापंथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 5 जनवरी 1900 तक पूरे मंडा अंचल में विद्रोह की चिंगारियां फैल गई। 9 जनवरी 1900 को डोम्बार पहाड़ी पर अंग्रेजों से लड़ते हुए सैंकड़ों मुंडाओं ने शहादत दी। ब्रिटिश फौज ने आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया। गिरफ्तार किए गए मुंडाओं में से दो को फांसी, 40 को आजीवन कारावास, 6 को चौदह वर्ष की सजा, 3 को 4 से 6 बरस की जेल और 15 को तीन बरस की जेल हुई।
बिरसा मुंडा काफी समय तक पुलिस की पकड में नहीं आये थे, लेकिन एक स्थानीय गद्दार की वजह से 3 मार्च 1900 को वे गिरफ्तार हुए। लगातार जंगलों में भूखे-प्यासे भटकने की वजह से वह कमजोर हो चुके थे। जेल में उन्हें हैजा हो गया और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जैसा कि बिरसा कहते थे, व्यक्ति को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। बिरसा के विचार मुंडाओं और पूरी आदिवासी कौम को संघर्ष की राह आज भी दिखाती है।
(लेखक एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तथा वर्तमान में फॉरवर्ड प्रेस नई दिल्ली में सलाहकार संपादक है।)



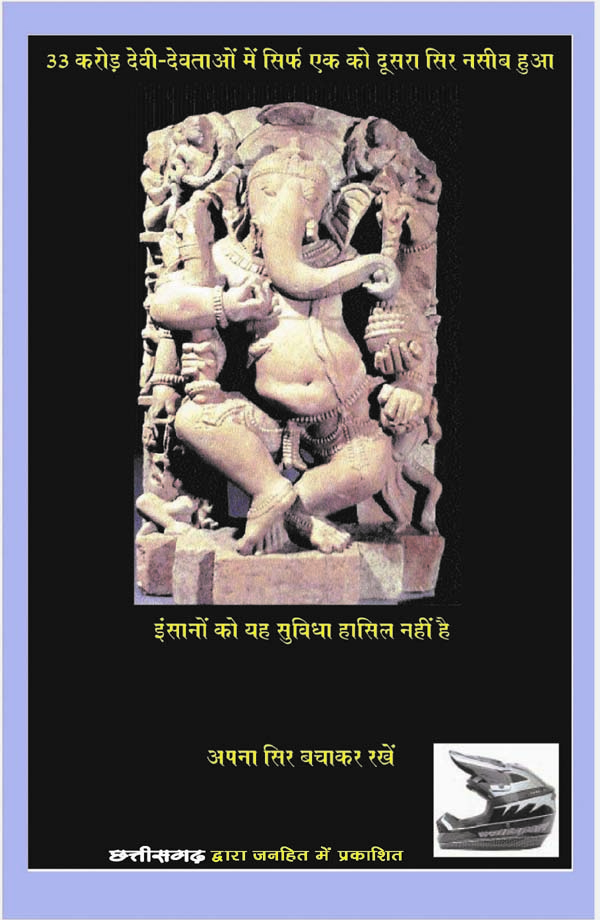


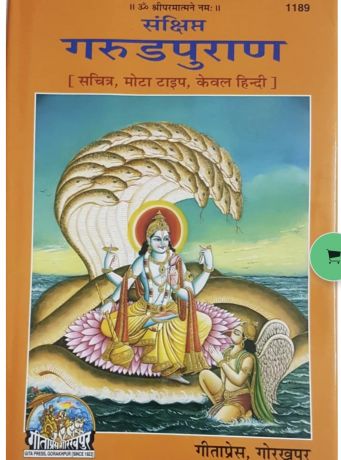










.jpg)

.jpg)













.jpg)










