साहित्य/मीडिया

उदय प्रकाश और दिनेश श्रीनेत (भीतर की तस्वीर) की ताजा तस्वीरें उनके फेसबुक पेज से
-दिनेश श्रीनेत
साल था 1997 और मेरी उम्र थी करीब 25 वर्ष। मैं इलाहाबाद में था। नौकरी की तलाश थी। अखबारों में काम खोज रहा था। उन दिनों इलाहाबाद से मित्र प्रकाशन की साप्ताहिक पत्रिका 'गंगा यमुना' निकलती थी। चर्चित कथाकार रवींद्र कालिया उसके संपादक थे। वही मेरे पहले संपादक भी थे। मुझे हर हफ्ते उस टेब्लॉयड साप्ताहिक के लिए खास खबर लिखनी होती थी। इसके बदले 175 रूपये मिलते थे। उन्हीं दिनों उपेंद्रनाथ अश्क की स्मृति में पहले अश्क सम्मान का आयोजन हुआ था। इसमें कृष्णा सोबती, अली सरदार जाफरी, उदय प्रकाश, वीरेन डंगवाल, अनामिका, कात्यायनी, पंकज विष्ट और खालिद जावेद जैसे साहित्यकारों ने शिरकत की थी। मेरा मन था कि मैं उदय प्रकाश का इंटरव्यू करूं। कालिया जी से पूछा तो उन्होंने तुरंत 'हां' कर दिया। वैसे भी बतौर संपादक वे कभी किसी बात के लिए ना नहीं करते थे। उस वक्त तक उदय प्रकाश की कहानियों की दो किताबें 'दरियाई घोड़ा' और 'तिरिछ' आ चुकी थीं। मैंने ग्रेजुएशन के दौरान ही 'तिरिछ' पढ़ा था और बहुत प्रभावित था। जब सत्र समाप्त होने पर मैंने उनसे बातचीत करनी चाही तो उन्होंने भी 'हां' कर दिया। जनवरी के दिन थे और बहुत अच्छी धूप खिली थी। हम हिन्दुस्तानी अकादमी के बाहर बागीचे में बैठकर बातचीत करते रहे। उदयजी बहुत खुश थे और बातचीत बहुत अच्छी रही। यह मेरे जीवन का सबसे पहला इंटरव्यू था। आज दो दशक पुरानी इस बातचीत को दोबारा पढऩा खासा दिलचस्प है। अतीत और वर्तमान की बहुत सी चिंताओं में साम्यता दिखती है हालांकि भविष्य के बारे में बहुत सी उम्मीदें समय की कसौटी पर सही नहीं साबित हुईं।
प्रश्न: आपने अपने लेखकीय संस्कार कैसे ग्रहण किए? किन रचनाओं व लेखकों ने आपको प्रभावित किया?
उदय प्रकाश: बचपन से ही अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण और विशेष रूप से अपने पिता जी के कारण रचनात्मक स्तर पर सबसे पहले मैंने चित्र बनाए फिर कैमरा और अंत में कविता। कहानी मैंने कभी नहीं लिखी। पढऩे की आदत शुरू से थी। जिन पुस्तकों को मैंने पढ़ा उनमें उपनिषद, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ भी थे। दूसरी तरफ आधुनिक लेखकों की रचनाएं थीं- जिनमें दोस्तोएवस्की, तोलस्तोय, श्रीलाल शुक्ल और धर्मवीर भारती से लेकर वे रचनाकार भी शामिल थे जो उन दिनों कल्पना, ज्ञानोदय जैसी पत्रिकाओं में छपते थे।
इसी दौर में मैंने सार्त्र की किताब 'एक्जिस्टेंशियलिज्म' का अनुवाद अपनी अधकचरी अंग्रेजी की समझ के साथ गांव में रहते हुए किया था। इसी दौरान मैंने मोपांसा को भी पढ़ा व अनुवाद किया। 1968 में जब मैं 16 वर्ष का था, मैं माक्र्सवादी साहित्य के संपर्क में आया और एआइएसएफ का सक्रिय सदस्य बना। बाद में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य बना। 1982 के बाद मैंने सभी राजनीतिक संगठनों से संबंध लगभग समाप्त कर लिए। लेकिन वह साहित्य जो किसी भी देश के समाज और उसकी साधारण जनता के जीवन संघर्षों और उसके अनुभवों को व्यक्त करता है वह आज भी मुझे एक नई राह देता है। माक्र्सवादी विचारधारा के सैद्धांतिक पक्षों की बजाय मुझे इन देशों का रचनात्मक साहित्य अपने लिए ज्यादा उपयुक्त लगता है। जैसे इन दिनों मैं एक सर्बियन कवि-उपन्यासकार मिलोराद पाविच से बहुत प्रभावित हूँ।
प्रश्न: आपकी कहानियों की संरचना जटिल व बहुस्तरीय है- यहां यथार्थ को बहुआयामी रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जाता है- एक ही घटना या चरित्र को अनेक दृष्टिकोणों से देखा जाता है। क्या फार्म के स्तर पर अब तक विकसित शिल्प जिसका चरम निर्मल वर्मा में दिखता है- जहां शब्द उस पार के संसार को संप्रेषित करते हैं- बदलते हुए यथार्थ को संप्रेषित करने में समर्थ नही हैं?
उदय प्रकाश: निर्मल वर्मा मेरे बहुत प्रिय कथाकार हैं। भाषा, संरचना और रुप के स्तर वे नई कहानी के दौर के सबसे उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण कथाकार हैं। लेकिन उनकी कहानियां जिन अनुभवों और जिस जीवन को व्यक्त करती हैं वो मेरा अनुभव नहीं है। चेखोव से लेकर तीसरी दुनिया के लैटिन अमेरिकी देशों के महान कथाकारों व उपन्यासकारों ने जिस जटिल सामाजिक यथार्थ का वर्णन अपनी कहानियों व उपन्यासों में किया है- उनकी तुलना में मेरी रचनाओं का यथार्थ कम संश्ष्टि है।
मैं लगातार कोशिश करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि मेरी हर कहानी किसी प्रचलित कथारूढि़ का शिकार न होकर आज के किसी नए सामाजिक अंतर्विरोध और यथार्थ के नए पक्ष को सामने लाए। स्पष्ट है कि ऐसी कहानी से हिंदी के साधारण तथा अभ्यस्त हो चुके पाठकों की रूचि और सोच पर एक चोट पड़ती है। नतीजे में मेरी रचना प्रारंभ में कुछ समय तक विवादों और चर्चाओं का केंद्र बनती है। लेकिन धीरे-धीरे लोग उस रचना में अंतर्निहित गंभीर आशयों को और समकालीन मनुष्य के एक नए अप्रत्याशित गहरे सामाजिक या सांस्कृतिक संकट को समझ जाते हैं और उनकी दृष्टि रचना के प्रति बदल जाती है। यह मेरा आज तक का अनुभव रहा है।
प्रश्न: आपकी रचनाओं में दो संसार हैं- 'पाल गोमरा' का महानगरीय यथार्थ तथा 'द्द्दू तिवारी: गणनाधिकारी' का कसबा। 'पाल गोमरा' कहानी पढऩे के बाद गहरी निराशा पैदा करती है। वह जिन समसामायिक घटनाओं को पैरोडी में बदलकर 'ब्लैक ह्यूमर' प्रस्तुत करती है- वह स्थितियां भी। क्या यह सुनियोजित सा नहीं है? 'पाल गोमरा' का महानगरीय यथार्थ क्या इतना आतंककारी है कि इसे एक युग सत्य के रूप में स्वीकार किया जाए? अथवा भारतीय जीवन के यथार्थ को इसी रूप में परखा जाए? अपेक्षाकृत कम चर्चित कहानी 'दद्दू तिवारी...' इस यथार्थ को अधिक सूक्ष्म स्तर पर व्यक्त नहीं करती? आप एक अवधारणा के स्तर पर भारतीय जीवन के यथार्थ को किस रूप में महसूस करते हैं? जबकि आपके रचना संसार में वह ढहते हुए सामंतवाद, पूंजीवाद, जकडऩ व बाजार तक फैला है।
उदय प्रकाश: भारतीय यथार्थ किसी भी अन्य पश्चिमी अथवा एशियाई देश की तुलना में- आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक ही नहीं पर्यावरण, भाषा, खाना-पान हर स्तर पर बहुविध, बहुलतवादी, अनेकात्मक यथार्थ है। यहां महानगर भी है। शहर, कसबे, गांव और कबीलाई आदम बस्तियां भी।
बस्तर के या मयूरभंज के आदिवासी गांव उत्तर प्रदेश के गांव से बहुत भिन्न हैं। इसी तरह भी महानगर भी एक जैसे सपाट नहीं हैं- दिल्ली कलकत्ता से भिन्न है, उसी तरह जैसे बंगलूर बनारस से। यह हर कोई जानता है कि भारत में सभ्यता की तमाम अवस्थाएं आज भी मौजूद हैं। ऐसे भी जनसमूह जहां अभी व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ही नहीं पैदा हुई। ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का भी आगमन नहीं हुआ। ऐसे गांव हैं जहां प्रेमचंद के उपन्यासों का सामंती और महाजनी यथार्थ है और ऐसे भी गांव हैं जहां नए जन-आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन बहुत बड़े हिस्से में जहां हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति हो चुकी है वहां ऐसा भी समृद्ध किसान वर्ग है जो अमेरिकी या स्वीडेन के किसानों की संपन्नता से होड़ लेता है।
हमारे महानगरों में आने वाली अधिकांश जनसंख्या इन्हीं तमाम अलग-अलग पृष्ठभूमियों से आई हुई प्रवासी जनसंख्या है- जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैं लगातार प्रयत्न करता हूँ कि मैं लेखकों से नहीं बल्कि ऐसे तमाम लोगों से मिलूं, उनके जीवन के बारे में जानूं और संभव हो तो उनके इलाके में घुसूं। इसलिए मैं भारतीय समाज की किसी एक कट्टर व्याख्या से सहमत नहीं हूँ। महाश्वेता देवी के उपन्यास से लेकर कृश्न बलदेव वैद के उपन्यासों तक फैला हुआ कथा संसार हमारे देश की विराट सामाजिक विविधता को व्यक्त करता है।
भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक गद्दारी, संस्थानों का अध:पतन, शिखर संस्थाओं का निर्लज्ज और आपराधिक दुरुपयोग, सार्वजनिक कोषों से गबन इत्यादि 50 साल में उस औपनिवेशिक विरासत की कलई खोल डालते हैं- जिसका हम अब तक गुणगान करते आए हैं। इसलिए मेरी नई कहानी 'वारेन हेस्टिंग्ज का सांड़Ó इस आसन्न खतरे से अपने स्तर पर मुठभेड़ करने का एक नया प्रयत्न है-मुझे पूरी उम्मीद है इसे फिर विवाद का केंद्र बनाया जाएगा।
प्रश्न: यदि सांस्कृतिक पर्यावरण नष्ट हो रहा है तो क्या आज के माहौल में सांस्कृतिक प्रतिरोध या प्रतिरोध की संस्कृति के विकसित होने की उम्मीद कर सकते हैं?
उदय प्रकाश: सांस्कृतिक पर्यावरण इसलिए नष्ट हो रहा है या होता दिख रहा है- क्योंकि हमें पश्चिमी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आदि बनाया जा रहा है। तीसरी दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले मध्यवर्ग की सबसे बड़ी संख्या भारत में ही है। हमारी पिछली तमाम आर्थिक नीतियों के दौरान इसकी सुविधाओं व क्रय शक्ति में बढ़ोत्तरी हुई है।
नई हाईटेक कारों व घरेलू उपकरणों को ऋण में लेने की सुविधाएं इस वर्ग को प्रदान की जा रही हैं। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों के लिए यूजीसी पिछले तीन सालों से मारुति या एस्टीम खरीदने की सुविधा प्रदान करती है।
हमारे इस सांस्कृतिक पर्यावरण का क्षरण उसी पारंपरिक मूल्यों के टूटने से हो रहा है जो हमारी अब तक की जीवन शैली से थे। पश्चिम की क्रांति ने हमारे संयुक्त परिवारों को तोड़ा था, यह नई क्रांति हमारे दांपत्य जीवन में भी सेंध लगा रही है। औद्योगिक क्रांति ने हमारे दस्तकारों को नष्ट किया था, यह देसी उद्योगों को नष्ट कर रही है। पश्चिमीकरण सिर्फ मूल्य के रूप में सामने नहीं आता- वह साबुन, सेंट, तौलिया, दवाएं, गर्म-शीतल पेय, कपड़े-लत्ते व शिक्षा के साथ भी आता है। कानवेंट स्कूल पहले जा चुके थे पब्लिक स्कूलों की संख्या अब बढ़ी है।
लेकिन विश्वास रखिए जैसा कि पीसी जोशी कहते हैं, हमारे देश की गरीबी व विशाल जनसंख्या हमारे सामाजिक मूल्यों की व परंपराओं की सबसे बड़ी रक्षक है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर, हमारी धरती को खोखला व बंजर बनाकर, हमारे सामुदायिक रिश्तों को तोड़कर हमें भौतिक उपकरणों व पैसे का लोलुप बनाने वाला यह नया हमला बहुत कारगर नहीं हो पाएगा क्योंकि वह जनसंख्या जिसकी क्रय शक्ति दिनों-दिन घटती जा रही है- इस शीशे के घरों पर ढेले जरूर मारेगी। हमारी प्रतिरोध की संस्कृति और प्रतिरोध के नए सामाजिक तरीके इसी जटिल प्रक्रिया के बीच में जन्म लेंगे।
प्रश्न: क्या आप आज के समय से जूझने का कोई सकारात्मक मूल्य परंपरा और इतिहास में पाते हैं?
उदय प्रकाश: इतिहास हमेशा एक रोशनी देता है- लेकिन वह इतिहास जो वैज्ञानिक हो। कबीर नै उस वैभव को माया और ठगिनी कहा था जो 95वीं, 96वीं सदी में इस देश में आई थी। मखदूम मोइउद्दीन, दीनानाथ मित्र, सुकांत, निराला- तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके बाद के पूंजी के वैभव व सत्ता का विरोध किया।
यह स्पष्ट है कि हमारी आर्थिक स्थितियां आज उसी रास्ते पर जा रही हैं- जिस रास्ते पर आज से पांच वर्ष पूर्व चिली, मैक्सिको व ब्राजील के देशों मे गई थीं। बेतहाशा बढ़ता कर्ज, गरीबी, घटती क्रय-शक्ति, मुद्रास्फीति, गावों में लोगों का लगातार उजडऩा व शहरों में जनसंख्या की बढ़ोत्तरी, सत्ता की संस्थाओं का पतन, भ्रष्टाचार व घोटालों के नए उदाहरण अभी और सामने आएंगे तब तक जब तक हम इन्हें बदल नहीं देते।





.jpg)
.jpg)
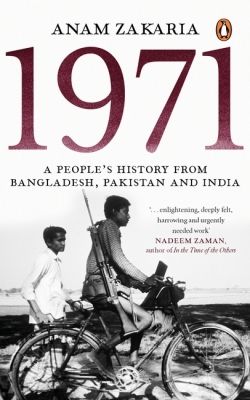
.jpg)
.jpg)
.jpg)








